-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने सोचा था कि UN शांति की अंतिम गारंटी बनेगा और युद्ध सिर्फ इतिहास की बात होगा लेकिन हालात उलट हो गए. अब कई देश आत्मरक्षा के नाम पर ही युद्ध को वैध ठहराने लगे हैं.

दूसरे विश्व युद्ध और राष्ट्र संघ के पतन के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई. इसका उद्देश्य दुनिया भर में हथियारबंद संघर्षों को रोकना था. UN चार्टर के अनुच्छेद 2(3) और 2(4) में एक सामान्य लेकिन गंभीर नियम है: अलग-अलग देशों को विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए और एक-दूसरे के विरुद्ध धमकी या बल प्रयोग से बचना चाहिए. सामान्य भाषा में कहें तो इसका ये मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की ये कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो किसी अन्य देश के ख़िलाफ युद्ध नहीं छेड़ें.
ऐसे नियम के बावजूद पिछले लगभग चार दशकों से दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी का सामना क्यों कर रही है? यूक्रेन पर रूस के हमले से लेकर गाज़ा में इज़राइल के मौजूदा अभियान तक पिछले दो दशकों के रुझान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नीतिगत साधन के रूप में बल प्रयोग धीरे-धीरे सामान्य हो गया है. हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात ऐसे संघर्षों का बढ़ना नहीं बल्कि उनके लिए पेश किए जा रहे कानूनी औचित्य हैं. आक्रमण करने वाले और हमले से ख़ुद को बचाने वाले- दोनों तरह के देश अब ये दावा करते हैं कि वो आत्मरक्षा और राष्ट्रीय हित को देखते हुए काम कर रहे हैं. रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले को सही बताने के लिए अनुच्छेद 51 का सहारा लिया; 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गज़ा पर अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए इज़राइल ने भी इसी अनुच्छेद का प्रयोग किया. हालांकि UN के जांच आयोग ने गज़ा पर इज़राइल के हमले की निंदा करते हुए इसकी तुलना नरसंहार से की है.
“पिछले दो दशकों के रुझान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नीतिगत साधन के रूप में बल प्रयोग धीरे-धीरे सामान्य हो गया है.”
सभी पक्षों के द्वारा आत्मरक्षा के व्यापक इस्तेमाल (भले ही संदर्भ कुछ भी हो) से पता चलता है कि एक कानूनी प्रावधान रणनीतिक औजार में बदल गया है. मूल रूप से अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार ताकत के इस्तेमाल के मामले में एक अपवाद था लेकिन इसकी व्याख्या इतने व्यापक ढंग से की गई है कि अब छोटी सी बात पर भी इसी का सहारा लिया जाता है. ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुच्छेद 51 के अर्थ में ये बदलाव क्यों और कैसे आया है. इस सवाल का जवाब इसकी दो व्याख्याओं में है.
प्रतिबंधात्मक व्याख्या ‘हथियारबंद हमले’ की घटना की शर्त को पूरा करने के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान देती है कि ऐसे हमले में क्या-क्या शामिल है. इस व्याख्या के अनुसार किसी देश के द्वारा ख़ुद को बचाने का विशेषाधिकार उसी स्थिति में लागू होता है जब दूसरे देश की सेना ने उसकी सीमा पार की हो और वो भी उसी समय तक जब तक कि सुरक्षा परिषद शांति की बहाली के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाती है. ये बात अनुच्छेद में बताई गई है. आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर बातचीत का इतिहास इस व्याख्या का समर्थन करता है.
दूसरी तरफ विस्तृत व्याख्या में कहा गया है कि आत्मरक्षा का अधिकार उस समय भी होता है जब सशस्त्र हमला ‘जल्द होने का ख़तरा’ होता है. इस व्यापक परिभाषा में बताया गया है कि अनुच्छेद 51 जल्द ख़तरे की स्थिति में आत्मरक्षा के अधिकार को अलग नहीं करता है और अनुमान लगाकर आत्मरक्षा के अधिकार का सहारा लेना वास्तव में आज की दुनिया में आवश्यक है. इस व्याख्या में किसी देश के लिए ये व्यापक गुंजाइश भी छोड़ी गई है कि किस देश पर हमला किया गया है, किसके द्वारा किया गया है और कैसे किया गया है के संबंध में आत्मरक्षा के अधिकार को अपनाए. यही कारण है कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग अलग-अलग देशों की सवालों से घिरी कार्रवाई को कानूनी ढाल देने के रूप में किया जा रहा है.
9/11 की घटना तक केवल अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी- जिनमें इज़राइल और यूनाइटेड किंगडम (UK) शामिल हैं- ही इस व्याख्या का समर्थन करते थे. बाकी दुनिया काफी हद तक प्रतिबंधात्मक व्याख्या का समर्थन करती थी. लेकिन 9/11 की घटना और इसके जवाब में अमेरिका के द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में लंबे सशस्त्र अभियान ने आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर कानूनी बाध्यताओं को ढीला कर दिया. इसकी वजह से जल्द नहीं होने वाले हमले के ख़िलाफ़ इसका दायरा बढ़ गया. इसे पूर्व-निवारक आत्मरक्षा का सिद्धांत कहा गया. इस नए और अपेक्षाकृत ख़तरनाक नज़रिए का प्रदर्शन ऑपरेशन इराक़ी फ्रीडम (2003) में हुआ जब अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक़ पर हमला किया और इस बुनियाद पर सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया कि वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और उनके पास सामूहिक विनाश का हथियार (WMD) है. बाद में दोनों आरोप पूरी तरह से झूठे पाए गए. ऐसा नहीं था कि दुनिया ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने-मरोड़ने को स्वीकार कर लिया. लेकिन इसके बावजूद दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इसकी निंदा करने से परहेज किया. इस तरह आत्मरक्षा के अधिकार की व्यापक व्याख्या को मौन सहमति दे दी गई.
“9/11 की घटना और इसके जवाब में अमेरिका के द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में लंबे सशस्त्र अभियान ने आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर कानूनी बाध्यताओं को ढीला कर दिया.”
उस समय से अनुच्छेद 51 के दायरे का केवल विस्तार ही हुआ है. आत्मरक्षा के अधिकार का उल्लेख दूसरे देश के गैर-सरकारी तत्वों जैसे कि आतंकवादी समूहों की हरकतों के लिए किया जाता है. वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 2004 में अपनी वॉल एडवाइज़री ओपिनियन में कहा था कि इस तरह की व्याख्या संहिताबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून में नहीं है (जैसा कि निकारागुआ मामले में देखा गया) लेकिन वो अनुच्छेद 51 के बदलते स्वरूप को भी मान्यता देता है जिसकी समय के साथ किसी देश के व्यवहार के आधार पर फिर से व्याख्या की जा सकती है. यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अल-क़ायदा जैसे गैर-सरकारी तत्वों के द्वारा हमले की स्थिति में आत्मरक्षा के अधिकार का ज़िक्र किया है. वास्तव में अमेरिका ने विशेष रूप से इस व्यापक व्याख्या का प्रयोग करके सीरिया और अफ़ग़ानिस्तान में गैर-सरकारी तत्वों के ख़िलाफ़ अपने अभियानों को सही ठहराया है.
इसका ये अर्थ है कि अनुच्छेद 51 का मूल दायरा प्रतिबंधात्मक होने के बावजूद पश्चिमी देशों की अगुवाई में अलग-अलग देशों ने व्यवहार में इसका विस्तार उस बिंदु तक कर लिया है जहां कोई देश किसी दूसरे देश या किसी गैर-सरकारी तत्व पर हमला करते हुए आत्मरक्षा का हवाला दे सकता है, भले ही ख़तरे की आशंका मात्र हो और पहले कोई हमला नहीं हुआ हो. इसका समर्थन करने वाले हथियारों में तकनीकी प्रगति और परमाणु ख़तरों के साथ-साथ गैर-सरकारी तत्वों से उत्पन्न जोखिम का ज़िक्र ऐसी व्यापक व्याख्या के लिए आधुनिक आवश्यकता के रूप में करते हैं.
वैसे तो आत्मरक्षा के अधिकार की व्यापक व्याख्या के समर्थन में दलीलें निश्चित रूप से अकाट्य हैं लेकिन इस तरह के दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के उसी बुनियाद को नष्ट किया है जो दूसरे विश्व युद्ध के अवशेषों से उभरी थी. एक समय में अनुच्छेद 51 ताकत के प्रयोग को रोकने के मामले में एक अपवाद था लेकिन इसका व्यापक इस्तेमाल अब सुविधा के मामले में एक कानूनी साधन बन गया है. इसकी वजह से अलग-अलग देश अपने ख़िलाफ़ हमला रोकने की आड़ में आक्रमण को सही ठहराने में सक्षम हो गए हैं.
“पश्चिमी देशों ने अनुच्छेद 51 का दायरा इतना बढ़ा दिया कि संभावित खतरे पर भी हमले को आत्मरक्षा कहा जा सके.”
ये बदलाव UN चार्टर के मुख्य उद्देश्य यानी शांति को आदर्श और युद्ध को आख़िरी उपाय बनाने को कमज़ोर करता है. अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह से नहीं बने होते हैं कि अलग-अलग देशों की हर रणनीतिक बेचैनी को शामिल किया जाए, इसका अर्थ उन्हें संयमित करना है. “आत्मरक्षा” के विचार को कथित या काल्पनिक ख़तरों को शामिल करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके अलग-अलग देशों ने चार्टर के तर्कों को उलट दिया है और अपवाद को नियम बना दिया है.
अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह की व्यापक व्याख्या को स्वीकार और लागू करना जारी रखता है तो ताकत के इस्तेमाल पर रोक के महत्वहीन हो जाने का ख़तरा है. शांति के लिए प्रतिबद्ध विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यकता, आनुपातिकता और शीघ्रता पर आधारित अनुच्छेद 51 की प्रतिबंधात्मक व्याख्या की ओर लौटना ज़रूरी है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
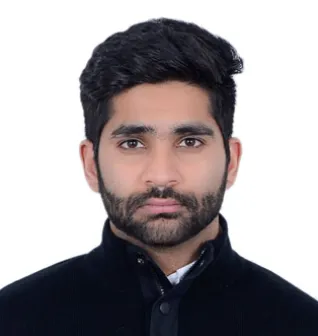
Udayvir Ahuja recently completed his LLM in International Law from SOAS, University of London, where he focused on contemporary issues at the intersection of international ...
Read More +