-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
संस्था को बदले हुए हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालना होगा. उन्हें अपना विस्तार करना होगा और आधुनिक भारत की ज़रूरतों को पूरा करना होगा.

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले पांच साल से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर विचारधाराओं के खूंटे से बंधी एक बहस चल रही है. इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए विश्लेषण की ज़हमत नहीं उठाई गई. इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने के बजाय अपनी-अपनी विचारधारा के हिसाब से फैसला सुना दिया गया. इसमें तथ्यों की अनदेखी हुई और निजी तजुर्बों के आधार पर राय बना ली गई. लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर चल रहे इस विमर्श पर राजनीतिक निष्ठा हावी है और उसी से इस बहस की दिशा तय हो रही है. अगर कोई सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन सरकार का सहयोगी या समर्थक है तो उसे लगता है कि सरकार सांस्थानिक ढांचे में बदलाव करके उसकी ग़लतियों को दूर कर रही है. योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग के मामले में ऐसा ही हुआ. योजना आयोग संवैधानिक संस्था थी, लेकिन नीति आयोग ने उससे कहीं अधिक शक्तियां हासिल कर लीं. दूसरी तरफ, कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के सदस्य या मोदी विरोधियों का आरोप रहा है कि ये सारे कदम संस्थाओं को बर्बाद करने के लिए उठाए जा रहे हैं. यह पिछले कई दशकों से चल रहे देश के सामाजिक-राजनीतिक ध्रुवीकरण का नतीजा है, जो हाल के वर्षों में चरम पर पहुंच गया है.
मौजूदा सरकार को संस्थानों को बर्बाद करने वाले और आंकड़ों में हेराफेरी करने वाला बताया जा रहा है. उसे न्यायपालिका, विपक्ष, चुनाव आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और विश्वविद्यालयों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा. वैसे, सरकार इस मामले में सारे आरोपों के जवाब दे चुकी है, लेकिन संस्थाओं को लेकर मोदी सरकार के कदम का मतलब लोग अपनी-अपनी विचारधारा और राजनीतिक खेमेबाज़ी के आधार पर निकाल रहे हैं. इसके बावजूद इस मुद्दे पर राजनीतिक विमर्श की जरूरत है क्योंकि देश और नागरिकों के भविष्य के लिए ये संस्थाएं काफी अहमियत रखती हैं. इस रिपोर्ट में लोकतांत्रिक संस्थाओं के बुनियादी सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है जो ऐसी किसी बहस की पूर्वशर्त है.
सरकार के कामकाज के तरीकों पर संदेह की धुंध छाई हुई है. विपक्ष या सिविल सोसायटी की तरफ से इस पर किसी भी विरोध को सरकार की तरफ से पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है. असल में इस धुंध के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ज़िम्मेदार हैं. वे सत्तारूढ़ सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने के लिए इसका इस्तेमाल करती आई हैं. इस मुद्दे पर ईमानदार बहस के लिए संस्थानों को बनाने और उन्हें टिकाऊ बनाने के बुनियादी सिद्धांतों का विश्लेषण करना होगा, मसलन — सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका के कथित तौर पर सरकार का साथ देने के आरोप, आरबीआई के कामकाज को लेकर टकराव, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (सीबीआई) में नियुक्तियां और उसका ढांचा या रोज़गार के आंकड़े जारी न करना.
किसी भी समाज और खासतौर पर लोकतंत्र में नागरिकों की रक्षा के लिए ऐसे संस्थान जरूरी हैं, जो कानून का राज सुनिश्चित करें. इनमें लोकतंत्र के तीनों स्तंभों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ केंद्रीय बैंक (आरबीआई), जांच एजेंसी (सीबीआई) और सरकार के बहीखाते का ऑडिट करने वाला (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) जैसे सहयोगी संस्थाएं भी शामिल हैं.
दिक़्क़त यह है कि मौजूदा बहस में पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सवाल पूछे जा रहे हैं. विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार संस्थाओं को बर्बाद कर रही है. इसे लेकर सरकार भी विपक्ष पर जवाबी तीर चला रही है. इस बहस से अगर आप कोई जवाब हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस बुनियादी और नाज़ुक डोर की पड़ताल करनी होगी, जिसने इन सभी को जोड़ रखा है. वह डोर है — लोकतंत्र. जाने-माने संस्थागत सिद्धांतवादी जैक नाइट और जेम्स जॉनसन का कहना है, ‘संस्थान असल में वो नियम (भूमिका, प्रक्रिया, कार्यालय संबंधी) होते हैं, जो सामाजिक ढांचे और राजनीतिक विमर्श से निकलते हैं. वे ऐसे टिकाऊ संसाधन होते हैं, जिनकी मदद से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चर्चाएं और मंथन किए जाते हैं.’ डगलस सी नॉर्थ के मुताबिक, ‘मानवीय आदान-प्रदान में अनिश्चितता घटाने’ के लिए उन्हें बनाया जाता है.
किसी भी समाज और खासतौर पर लोकतंत्र में नागरिकों की रक्षा के लिए ऐसे संस्थान जरूरी हैं, जो कानून का राज सुनिश्चित करें. इनमें लोकतंत्र के तीनों स्तंभों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ केंद्रीय बैंक (आरबीआई), जांच एजेंसी (सीबीआई) और सरकार के बहीखाते का ऑडिट करने वाला (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) जैसे सहयोगी संस्थाएं भी शामिल हैं. सच यह भी है कि इन संस्थाओं को इंसान चलाते हैं, जिनके हमेशा निष्पक्ष होने की गारंटी नहीं दी जा सकती. इसके अलावा, मार्केट भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता और न ही सूचनाएं पूर्ण रूप से संतुलित होती हैं. हमें यहीं व्यवस्था को संतुलित रखने की जरूरत पड़ती है. उदार लोकतंत्र में सारे बड़े संस्थानों को स्वतंत्र ढंग से चलाया जाना जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र इन संस्थाओं से जवाबदेही की भी मांग करता है. इसके लिए नीतिगत बदलाव में दो लक्ष्यों के बीच संतुलन साधना होता है. पहला, संस्थान के कामकाज में राजनीतिक दख़लअंदाज़ी न हो और उसकी स्वायत्तता बनी रहे. दूसरा, गवर्नेंस सिस्टम की जवाबदेही. कुछ साल के अंतराल पर संस्थान की स्वायत्तता और जवाबदेही की पड़ताल करती रहनी चाहिए. ख़ासतौर पर आज के डिसरप्टिव यानी भारी उथलपुथल वाले दौर में यह और भी जरूरी हो जाता है. कई लोग मानते हैं कि डिसरप्शन सिर्फ़ नागरिकों के लिए सामाजिक बदलाव की निशानी है और सरकारी संस्थान इससे बेअसर रहते हैं. मिसाल के लिए, जजों की नियुक्तियों में जवाबदेही बढ़ाने को लेकर सभी सरकारों को संघर्ष करना पड़ा है. जजों के सेलेक्शन प्रोसेस को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए द ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड एकाउंटिबिलिटी बिल, 2020 और ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल, 2013 नाम से दो विधेयक लाए गए थे, लेकिन न्यायपालिका ने दोनों को ख़ारिज कर दिया. उसने इन विधेयकों को असंवैधानिक करार दिया था. कभी न कभी न्यायपालिका को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वह कानून और संविधान से ऊपर नहीं है.
मोदी सरकार ने 33 नए संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं, जिनमें से सिर्फ सात आईएएस से हैं. इससे पता चलता है कि नॉन-आईएएस किस तरह से मौजूदा नौकरशाही व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा रहे हैं.
देश में ऐसे कई संस्थान भी हैं, जिनकी ताकत उनका नेतृत्व करने वालों की निजी हैसियत से तय होती है. इनमें रिटायर्ड नौकरशाह शामिल हैं, जो कई रेगुलेटरी (नियामकीय) संस्थाओं के प्रमुख बन जाते हैं. इनमें रिटायर्ड जज भी हैं, जो कमीशन और ट्रिब्यनल के प्रमुख बनाए जाते हैं. पूरी व्यवस्था बाहरी लोगों को दूर रखने के लिए उनके साथ वैसा ही सलूक करती है, जैसे शरीर में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी करते हैं. मोदी सरकार ने 33 नए संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं, जिनमें से सिर्फ सात आईएएस से हैं. इससे पता चलता है कि नॉन-आईएएस किस तरह से मौजूदा नौकरशाही व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा रहे हैं. क्या वे आईएएस लॉबी के आगे हार मान लेंगे या वैसे बदलाव करने में सक्षम होंगे, जिसकी देश को जरूरत है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा.
21वीं सदी के भारत को नए नैरेटिव की ज़रूरत है. 3 लाख करोड़ डॉलर के साथ हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अगले लोकसभा चुनाव तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, सांस्थानिक स्तर पर इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर कोई झलक नहीं दिख रही है. उदारीकरण से पहले सरकारी नियंत्रण को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती थीं. तब उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का दौर था, टैक्स की दरें बहुत ऊंची थीं और लेबर पॉलिसी पर भी सरकारी नियंत्रण वाली मंशा की छाप थी. उदारीकरण के बाद के वर्षों में नीतियां तुलनात्मक तौर पर मार्केट फ्रेंडली रही हैं.
उदारीकरण के पहले दशक यानी 1991 से 2001 के बीच जो संस्थान बनाए गए, उनसे अर्थव्यवस्था में बदलाव करने का एक आधार मिला. इन संस्थानों में 1991 में फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी, जिसे कुछ समय पहले खत्म कर दिया गया), 1992 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) और 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) शामिल हैं. पिछले 10 साल में जो संस्थान बनाए गए, जैसे — 2017 में ऑल डिजिटल जीएसटी या जन धन योजना जैसी सरकार की कई योजनाएं, उन्होंने इन बदलावों को समझा है और अपने ढांचे में तकनीक को भी शामिल किया है. 1991 में 270 अरब डॉलर के जीडीपी वाले भारत के संस्थान जिन मुद्दों पर विमर्श कर रहे थे, वो आज से बिल्कुलअलग थे. तब देश संस्थानों के निर्माण में जुटा था. 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और 2002 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग) का गठन हुआ. आज तकनीक, समाज और अर्थव्यवस्था को नई शक्ल दे रही है. क्या ऐसे में संस्थान अतीत के खोल में सुरक्षित रह सकते हैं? हर संस्था को बदले हुए हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालना होगा. उन्हें अपना विस्तार करना होगा और आधुनिक भारत की ज़रूरतों को पूरा करना होगा. उन्हें जनता के प्रति अपनी जवाबदेही पूरी करनी होगी.
सांस्थानिक ढांचे पर जो बहस चल रही है, उसमें हमें दो पहलुओं का ध्यान रखना होगा. इनमें पहला है प्रक्रिया और शख्सियतों के बीच टकराव. किसी भी संस्थान को बनाते वक्त ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी ताकि उसके कामकाज पर शख्सियतों का असर न पड़े. इसका मतलब यह है कि संस्थान की बुनियाद और प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए. अगर किसी शख्स को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और वह योग्यता की शर्तें पूरी करता है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि वह संस्थान में अपनी भूमिका में आसानी से फिट बैठ सके. हालांकि, इंसान को प्रक्रिया की बंदिशों में बांधना भी ठीक नहीं होता है. अगर कोई करिश्माई शख़्सियत बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हो तो वह प्रक्रियाओं से खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकता है. संस्थान का ढांचा उसे बोझ लग सकता है और इससे उसकी काम करने की क्षमता प्रभावित होगी.
दूसरी तरफ, यह भी हो सकता है कि संस्थान की जो जवाबदेही तय की गई है, उसका कागज पर तो पालन हो रहा हो, लेकिन उसकी भावना की अनदेखी हो रही हो. यानी संस्थान का प्रमुख नियम-कायदों पर खरा उतरने के बावजूद उसका लक्ष्य हासिल न कर पा रहा हो. इस संतुलन का बोझ आखिर में देश के नागरिकों को उठाना पड़ेगा. दूसरी, लोकतंत्र, स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच का द्वंद्व. कुछ संस्थानों के मेनिफेस्टो में गोपनीयता भी जुड़ी होती है. इस संदर्भ में राट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं का जिक्र किया जा सकता है. हालांकि, इन संस्थाओं को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा करने से लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित होगी. मिसाल के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक महिला के लगाए गए आरोपों पर उसके जजों का सिर्फ पुरुष कर्मचारियों से प्रतिक्रिया लेना जल्दबाजी में उठाया गया कदम था और इसमें लैंगिक समानता और न्याय का ख्याल नहीं रखा गया. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्द निपटा दिया. इसमें कोई शक नहीं है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो वह दूसरे संगठनों के लिए नज़ीर बन जाता है. लोकतंत्र में ऐसी ग़लतियोंको ठीक किया जाना चाहिए, जैसा कि पूर्व लॉ क्लर्कों ने बयान जारी करके इस मामले में लैंगिक न्याय की मांग की थी. इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या विधायिका या कार्यपालिका कम महत्वपूर्ण हैं? क्या यूनिवर्सिटी, कंपनियों या यहां तक कि इंडिविजुअल ऑर्गनाइजेशंस का कद न्यायपालिका के मुकाबले छोटा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे सवाल किसी भी संस्थान में उथलपुथल मचा सकते हैं, लेकिन इनका जवाब देना जरूरी है. कानून के राज को बनाए रखना होगा और किसी भी मनमानी को रोकना होगा.
आगे क्या करना चाहिए?
मोदी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है और उसे इस मामले में भी पहल करनी चाहिए. उसे संस्थानों, उनके ढांचे, रिजल्ट और इवैल्यूएशन पर पुनर्विचार करना होगा. इसके साथ उसे यह बात भी ज़हन में रखनी होगी कि संस्थानों को बनाने का काम चुनौतीपूर्ण होता है. यह इंध्रधनुष का पीछा करने जैसा है, जिसकी मंजिल लगातार बदलती रहती है. इसमें बदलाव की मांग और स्थिरता की जरूरत के बीच हमेशा द्वंद्व बना रहता है. संस्थान और उसे चलाने वाली शख्सियत के बीच भी टकराव की नौबत आती है. ऐसे में सहमति के साथ संस्थानों में बदलाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए. ये लोगों के साथ संवाद कायम करने और जुड़ने का अहम जरिया हैं. सरकार को इन सबके बीच तालमेल बनाना होगा. फरवरी, 1910 में श्री अरबिंदो ने लिखा था, ‘जीवन संस्थाओं का निर्माण करता है. संस्थाएं सिर्फ रचना तक सीमित नहीं रहती, ये जीवन को संजोने और अभिव्यक्ति का ज़रिया भी बनती हैं.’ 21वीं सदी के भारत को अपनी संस्थाओं पर इस बात को लागू करना चाहिए.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
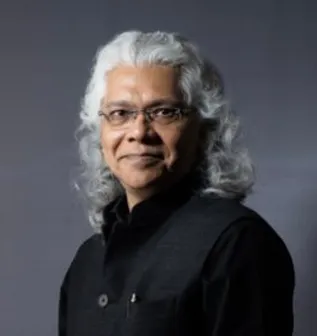
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +