-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में तेज़ी से अफ्रीका के उभरने और इस महाद्वीप में वर्चस्व रखने वाले व्यापारिक साझेदार के तौर पर चीन के बने रहने के साथ अमेरिका, EU और भारत को अफ्रीका में विकास से जुड़ी अपनी सहायता को लेकर तालमेल करना चाहिए.

Image Source: Getty
आज की उभरती वैश्विक व्यवस्था में विकास सहायता और कनेक्टिविटी से जुड़े सहयोग विकासशील दुनिया में भू-राजनीतिक प्रभाव के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरे हैं. इस प्रतिस्पर्धा की रूप-रेखा सबसे अधिक अफ्रीका में नज़र आती है जो अपार आर्थिक संभावनाओं, महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों और एक युवा एवं बढ़ते वर्कफोर्स वाला महाद्वीप है. अफ्रीका के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना- न केवल सड़कों और पुलों के माध्यम से बल्कि अग्रणी डिजिटल परिवहन प्रणालियों, हरित तकनीकी केंद्रों, क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों और अन्य के साथ भी- अपने साथ अधिक आर्थिक गतिविधि एवं व्यापार के लिए अवसर लाता है जिससे अफ्रीकी देशों और उनके व्यापार एवं विकास साझेदारों- दोनों को लाभ होता है.
दुनिया की ताकतों और उभरते आर्थिक किरदारों ने इन रुझानों को लेकर अपनी आंखें नहीं बंद कर रखी है. अफ्रीका में विकास ध्यान देने का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र रहा है लेकिन चीन दूसरे देशों से काफी आगे है.
दुनिया की ताकतों और उभरते आर्थिक किरदारों ने इन रुझानों को लेकर अपनी आंखें नहीं बंद कर रखी है. अफ्रीका में विकास ध्यान देने का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र रहा है लेकिन चीन दूसरे देशों से काफी आगे है. चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से अफ्रीका में सफलतापूर्वक चल रही है. इसके नतीजतन अफ्रीका में चीन ने गहरी पैठ बना ली है. चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्ज़दाता है. 2023 तक चीन ने अफ्रीका को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा कर्ज दे रखा था. BRI के तहत चीन ने 2013 से 2023 के बीच अफ्रीका में 150 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा कीमत का निवेश, कर्ज या परियोजनाओं का ठेका भी दिया था. दिलचस्प बात ये है कि अफ्रीका में BRI की आर्थिक भागीदारी का लगभग 43 प्रतिशत ऊर्जा, धातु और खनन के क्षेत्रों में है.
समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने अफ्रीका में बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना ध्यान बढ़ाया है लेकिन उनको अपने प्रयास और तेज़ करने चाहिए. अलग-थलग होकर काम करने, जैसा कि वो ऐतिहासिक रूप से करते आए हैं, के बदले उन्हें मिल-जुलकर ये काम करना चाहिए. इसकी आज सख़्त ज़रूरत है क्योंकि पहले की तुलना में आज इन देशों के बीच अधिक सामरिक मेलजोल है. ये लेख अफ्रीका में यूरोपीय, अमेरिकी और भारतीय कनेक्टिविटी एवं सहयोग का विश्लेषण करता है और व्यापक सहकारी तौर-तरीकों के लिए एक रूप-रेखा का सुझाव देता है.
अफ्रीका के आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए अमेरिका, EU और भारत के पास मिलते-जुलते कारण हैं. ये महाद्वीप आर्थिक क्षमताओं का बढ़ता केंद्र है. अफ्रीका की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ एक उत्सुक उद्यमशील वर्कफोर्स आता है. अफ्रीका के साथ एकीकृत व्यापार नेटवर्क और बाज़ार अमेरिका, यूरोप और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी उतना ही लाभकारी है जितना अफ्रीकी देशों के लिए. इस प्रयास के लिए सेवाओं को प्रदान करने और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रमुख बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण होगा.
आर्थिक सुरक्षा के लिए भी अफ्रीका के साथ स्थिर व्यापार संबंध अहम हैं. ये महाद्वीप महत्वपूर्ण संसाधनों से भी समृद्ध है जिन पर हरित तकनीकों की अगली पीढ़ी निर्भर होगी. इन सामग्रियों के लिए स्थिर और विश्वसनीय सप्लाई चेन को विकसित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका, EU और भारत ऐसी सामग्रियों के लिए चीन पर निर्भरता से हटना चाहते हैं. सतत रूप से ऐसा करने से इन महत्वपूर्ण सामानों के व्यापार से अफ्रीकी देशों को भी मदद मिलेगी और शोषणकारी प्रवृत्तियां जारी नहीं रहेंगी.
अंत में, अफ्रीका की क्षमता को दुनिया की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह जोड़ने से वैश्विक मुक्त व्यापार के एजेंडे को मज़बूत करने में मदद मिलेगी जो दूसरे विश्व युद्ध के युग के बाद अपनी स्थापना के समय से सबसे बड़े ख़तरे का सामना कर रहा है. इस क्षेत्र में चीन का निवेश एक उपयोगी केस स्टडी है. चीन का निवेश पूरे अफ्रीका में चीन और उसके आर्थिक मॉडल के बारे में बढ़ते सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा है. अमेरिका, EU और भारत वैश्विक आर्थिक एजेंडा को फिर से मज़बूत (नया आकार नहीं) करने के लिए उत्सुक हैं और उन्हें अफ्रीका में निवेश करने के महत्व का ध्यान रखना चाहिए.
अमेरिका, यूरोप और भारत के नीति निर्माता इन रुझानों को लेकर आंखें बंद कर नहीं बैठे हुए हैं और तीनों ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में अपनी मौजूदगी और निवेश में बढ़ोतरी की है.
बाइडेन प्रशासन के तहत अमेरिका ने बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है. उसने अपनी विकास एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से 2022 से अफ्रीका में बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं में 65 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है.
बाइडेन प्रशासन के तहत अमेरिका ने बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है. उसने अपनी विकास एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से 2022 से अफ्रीका में बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं में 65 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है. अमेरिका ने विशेष रूप से अफ्रीका में निवेश पर ध्यान दिया है. वैसे तो ये तय है कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने और हरित परिवर्तन को लेकर ट्रंप का दूसरा प्रशासन उस गति को जारी नहीं रखेगा लेकिन एक व्यापारिक साझेदार और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर के रूप में अफ्रीका के विकास से जुड़े एजेंडे को समर्थन देने के लिए एक अधिक लेन-देन वाला दृष्टिकोण इस महाद्वीप के बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान केंद्रित कर सकता है.
EU भी सक्रिय है. पुराने यूरोपीय आयोग के निर्देश के तहत EU ने ग्लोबल गेटवे की शुरुआत की जिसका लक्ष्य दुनिया भर में 309.34 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना है और इसका ध्यान सबसे अधिक अफ्रीका पर है. EU ने ग्लोबल गेटवे ढांचे के तहत अकेले अफ्रीका में 100 से ज़्यादा परियोजनाओं की सूची तैयार की है. अगला यूरोपीय आयोग इस फोकस को जारी रखेगा. EU के अलग-अलग सदस्यों ने भी अपनी पहल की है जैसे कि इटली की मैटेई योजना. हालांकि आर्थिक रूप से (8.4 अरब अमेरिकी डॉलर) और भौगोलिक दायरे (ये काफी हद तक उत्तर अफ्रीका पर केंद्रित है) में ये छोटी है.
अफ्रीका में भारत एक और बड़ा किरदार है, विशेष रूप से जब बात वित्त प्रदान करने की आती है. भारत अफ्रीका में कर्ज़ देने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है और उसने इस महाद्वीप में 200 से ज़्यादा बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को पूरा किया है जबकि 69 अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है. भारत में भी एक उत्सुक निजी क्षेत्र है जो इसमें शामिल होना चाहता है. ख़बरों से पता चलता है कि बुनियादी ढांचे से जुड़ी भारत की निजी कंपनियां हर साल अफ्रीका में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश कर सकती हैं.
अमेरिका और EU ग्रुप ऑफ 7 (G7) के ज़रिए पहले से साझेदारी में काम कर रहे हैं. G7 के स्तर पर सदस्यों ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) के माध्यम से विकासशील देशों में 600 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का वादा किया है. इसमें साझा परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम करना भी शामिल है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC), ज़ाम्बिया और अंगोला के बीच पूरे लोबिटो कॉरिडोर में परिवहन के नेटवर्क में निवेश ऐसी परियोजनाओं के लिए मानक है. परिवहन, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटल क्षेत्रों में इस कॉरिडोर में 6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश किया गया है.
अमेरिका, EU और भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आवश्यक कारण हैं. पहला कारण ये है कि अफ्रीका में विकास से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए अधिक फंड की ज़रूरत है और तीनों में से कोई अकेले दम पर ये फंड नहीं दे सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि दुनिया भर में 2030 तक बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और खर्च के बीच 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर है. इसकी वजह से विकासशील देशों जैसे कि अफ्रीका के देशों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है. G7 की तरफ से PGII के ज़रिए 2027 तक 600 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने की महत्वाकांक्षा आवश्यकता की तुलना में कुछ भी नहीं है. इसके अलावा, हर देश अपने साथ अपने फायदे भी लाता है. भारत पूंजी के मामले में एक बड़ा देश है, उसके पास अफ्रीका के साथ भागीदारी करने का दशकों पुराना अनुभव है और उसका निजी क्षेत्र निवेश के लिए उत्सुक है. अमेरिका प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग खोलने में मदद कर सकता है और EU एवं इसके सदस्य देश अपनी स्थानीय सप्लाई चेन को एकीकृत करने में मदद कर सकते हैं.
दूसरा कारण ये है कि साझा परियोजनाओं पर सहयोग हर किसी के लिए जोखिम से बचने के एजेंडे का समर्थन करता है और चीन पर निर्भरता के ख़िलाफ एक महत्वपूर्ण संतुलन प्रदान करता है. भरोसेमंद सहयोगियों और साझेदारों के द्वारा समर्थित बुनियादी ढांचे के साथ महत्वपूर्ण सामग्रियों और खनिजों के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन की स्थापना करना तीनों पक्षों के लिए आपूर्ति की अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है. सुरक्षित सप्लाई लाइन से अमेरिका, यूरोप और भारतीय प्रयासों को भी फायदा होगा क्योंकि तीनों ने अपनी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक-दूसरे की तरफ रुख किया है. अगर जोखिम से अलग होने के ढांचे को साकार करना है तो तीनों को एक-दूसरे के साथ अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी.
जोख़िम से अलग होने का ये एजेंडा अफ्रीका तक जाना चाहिए. सामग्रियों के केवल खनन के बदले उन्हें प्रसंस्कृत करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इस महत्वपूर्ण सप्लाई चेन में अफ्रीका को जोड़ना अफ्रीकी देशों को एक अधिक आकर्षक प्रस्ताव प्रदान करता है जो चीन के द्वारा दिए जा रहे मॉडल के विपरीत है.
तीसरा कारण ये है कि सहयोग करना अमेरिका और EU के भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में मदद करता है. वैश्विक नेतृत्व के लिए एक साझेदार के रूप में भारत के साथ जुड़कर अमेरिका और EU ये संकेत दे सकते हैं कि वो भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को कितनी गंभीरता से लेते हैं. भारत के साथ अमेरिका और EU के ज़्यादातर द्विपक्षीय समझौते भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं. वैसे तो ये एक अच्छा प्रयास है लेकिन ये एक साझेदार के रूप में भारत की क्षमता के व्यापक दायरे पर ध्यान देने में नाकाम है और इसे सम्मान नहीं देने की आलोचना का सामना करना पड़ता है. इस मामले में बहुत कुछ किया जा सकता है.
उदाहरण के लिए EU ने अप्रैल 2022 में भारत के साथ सहयोग के दृष्टिकोण की रूप-रेखा सामने रखी जिसमें नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और डिजिटल परिवर्तन का समर्थन देने पर ध्यान दिया गया. EU के ग्लोबल गेटवे ने “भारत और इस क्षेत्र में सुरक्षित एवं टिकाऊ बुनियादी ढांचे में सहयोग और निवेश के लिए नए अवसरों” के उद्देश्य से विकास सहायता के एक भागीदार के रूप में भारत को रखा है.
भारत के साथ अमेरिका और EU के ज़्यादातर द्विपक्षीय समझौते भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं. वैसे तो ये एक अच्छा प्रयास है लेकिन ये एक साझेदार के रूप में भारत की क्षमता के व्यापक दायरे पर ध्यान देने में नाकाम है और इसे सम्मान नहीं देने की आलोचना का सामना करना पड़ता है.
अमेरिका ने भी EU की तरह भारत के विकास का समर्थन करने पर ध्यान दिया है, इसमें वैश्विक विकास की पहल के लिए एक साझेदार के रूप में भारत को नहीं रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान मोदी-बाइडेन दृष्टिकोण में इस बात का हवाला दिया गया है कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, विशेष रूप से “सॉवरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस (संप्रभु ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया) को बेहतर बनाने; सभी विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक में नए रियायती वित्त जमा करने समेत बहुपक्षीय विकास बैंक को विकसित करने के एजेंडे को आगे बढ़ाने; और PGII के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ एवं लचीले बुनियादी ढांचे के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने की महत्वाकांक्षा के स्तर को बढ़ाने में.”
चूंकि नियम आधारित विश्व व्यवस्था में कमज़ोरी को देखते हुए अमेरिका और यूरोप की नज़र दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने पर है, ऐसे में केवल विकास सहायता हासिल करने वाले देश की तुलना में एक साझेदार के रूप में भारत के साथ जुड़ने से दुनिया को लेकर पश्चिमी देशों के नज़रिए में चीन के मुकाबले भारत को और अधिक करीब लाने में मदद मिलेगी. पश्चिमी देशों के लिए, जहां भारत को एक महत्वपूर्ण “स्विंग स्टेट (जो किसी भी तरफ जा सकता है)” के रूप में देखा जाता है, भारत के साथ काम करने को सफल भागीदारी के एक तरीके के रूप में भी देखा जाएगा. ये अलग बात है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण समेत दूसरी भू-राजनीतिक चुनौतियों के बारे में भारत की दुविधा को लेकर पश्चिमी देश निराश हैं. इस तरह तालमेल के तरीके खोजना और भारत को पश्चिमी देशों के नज़दीक लाना अमेरिका और EU- दोनों के नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है.
भारत ने दशकों पुराने अपने गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक जारी रखा है और इस बात की संभावना है कि आगे भी वो ऐसा करेगा लेकिन उसे अफ्रीका में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर भी चिंतित होना चाहिए.
भारत की तरफ से देखें तो इस साझेदारी में शामिल होने के कई कारण हैं. तेज़ी से बनते बहुध्रुवीय विश्व में भारत की बेहतर स्थिति की राह में अफ्रीका में अपने संबंधों और मौजूदगी को बढ़ाना शामिल होगा. अमेरिका और यूरोप के साथ साझेदारी करना इस लक्ष्य को हासिल करने का एक आधार प्रदान करता है. भारत ने दशकों पुराने अपने गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक जारी रखा है और इस बात की संभावना है कि आगे भी वो ऐसा करेगा लेकिन उसे अफ्रीका में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर भी चिंतित होना चाहिए. अमेरिका और EU के साथ कनेक्टिविटी और सहयोग को गहरा करना वैश्विक व्यापार प्रणाली की सहायता करने में उसकी गंभीरता को दिखाएगा.
इस संभावना को वास्तविकता में बदलने के साधन और रूप-रेखा पहले से ही मौजूद हैं. G7 से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. जैसा कि बताया गया है, G7 की PGII ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अमेरिका और यूरोपीय दृष्टिकोणों में तालमेल की शुरुआत पहले ही कर दी है. फिर भी तालमेल में बढ़ोतरी के लिए और भी काम किया जा सकता है और करना भी चाहिए. आख़िरी G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने PGII पर बातचीत की. PGII पर चर्चा के लिए भारत को G7+ प्रारूप में शामिल करना एक अच्छी शुरुआत होगी. पूरे साल मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत को आमंत्रित करना एक अतिरिक्त लाभ होगा.
G7 के ज़रिए हो या किसी दूसरे तरीके से लेकिन भारत, अमेरिका और EU सबसे बुनियादी स्तर पर कर्मचारियों के बीच संपर्क की शुरुआत कर सकते हैं ताकि अफ्रीकी महाद्वीप में अपने समर्थन से चल रही मौजूदा या प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में एक-दूसरे को जानकारी दे सकें. इस प्रयास से संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी और विवेकपूर्ण सहयोग के क्षेत्रों की तलाश की जा सकती है.
जेम्स बैचिक अटलांटिक काउंसिल के यूरोप सेंटर में एसोसिएट डायरेक्टर हैं.
पृथ्वी गुप्ता ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रैटजिक स्टडीज़ प्रोग्राम में जुनियर फेलो हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

James Batchik is an associate director at the Atlantic Council’s Europe Center, where he supports programming on the European Union, the United Kingdom, Germany, the ...
Read More +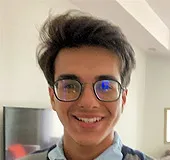
Prithvi Gupta is a Junior Fellow with the Observer Research Foundation’s Strategic Studies Programme. Prithvi works out of ORF’s Mumbai centre, and his research focuses ...
Read More +