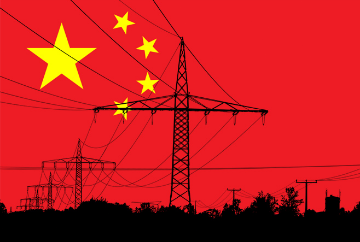भूमिका
ORF का चार्टर (संविधान) भारत के आर्थिक विकास से ताल्लुक रखता है. 1991 में इसके पहले पब्लिकेशन को पी एन धर, एम नरसिम्हन, आई जी पटेल और आर एन मल्होत्रा ने शक्ल दी थी, जिसका शीर्षक था, ‘आर्थिक सुधार का एजेंडाः संयुक्त बयान.’ इस दस्तावेज़ को लिखने वाले अपने-अपने क्षेत्र के दिग्गज थे. वे देश में नीति-निर्माण की उलझनों को बखूबी समझते थे. उन्हें यह भी पता था कि इसके लिए पहले से चले आ रही समस्याएं कितनी ज़िम्मेदार हैं. वे समस्याएं, जिन्हें बदलाव का राजनीतिक अर्थशास्त्र (पॉलिटिकल इकॉनमी) कहा जाता है. ये तब की पॉलिटिकल इकॉनमी की सीमाओं को अच्छी तरह समझते थे.
मुझे यहां कई आलेखों का सारांश समेटते हुए एक भूमिका लिखने का सम्मान मिला है. इन लेखों में देश की पिछले 30 साल की यात्रा का जिक्र है. जिन लोगों ने ये लेख लिखे हैं, वे हमारी समस्याओं और चुनौतियों को बखूबी समझते हैं और इनमें से कइयों ने पिछले 30 वर्षों में देश में हुए बदलावों को काफी करीब से देखा है. इनमें से हरेक ने इस दौरान हुए बदलावों के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू पर टिप्पणी की है. इसके साथ उन्होंने उन बदलावों की ओर भी ध्यान दिलाया है, जो नहीं हो सके. सबसे बड़ी बात यह है कि लेखकों ने भविष्य पर अपनी नज़र बनाए रखी है.
इसमें कोई शक नहीं कि 1991 का भुगतान संतुलन संकट अचानक नहीं आ खड़ा हुआ था. 80 के दशक में कई संकट और चुनौतियां सामने आए, जिन्होंने 1991 में एक बड़े संकट का रूप ले लिया. 80 के दशक में हमारे सामने जो चुनौतियां आईं, उनकी वजह तत्कालीन सरकारों का हद से अधिक ख़र्च रहा. हमने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की. दूसरे देशों के साथ देश ने रुपये में व्यापार करने का समझौता किया हुआ था. इसके साथ केंद्रीय योजना पर चलने वाले देशों और अन्य राष्ट्रों के साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे थे. इससे तत्कालीन भारतीय सरकारों को तसल्ली मिलती थी. उन्हें लगता था कि कोई संकट खड़ा हुआ तो भी इन देशों की बदौलत उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा. कई बार तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत वैश्विक संस्थाओं और दूसरे जरियों से कर्ज लेता रहता था. इन मुश्किलों से उबरने के लिए जरूरी राजकोषीय और ढांचागत (स्ट्रक्चरल) बदलाव नहीं किए गए. हम उन्हें टालते रहे, जबकि चीन और दूसरे एशियाई देशों ने ऐसी पहल हमसे काफी पहले कर दी थी. कहते हैं कि पांव उतना ही पसारना चाहिए, जितनी लंबी चादर हो. सरकारी खजाने की हालत की परवाह किए बिना खर्च करने की आदत 1991 में एक डरावने रूप में हमारे सामने आई. यूं तो इस संकट की आहट 1989 से ही दिखने लगी थी, लेकिन तब इस पर ध्यान नहीं दिया गया. हमने इस बारे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की चेतावनी की भी अनदेखी की, जिसने संकट से बचने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा था. इस मुश्किल को टालने की पहल आगामी चुनावों तक टाल दी गई. लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि इतिहास अक्सर आपको दूसरा मौका नहीं देता.
इसमें कोई शक नहीं कि 1991 का भुगतान संतुलन संकट अचानक नहीं आ खड़ा हुआ था. 80 के दशक में कई संकट और चुनौतियां सामने आए, जिन्होंने 1991 में एक बड़े संकट का रूप ले लिया. 80 के दशक में हमारे सामने जो चुनौतियां आईं, उनकी वजह तत्कालीन सरकारों का हद से अधिक ख़र्च रहा. हमने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की
1989 से 1991 के बीच चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने इन हालात में कई निर्णायक कदम उठाए. इनमें से एक था सोना गिरवी रखना ताकि देश बकाए कर्ज़ की किस्तें चुका पाए. उस दौर में केंद्र में बार-बार सरकारें बदल रही थीं और उससे अस्थिरता की स्थिति बनी थी. इन वजहों से संकट से निपटने के लिए अक्सर जिस तेज़ी से राजनीतिक पहल की जरूरत थी, वह भी धीमी पड़ने लगी. कर्ज़ संकट और हद से अधिक ख़र्च करने पर भी रोक लगाने की कोशिश हुई, जो उस वक्त तक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था कि उसका टिकाऊ रहना मुश्किल हो गया था.
1991 के सुधार और उसकी महत्ता
ये सारी बातें अब इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं. 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए, वे बहुत व्यापक थे. उनका अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर असर पड़ा. हालांकि, तब उन सुधारों का पूरा फ़ायदा माकूल राजनीतिक हालात नहीं होने के कारण नहीं उठाया जा सका. इस पहलू की ओर ए.के.भट्टाचार्य ने अपने लेख में ध्यान दिलाया है. इसे विडंबना ही कहा जाएगा, लेकिन 1991 के संकट ने देश के सामने कई अवसर भी पेश किए थे. अफ़सोस की बात है कि तत्कालीन पॉलिटिकल इकॉनमी और राजनीतिक माहौल के कारण हम उनका लाभ नहीं ले सके. 1991 में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बहुत संभलते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के साथ नियम-कायदों में ज़बरदस्त बदलाव किए गए, इसमें कोई शक नहीं कि मैक्रो इकॉनमी, राजकोषीय और ढांचागत स्तर पर ये दूरगामी बदलाव लाने वाले कदम थे. लेकिन शायद इन सुधारों पर हमारा भरोसा नहीं था, जिसकी ओर गौतम चिकरमाने ने अपने दो लेखों- ‘ऑन विंडोज़ ऑन रिफॉर्म्स’ यानी सुधारों की खिड़की और ‘ऑन कंस्ट्रेंट्स टू कन्विक्शन’ यानी भरोसे की सीमाएं – में इशारा किया है. सुधारों को लेकर यह वही मानसिक बोझा था, जिसे हम ढोते रहे. निजी क्षेत्र की पूंजी पर हमारा संदेह बना रहा. आर्थिक विकास सरकारी ख़र्च की बदौलत ही हो सकता है, इस भ्रम से भी हमें नुकसान हुआ.
इसी तरह से, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को लेकर चुनौतियों की ओर मोनिका हालन के आलेख में ध्यान दिलाया गया है. नरसिम्हन कमिटी की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के कारण बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए. उन्हें काम करने की अधिक स्वायत्ता मिली. प्रायॉरिटी सेक्टर को कर्ज़ देने और सरकार की ओर से ब्याज़ दरें तय किए जाने के मामलों में भी उन्हें राहत दी गई. प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक स्वतंत्र नियामक के रूप में स्थापना हुई, जो महत्वपूर्ण बदलाव था. हालांकि, बैंकों को पूरी तरह से मुक्त करने या वित्तीय इकाइयों के निजीकरण की पहल नहीं हुई. पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण में भी हमें सफ़लता नहीं मिली है और यह अभी तक एक अभिशाप बना हुआ है.
आर्थिक सुधारों और विदेश नीति के संबंधों पर हर्ष वी पंत ने इस सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण लेख लिखा है. इसमें दो राय नहीं है कि शक्तिशाली सोवियत संघ के टूटने और रूस की आर्थिक मुश्किलें बढ़ने के साथ कुवैत-इराक युद्ध का हमारे निर्यात और हमारे सामने मौजूद विकल्पों पर असर पड़ा. इसके साथ ही अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों और दूसरे द्विपक्षीय और वैश्विक संस्थाओं के जरिये देश को जो वित्तीय मदद मिली, उसमें आर्थिक नीतियों के साथ विदेश नीति का भी सहयोग रहा. इस तालमेल का ही नतीजा था कि आर्थिक सुधारों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को खोलने का सकारात्मक असर हुआ.
1991 में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बहुत संभलते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के साथ नियम-कायदों में ज़बरदस्त बदलाव किए गए, इसमें कोई शक नहीं कि मैक्रो इकॉनमी, राजकोषीय और ढांचागत स्तर पर ये दूरगामी बदलाव लाने वाले कदम थे. लेकिन शायद इन सुधारों पर हमारा भरोसा नहीं था
इन बातों से स्पष्ट है कि आर्थिक सुधारों के 30 साल के दौरान हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे आज अलग-अलग रूप में हमारे सामने हैं. इन सुधारों से देश की विकास दर तेज हुई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद मिली. पिछले साल एक रिपोर्ट आई. 2005-2016 के आंकड़ों पर आधारित UNDP की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस दशक में 27.3 करोड़ लोग गरीबी की दलदल से बाहर निकले. इस दौरान अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हुई. लोगों को अपनी पसंद के सामान खरीदने की आजादी मिली और नए दौर के उद्यमी और छोटे कारोबारी वजूद में आए. इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र ने महत्वपूर्ण जगह बनाई. 1991 में जहां उपभोक्ताओं के सामने सीमित विकल्प थे, उसके मुकाबले उन्हें आज बेशुमार विकल्प मिल रहे हैं. पिछले 30 साल में ज़बरदस्त बदलाव हुए हैं और इन पर यहां शानदार चर्चा भी हुई है.
इस तरह का परिवर्तन उस देश के लिए बहुत बड़ी बात है, जो लंबे वक्त तक ऐसी सुस्त ग्रोथ में फंसा हुआ था, जिसे राज कृष्ण ने तिरस्कार की भावना से ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ का नाम दिया. हम इस सुस्त ग्रोथ के कुचक्र से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, वे बिल्कुल अलग हैं. आज हमें दहाई अंकों में विकास दर की जरूरत है, ताकि देश में गरीबी कम से कम की जा सके और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके. इसके साथ ही, हमें भौतिक के साथ सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार लाना होगा, इनोवेशन (नई खोजों) को बढ़ावा देना होगा. तकनीक से होने वाले फायदों को गले लगाना होगा और नीतियों में खुलापन लाकर व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी ताकि वह देश के विकास का इंजन बन सके. इस सीरीज में जो लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं, उनमें इन बातों का जिक्र है. ऐसा एक लेख पूजा मेहरा ने लिखा है, जिसमें आज की नजर से वह 1991 के सुधारों का विश्लेषण कर रही हैं. एक लेख मिहिर शर्मा का भी है, जो चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए सुधारों पर जोर दे रहे हैं.
भविष्य से सुधारों की सफ़लता की शर्त
आर्थिक विकास दर को दहाई अंकों में ले जाने के लिए पॉलिटिकल इकॉनमी के लिहाज़ से हमें नीचे दिए गए कदम उठाने होंगेः पहला, यह बात समझनी और हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि ढांचागत सुधारों और मैक्रो-इकॉनमिक स्थिरता के बीच सीधा रिश्ता है. इस बात पर भी ग़ौर करना होगा कि कर्ज़ उतना ही हो, जिसे संभाला जा सके. राजकोषीय घाटा भी बेकाबू न हो. ये बातें हमारी प्राथमिकताओं में होनी चाहिए. यूं भी किसी वैश्विक संकट या महामारी की स्थिति में सरकारी खर्च़ को सीमित रखना संभव नहीं हो पाता, लेकिन लंबी अवधि में यह हमारी नीतियों की बुनियाद बना रहे. खुशकिस्मती की बात यह है कि देश का मौजूदा नेतृत्व मैक्रो-इकॉनमिक स्थिरता की अहमियत समझता है. उसे पता है कि कर्ज़ और राजकोषीय घाटा को एक स्तर से अधिक ऊपर नहीं जाने देना चाहिए.
इसके अलावा, हमें वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के रास्तों की उलझनों को दूर करना होगा और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में सुधार लाकर किसी निवेश से बाहर निकलने का रास्ता आसान बनाना होगा. अभी पायलट एक्सपेरिमेंट के तौर पर बैंकों में पब्लिक ओनरशिप (मालिकाना हक़) की जो जांच हो रही है, वह इतिहास का बोझा उतारने की पहल का हिस्सा होना चाहिए. किफायती कर्ज़ और कर्ज़ देने वाले समावेशी संस्थानों के मद्देनजर बैंकिंग और बीमा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अनिवार्य भूमिका है और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए ये जरूरी हैं. इनकी यह भूमिका संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों के लिए ही है.
दूसरा, सुधारों की प्रक्रिया और संस्थानों के बीच तालमेल ज़रूरी है, तभी तेज़ टिकाऊ आर्थिक विकास दर हासिल हो पाएगी. इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का भी बड़ा रोल है. संसद की ओर से उसे महंगाई दर को एक सीमा के अंदर रखने का निर्देश मिला है, लेकिन इसके साथ रिज़र्व बैंक को लचीली मौद्रिक नीति भी अपनानी होगी. इससे कॉरपोरेट क्षेत्र को सस्ता कर्ज़ मिल सकेगा और आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने में मदद मिलेगी.
सुधारों की प्रक्रिया और संस्थानों के बीच तालमेल ज़रूरी है, तभी तेज़ टिकाऊ आर्थिक विकास दर हासिल हो पाएगी. इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का भी बड़ा रोल है. संसद की ओर से उसे महंगाई दर को एक सीमा के अंदर रखने का निर्देश मिला है, लेकिन इसके साथ रिज़र्व बैंक को लचीली मौद्रिक नीति भी अपनानी होगी.
तीसरा, गवर्नेंस संहिता के तहत संस्थानों को बेहतर बनाना होगा. इस मामले में प्रशासनिक सेवाओं के गवर्नेंस के ढांचे पर गौर किया जा सकता है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों की ज़रूरतें पूरी होती हैं. इसमें जहां समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रतिभा का भी सम्मान होता है. आख़िरकार यह एक आधार की तरह काम करता है, जिससे एक तरह की स्थिरता मिलती है. राज्यों में कई बार राजनीतिक अस्थिरता का दौर आता रहता है, उसे देखते हुए स्थायी प्रशासनिक सेवा की महत्ता और बढ़ जाती है. इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की कैबिनेट ऑफ़िस के तालमेल के साथ केंद्रीय भूमिका निरंतरता और स्थिरता का संकेत होगी. इन सबके साथ मंत्रालयों, व्यवस्था और संगठन में बदलाव और गवर्नेंस के लिए नई संहिता बनाना आने वाले दौर में चुनौती होगी.
ईज़ ऑफ़ डुइंग बिजनेस यानी सुगम कारोबार, न्यायिक सुधार के मामलों में बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर इस बात को देखते हुए कि हमारे यहां मुकदमे की सुनवाई में काफ़ी वक्त़ लगता है और इसलिए विवादों को निपटाने में काफी वक्त़ जाया होता है. इस पर भी ग़ौर करना चाहिए कि इन मुकदमों में एक पक्ष सरकार होती है. ऐसे में कानून और उस पर न्यायिक अमल के बीच एक तालमेल दिखना चाहिए.
चौथा, अभी का सामाजिक ढांचा हमारी चाहतों को पूरा नहीं कर पा रहा है. इस लिहाज़ से नई शिक्षा नीति पर अमल और उसकी निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षण और उसके तौर-तरीकों को लेकर नई अप्रोच पर ज़ोर दिया गया है. हमें शिक्षा के क्षेत्र में विकल्प बढ़ाने होंगे. उच्चा शिक्षा से जुड़े संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देनी होगी. इसके साथ विश्वस्तरीय विदेशी संस्थानों की स्थापना के अवसर पैदा करने होंगे. इन संस्थानों को देश की शिक्षा प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा. इससे कौशल, रोज़गार के विकल्प बढ़ाने में ऐसी मदद मिलेगी, जिसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती.
नई शिक्षा नीति पर अमल और उसकी निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षण और उसके तौर-तरीकों को लेकर नई अप्रोच पर ज़ोर दिया गया है. हमें शिक्षा के क्षेत्र में विकल्प बढ़ाने होंगे. उच्चा शिक्षा से जुड़े संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देनी होगी.
पांचवां, लंबे वक्त से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अनदेखी के नतीजे महामारी के दौर में हमारे सामने आए और इसे दूर करने को लेकर कई पहल की जा सकती है. स्वास्थ्य पर ख़र्च जीडीपी के एक फीसदी पर रुका हुआ है, इसे बढ़ाकर करीब 3 फीसदी करना होगा. इसके साथ हमें मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया जैसे संस्थानों के लिए नियम-कायदे भी बदलने होंगे. स्वास्थ्य से जुड़े सहयोगी क्षेत्रों में हमें प्रतिभाओं को तैयार करना और निखारना होगा. इसकी ख़ातिर डिप्लोमेट ऑफ़ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) में ट्रेनिंग देने के साथ ज़मीनी स्तर पर चिकित्सा तंत्र में सुधार करना होगा. ख़ासतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला स्वास्थ्य केंद्रों में. इससे देश को मौजूदा महामारी के साथ भविष्य की आपदाओं के लिए ख़ुद को तैयार करने में मदद मिलेगी और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे निचले स्तर तक सुधार होगा.
छठा, टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं (सीमा शुल्क बढ़ाकर या दूसरे ज़रियों से आयात को बाधित करना) को लेकर हमें अपनी सोच दुरुस्त करनी होगी. अगर इस मामले में हमने अपनी सोच बदली तो विदेशी व्यापार देश की आर्थिक तरक्की का इंजन बन सकता है. इससे देश में उत्पादकता बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था कहीं अधिक सक्षम होगी. दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था अलग-थलग रहने के बाद भी तरक्की की राह पर बढ़ती रही. जो देश वैश्विक स्तर पर अर्थपूर्ण सहयोग करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, उन देशों में रोज़गार के मौके बढ़ते हैं और उन्हें अपने नागरिकों की स्किल (कौशल विकास) बेहतर करने में भी मदद मिलती है. जिन देशों ने ऐसा किया है, वहां लंबे समय तक समृद्धि बनी रही है. इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत के साथ हम एक प्रतिस्पर्धी व्यापारिक तंत्र नहीं बना सकते.
सातवां, चौथी औद्योगिक क्रांति को गले लगाने का मतलब है कि हमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कई तरह से और कई मोर्चों पर करना होगा. कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनेफिट (लाभार्थी के बैंक खाते में सरकारी मदद का पैसा सीधे भेजना), किसी परियोजना पर चल रहे काम की निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया की मुख्यधारा में लाना होगा. इनसे हमें 5जी की ओर शिफ्ट करने में आसानी होगी. आख़िर में यह हमारे आर्थिक और सामाजिक प्रबंधन का केंद्र बिंदू बन जाएगा.
जो देश वैश्विक स्तर पर अर्थपूर्ण सहयोग करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, उन देशों में रोज़गार के मौके बढ़ते हैं और उन्हें अपने नागरिकों की स्किल (कौशल विकास) बेहतर करने में भी मदद मिलती है. जिन देशों ने ऐसा किया है, वहां लंबे समय तक समृद्धि बनी रही है.
आठवां, कृषि क्षेत्र में कई सुधारों की ज़रूरत है. खेती-किसानी से आय कम से कम दोगुनी करने के लक्ष्य से इस क्षेत्र में सुधारों का रास्ता खुलेगा, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं. इसके साथ, कृषि क्षेत्र में तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा. इन सबसे कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में रोजगार के नए मौके बनेंगे. इसके साथ पानी की कमी, अधिक सिंचाई के कारण बिजली की ज्य़ादा खपत जैसी चुनौतियों का समाधान निकलेगा और खेती अधिक टिकाऊ हो पाएगी.
नौवां, बिजली के क्षेत्र में हमें ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए तरक्की की राह तैयार करनी होगी. अक्षय ऊर्जा के नए रूपों का फायदा उठाने के लिए नई आर्थिक गतिविधियों की ख़ातिर माहौल बनाना होगा. इसे हमें अपना नया मंत्र बनाना होगा. आज जब हम कोयले से चलने वाले बिजली के कारखानों से पीछे हट रहे हैं और इसके लिए अक्षय ऊर्जा के नए ज़रियों को अपना रहे हैं तो सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी की कहीं अधिक ज़रूरत है. इसके लिए कॉरपोरेट सेक्टर को रियायतें देनी होंगी, जिससे वह सौर, वायु और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाए. बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुसंधान की ख़ातिर भी वित्तीय मदद की दरकार होगी.
दसवां, कानून बनाने या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस के लिए तो संसद मंच बना हुआ है, लेकिन हमारी आर्थिक रणनीति को गढ़ने में इसकी भूमिका मुख्यधारा वाली नहीं रही है. संसद की स्थायी समितियों के कार्यकलाप में बदलाव, संसदीय बहस की प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ संसदीय सुधारों के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर जनप्रतिनिधियों का सहयोग हासिल करना होगा. अभी स्वतंत्र नियामक मंत्रालय या संसद की पड़ताल से बच जाते हैं. इस मामले में सुधार की ज़रूरत है.
आखिरी बात, पिछले बजट में सरकार की मानसिक सोच में एक बदलाव दिखा, जिसमें फेबियन समाजवाद से एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ने का संकेत दिया गया, जहां लोगों की अधिक से अधिक भलाई की ख़ातिर सरकारी पैसा ख़र्च करने की बात थी. यहां ज़रा फेबियन समाजवाद को भी समझ लेते हैं. यह एक किस्म का समाजवाद है, जिसकी स्थापना 1884 में लंदन में हुई. इसमें लोकतांत्रिक ढांचे का इस्तेमाल धीरे-धीरे समाजवाद को अपनाने की ख़ातिर करना था. खैर, पिछले बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की मौजूदगी घटाने का जो संकेत दिया गया, वह बहुत बड़ा बदलाव था.
.संसद की स्थायी समितियों के कार्यकलाप में बदलाव, संसदीय बहस की प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ संसदीय सुधारों के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर जनप्रतिनिधियों का सहयोग हासिल करना होगा. अभी स्वतंत्र नियामक मंत्रालय या संसद की पड़ताल से बच जाते हैं. इस मामले में सुधार की ज़रूरत है.
इसके साथ संघवाद (फेडरलिज़्म) का एक नया मॉडल आर्थिक विकास के हमारे किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी है. इसमें राज्य विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होंगे और आपसी बातचीत के ज़रिये इस योजना को सार्थक करना होगा. भविष्य में राज्यों की संख्या बढ़ सकती है और इसके साथ क्षेत्रीय दलों की संख्या भी बढ़ेगी. इसलिए मौजूदा और भविष्य के गठबंधन को एक स्थायी विमर्श तंत्र स्थापित करना होगा, जिस पर राज्य भरोसा करें. अभी जो सुधार हो रहे हैं और भविष्य में जो सुधार होंगे, उनके लिए भी यह व्यवस्था कारगर होगी.
इसके साथ हमें संविधान की एक बुनियादी समीक्षा भी करनी होगी. मिसाल के लिए, इसके 7वें शेड्यूल को बदला जा सकता है. इसे जिस मक़सद से लाया गया था, वह समय के साथ कमज़ोर पड़ता गया. आज इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है. यह बात याद रखनी होगी कि 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के संस्थान नहीं निपट सकते.
‘हम आज जो करते हैं, उसी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है.’- महात्मा गांधी
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV