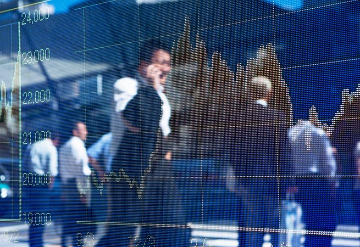अब जबकि ग़ज़ा में नाज़ुक युद्ध विराम लागू हो गया है, तो एक फिर से वही निराशाजनक माहौल दिख रहा है. बेहद भड़काऊ किस्म की एक कार्रवाई ने शोले भड़काए, हमास ने इज़राइल में बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाकर रॉकेट दाग़े और उसके बाद इज़राइल ने उसका कई गुना ज़्यादा ताक़त से जवाब दिया. इससे ग़ज़ा में जो तबाही मची, उसका मंज़र बेहद भयानक था. औरतों और बच्चों की मौत और पहले से ही बर्बादी के कगार पर खड़े ग़ज़ा में बेहद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की तबाही..! ग़ज़ा में हमने जो कुछ होता हुआ देखा वो वर्ष 2008 में तीन हफ़्ते तक चले संघर्ष की शो–रील देखने जैसा था. उस संघर्ष में क़रीब एक हज़ार फ़लिस्तीनी और क़रीब दर्जन भर इज़राइली नागरिक मारे गए थे. 2014 में दोहराया गया वैसा ही संघर्ष और भी लंबा और हिंसक था, जो क़रीब सात हफ़्तों तक चला था. उस युद्ध में दो हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए थे. इनमें से ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी थे.
राहत की बात बस यही है कि पिछली लड़ाइयों की तुलना में, 2021 के संघर्ष की मियाद कम थी. ये युद्ध केवल 11 दिनों तक चला. फिर भी इसमें क़रीब 250 लोगों की जान चली गई. हालांकि तरीक़ा वैसा ही था. संघर्ष के हर दौर के बाद युद्ध विराम की अपीलें होती हैं. पर्दे के पीछे से अमेरिकी प्रशासन और मिस्र के ख़ुफ़िया अधिकारियों की कोशिशें होती हैं, जो आपस में मिलकर एक नए युद्धविराम की पटकथा लिखते हैं. वहीं, ग़ज़ा में हर युद्ध विराम के बाद इज़राइल यही दावा करता है कि उसने हमास और उसके आतंकी ढांचे को कुचल दिया है. वहीं, हमास ये दावा करता है कि उसने बड़ी मज़बूती से इज़राइल के विस्तारवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है. दो तजुर्बेकार मुक्केबाज़ों की तरह वो थोड़ी देर ठहरकर सांसें लेंगे और फिर अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर देंगे.
राहत की बात बस यही है कि पिछली लड़ाइयों की तुलना में, 2021 के संघर्ष की मियाद कम थी. ये युद्ध केवल 11 दिनों तक चला. फिर भी इसमें क़रीब 250 लोगों की जान चली गई.
इन जानी-पहचानी निराशाजनक समानताओं के बावजूद, इस बार के युद्ध में कुछ बिल्कुल नई बातें हुई हैं. ये बातें इतनी अहम हैं जिनका असर हम स्थानीय ही नहीं व्यापक स्तर पर होते देखेंगे, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ तो क्षेत्रीय राजनीति से भी बाहर असर दिखाएं. ऐसे में इन सभी तत्वों और उनसे पैदा हुए सवालों पर नज़र डालना ज़रूरी है:
तीन संघर्षों की एक कहानी
ज़ाहिर है कि इस युद्ध के दौरान लोगों का ध्यान मोटे तौर पर तो ग़ज़ा में तबाही पर था. लेकिन, इससे हमें ग़ज़ा के अन्य पहलुओं पर हुए असर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. ये लड़ाई तब शुरू हुई थी, जब पूर्वी येरूशलम के शेख़ जर्राह इलाक़े में फ़लिस्तीनी जमा हुए थे, ताकि वो उस इकतरफ़ा और ज़बरदस्ती के क़ानून का विरोध कर सकें, जिससे उन्हें अपनी जगह ख़ाली करने का आदेश जारी होने का अंदेशा था. इस क़ानून के तहत यहूदी, पूर्वी येरूशलम और वेस्ट बैंक में उन इलाक़ों की संपत्तियों पर फिर से अपना दावा कर सकते, जिन पर 1948 से पहले उनका क़ब्ज़ा रहा हो. लेकिन, इस क़ानून में फ़लिस्तीनियों को पश्चिमी येरूशलम या इज़राइल में ऐसा ही दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है.
जल्द ही ये झड़प पास स्थित अल अक़्सा मस्जिद तक फैल गई. हिंसा ने पूर्वी येरूशलम के अलावा अन्य इलाक़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया. ये टकराव पश्चिमी बैंक के क़स्बों जैसे कि रामल्ला, नाज़रेथ और बेथलहम में भी फैल गया. यहां पर फ़लिस्तीनी बाशिंदों और इज़राइल के सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ. सबसे अहम बात ये कि, कई दशकों में पहली बार मिली–जुली आबादी वाले शहरों जैसे कि जफ़ा, टिबेरियास, एकर और लॉड में भी सांप्रदायिक हिंसा हुई. इस टकराव से ये चेतावनी भी दोहराई गई है कि 21 फ़ीसद इज़राइली नागरिक, फ़लिस्तीनी हैं, जो न केवल भेदभाव वाले क़ानूनों का सामना करते हैं, बल्कि वो उनको पड़ोस के पश्चिमी तट में भेदभाव से लागू किए जाने का भी विरोध करते हैं. इज़राइल, जैसा बर्ताव अपने फ़लिस्तीनी नागरिकों से करता है, उसकी तुलना अक्सर दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद से की जाती है. वैसे तो दोनों में बहुत फ़र्क़ है, लेकिन ये सवाल उठना तो वाजिब ही है कि क्या इज़राइल एक साथ यहूदी राष्ट्र और एक लोकतांत्रिक देश बना रह सकता है.
नेतन्याहू को सहारा?
इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ‘किसी संकट को हाथ से मत जाने दो’ के जुमले का बख़ूबी इस्तेमाल करते रहे हैं. लेकिन, इज़राइल की कट्टर दक्षिणपंथी और धार्मिक पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाकर, सबसे लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री बने रहने की उनकी उम्मीद टूट चुकी है. दो साल में चार आम चुनावों के बाद, एक गठबंधन सरकार बनाने की उनकी कोशिशें नाकाम रहीं. 120 सदस्यों वाली इज़राइली संसद नेसेट में वो अपने समर्थन में 61 सांसद नहीं जुटा सके. यहां तक कि नेतन्याहू ने चार सदस्यों वाली अरब इस्लामिक रआम पार्टी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की. लेकिन, नेतन्याहू का ये दांव उस वक़्त नाकाम रहा, जब कट्टर दक्षिणपंथियों ने इस क्रांतिकारी राजनीतिक क़दम को अस्वीकार कर दिया.
7 मई को इज़राइली पुलिस पवित्र अल अक़्सा मस्जिद में घुस गई, जिसके बाद हमास ने चेतावनी दी कि वो 10 मई तक मस्जिद कैंपस को ख़ाली कर दे. इज़राइलियों ने ऐसा नहीं किया और उसी रात हमास ने पहली बार इज़राइल पर रॉकेट दाग़े.
5 मई को राष्ट्रपति रिवलिन ने मध्यमार्गी येश एतिड पार्टी के यैर लैपिड को 28 दिनों के भीतर सरकार बनाने का न्यौता दिया. इसके अगले ही दिन इज़राइली पुलिस और फ़लिस्तीनियों के बीच संघर्ष हुआ. फ़लिस्तीनी नागरिक, सुप्रीम कोर्ट के उस अपेक्षित फ़ैसले का विरोध कर रहे थे, जिसके तहत छह फ़लिस्तीनी परिवारों को पूर्वी येरूशलम के शेख़ जर्राह इलाक़े में स्थित उनके घरों को ख़ाली कराकर उसे इज़राइलियों के हवाले किए जाने का डर था. 7 मई को इज़राइली पुलिस पवित्र अल अक़्सा मस्जिद में घुस गई, जिसके बाद हमास ने चेतावनी दी कि वो 10 मई तक मस्जिद कैंपस को ख़ाली कर दे. इज़राइलियों ने ऐसा नहीं किया और उसी रात हमास ने पहली बार इज़राइल पर रॉकेट दाग़े. इज़राइल ने इसका कई गुना अधिक ताक़त से जवाब दिया और इससे नेतन्याहू, ‘सबसे पहले सुरक्षा’ के अपने सिद्धांत के साथ एक बार फिर इज़राइली राजनीति के केंद्र में आ गए.
हालांकि, युद्ध विराम के बाद, नेतन्याहू के हाथ से सत्ता चली गई. कभी उनके साथी रहे कट्टरपंथी नेता नफ्टाली बेनेट 13 जून को इज़राइल के प्रधानमंत्री बन गए. बेनेट ने यैर लैपिड और अरब इस्लामिक रआम पार्टी जैसे कई छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई है. ये बात और है कि विश्लेषक आशंका जता रहे हैं कि बेनेट सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी.
पोटोमैक नदी में उठी लहरें
ग़ज़ा में हुए संघर्ष की अमेरिका की ओर से अजीब प्रतिक्रिया देखने को मिली. इसकी शुरुआत उसी जाने-पहचाने अंदाज़ से हुई, जो हम पहले भी देख चुके हैं. इज़राइल के पुराने समर्थक राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान दिया कि इज़राइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है. बाइडेन ने अपने पहले बयान में युद्ध विराम का ज़िक्र शायद बाद के लिए छोड़ दिया. लेकिन, ख़ुद बाइडेन की पार्टी के भीतर इज़राइल को मज़बूत समर्थन वाली दीवार में दरार आ रही है. महत्वपूर्ण बात ये है कि अमेरिकी प्रशासन के रवैये का विरोध केवल, डेमोक्रेटिक पार्टी के वो तरक़्क़ीपसंद नेता जैसे कि सीनेटर बर्नी सैंडर्स और रिप्रेज़ेंटेटिव एलेक्ज़ेंड्रिया ओकैसियो-कॉर्टेज़ व राशिदा त्लाइब नहीं कर रहे थे, जो पिछले चुनावों से ताक़तवर हो गए हैं. इन नेताओं ने इज़राइल द्वारा फ़लिस्तीनियों के मानव अधिकारों का मज़बूती से विरोध किया था. सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के आधे से ज़्यादा, 28 सदस्यों ने एक बयान जारी करने तुरंत युद्ध विराम की मांग की. वहीं, निचले सदन में ताक़तवर विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष रिप्रेज़ेंटेटिव ग्रेगरी मीक्स अपनी समिति के डेमोक्रेटिक सदस्यों को बता रहे थे कि वो राष्ट्रपति बाइडेन से मांग करेंगे कि वो इज़राइल को 73.5 करोड़ डॉलर के हथियारों का पैकेज देना टालने की मांग करेंगे.
जब 20 मई को युद्ध विराम का ऐलान किया गया, तब बाइडेन ने मीडिया से बात करके ख़ुद को ‘चुपचाप मज़बूत कूटनीतिक’ रास्ता अपनाने का श्रेय दिया, और बताया कि उन्होंने ख़ुद नेतन्याहू से छह बार फ़ोन पर बात की थी.
पार्टी का ये इशारा मिलते ही बाइडेन प्रशासन सक्रिय हो गया. इज़राइल के सैन्य अभियान को शुरुआत में हरी झंडी देने के बाद, 17 मई को राष्ट्रपति कार्यालय से युद्ध विराम का सख़्त बयान जारी किया गया. इसके बाद 19 मई को ख़ुद बाइडेन की ओर से नेतन्याहू को कड़ा संदेश देने वाला बयान जारी करके संघर्ष को ख़त्म करने की मांग की गई. जब 20 मई को युद्ध विराम का ऐलान किया गया, तब बाइडेन ने मीडिया से बात करके ख़ुद को ‘चुपचाप मज़बूत कूटनीतिक’ रास्ता अपनाने का श्रेय दिया, और बताया कि उन्होंने ख़ुद नेतन्याहू से छह बार फ़ोन पर बात की थी.
इस मामले में बाइडेन प्रशासन के रुख़ में बदलाव से फ़र्क़ ये पड़ा कि लड़ाई कुछ हफ़्ते चलने के बजाय कुछ दिनों में ही रुक गई. इससे ये भी पता चलता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर बदलाव आ रहा है. अमेरिकी युवा यहूदी, इज़राइल समर्थक संगठन जे-स्ट्रीट की तरफ़ झुकाव रखते हैं, तो मुखर यहूदी पीएसी के सदस्य ये मांग कर रहे हैं कि अमेरिका, इज़राइल के प्रति संतुलित नीति अपनाए जिससे कि दो राष्ट्रों के निर्माण से मसले का हल निकले, और इज़राइल के साथ साथ फिलिस्तीनियों की भी वाजिब उम्मीदें पूरी हों. युद्ध विराम की मांग की अगुवाई जॉर्जिया से नए चुने गए 34 साल के सीनेटर जॉन ओसॉफ ने की. ओसॉफ को संसद में अमेरिकी यहूदियों की नुमाइंदगी करने वाला नयी पीढ़ी का चेहरा माना जाता है. ये इस बात का सुबूत है कि इज़राइल को लेकर अमेरिका की सोच में बदलाव आ रहा है.
अब्राहम समझौतों की नाज़ुक स्थिति
अल अक़्सा मस्जिद में हिंसा और ग़ज़ा में इज़राइल की भयंकर बमबारी ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे खाड़ी देशों को मुश्किल में डाल दिया है. इन देशों ने अगस्त 2020 में हुए अब्राहम समझौतों के ज़रिए इज़राइल से कूटनीतिक रिश्ते क़ायम किए हैं. पिछले कुछ महीनों के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने तो बड़ी तेज़ी से इज़राइल के साथ वित्त, तकनीक, कृषि, पर्यटन और सुरक्षा संबंधी समझौते किए हैं; और हमास और उसके उग्र इस्लामकि एजेंडे को संयुक्त अरब अमीरात से समर्थन नहीं मिलता है. लेकिन, अल अक़्सा मस्जिद में इज़राइल की उकसावे वाली और वो भी रमज़ान की सबसे पाक रात लेलत अल क़द्र के दौरान कार्रवाई बिल्कुल अलग मसला है. मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद पर हमले के प्रति कड़ा क़दम उठाने की अपेक्षा की जाती है. संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के अलावा इस्लामिक देशों के संगठन ने इस पर तीख़ी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की. इस घटना से अरब देशों को ये बात भी याद दिलाई गई कि इज़राइल और फ़लिस्तीन का ये अनसुलझा राजनीतिक विवाद और फिलिस्तीनियों की अधूरी राष्ट्रीय ख़्वाहिशें, किसी भी क्षेत्रीय समीकरण को बिगाड़ने की ताक़त रखती हैं. संयुक्त अरब अमीरात ने फौरन ये याद दिलाई कि अब्राहम समझौते ने पश्चिमी तट के कई इलाक़ों पर इज़राइल का क़ब्ज़ा होने से रोका है. लेकिन एक स्थायी शांति प्रक्रिया के अभाव में ये विस्तार टिकाऊ तौर पर रुकने की उम्मीद नहीं.
फ़लिस्तीन का क्या होगा?
नेतन्याहू सरकार की सरपरस्ती में यहूदी बस्तियों के फ़लिस्तीनी इलाक़ों में लगातार विस्तार ने न केवल पश्चिमी तट को एक छोटे से इलाक़े में तब्दील कर दिया है, बल्कि एक फ़लिस्तीनी राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक उपयोगिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इस बात की कोई संभावना है नहीं कि भविष्य में कोई इज़राइली सरकार इन अवैध यहूदी बस्तियों को समेटेगी. इसके लिए ज़रूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से दो राष्ट्रों के समाधान का नुस्ख़ा भी कमज़ोर हुआ है. इन हालात में एक नई कोशिश होनी चाहिए. लेकिन, ये ट्रंप/कुशनर की ‘सदी के समझौते’ से बिल्कुल अलग होगी. क्योंकि ‘डील ऑफ़ सेंचुरी’ के तहत पश्चिमी तट और ग़ज़ा को ज़मीन के मसले के तौर पर देखा था और इससे जवाब तो कम मिले, सवाल ज़्यादा खड़े हो गए. क्या जो बाइडेन प्रशासन इस मसले में दख़ल देने का साहस दिखाएगा, जो पिछले पचास साल से हर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पहेली बना हुआ है? सवाल ये भी है कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी के तरक़्क़ीपसंद नेता ज़मीन पर वास्तविक शांति प्रक्रिया शुरू करने तक अपना दबाव बनाए रख पाएंगे? उतना ही अहम सवाल ये भी है कि क्या फ़लिस्तीनी नेतृत्व एकजुट होकर ग़ज़ा में हमास और रामल्ला में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच किसी तरह का राब्ता क़ायम कर पाएगा, जिससे वो एक सुर में बोल सकें? इनमें से कुछ सवालों के जवाब अगले कुछ महीनों में मिल सकते हैं.
नेतन्याहू सरकार की सरपरस्ती में यहूदी बस्तियों के फ़लिस्तीनी इलाक़ों में लगातार विस्तार ने न केवल पश्चिमी तट को एक छोटे से इलाक़े में तब्दील कर दिया है, बल्कि एक फ़लिस्तीनी राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक उपयोगिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
भारत के लिए मुश्किल
इस मामले में भारत एक बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है. वो फ़लिस्तीनियों को अपने पारंपरिक समर्थन और इज़राइल के साथ तेज़ी से बढ़ रहे संबंधों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. भारत की दुविधा समझने के लिए हमें एक नज़र इतिहास पर डाल लेनी चाहिए. भारत ने इज़राइल को मान्यता तो 1948 में ही दे दी थी. लेकिन, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध केवल 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने क़ायम किए थे. तब तक इज़राइल की मुंबई में एक कॉन्सुलेट के ज़रिए मामूली मौजूदगी थी, वहीं भारत का इज़राइल में कोई कूटनीतिक ठिकाना नहीं था. इसकी तुलना में भारत ने 1980 में ही फ़लिस्तीनी मुक्ति संगठन को कूटनीतिक दर्जा दे दिया था. जब पीएलओ ने 1988 में स्वतंत्र फ़लिस्तीनी राष्ट्र और पूर्वी येरूशलम को इसकी राजधानी घोषित किया था, तब से भारत, यासिर अराफ़ात को एक देश के प्रमुख का दर्जा देने लगा था.
भारत ने पहले ग़ज़ा में अपने प्रतिनिधि का दफ़्तर 1996 में खोला था. लेकिन, जब ग़ज़ा पर हमास का क़ब्ज़ा हो गया, और फ़लिस्तीनी मुक्ति संगठन का प्रभाव केवल पश्चिमी तट तक रह गया, तो भारत अपना कूटनीतिक दफ़्तर ग़ज़ा से रामल्ला ले गया था. इज़राइल के साथ भारत के संबंध तो तेज़ी से बढ़े. लेकिन, कभी इनका शोर नहीं मचाया गया. वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य मंचों पर भारत, फिलिस्तीनी के हक़ में खुलकर आवाज़ उठाता रहा. वाजपेयी सरकार के दौरान धीरे–धीरे इसमें बदलाव आने लगा. तब पहली बार भारत से इज़राइल के बीच मंत्रिस्तर के दौरे हुए. 2003 में एरियल शैरोन, भारत आने वाले पहले इज़राइली प्रधानमंत्री बने. 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भारत की नीति में और बदलाव आया. 2015 में प्रणब मुखर्जी रामल्ला जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने. वहीं, 2018 में नरेंद्र मोदी इज़राइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. इन दो ऐतिहासिक दौरों के बीच फ़लिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, 2017 में भारत के दौरे पर आए. भारत ने इज़राइल और फ़लिस्तीन का समर्थन करने के साथ साथ पूर्वी येरूशलम के मसले पर ज़्यादा संतुलित रुख़ अपनाना शुरू किया.
भारत ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की हिदायत देने के साथ ये कहा था कि वो ऐसा कोई क़दम न उठाएं जिससे तनाव बढ़े या पूर्वी येरूशलम व अन्य इलाक़ों की यथास्थिति में बदलाव हो.
मौजूदा संकट ने संतुलित नीति पर चलने की चुनौतियों को फिर से उजागर कर दिया है. भारत को समय पर बिना शर्त सैन्य सहायता देने वाले इज़राइल का, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के बयान पर नाख़ुशी जताना तो बनता है. भारत ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की हिदायत देने के साथ ये कहा था कि वो ऐसा कोई क़दम न उठाएं जिससे तनाव बढ़े या पूर्वी येरूशलम व अन्य इलाक़ों की यथास्थिति में बदलाव हो. जब नेतन्याहू ने इस संघर्ष के दौरान इज़राइल के साथ मज़बूती से खड़े होने वाले देशों को शुक्रिया कहने वाला ट्वीट किया, तो उसमें भारत के झंडे की नामौजूदगी ज़ाहिर थी.
आगे का रास्ता
मौजूदा युद्ध विराम से इज़राइल और फ़लिस्तीन के रिश्तों की मरहम पट्टी भर हुई है. इससे दोनों पक्षों के गंभीर मतभेदों वाले पेचीदा विवाद का हल निकलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है. भले ही इस संघर्ष ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा हो, लेकिन स्थायी शांति बहाल करने के लिए इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को मज़बूती से कोशिश करनी होगी. इसमें अमेरिकी सरकार को सबसे बड़ी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी. लेकिन, किसी भी कोशिश को सफ़ल बनाने के लिए इसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिस्र, जॉर्डन और क़तर को भी जोड़ना होगा.
मिस्र के इज़राइल के साथ कूटनीतिक संबंध हैं और वो ग़ज़ा जाने के लिए अहम रफ़ा के रास्ते पर नियंत्रण रखता है. मिस्र की सिसी सरकार भले ही हमास को सख़्त नापसंद करती हो. लेकिन, मिस्र की ख़ुफ़िया एजेंसियों का हमास पर हमेशा ही अच्छा प्रभाव रहा है. वहीं, इज़राइल के साथ लंबे समय से कूटनीतिक रिश्ते रखने वाला जॉर्डन का 1967 के युद्ध के बाद से ही अल अक़्सा मस्जिद पर नियंत्रण है. ये पश्चिमी तट पर रहने वाले फिलिस्तीनियों को बाहरी दुनिया से जोड़ने का अहम काम करता है और ख़ुद जॉर्डन में भी काफ़ी तादाद में फ़लिस्तीनी रहते हैं. वहीं, क़तर इसलिए अहम है, क्योंकि उसके संबंध हमास से हैं और वो ग़ज़ा का प्रशासन चलाने में हमास की वित्तीय मदद करता है. हमास के पूर्व प्रमुख ख़ालिद अल मशाल और कई दूसरे नेता दोहा से ही अपना नेटवर्क चलाते हैं. फ़लिस्तीन के पूर्व सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद दहलान अबू धाबी में रहते हैं. वहीं राष्ट्रपति महमूद अब्बास और उनके समर्थकों पर सऊदी अरब का अच्छा प्रभाव है.
इज़राइल ने ख़ुद से तो फ़लिस्तीनियों की उम्मीदें जगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है. उसकी कई गुना ज़्यादा सैन्य ताक़त और अमेरिका से मिलने वाले राजनीतिक समर्थन ने समस्या को बातचीत से सुलझाने की राह में रोड़े ही अटकाए हैं. वहीं, यथास्थिति बनी रहने और फ़लिस्तीनी इलाक़ों में बस रहे यहूदियों के बढ़ते विस्तारवादी दुस्साहस से फ़लिस्तीनियों की बढ़ती नाराज़गी पर लंबे समय तक क़ाबू नहीं रखा जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से ठोस प्रयास न हुए तो एक और संघर्ष लगभग तय है. तो, ग़ज़ा में अगली लड़ाई छिड़ने तक, ये युद्धविराम स्वागतयोग्य है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV