-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने का वादा किया है. लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने इजराइल का समर्थन करने की मंशा जताई है और अहम मुद्दों पर उनका जो विरोधाभासी नज़रिया रहा है, वो पश्चिम एशिया के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करता है.

Image Source: Getty
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपने समर्थकों को संबोधन के दौरान गाज़ा में चल रहे युद्ध का जिक्र किए बगैर कहा था, "मैं युद्ध रोक दूंगा". ट्रंप ने दुनिया में शांति स्थापित करने के अपने इरादे को ज़ाहिर करते हुए यह भी कहा था कि वर्ष 2017-2020 के दौरान उनके राष्ट्रपति रहते हुए विश्व में कोई भी ऐसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ, जिसमें अमेरिका का दख़ल रहा हो. उन्होंने अपने समर्थकों से ज़ोर देकर कहा कि आने वाले वर्ष, "सही मायनों में अमेरिका के लिए स्वर्णिम काल की तरह होंगे". ट्रंप ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन अपनी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के माध्यम से अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे. इस लेख में राष्ट्रपति ट्रंप के विश्व में शांति स्थापित करने के दावों और इरादों की विस्तार से पड़ताल की गई है. साथ ही इस लेख में ख़ास तौर पर पश्चिम एशिया को लेकर ट्रंप द्वारा कही गई बातों की ज़मीनी हक़ीक़त जानने की कोशिश की गई है. इसके लिए राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान पश्चिम एशिया को लेकर अपनाई गई अमेरिकी विदेश नीति का विश्लेषण किया गया है, साथ ही आकलन किया गया है कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मिडिल ईस्ट में व्यापक रूप से क्या प्रभाव पड़ सकता है.
इस लेख में राष्ट्रपति ट्रंप के विश्व में शांति स्थापित करने के दावों और इरादों की विस्तार से पड़ताल की गई है. साथ ही इस लेख में ख़ास तौर पर पश्चिम एशिया को लेकर ट्रंप द्वारा कही गई बातों की ज़मीनी हक़ीक़त जानने की कोशिश की गई है.
डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे. ट्रंप ने तब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को चुनाव में हराया था. हिलेरी क्लिंटन को 232 वोट मिले थे, जबकि ट्रंप को 306 वोट हासिल हुए थे. ट्रंप के पूर्ववर्ती यानी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2014 में दाएश आतंकवादी संगठन (जिसे ISIS/ISIL या इस्लामिक स्टेट के तौर पर भी जाना जाता है) ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था. दाएश इराक़ में आतंकी संगठन अलकायदा का सहयोगी रह चुका था. दाएश पर पूरी दुनिया की नज़र उस समय पडी थी, जब इसके आतंकवादियों ने उस समय सीरिया में चल रहे गृह युद्ध और इराक़ में चल रहे मजहबी टकराव का फायदा उठाते हुए इराक़ और सीरिया के बड़े भूभाग पर कब्ज़ा कर लिया था. वर्ष 2014 में ही ओबामा प्रशासन ने दाएश के ख़िलाफ़ "इनहेरेंट रिजॉल्व" नाम का एक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें अमेरिका समेत सहयोगी देशों की सेनाएं शामिल थीं. इसके तहत अमेरिका ने दाएश के विरुद्ध कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन नहीं चलाया था, बल्कि आतंकी संगठन के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे दूसरे स्थानीय सहयोगी अभियानों की खुलकर मदद की थी.
गाज़ा में युद्ध रोकने के लिए ट्रंप जिस दूसरे विकल्प पर विचार कर सकते हैं, वो इजराइल को अपना समर्थन बनाए रखते हुए, ज़रूरत पड़ने पर नेतन्याहू को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना हो सकता है.
2017 में अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने दाएश आतंकी संगठन के ख़िलाफ़ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की रणनीति को ही लागू रखा. इसके अलावा, ट्रंप ने कुछ नए क़दमों को भी उठाया, जिनमें तेज़ कार्रवाई के साथ ही ज़्यादा निर्णायक अभियानों का संचालन शामिल था, हालांकि इसमें जोख़िम अधिक था. ज़ाहिर है कि अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन देशों की वायु सेनाओं द्वारा चलाए गए अभियान की बदौलत ही इराक़ी एवं सीरियाई सेनाओं को बड़ी क़ामयाबी मिली थी. कई महीनों तक चले इस संघर्ष के बाद आख़िरकार जुलाई 2017 में इराक़ी सेनाओं ने मोसुल पर और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) ने अक्टूबर 2017 में रक़्क़ा पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया. अमेरिका की अगुवाई में चलाए गए इन अभियानों का ही नतीज़ा था कि दिसंबर 2017 में इराक़ ने दाएश का सफाया करने का ऐलान कर दिया और सीरियाई सेनाओं ने फरवरी 2019 में दाएश आतंकियों को सीमा पर स्थित बागौज़ गांव तक सीमित कर दिया. इस प्रकार से इराक़ और सीरिया दोनों ही देशों में आईएसआईएस आतंकियों का नामोनिशान मिट गया और उनके कब्ज़े से पूरे इलाक़े को खाली करा लिया गया. यहां गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के दौरान ढाई वर्षों तक चले सैन्य अभियान में दाएश आतंकी संगठन को तुर्किये के साथ लगी अपनी इकलौती अंतर्राष्ट्रीय सीमा को खोना पड़ा. इतना ही नहीं, ओबामा के जाने के बाद और ट्रंप प्रशासन के आने तक दाएश के कब्ज़े वाले आधे इलाक़ों को आज़ाद करा लिया गया था. जबकि, दाएश द्वारा इराक़ और सीरिया में कब्ज़ाए गए बाक़ी आधे क्षेत्र को ट्रंप शासन के नौ महीनों के भीतर ही मुक्त कराने में सफलता मिल गई थी. यह दिखाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दाएश के ख़िलाफ़ कितनी सख़्ती के साथ सैन्य अभियानों को संचालित किया गया.
देखा जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप के शासन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ओबामा द्वारा अपनाई गई सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण सामरिक बदलाव किए गए थे. उदाहरण के तौर पर ट्रंप ने "सैन्य अभियान संचालित करने वालों को दुश्मन की कमज़ोरियों पर नज़र रखने और उनके खिलाफ़ आक्रामक व तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्हें ज़ल्द निर्णय लेने के भी अधिकार दिए." कहने का मतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने ऐसी प्रक्रिया बनाई, जो ज़्यादा पेचीदा नहीं थी और दुश्मन पर हमले की अनुमति में देरी नहीं होती थी. यानी ज़मीन पर आतंकियों के ख़िलाफ़ लड़ रही सहयोगी सेनाओं ने जब भी हवाई हमले का आग्रह किया तो बिना समय गंवाए कार्रवाई की अनुमति दी गई. तब ट्रंप द्वारा कहा भी गया था कि "हमने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों में पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक प्रगति की है." इसके अलावा, दाएश आतंकी संगठन को धूल चटाने के पीछे ट्रंप का मुख्य मकसद पश्चिम एशिया में शांति की बहाली नहीं था, बल्कि अमेरिकी नागरिकों को होने वाले नुक़सान को रोकना था, जो दिखाता है कि वो “अमेरिका फर्स्ट” के अपने नारे को लेकर कितने गंभीर है. कहा जाता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के एक साल के अंदर ही आतंकी संगठन दाएश का लगभग पूरी तरह से सफाया हो गया था. इसी के चलते इराक़ और सीरिया दाएश के कब्ज़े वाले क्षेत्रों को दोबारा हासिल करके और वहां पुनर्निर्माण व शांति स्थापना की शुरुआत कर पाए.
ट्रंप के पहले कार्यकाल पर नज़र डालें तो लगातार विवादों में कूदने और उनसे बाहर निकलने की वजह से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का ख़तरा पैदा हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका की मौज़ूदगी को काफ़ी हद तक कम कर दिया था, जिससे कहीं न कहीं अमेरिका को कभी ख़त्म नहीं होने वाले युद्धों से बाहर निकालने का उनका वादा पूरा हुआ था. ट्रंप ने वर्ष 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते से क़दम वापस खींच लिए थे. इस परमाणु समझौते का मकसद P5 + 1 द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के बदले, ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध लगाना था, जिसमें कहीं न कहीं ईरान की भी रज़ामंदी शामिल थी. अमेरिका द्वारा इस परमाणु समझौते से अपने क़दम पीछे खींचने के कारण एक नया संकट पैदा हो गया था. ट्रंप प्रशासन ने उसी दौरान ईरान के विरुद्ध अधिक से अधिक दबाव बनाने की मुहिम भी शुरू की थी, जिससे ईरान के साथ टकराव की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. हालांकि, वर्ष 2019 की गर्मियों में फारस की खाड़ी में ईरान की आक्रामकता पर ट्रंप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिसके चलते मिडिल ईस्ट की शांति को कोई झटका नहीं लगा था.
ट्रंप ने जिस प्रकार से एक विवादास्पद फैसले के तहत अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरुशलम में स्थानांतरित किया था, उससे फिलिस्तीनियों को उनकी बातों पर यकीन नहीं है.
ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर उनकी नीति की बात करें, तो उन्होंने एक तरफ हमेशा इजराइल के अपनी सुरक्षा के अधिकार की तरफदारी की, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के आज़ादी के अधिकार को भी मान्यता दी. वर्ष 2018 में जिस प्रकार से ट्रंप ने दो-राष्ट्र समाधान पर ज़ोर दिया था, उसमें उनकी इसी नीति की झलक दिखाई देती है. तब उन्होंने कहा था कि दो-राष्ट्र का फार्मूला मध्य-पूर्व में व्यापक स्तर पर शांति की स्थापना के लिहाज़ से सबसे उपयुक्त और कारगर सिद्ध होगा. ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दौरान कहा था कि, "मेरा यह दृष्टिकोण दोनों पक्षों के लिए एक "विन-विन" की स्थिति उपलब्ध कराता है. दो-राष्ट्र समाधान वर्तमान हालातों के मुताबिक़ सबसे उचित और व्यावहारिक विकल्प है, जो इजराइल की सुरक्षा से लेकर फिलिस्तीनी के एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व के मुद्दे का सबसे अच्छा समाधान पेश करता है." इतना ही नहीं, ट्रंप ने आगे कहा कि वे कुछ महीनों के भीतर अपने शांति समझौते की अंतिम योजना का खुलासा करेंगे. उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि मैं राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस फार्मूले को मुकम्मल कर पाऊं." जहां तक फिलिस्तीनियों की बात है, तो उन्हें ट्रंप के वादों और इरादों पर संदेह है. ख़ास तौर पर वर्ष 2017 में ट्रंप ने जिस प्रकार से एक विवादास्पद फैसले के तहत अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरुशलम में स्थानांतरित किया था, उससे फिलिस्तीनियों को उनकी बातों पर यकीन नहीं है.
पुरानी बातों से आगे बढ़कर अगर वर्ष 2024 के ताज़ा सूरते हाल पर नज़र डालें, तो वर्तमान में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत लिया है. राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कमला हैरिस ने अपने आख़िरी भाषण में गाज़ा में जारी युद्ध को समाप्त करने का वादा किया था. उनके इस वादे से साफ ज़ाहिर होता है कि उनकी पार्टी की सरकार द्वारा जिस प्रकार से इजराइल को लगातार सैन्य मदद दी जा रही थी, यह उससे हुए नुक़सान को भरपाई की ही एक कोशिश थी. चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी मध्य-पूर्व में "शांति" बहाली का वादा किया है. अपने भाषणों के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे गाज़ा में चल रहे युद्ध को समाप्त कर देंगे. ज़ाहिर है कि गाज़ा की लड़ाई में क़रीब 45,000 लोग मारे गए हैं और इस युद्ध में गाज़ा का पूरा इलाक़ा तहस-नहस हो चुका है. इतना ही नहीं लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान जैसे पड़ोसी देशों पर भी गाज़ा युद्ध के छींटे पड़े हैं. यह अलग बात है कि विदेश नीति को लेकर ट्रंप अक्सर विरोधाभासी और दुविधापूर्ण बयानबाज़ी करते रहते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई संदेह नहीं है कि चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप जो भी वादे करते हैं, उन्हें हर हाल में पूरा करते हैं.
ज़ाहिर है कि गाज़ा की लड़ाई न केवल मिडिल ईस्ट, बल्कि अन्य क्षेत्रों की शांति के लिए एक गंभीर ख़तरा बन चुकी है. ऐसे में यह निश्चित है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद ट्रंप इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए कुछ कड़े फैसले ज़रूर लेंगे. हालांकि, ट्रंप के फैसलों में इजराइल को जारी समर्थन और दुनिया में शांति स्थापित करने के उनके संकल्प के बीच संतुलन ज़रूर दिखाई देगा. महीनों तक चले अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई मौक़ों पर गाज़ा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के अपने इरादों को खुलकर ज़ाहिर किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध की समाप्ति के लिए इजराइल को भी साफ शब्दों में बता दिया है कि उसे कब तक ऐसा करना होगा. उन्होंने कहा है कि उनके औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले इजराइल को हमास के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे अपने अभियान को ख़त्म करना होगा. ख़बरों के मुताबिक़ ट्रंप ने हाल ही में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल से हुई बातचीत के दौरान हमास पर भी दबाव डाला है और उससे बड़े मसलों पर अपने क़दम वापस खींचने को कहा है. लग रहा है कि हमास भी ट्रंप के सामने झुक गया है. ऐसा इसलिए, क्योंकि हमास ने इस बात पर सहमति जता दी है कि लड़ाई समाप्त होने के पश्चात गाज़ा पट्टी में इजराइली सेनाएं अस्थाई रूप से अपना दख़ल दे सकती हैं. इसके अलावा, हमास बंधक बनाए गए अमेरिकियों समेत सभी विदेशी नागरिकों की सूची देने पर भी राज़ी हो गया है. साथ ही हमास इस पर भी मान गया है कि इन विदेशी नागरिकों को युद्ध विराम समझौते की शर्तों के मुताबिक़ रिहा किया जाएगा. माना जा रहा है कि जिस प्रकार से ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनके पदभार ग्रहण करने से पहले यह समझौता पूरा हो जाना चाहिए, हमास के लचीले रुख के पीछे इसी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है. ट्रंप युद्धों के विरोधी रहे हैं, ऐसे में इजराइल के समर्थन में अमेरिका द्वारा क्षेत्र में युद्ध को हवा दी जाएगी, इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती है.
ज़ाहिर है कि गाज़ा की लड़ाई न केवल मिडिल ईस्ट, बल्कि अन्य क्षेत्रों की शांति के लिए एक गंभीर ख़तरा बन चुकी है. ऐसे में यह निश्चित है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद ट्रंप इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए कुछ कड़े फैसले ज़रूर लेंगे.
निसंदेह तौर पर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप "अमेरिका को फिर से महान बनाने" के अपने वादे को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे और उनके हर क़दम में यह दिखाई देगा. ऐसे में यह तय है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका की विदेश नीति में दूसरे राष्ट्रों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती करने पर ज़ोर होगा और इसमें इजराइल भी शामिल होगा. यानी इजराइल को दी जाने वाले अमेरिकी सैन्य मदद पर भी लगाम लगाई जाएगी. ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में कई बार गाज़ा में चल रहे युद्ध ख़त्म करने को लेकर बयान दिए हैं. अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ट्रंप के संबंधों की बात की जाए, तो दोनों नेताओं के बीच बेहद जटिल रिश्ते रहे हैं. हालांकि, ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप नेतन्याहू पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बना सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू पर युद्ध ख़त्म करने का घरेलू दबाव बढ़ना भी लाज़िमी है. गाज़ा में युद्ध रोकने के लिए ट्रंप जिस दूसरे विकल्प पर विचार कर सकते हैं, वो इजराइल को अपना समर्थन बनाए रखते हुए, ज़रूरत पड़ने पर नेतन्याहू को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना हो सकता है. डोनाल्ड ट्रंप के अरब देशों के नेताओं से मज़बूत रिश्ते हैं, ऐसे में यह भी हो सकता है कि अरब देशों के नेता ट्रंप के कहने पर हमास पर दबाव बना सकते हैं और उसे बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए तैयार कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक इसके बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ट्रंप इजराइल को अपना समर्थन देते हुए गाज़ा में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए क्या क़दम उठाएंगे. यानी अभी ये पता नहीं है कि ट्रंप ऐसी क्या नीति अपनाएंगे, जिससे इजराइल के साथ मज़बूत रिश्ते पर भी कोई आंच नहीं आए और फिलिस्तीनियों के सम्मान, गरिमा, स्वतंत्रता, मानवता और अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित हो सके.
जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात है, तो उसे रणनीतिक सैन्य अभियानों के ज़रिए ज़ल्द से ज़ल्द नतीज़े हासिल करने के लिए जाना जाता है. ट्रंप ने दाएश आंतकी संगठन को जिस प्रकार धूल चटाई और अपने “अमेरिका फर्स्ट” नज़रिए को बरक़रार रखा, यह उससे ज़ाहिर भी होता है. हालांकि, जिस तरह से अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर रुख अपनाया और जिस प्रकार उन्होंने अचानक ईरान परमाणु समझौते से क़दम वापस खींच लिए, उससे यह भी पता चलता है कि एक वैश्विक नेता के तौर पर उनके पास न तो निर्णायक फैसले लेने की कुव्वत है और न ही ज्वलंत वैश्विक मुद्दों का कोई कूटनीतिक हल खोजने की क्षमता है. इसके बावज़ूद, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जिस प्रकार ट्रंप को बंपर जीत मिली है, उससे यह ज़रूर लगता है कि उनके नेतृत्व में पश्चिम एशिया को लेकर अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव आएगा और वो दूरगामी सोच के साथ फैसले लेंगे. लेकिन उनके पूर्व के रवैये को देखते हुए लगता है कि इससें सफलता और विफलता दोनों की गुंजाइश बनी हुई है. ट्रंप द्वारा “अमेरिका फर्स्ट” के नारे को जिस तरह से चुनावों के दौरान बुलंद किया गया है, उससे लगता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में एहतियात के साथ क़दम उठाएगा और अपने फैसलों में संयम बरतेगा. ऐसा इसलिए है, क्योंकि ट्रंप के लिए गाज़ा युद्ध समाप्त करने के वादे और मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के अपने इरादे को धरातल पर उतारना आसान नहीं है और इसके लिए उन्हें तमाम पापड़ बेलने पड़ेंगे. कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कांटों भरा रह सकता है. इस दौरान यह भी पता चलेगा कि हितों के टकराव से संतुलन बनाते हुए पश्चिम एशिया की तेज़ी से बदलती भू-राजनीति को दिशा देने के लिहाज़ से उनमें कितनी काबिलियत है.
सबीन अमीर ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स में डॉक्टोरल रिसर्चर हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
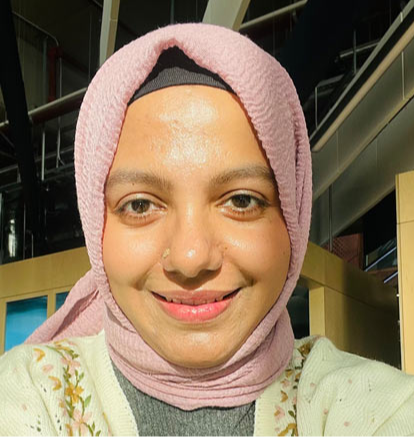
Sabine Ameer is a doctoral researcher in Politics and International Relations at the University of Glasgow, United Kingdom. Her research analyses whether there has been ...
Read More +