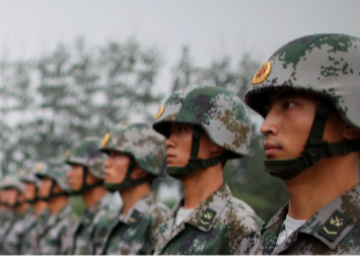जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने का एलान किया है. इस सफ़र को तय करने के लिए भारत को कोयले पर अपनी निर्भरता पर फिर से विचार करने और आने वाले समय में नए सिरे से कार्बन उत्सर्जन कम करने की रणनीति बनानी होगी.
स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में जलवायु परिवर्तन पर हुए वैश्विक शिखर सम्मेलन COP26 को लेकर पूरी दुनिया में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला था. ये उत्साह वैसा ही था, जैसा होना भी चाहिए. हम जैसी दुनिया देखते आए हैं, वैसे ही बनाए रखने के लिए हर साल 34 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड (2018) का उत्सर्जन कम करना होगा. इसमें से 37 फ़ीसद कार्बन उत्सर्जन दुनिया की वो 16 प्रतिशत आबादी करती है, जो दुनिया के विकसित देशों में रहती है.
यहां ये बात समझनी होगी कि आमदनी में असमानता की समस्या पूरी दुनिया में है. ‘दोहरी अर्थव्यवस्था’ का फ़ायदा लेता आया, पूरी दुनिया और ख़ास तौर से विकासशील देशों का शक्तिशाली समृद्ध वर्ग, अमीर देशों के रहन-सहन का लुत्फ़ उठाता रहा है और अब ये वर्ग अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता है. दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फैली इस असमानता को ही आधार बनाकर, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की ज़िम्मेदारी ‘साझा’ करने का तर्क दिया जाता है. लेकिन, इसी आधार पर हर देश की अलग ज़िम्मेदारी तय करने का तर्क भी दिया जा सकता है. सबसे पहले तो ये अमीर देशों की संस्थागत मज़बूती और वित्तीय क्षमता के ज़रिए जीवाश्म ईंधन की खपत को नई तकनीक के ज़रिए कम करने पर ज़ोर देती है. जबकि विकासशील देशों के पास ये क्षमता कम है. दूसरी बात ये कि इससे ‘जलवायु परिवर्तन का इंसाफ़’ होता भी दिखता है. क्योंकि इस तर्क से उन लोगों से अपील की जाती है, जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम सीमा का लाभ उठाकर तरक़्क़ी कर ली है और अब ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने जो लाभ उठाया है, उसकी क़ीमत अदा करें और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाएं.
‘अलग अलग ज़िम्मेदारियों के बोझ’ वाली ये ख़ूबी हमें 1997 में क्योटो में हुए सम्मेलन में दिखी थी. लेकिन, 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन तक आते आते, ये मामला सबके लिए ‘अपने मन की करने’ की आज़ादी तक पहुंच गया था. हर देश अपने अपने स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को हरित बनाने की कोशिशों से जुड़ी जानकारियां बड़ी मशक़्क़त से साझा कर रहा था. ये ठीक वैसा ही बर्ताव था, जैसा एक दूसरे से तलाक़ ले रहा जोड़ा अपनी पुरानी ज़िम्मेदारियों को लेकर अपनाता है.
पिछले छह सालों में संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन को लेकर संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं, चिंतित नागरिकों और कुछ गिने-चुने औद्योगिक समूहों ने और व्यापक क़दम उठाने की ज़रूरतों को जीवित बनाए रखा है. ये एक ऐसी ज़रूरत है, जिसकी अहमियत पर IPCC की छठवीं रिपोर्ट से जुड़े वर्किंग ग्रुप ने भी मुहर लगाई थी.
ग्लासगो में 26वें शिखर सम्मेलन की तैयारी करते हुए, संयुक्त राष्ट्र ज़ोर देकर ये कहता रहा था कि सभी देशों को वर्ष 2030 तक 2010 के स्तर के बराबर कार्बन उत्सर्जन से भी 45 प्रतिशत नीचे उत्सर्जन का वादा करना चाहिए. तभी पूरी दुनिया वर्ष 2050 तक धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने तक सीमित रख सकेगी.
चीन और इंडोनेशिया ने साल 2060 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य निर्धारित करके एक तरह से विकासशील देशों के लिए लक़ीर खींच दी है. वहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट हासिल करने का एलान किया है. चीन के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (2019) की तुलना में सिर्फ़ एक तिहाई उत्सर्जन करने के चलते भारत को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो नेट ज़ीरो का 2060 से आगे का लक्ष्य लेकर चले.
ग्लासगो सम्मेलन में भारत के सामने तीन चुनौतियां थीं. पहली तो ये कि क्या भारत को अपने नेट ज़ीरो की तारीख़ का एलान करना चाहिए? और अगर हां तो ये कौन सा साल होना चाहिए? दूसरी चुनौती ये थी कि क्या हमें नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए परिवर्तन की राह के प्रति वचनबद्धता ज़ाहिर करनी चाहिए? और तीसरा बड़ा सवाल, दूसरे से जुड़ा हुआ था कि क्या हमें अपने कार्बन उत्सर्जन के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की तारीख़ का एलान भी करना चाहिए- असल में ये असल में एक गुप्त संदेश होता कि हम उस तारीख़ के बाद, अपने ईंधन के सबसे प्रमुख स्रोत के तौर पर कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे, जबकि ये भारत के पास सबसे अधिक उपलब्धता वाला ऊर्जा का क़ुदरती संसाधन है.
नेट ज़ीरो की तरफ़ कैसे आगे बढ़ रहे हैं
चीन और इंडोनेशिया ने साल 2060 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य निर्धारित करके एक तरह से विकासशील देशों के लिए लक़ीर खींच दी है. वहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट हासिल करने का एलान किया है. चीन के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (2019) की तुलना में सिर्फ़ एक तिहाई उत्सर्जन करने के चलते भारत को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो नेट ज़ीरो का 2060 से आगे का लक्ष्य लेकर चले.
भारत और चीन के आर्थिक विकास के बीच भी 20 साल का फ़ासला है. 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP (2010 के डॉलर मूल्य के हिसाब से) 1961 डॉलर थी. चीन ने आर्थिक विकास ये मंज़िल 2001 में ही तय कर ली थी. लंबे समय तक चीन की दोहरे अंकों वाली शानदार आर्थिक विकास की दर, उसकी ख़ास ख़ूबियों का नतीजा थी. चीन ने समानता, मानव अधिकारों या क़ानून के राज पर आर्थिक विकास को तरज़ीह दी थी. जबकि ये बात भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों की मूल भावना के ही ख़िलाफ़ है.
दो दशकों के दौरान, हमारी सबसे अधिक वार्षिक आर्थिक विकास की दर 6.5 प्रतिशत रही थी, वो भी वर्ष 1993 से 2012 के दौरान. भारत ने ये विकास दर तब हासिल की थी, जब देश में उदारीकरण के ज़रिए से अर्थव्यवस्था को खोला गया था. अगर हम 8 प्रतिशत की औसत सालाना विकास दर से भी तरक़्क़ी करते हैं, तो हमें चीन की 2020 की प्रति व्यक्ति (2010 के मानक के हिसाब से) 8405 डॉलर GDP तक पहुंचने में 2040 तक का समय लगेगा. इस हिसाब से अगर चीन ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए चार दशक का लंबा अंतराल तय किया है, तो उसकी तुलना में अगर हम नेट ज़ीरो के लिए साल 2080 का लक्ष्य निर्धारित करते से भी ग़लत नहीं होता.
भारत अपवाद क्यों है?
ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि अगर इंडोनेशिया जैसा बड़ा निम्न मध्यम आमदनी वाला देश, जिसकी आबादी 27.3 करोड़ है और प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन भारत के 2018 के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से 19 फ़ीसद ज़्यादा है, वो 2060 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं? बिजली के लिए इंडोनेशिया की कोयले पर निर्भरता केवल 30 प्रतिशत है. वहीं, भारत की ये निर्भरता 28 प्रतिशत और चीन की 20 फ़ीसद है.
हालांकि, तीन बातें ऐसी हैं जो भारत को इंडोनेशिया और चीन से अलग करती हैं. पहली तो ये कि 2020 में इंडोनेशिया की प्रति व्यक्ति GDP 4312 डॉलर (2010 के मानकों पर) सालाना थी. ये भारत से लगभग दोगुना और चीन का आधा है. चीन और इंडोनेशिया की तुलना में भारत पर विकास करने का दबाव अधिक है. दूसरी बात ये कि, न तो इंडोनेशिया और न ही चीन, दोनों ही देश घरेलू जीवाश्म ईंधन के लिए मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर हैं. भारत के उलट, इंडोनेशिया और चीन दोनों ही देशों के पास तेल के घरेलू भंडार अधिक हैं. प्रति व्यक्ति को आधार बनाएं, तो इंडोनेशिया के पास ढाई गुना और चीन के पास भारत से 5.6 गुना अधिक बड़े तेल के भंडार हैं. वहीं, प्राकृतिक गैस की बात करें तो भारत की तुलना में, इंडोनेशिया के पास गैस के भंडार 4.7 गुना और चीन के पास 6.1 गुना अधिक हैं.
क्या अच्छी नीयत वाले नेट ज़ीरो के दूरगामी लक्ष्य उपयोगी हैं?
अगर हम तकनीक के पुरानी पड़ने के लिहाज़ से देखें, तो लंबी अवधि की योजनाएं बनाना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं. ऐसे लक्ष्य 20 साल में ही पुराने लगने लगते हैं. नवीनीकरण योग्य ऊर्जा की बात करें, तो इससे जुड़ी तकनीक के पुरानी पड़ने का ख़तरा तो और भी अधिक है. इससे जुड़ी तकनीकें तो पांच से दस साल में ही पुरानी पड़ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा पूंजी वाले पुराने संसाधन, महंगे मालूम देने लगते हैं. जलवायु परिवर्तन को लेकर संघर्ष कर रहीं भारत की पुरानी पर्यावरण कार्यकर्ता, सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरमेंट की सुनीता नारायण कहती हैं कि फ़ैसले लेने के लिए दस साल से ज़्यादा के लक्ष्य नहीं तय किए जाने चाहिए. ग्लासगो सम्मेलन में अगर मध्यम अवधि की योजनाओं पर सहमति बनती और सीमित अवधि के नतीजों पर आधारित योजनाओं को मज़बूती दी जाती तो अच्छा होता. इसके लिए हरित निवेश के साथ साथ लंबी अवधि में बदलाव लाने के लिए सस्ते वित्तीय संसाधन आसानी से जुटाए जा सकते थे.
फ़ैसले लेने के लिए दस साल से ज़्यादा के लक्ष्य नहीं तय किए जाने चाहिए. ग्लासगो सम्मेलन में अगर मध्यम अवधि की योजनाओं पर सहमति बनती और सीमित अवधि के नतीजों पर आधारित योजनाओं को मज़बूती दी जाती तो अच्छा होता. इसके लिए हरित निवेश के साथ साथ लंबी अवधि में बदलाव लाने के लिए सस्ते वित्तीय संसाधन आसानी से जुटाए जा सकते थे.
एक न्यायोचित परिवर्तन
IPCC की छठवीं रिपोर्ट में 2030 तक 2010 के स्तर से भी 45 प्रतिशत कम उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की ज़िम्मेदारी अलग अलग देशों के बीच किस तरह साझा की जा सकती है? ‘ज़िम्मेदारियों’ को देखने का एक अच्छा तरीक़ा ये हो सकता है कि हम देशों को आमदनी के आधार पर बांटें. समस्या के समाधान का ये पैमाना वित्तीय और तकनीकी क्षमता के एक विकल्प के तौर पर आज़माया जा सकता है. प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन भी कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य मापने का अच्छा मानक हो सकता है. चूंकि उत्सर्जन बहुत नज़दीकी से मानवीय गतिविधियों से जुड़ा होता है.
दिलचस्प बात ये है कि कम आमदनी वाले उन देशों- जिनकी दुनिया की कुल आबादी में हिस्सेदारी 8 प्रतिशत (2019) और प्रति व्यक्ति आमदनी 821 डॉलर है- ने साल 2010 से 2018 के बीच अपने हिस्से की कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में क़रीब 25 प्रतिशत की कमी की थी. इसी दौरान बड़े देश इस समूह से अलग हो गए थे. 1998 से 2018 के दौरान उनके उत्सर्जन में 7 फ़ीसद की बढ़ोत्तरी हुई थी.
अधिक आमदनी वाले देशों- जिनकी कुल आबादी में हिस्सेदारी 16 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय 46,036 डॉलर है- ने 2010 से 2018 के बीच अपना उत्सर्जन केवल पांच फ़ीसद और 1998-2018 के दौरान सिर्फ़ 2 प्रतिशत कम किया.
इन दोनों ही समय कालों के दौरान अधिक आमदनी और कम व मध्यम आमदनी वाले देशों का उत्सर्जन बढ़ा. लेकिन, दोनों की रफ़्तार में फ़र्क़ था. ऊपरी मध्यम वर्ग वाले देशों का कार्बन उत्सर्जन बढ़ने की रफ़्तार कम थी, वहीं निम्न मध्यम आमदनी वाले देशों का उत्सर्जन अधिक तेज़ी से बढ़ा. दोनों वर्गो के देशों के उत्सर्जन और उस पर नियंत्रण के ये आंकड़े ये इशारा करते हैं कि उत्सर्जन कम करने के लिए आर्थिक विकास मददगार हो सकता है, क्योंकि इससे नागरिकों की अपेक्षा बढ़ती है और आमदनी बढ़ने पर इन देशों की उत्सर्जन घटाने के लिए बेहतर तकनीक हासिल करने की क्षमता बढ़ती है.
पेरिस जलवायु समझौते के दौरान इसी आधार पर वादा किया गया था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर दिए जाएंगे. हालांकि ये वादा निभाया नहीं गया. कड़ी शर्तों के साथ दी जाने वाली रक़म सीधे मदद पाने वाले देश के लिए फ़ायदेमंद होती है. लेकिन, अगर जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए ग़रीब देशों की घरेलू वित्तीय ताक़त को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाए, तो इससे दानदाता देशों पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो सकेगा.
सारणी 1 दिखाती है कि भारत जैसे निम्न मध्यम आमदनी वाले देश क्यों फ़ौरी तौर पर उत्सर्जन कम करने में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं. इसके चलते पड़ने वाला आर्थिक बोझ, विकास की रफ़्तार धीमी कर देता है. फिर भले ही ये बोझ उनकी वैश्विक GDP के आधार पर ही क्यों न डाला जाए. नतीजा ये होता है कि सबसे अमीर देशों के 45 प्रतिशत उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य दोगुना या इससे भी ज़्यादा हो जाता है. इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के अलग अलग लक्ष्य और तारीख़ों में एक साझा अंतर पर सहमति बनाई जाए. इसके साथ साथ हरित विकास में निवेश के ख़ुद से तय की गई व्यवस्था बनाने की इजाज़त दी जाए.
भारत ने इंटेंडेड नेशनली डेटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (INDC) के तहत अपनी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की खपत 2005 के स्तर के आधार पर, वर्ष 2030 तक 35 प्रतिशत से घटाकर 33 फ़ीसद करने का लक्ष्य रखा है. ये लक्ष्य भविष्य में हरित विकास की सीमाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है. होना तो ये चाहिए कि इस लक्ष्य के लिए साल 2010 को आधार बनाया जाए.
कोयले की पहेली
भारत को अगर- मुख्य रूप से अपनी GDP को वर्ष 2040 तक चार गुना करने के साथ- भविष्य में कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत तेज़ी से बढ़ती बिजली की मांग पूरी करने के लिए कोयले पर अपनी निर्भरता कैसे कम करता है.
वर्ष 2040 तक भारत के पास कोयले के विकल्प प्राकृतिक गैस या परमाणु ऊर्जा ही है. इन दोनों ही विकल्पों से सुरक्षा और लागत की अलग अलग तरह की चुनौतियां जुड़ी हुई हैं. 2040 के बाद, प्राकृतिक गैस में हाईड्रोजन मिलाकर एक नया विकल्प भी तैयार किया जा सकता है. लेकिन ऐसा तब हो सकेगा जब ग्रीन हाईड्रोजन सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध होगी.
अकेला भारत ही नहीं है, जो इस दुविधा का शिकार है. बिजली के लिए कोयला इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत का नंबर चीन और अमेरिका के बाद आता है. कोयले से बिजली बनाने के मामले में इंडोनेशिया, दुनिया का दसवां बड़ा देश है. प्रति व्यक्ति को आधार बनाएं तो चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया की क्षमता चार गुनी है; जर्मनी की तीन गुनी अधिक है; जापान की दोगुना अधिक है; तो, भारत की तुलना में पोलैंड की क्षमता पांच गुना अधिक है. यानी बिजली बनाने में कोयले का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये काम सिर्फ़ ग़रीब देश ही नहीं कर रहे हैं.
(Table 2-Use Original)
बिजली बनाने के लिए भारत की कोयले पर निर्भरता को देखते हुए, भारत का उत्सर्जन कम से कम 2040-2050 तक बढ़ता रहेगा. इसके बाद जाकर उत्सर्जन की दर में गिरावट आनी शुरू होगी. ऐसे में भारत का 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य तय करना उचित ही है.
ग्लासगो के लक्ष्य
कार्बन उत्सर्जन कम करने की असमान समय-सीमा तय करने से अलग अलग आमदनी वाली अर्थव्यवस्थाओं पर न्यायोचित बोझ पड़ेगा. ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकें, कार्बन कैप्चर और उसका भंडारण, गीगावाट के स्तर पर बैटरी में भंडारण के ज़रिए पवन और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने की चुनौतियों से पार पाया जा सकता है. इनके ज़रिए ग्रिड को बिजली की वैकल्पिक आपूर्ति की जा सकेगी. बिजली का उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सुधार से कुशलता आएगी. और खुले स्रोत वाली तकनीकों को लेकर, सभी देशों, वित्तीय संगठनों और ख़रीद फ़रोख़्त करने वालों के बीच साझा रिसर्च और विकास की ज़रूरत होगी.
भारत के लिए क्वाड ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी तकनीकों के नेटवर्क में शामिल होने के मौक़े मुहैया कराए हैं. ग्लासगो में सभी देशों को ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे उत्सर्जन कम करने का सभी देशों के बीच न्यायोचित और उनकी क्षमता के अनुरूप बोझ पड़े. इसके साथ-साथ आमदनी के पांच पैमानों के हिसाब से तेज़ आर्थिक विकास पर भी ज़ोर हो. बाक़ी का काम तो तकनीक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार से अपने आप हो रहा है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV