-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
हर महीने अर्थव्यवस्था से जो संकेत उभर रहे हैं वो उम्मीद जगाते हैं कि जल्द ही कोरोना महामारी के चंगुल से अर्थव्यवस्था बाहर निकलेगी.
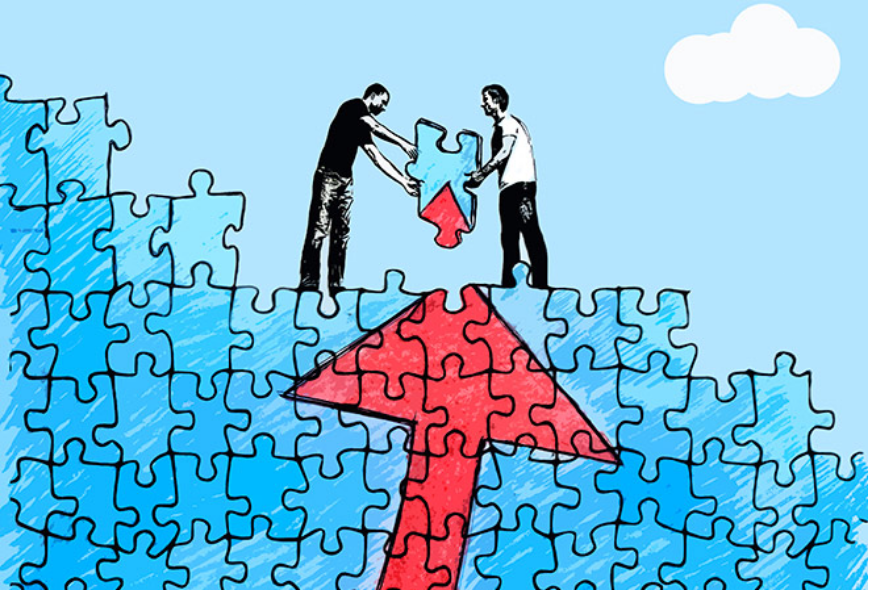
पिछले 15 महीने से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार की कोशिशों के बावजूद वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था अभी भी लंगड़ा कर चलने पर मज़बूर है. मौजूदा वित्तीय वर्ष (अप्रैल – जून वित्तीय वर्ष 2021-22) की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 32.4 ट्रिलियन रूपए की रही जो वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान 35.7 ट्रिलियन रुपए की थी, और जिसमें 9 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज़ की गई. हालांकि अच्छी ख़बर यह है कि पिछली तिमाही (जनवरी – मार्च वित्तीय वर्ष 2020 – 21 ) के मुकाबले यह 21 फ़ीसदी ज़्यादा है. हर महीने अर्थव्यवस्था से जो संकेत उभर रहे हैं वो उम्मीद जगाते हैं कि जल्द ही कोरोना महामारी के चंगुल से अर्थव्यवस्था बाहर निकलेगी.
हालांकि यहां यह याद रखना ज़रूरी है कि बाहरी दुष्प्रभावों के हमले, जैसे कोरोना महामारी, के बीच आर्थिक सेहत में सुधार वास्तविक तौर पर जीडीपी के बढ़ने से काफी अलग है, जैसा कि पहले भी सामान्य समय, जैसे कि 2019-20 में जीडीपी के ऐसे स्तर को पाया गया था. “सुधार की स्थिति” से बाहर निकल कर “पुनर्स्थापन स्तर” की ओर बढ़ना जो पहले “विकास के सारे इंजन के दौड़ लगाने” वाला स्तर है, जिसका मतलब है कि बची हुई तीनों वित्तीय तिमाही में 8.5 फ़ीसदी की औसत दर से अर्थव्यवस्था में विकास हो, जिससे 2019-20 में जीडीपी का स्तर 145.7 ट्रिलियन रूपए (स्थायी स्तर पर) तक पहुंच पाए.
भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इस साल विकास की दर 9.5 फ़ीसदी रहेगी जो अगर प्राप्त कर लिया जाता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए “पुनर्स्थापन” दौर का मंच तैयार करेगा
यह बेहद आसान है ख़ासकर तब जबकि पहली तिमाही में पिछले वित्तीय वर्ष के इसी समय के मुकाबले अर्थव्यवस्था में 21 फ़ीसदी की तेजी दर्ज़ की गई हो. लेकिन जैसा कि नीचे दिए ग्राफ से स्पष्ट है, यह कुछ भी है, लेकिन , पिछले वर्ष के मुकाबले दूसरी से चौथी तिमाही के दौरान जीडीपी के आंकड़े वर्ष 2019-20 की अपेक्षा ना सिर्फ बेहतर थे बल्कि पहली तिमाही के मुकाबले काफी ज़्यादा थे. ये इस बात को दिखाता है कि अर्थव्यवस्था वी, यू या एल आकार वाले टेढ़ी लाइन के नीचे है. ग्राफ में लाल लाइन इस साल बनाम पिछले वर्ष में आर्थिक विकास की तिमाही तेजी का आकलन करती है. इससे साफ है कि यह पहली तिमाही के 21 फ़ीसदी से धीरे-धीरे आने वाली तिमाही के दौरान विकास के 4 से 5 फ़ीसदी स्तर की ओर बढ़ रहा है, जो साल के अंत में औसत विकास के साथ 8.5 से 9.5 फ़ीसदी तक पहुंच जाएगा .
इस अप्रत्याशित सूचना को उदाहरण के तौर पर देखें. पहली तिमाही में 21 फ़ीसदी की तेजी के बावजूद अर्थव्यवस्था में वास्तव में जोड़ा गया मूल्य (32.9 ट्रिलियन रुपए) पिछली तिमाही के मुकाबले 17 फ़ीसदी कम है, पिछले वर्ष की तिमाही (वित्तीय वर्ष 2020 – 21) में वास्तव में अर्थव्यवस्था में जोड़ा गया मूल्य 39 ट्रिलियन रुपए था. भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इस साल विकास की दर 9.5 फ़ीसदी रहेगी जो अगर प्राप्त कर लिया जाता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए “पुनर्स्थापन” दौर का मंच तैयार करेगा, हालांकि इसमें सामाजिक सुरक्षा के बड़े-बड़े लुभावने वादे भी रहेंगे.
ऐसा तब है जब हम अर्थव्यवस्था के मजबूत पहलू का परीक्षण करेंगे – मसलन, उत्पादक निवेश को बढ़ाने की हमारी क्षमता, मौजूदा निवेश से बेहतर उत्पादन निकाल लेने की हमारी काबिलियत और अगली पीढ़ी के स्तर तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर निवेश या खरीदने की हमारी क्षमता कितनी है. वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए यह मुद्दे प्रमुख होंगे, यह साल नहीं, जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता से ज़्यादा संबंधित है. हालांकि इन कोशिशों में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना प्रमुख है, जो 6 फ़ीसदी के ऊपरी स्तर पर साथ-साथ आगे बढ़ रहा है.
हमें इस बात का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि कोरोना महामारी के दौरान प्रकृति हम पर मेहरबान रही. कृषि जिसने पिछले वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया और 3.6 फ़ीसदी की वार्षिक दर से 2019-20 में तेजी दर्ज़ की, इस बार भी रोजगार और विकास की वजह बना. पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कृषि में 4.5 फ़ीसदी की तेजी दर्ज़ की गई. अगली तिमाही तक यह खुशनुमा स्थिति बदल भी सकती है अगर खरीफ़ फसल पर देर से बुआई और इस गर्मी में बारिश के पैटर्न में गड़बड़ी का असर होता है.
अगर कृषि सिर्फ घरेलू अनाज उत्पादन का जरिया ना बन कर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के मौकों को लेकर ज़्यादा गतिशील और उत्तरदायी हो, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर बेहतर होगा और इससे रोजगार और आय में भी जबर्दस्त बढ़ोतरी हो सकती है.
अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात दूसरा सबसे बड़ा तारनहार साबित हुआ है, जिसमें पिछले वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में 7.7 फ़ीसदी की तेजी दर्ज़ की गई है. कृषि और निर्यात दोनों ने ही विविध अर्थव्यवस्था और बाज़ार के फायदे को दिखाया है और जिसका घरेलू आर्थिक गिरावट को रोकने में अहम भूमिका है. अगर कृषि सिर्फ घरेलू अनाज उत्पादन का जरिया ना बन कर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के मौकों को लेकर ज़्यादा गतिशील और उत्तरदायी हो, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर बेहतर होगा और इससे रोजगार और आय में भी जबर्दस्त बढ़ोतरी हो सकती है.
निवेश का समीकरण किसी भी अर्थव्यवस्था की तेजी का बेहतर सूचक होता है. लेकिन यह दुखद है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में निवेश का स्तर 10.2 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े के साथ बेहद निराशाजनक रहा. ये ठीक है कि पिछले वर्ष इसी तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में निवेश में तेजी दर्ज़ की गई लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसी तिमाही के दौरान निवेश की मात्रा 12.33 ट्रिलियन रुपए थी जिसके मुकाबले इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान इस आंकड़े में 17.1 फ़ीसदी गिरावट दर्ज़ की गई.
निवेश की मात्रा में 2.1 ट्रिलियन रुपए की कमी इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो 7 से 8 ट्रिलियन रुपए की तरलता को अर्थव्यवस्था में झोंका था उसकी उत्पादकता का नतीजा अर्थव्यवस्था में नहीं दिखा. इसके बदले इसने “विश्वसनीय” मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं या कंपनियों को ऋण सुविधाएं मुहैया कर, यह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई. ऋण सुविधाएं मुद्रा लोन के जरिए बेरोजगार युवकों और छोटे कारोबारियों तक पहुंची जिनका एनपीए स्तर दहाई के कम आंकड़े को छूता है, या फिर जिनका शेयर बाज़ार में निवेश है, उन्हें औसत के मुकाबले उच्च स्तर पर बनाए रखता है. ऐसे में यह हैरान करता है कि 70 फ़ीसदी के करीब व्यावसायिक क्षमता की उपयोगिता के कम स्तर के साथ केवल ज़िद्दी या फिर जो लोग महामारी के दुष्प्रभावों से अछूते रहे, वही पूंजी निवेश के लिए आगे बढ़ सकते हैं.
निवेश की मात्रा में 2.1 ट्रिलियन रुपए की कमी इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो 7 से 8 ट्रिलियन रुपए की तरलता को अर्थव्यवस्था में झोंका था उसकी उत्पादकता का नतीजा अर्थव्यवस्था में नहीं दिखा.
हाल में ही सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के परिचालन परिसंपत्तियों से कमाई करने की पहल ज़्यादा प्रशंसनीय है जिसके तहत निजी निवेशकों को इन संपत्तियों को लंबे समय के लिए लीज पर देना शामिल है. यह सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी की जगह निजी पूंजी को जगह दे सकेगा और इससे सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी को निकाला जा सकेगा.
2017 में 12 वीं पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गई जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की ओर से करीब आधा निवेश जुटाने का था, जो निराधार साबित हुआ. नतीजतन, योजना के अंतिम वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर में जीडीपी के 9 फ़ीसदी के बराबर निवेश का जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो सका और यह आंकड़ा जीडीपी के 5.8 फ़ीसदी तक ही पहुंच पाया.
पिछले दशक में, साल 2011-12 में निवेश जीडीपी के 34 फ़ीसदी तक पहुंच गया था जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज़ करते हुए साल 2018-19 में 32.3 फ़ीसदी तक पहुंच गया. यह आंकड़ा 2019-20 में जीडीपी के 30 फ़ीसदी और 2020-21 में जीडीपी के 28 फ़ीसदी तक पहुंच गया जिसका असर हुआ कि पिछले नौ तिमाहियों के दौरान आर्थिक विकास में गिरावट आ गई.
जीडीपी के लिए कर का स्तर स्थिर होने के साथ, जैसा कि पूर्वी एशिया और यूरोप में देखने को मिलता है कि सामाजिक क्षेत्र को मदद करने के लिए सरकारी बज़ट में कमी आई है. कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ा सबक जो सीखने को मिला वह यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सेवाओं पर बज़ट की कमी का गहरा नकारात्मक आर्थिक परिणाम होता है. यहां तक कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की मदद से दी जा रही शिक्षा का स्तर भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसके जरिए युवाओं को ना तो रोजगार के लिए तैयार किया जा सका है और ना ही उन्हें ज़रूरी लाइफ स्किल ट्रेनिंग ही मिल पा रही है. दो राय नहीं कि सामाजिक सेवाओं पर बज़ट में खर्च की राशि को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए.
जैसा कि 2008-09 के पश्चिमी देशों के वित्तीय संकट से पहले तक यह माना जाता था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रमुख निवेशक सरकार हो, लेकिन अब इसे बदलने की ज़रूरत है और सरकार को इससे बाहर निकालना है
पिछले 15 महीने से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार की कोशिशों के बावजूद वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था अभी भी लंगड़ा कर चलने पर मज़बूर है. मौजूदा वित्तीय वर्ष (अप्रैल – जून वित्तीय वर्ष 2021-22) की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 32.4 ट्रिलियन रूपए की रही जो वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान 35.7 ट्रिलियन रुपए की थी, और जिसमें 9 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज़ की गई. हालांकि अच्छी ख़बर यह है कि पिछली तिमाही (जनवरी – मार्च वित्तीय वर्ष 2020 – 21 ) के मुकाबले यह 21 फ़ीसदी ज़्यादा है. हर महीने अर्थव्यवस्था से जो संकेत उभर रहे हैं वो उम्मीद जगाते हैं कि जल्द ही कोरोना महामारी के चंगुल से अर्थव्यवस्था बाहर निकलेगी.
हालांकि यहां यह याद रखना ज़रूरी है कि बाहरी दुष्प्रभावों के हमले, जैसे कोरोना महामारी, के बीच आर्थिक सेहत में सुधार वास्तविक तौर पर जीडीपी के बढ़ने से काफी अलग है, जैसा कि पहले भी सामान्य समय, जैसे कि 2019-20 में जीडीपी के ऐसे स्तर को पाया गया था. “सुधार की स्थिति” से बाहर निकल कर “पुनर्स्थापन स्तर” की ओर बढ़ना जो पहले “विकास के सारे इंजन के दौड़ लगाने” वाला स्तर है, जिसका मतलब है कि बची हुई तीनों वित्तीय तिमाही में 8.5 फ़ीसदी की औसत दर से अर्थव्यवस्था में विकास हो, जिससे 2019-20 में जीडीपी का स्तर 145.7 ट्रिलियन रूपए (स्थायी स्तर पर) तक पहुंच पाए.
भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इस साल विकास की दर 9.5 फ़ीसदी रहेगी जो अगर प्राप्त कर लिया जाता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए “पुनर्स्थापन” दौर का मंच तैयार करेगा
यह बेहद आसान है ख़ासकर तब जबकि पहली तिमाही में पिछले वित्तीय वर्ष के इसी समय के मुकाबले अर्थव्यवस्था में 21 फ़ीसदी की तेजी दर्ज़ की गई हो. लेकिन जैसा कि नीचे दिए ग्राफ से स्पष्ट है, यह कुछ भी है, लेकिन , पिछले वर्ष के मुकाबले दूसरी से चौथी तिमाही के दौरान जीडीपी के आंकड़े वर्ष 2019-20 की अपेक्षा ना सिर्फ बेहतर थे बल्कि पहली तिमाही के मुकाबले काफी ज़्यादा थे. ये इस बात को दिखाता है कि अर्थव्यवस्था वी, यू या एल आकार वाले टेढ़ी लाइन के नीचे है. ग्राफ में लाल लाइन इस साल बनाम पिछले वर्ष में आर्थिक विकास की तिमाही तेजी का आकलन करती है. इससे साफ है कि यह पहली तिमाही के 21 फ़ीसदी से धीरे-धीरे आने वाली तिमाही के दौरान विकास के 4 से 5 फ़ीसदी स्तर की ओर बढ़ रहा है, जो साल के अंत में औसत विकास के साथ 8.5 से 9.5 फ़ीसदी तक पहुंच जाएगा .
इस अप्रत्याशित सूचना को उदाहरण के तौर पर देखें. पहली तिमाही में 21 फ़ीसदी की तेजी के बावजूद अर्थव्यवस्था में वास्तव में जोड़ा गया मूल्य (32.9 ट्रिलियन रुपए) पिछली तिमाही के मुकाबले 17 फ़ीसदी कम है, पिछले वर्ष की तिमाही (वित्तीय वर्ष 2020 – 21) में वास्तव में अर्थव्यवस्था में जोड़ा गया मूल्य 39 ट्रिलियन रुपए था. भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इस साल विकास की दर 9.5 फ़ीसदी रहेगी जो अगर प्राप्त कर लिया जाता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए “पुनर्स्थापन” दौर का मंच तैयार करेगा, हालांकि इसमें सामाजिक सुरक्षा के बड़े-बड़े लुभावने वादे भी रहेंगे.
ऐसा तब है जब हम अर्थव्यवस्था के मजबूत पहलू का परीक्षण करेंगे – मसलन, उत्पादक निवेश को बढ़ाने की हमारी क्षमता, मौजूदा निवेश से बेहतर उत्पादन निकाल लेने की हमारी काबिलियत और अगली पीढ़ी के स्तर तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर निवेश या खरीदने की हमारी क्षमता कितनी है. वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए यह मुद्दे प्रमुख होंगे, यह साल नहीं, जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता से ज़्यादा संबंधित है. हालांकि इन कोशिशों में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना प्रमुख है, जो 6 फ़ीसदी के ऊपरी स्तर पर साथ-साथ आगे बढ़ रहा है.
हमें इस बात का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि कोरोना महामारी के दौरान प्रकृति हम पर मेहरबान रही. कृषि जिसने पिछले वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया और 3.6 फ़ीसदी की वार्षिक दर से 2019-20 में तेजी दर्ज़ की, इस बार भी रोजगार और विकास की वजह बना. पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कृषि में 4.5 फ़ीसदी की तेजी दर्ज़ की गई. अगली तिमाही तक यह खुशनुमा स्थिति बदल भी सकती है अगर खरीफ़ फसल पर देर से बुआई और इस गर्मी में बारिश के पैटर्न में गड़बड़ी का असर होता है.
अगर कृषि सिर्फ घरेलू अनाज उत्पादन का जरिया ना बन कर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के मौकों को लेकर ज़्यादा गतिशील और उत्तरदायी हो, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर बेहतर होगा और इससे रोजगार और आय में भी जबर्दस्त बढ़ोतरी हो सकती है.
अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात दूसरा सबसे बड़ा तारनहार साबित हुआ है, जिसमें पिछले वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में 7.7 फ़ीसदी की तेजी दर्ज़ की गई है. कृषि और निर्यात दोनों ने ही विविध अर्थव्यवस्था और बाज़ार के फायदे को दिखाया है और जिसका घरेलू आर्थिक गिरावट को रोकने में अहम भूमिका है. अगर कृषि सिर्फ घरेलू अनाज उत्पादन का जरिया ना बन कर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के मौकों को लेकर ज़्यादा गतिशील और उत्तरदायी हो, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर बेहतर होगा और इससे रोजगार और आय में भी जबर्दस्त बढ़ोतरी हो सकती है.
निवेश का समीकरण किसी भी अर्थव्यवस्था की तेजी का बेहतर सूचक होता है. लेकिन यह दुखद है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में निवेश का स्तर 10.2 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े के साथ बेहद निराशाजनक रहा. ये ठीक है कि पिछले वर्ष इसी तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में निवेश में तेजी दर्ज़ की गई लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसी तिमाही के दौरान निवेश की मात्रा 12.33 ट्रिलियन रुपए थी जिसके मुकाबले इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान इस आंकड़े में 17.1 फ़ीसदी गिरावट दर्ज़ की गई.
निवेश की मात्रा में 2.1 ट्रिलियन रुपए की कमी इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो 7 से 8 ट्रिलियन रुपए की तरलता को अर्थव्यवस्था में झोंका था उसकी उत्पादकता का नतीजा अर्थव्यवस्था में नहीं दिखा. इसके बदले इसने “विश्वसनीय” मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं या कंपनियों को ऋण सुविधाएं मुहैया कर, यह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई. ऋण सुविधाएं मुद्रा लोन के जरिए बेरोजगार युवकों और छोटे कारोबारियों तक पहुंची जिनका एनपीए स्तर दहाई के कम आंकड़े को छूता है, या फिर जिनका शेयर बाज़ार में निवेश है, उन्हें औसत के मुकाबले उच्च स्तर पर बनाए रखता है. ऐसे में यह हैरान करता है कि 70 फ़ीसदी के करीब व्यावसायिक क्षमता की उपयोगिता के कम स्तर के साथ केवल ज़िद्दी या फिर जो लोग महामारी के दुष्प्रभावों से अछूते रहे, वही पूंजी निवेश के लिए आगे बढ़ सकते हैं.
निवेश की मात्रा में 2.1 ट्रिलियन रुपए की कमी इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो 7 से 8 ट्रिलियन रुपए की तरलता को अर्थव्यवस्था में झोंका था उसकी उत्पादकता का नतीजा अर्थव्यवस्था में नहीं दिखा.
हाल में ही सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के परिचालन परिसंपत्तियों से कमाई करने की पहल ज़्यादा प्रशंसनीय है जिसके तहत निजी निवेशकों को इन संपत्तियों को लंबे समय के लिए लीज पर देना शामिल है. यह सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी की जगह निजी पूंजी को जगह दे सकेगा और इससे सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी को निकाला जा सकेगा.
2017 में 12 वीं पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गई जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की ओर से करीब आधा निवेश जुटाने का था, जो निराधार साबित हुआ. नतीजतन, योजना के अंतिम वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर में जीडीपी के 9 फ़ीसदी के बराबर निवेश का जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो सका और यह आंकड़ा जीडीपी के 5.8 फ़ीसदी तक ही पहुंच पाया.
पिछले दशक में, साल 2011-12 में निवेश जीडीपी के 34 फ़ीसदी तक पहुंच गया था जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज़ करते हुए साल 2018-19 में 32.3 फ़ीसदी तक पहुंच गया. यह आंकड़ा 2019-20 में जीडीपी के 30 फ़ीसदी और 2020-21 में जीडीपी के 28 फ़ीसदी तक पहुंच गया जिसका असर हुआ कि पिछले नौ तिमाहियों के दौरान आर्थिक विकास में गिरावट आ गई.
जीडीपी के लिए कर का स्तर स्थिर होने के साथ, जैसा कि पूर्वी एशिया और यूरोप में देखने को मिलता है कि सामाजिक क्षेत्र को मदद करने के लिए सरकारी बज़ट में कमी आई है. कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ा सबक जो सीखने को मिला वह यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सेवाओं पर बज़ट की कमी का गहरा नकारात्मक आर्थिक परिणाम होता है. यहां तक कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की मदद से दी जा रही शिक्षा का स्तर भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसके जरिए युवाओं को ना तो रोजगार के लिए तैयार किया जा सका है और ना ही उन्हें ज़रूरी लाइफ स्किल ट्रेनिंग ही मिल पा रही है. दो राय नहीं कि सामाजिक सेवाओं पर बज़ट में खर्च की राशि को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए.
जैसा कि 2008-09 के पश्चिमी देशों के वित्तीय संकट से पहले तक यह माना जाता था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रमुख निवेशक सरकार हो, लेकिन अब इसे बदलने की ज़रूरत है और सरकार को इससे बाहर निकालना है.
हाल में ही सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के परिचालन परिसंपत्तियों से कमाई करने की पहल ज़्यादा प्रशंसनीय है जिसके तहत निजी निवेशकों को इन संपत्तियों को लंबे समय के लिए लीज पर देना शामिल है. यह सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी की जगह निजी पूंजी को जगह दे सकेगा और इससे सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी को निकाला जा सकेगा.
केंद्र सरकार के जुलाई 2021 के खाते इस परिकल्पना का समर्थन करते हैं कि जहां निजी निवेश आसानी से नहीं पहुंच सके वहां सरकारी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सरकार को उन क्षेत्रों से निकल जाना चाहिए जहां निजी निवेशक निवेश करने में ज़्यादा आसान समझें. जुलाई 2021 तक कुल खर्च के 28.8 फ़ीसदी औसत निवेश के मुकाबले निवेश व्यय 5.5 ट्रिलियन रुपए(कुल बज़ट व्यय का 16 फ़ीसदी) के बज़ट प्रस्तावों का महज 23.2 फ़ीसदी था. बचे हुए ऋण पर ब्याज का भुगतान कुल व्यय का करीब 23 फ़ीसदी है.
राजकोषीय घाटे के बढ़ने से संसाधनों पर बढ़ता बोझ स्पष्ट है. परिचालन योग्य संपत्तियों को लीज पर देने से, जो नेशनल मॉनिटाइजेशन परियोजना का हिस्सा है, और विनिवेश की योजना को जारी रखने से जीडीपी (2 ट्रिलियन रु.) में 1 फ़ीसदी राजकोषीय स्थान बन पाएगा जो प्रस्तावित केंद्रीय बज़ट व्यय का करीब 6 फ़ीसदी है.
अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ-साथ हमारी सीमित निजीकरण के अनुभव (1999-2003) बताते हैं कि निजी निवेश, प्रोफेशनल एंटी ट्रस्ट, और पर्यावरण से जुड़े नियामकों की चुनौतियां, औद्योगिक उत्पादों और सार्वजनिक सेवाओं के निष्पादन के लिए सही सार्वजनिक विकल्प हो सकते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र को उबाऊ नियामकों की चुनौतियों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना, सट्टा निजी पूंजी की मांग के जवाब में ऐसा करना लंबे समय के लिए निवेश संसाधनों का उपयोगी इस्तेमाल नहीं है. यहां तक कि विकसित देशों में भी जहां सार्वजनिक व्यवस्था ज्यादा परिष्कृत और बेहतर है वहां भी यह उपयोगी नहीं है.
कारोबार में लगे सार्वजनिक पूंजी को निजी पूंजी से बदलने, सार्वजनिक पूंजी का सामाजिक क्षेत्र में निवेश, व्यापार और पर्यावरण नियमों को और प्रभावी साथ में किफायती बनाना वो प्राथमिकताएं हैं जिसे लेकर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है.
केंद्र सरकार के जुलाई 2021 के खाते इस परिकल्पना का समर्थन करते हैं कि जहां निजी निवेश आसानी से नहीं पहुंच सके वहां सरकारी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सरकार को उन क्षेत्रों से निकल जाना चाहिए जहां निजी निवेशक निवेश करने में ज़्यादा आसान समझें. जुलाई 2021 तक कुल खर्च के 28.8 फ़ीसदी औसत निवेश के मुकाबले निवेश व्यय 5.5 ट्रिलियन रुपए(कुल बज़ट व्यय का 16 फ़ीसदी) के बज़ट प्रस्तावों का महज 23.2 फ़ीसदी था. बचे हुए ऋण पर ब्याज का भुगतान कुल व्यय का करीब 23 फ़ीसदी है.
राजकोषीय घाटे के बढ़ने से संसाधनों पर बढ़ता बोझ स्पष्ट है. परिचालन योग्य संपत्तियों को लीज पर देने से, जो नेशनल मॉनिटाइजेशन परियोजना का हिस्सा है, और विनिवेश की योजना को जारी रखने से जीडीपी (2 ट्रिलियन रु.) में 1 फ़ीसदी राजकोषीय स्थान बन पाएगा जो प्रस्तावित केंद्रीय बज़ट व्यय का करीब 6 फ़ीसदी है.
अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ-साथ हमारी सीमित निजीकरण के अनुभव (1999-2003) बताते हैं कि निजी निवेश, प्रोफेशनल एंटी ट्रस्ट, और पर्यावरण से जुड़े नियामकों की चुनौतियां, औद्योगिक उत्पादों और सार्वजनिक सेवाओं के निष्पादन के लिए सही सार्वजनिक विकल्प हो सकते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र को उबाऊ नियामकों की चुनौतियों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना, सट्टा निजी पूंजी की मांग के जवाब में ऐसा करना लंबे समय के लिए निवेश संसाधनों का उपयोगी इस्तेमाल नहीं है. यहां तक कि विकसित देशों में भी जहां सार्वजनिक व्यवस्था ज्यादा परिष्कृत और बेहतर है वहां भी यह उपयोगी नहीं है.
कारोबार में लगे सार्वजनिक पूंजी को निजी पूंजी से बदलने, सार्वजनिक पूंजी का सामाजिक क्षेत्र में निवेश, व्यापार और पर्यावरण नियमों को और प्रभावी साथ में किफायती बनाना वो प्राथमिकताएं हैं जिसे लेकर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +