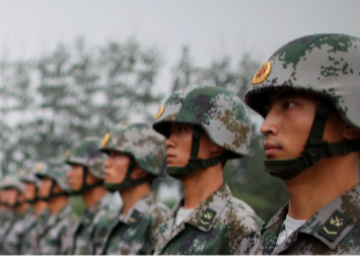पृष्ठभूमि
फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जोएल रुए ने 2000 के दशक की शुरुआत में भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर अध्ययन किया था. उन्होंने कहा था कि अगर लेनिन के मुताबिक़, समाजवाद का मतलब, ‘सोवियत और बिजली’ है, तो भारत काफ़ी हद तक, ‘लोकतंत्र और राज्य बिजली बोर्ड’ है. जोएल रुए की ये टिप्पणी राज्य बिजली परिषदों की उस अहम भूमिका को बख़ूबी बयां करती है, जिसे इन विद्युत परिषदों ने शुरुआत में तो ग्राहकों को सीधे बिजली पहुंचाने की विकास संबंधी नीति को लागू करने में निभाया था. लेकिन, बाद में यही राज्य विद्युत परिषद राजनीतिक मक़सद साधने का ज़रिया बन गईं. राज्य विद्युत परिषदों को अब टुकड़ों में बांट कर वितरण कंपनियों (discom) का रूप दे दिया गया है. लेकिन, ये आज भी राजनीतिक लाभ साधने का ज़रिया बनी हुई हैं. इसका एक नतीजा तो ये हुआ है कि बिजली की दरों को, ग्राहकों को बिजली आपूर्ति करने में आने वाली लागत के अनुपात में लाने की इन कंपनियों की क्षमता सीमित हो गई है, और यही डिस्कॉम की तमाम परेशानियों की जड़ है. हालांकि, इस समस्या को राज्य विद्युत परिषद (SEB) या डिस्कॉम के नाकारेपन के तौर पर पेश किया जाता है, और इससे बिजली वितरण के क्षेत्र में ईमानदार सुधारों की राह मुश्किल हो जाती है.
राज्य विद्युत परिषद
राज्यों की सरकारों ने राज्य विद्युत परिषदों की स्थापना 1950 और 1960 के दशकों में की थी. 1948 में बिजली क़ानून बनने के बाद, इन परिषदों को बिजली बनाने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी. 1948 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना भी की थी. हालांकि, इसकी भूमिका, बिजली क्षेत्र के तकनीकी पहलुओं के नियमन तक सीमित रखी गई थी. वैसे तो संविधान के मुताबिक़, बिजली समवर्ती सूची का हिस्सा है. यानी ये केंद्र के साथ साथ, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आती है. लेकिन, राज्य स्तर पर विद्युत परिषदों की स्थापना से बिजली बनाने, उसे पहुंचाने और ग्राहकों को वितरित करने में राज्य सरकारों को अधिक नियंत्रण हासिल होने से इस क्षेत्र में विद्युत परिषदों को एकाधिकार हासिल हो गया था. पहले 1949 और फिर 1951 में बिजली क़ानून में संशोधन से राज्य सरकारों को, विद्युत परिषदों में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का भी अधिकार हासिल हो गया. इसके अलावा, विद्युत परिषदों के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले ‘नीतिगत निर्देशों’ को स्वीकार करना भी अनिवार्य बना दिया गया. 1960 और 1970 के दशक में देश से बाहर के राजनीतिक हालात ने राज्य सरकारों को बिजली परिषदों पर अपना शिकंजा और भी कसने का मौक़ा दे दिया.
वैसे तो संविधान के मुताबिक़, बिजली समवर्ती सूची का हिस्सा है. यानी ये केंद्र के साथ साथ, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आती है. लेकिन, राज्य स्तर पर विद्युत परिषदों की स्थापना से बिजली बनाने, उसे पहुंचाने और ग्राहकों को वितरित करने में राज्य सरकारों को अधिक नियंत्रण हासिल होने से इस क्षेत्र में विद्युत परिषदों को एकाधिकार हासिल हो गया था.
1967 में देश के अहम राज्यों में कांग्रेस की चुनावी हार के चलते राजनीतिक और आर्थिक वार्तालाप में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ी. वैसे तो केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ज़मीन पर मालिकाना हक़ रखने वाली जातियों और समूहों को और पूंजी जमा करने दिया जाता रहा. लेकिन, बदले हुए राजनीतिक माहौल में समझौते के लिए नए नए उभरे ताक़तवर समुदायों, जैसे कि शहरों में मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्रांति से ताक़तवर बने किसानों को भी सामाजिक पूंजी में हिस्सेदारी देनी पड़ी. इन दोनों ही समूहों को लुभाने के लिए राज्य विद्युत परिषदों द्वारा सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराना सबसे आसान तरीक़ा था. इस तरह से धुआं उगलने वाली लालटेनों और चिमनियों की जगह आसानी से साफ़ रौशनी देने वाली बिजली के बल्ब और किसानों को पंप से अपनी ज़मीन की सिंचाई के लिए बिजली देने का मतलब, दो बड़े समूहों से सीधा राजनीतिक हासिल होना था.
इस राजनीतिक मॉडल की चुनावी सफलता को देखकर अन्य राज्यों ने भी बिजली बोर्ड के ज़रिए मध्यम वर्ग और किसानों को सस्ती बिजली देने का रास्ता अख़्तियार कर लिया. इसके एवज़ में औद्योगिक क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली की दरों में बड़े पैमाने पर इज़ाफ़ा किया गया, जिससे कि राज्यों के बिजली बोर्ड मुफ़्त बिजली देने से हो रहे घाटे की भरपाई कर सकें. जबकि, इससे पहले भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को काफ़ी सस्ती दरों पर बिजली दी जाती थी. राज्य विद्युत परिषदों को राजनीतिक औज़ार बनाकर संसाधनों के इस तरह से बंटवारे ने बिजली बोर्डों की हालत बिगाड़ कर रख दी. विद्युत परिषदों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो घटते मूल्य के बावजूद अपनी लागत और वित्तीय देनदारियां निपटाकर अपनी स्थायी संपत्ति से तीन प्रतिशत मुनाफ़ा कमाएंगी. शुरुआत में तो बिजली बोर्ड इन चुनौतियों से निपटकर मुनाफ़ा कमाने में सफल रहे. लेकिन, 1960 के दशक के आख़िर से उनकी हालत ख़राब होने लगी. इसके बाद बिजली बोर्ड राज्य सरकारों से मिलने वाली ख़ैरात और सब्सिडी पर निर्भर हो गए. 1970 के दशक से विद्युत परिषदों की देनदारियां काफ़ी बढ़ गईं. फिर उन्हें बिजली क्षेत्र की कमज़ोर कड़ी कहा जाने लगा.
फ्रेंच अर्थशास्त्री जोएल रुए ने कहा था कि राज्य विद्युत परिषद अकुशल संस्थान नहीं थे. असल में ये प्रशासन की अक्षमता थी, जो अलग अलग तरह के मक़सद साधने के लिए बिजली बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे. यानी बिजली बोर्ड के काम-काज को केवल आर्थिक पैमाने पर नहीं कसा जा रहा था.
विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राज्य विद्युत परिषदों की आर्थिक, तकनीकी और प्रबंधन संबंधी अक्षमता की नव उदारवादी आलोचना करनी शुरू कर दी. इसके साथ साथ, जब भारत ने 1990 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को बाज़ारवादी ताक़तों के लिए खोलने की शुरुआत की, तो कई अकादेमिक रिसर्च में भी बिजली बोर्ड की अकुशलता की बात दोहराई गई. विकास की फंडिंग करने वाली संस्थाओं ने राज्य विद्युत परिषदों की हालत सुधारने के लिए, जो समाधान सुझाए उनमें विद्युत परिषदों को बिजली बनाने, इसके ट्रांमिशन और वितरण की ज़िम्मेदारियों अलग अलग करके निजी क्षेत्र से पूंजी आकर्षित करने का सुझाव दिया. विद्युत परिषदों की बुरी हालत को उनका नाकारापन घोषित करके, बिजली सेक्टर को निजी क्षेत्र (विदेशी भी) से (ख़ास तौर से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में) पूंजी निवेश के लिए खोल दिया गया. इससे बिजली के मामले में राजनीतिक दलों और सरकारों से टकराव को एक तरह से बचने की कोशिश की गई. लेकिन, जैसा कि फ्रेंच अर्थशास्त्री जोएल रुए ने कहा था कि राज्य विद्युत परिषद अकुशल संस्थान नहीं थे. असल में ये प्रशासन की अक्षमता थी, जो अलग अलग तरह के मक़सद साधने के लिए बिजली बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे. यानी बिजली बोर्ड के काम-काज को केवल आर्थिक पैमाने पर नहीं कसा जा रहा था. राज्य विद्युत परिषदों ने विकास में जो योगदान दिया था, उसमें गांवों का विद्युतीकरण (जो सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन देने के लिए किया गया) और हरित क्रांति के ज़रिए खेती का विकास शामिल है. इसमें बाहरी वित्तीय बोझ तो बढ़ा. लेकिन, ये बिजली परिषदों की अकुशलता का नतीजा नहीं था. इसके बावजूद बिजली बोर्डों को अक्षम बताने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से सुविधाजनक था. इसका नतीजा ये हुआ कि बिजली क्षेत्र की एकीकृत वैल्यू चेन को बिजली बनाने, ट्रांसमिशन और वितरण की अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया. अब राज्य विद्युत परिषदों को बिजली वितरण कंपनियों (discom) का रूप दे दिया गया और उनसे ये उम्मीद की जाने लगी कि वो अपने घाटे की भरपाई करके कुशल और वित्तीय रूप से लाभकारी संस्थाएं बन जाएंगी.
बिजली वितरण कंपनियां (Discoms)
बिजली सप्लाई के लिए कंपनियां बनाए जाने के क़रीब तीन दशक बाद भी आज भारत के पावर सेक्टर में बिजली वितरण को ही सबसे कमज़ोर कड़ी बताया जाता रहा है. इन तीन दशकों में वितरण कंपनियों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उनके पुनर्गठन के कई क़दम उठाए गए हैं. इनमें सबसे हालिया योजना वर्ष 2015 में लाई गई उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) थी. उदय (UDAY) योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों की हालत सुधारने, उनका काम-काज सुधारने और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के विकास और बिजली की खपत कम करने और बचाने के साथ-साथ बिजली बनाने की लागत कम करने पर भी ज़ोर दिया गय था. नीतिगत क्षेत्र की बात करें तो, 1998 में विद्युत नियामक आयोग क़ानून लागू करके केंद्र और राज्य स्तर पर नियामक संस्थाओं का गठन किया गया था. इसके बाद 2003 में बिजली क़ानून लाया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, ये प्रावधान भी था कि बिजली वितरण कंपनियां (discoms) को केंद्र सरकार के नीतिगत निर्देशों को मंज़ूर करना होगा. इस क़ानून से प्राइवेट सेक्टर को भी बिजली बनाने के क्षेत्र में प्रवेश का मौक़ा दिया गया. इन तमाम क़दमों और नीतिगत स्तर पर बहुत से सुधारों के बावजूद, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में कोई ख़ास सुधार नहीं आया है. बिजली वित्त निगम के अनुमानों के अनुसार 2019-20 के दौरान बिजली वितरण कंपनियों के खाते में क़रीब 900 अरब का घाटा दर्ज था. ये तो उदय योजना की शुरुआत के समय दर्ज किए गए अधिकतम घाटे की रक़म से भी अधिक (चार्ट देखें) है.
नीतिगत क्षेत्र की बात करें तो, 1998 में विद्युत नियामक आयोग क़ानून लागू करके केंद्र और राज्य स्तर पर नियामक संस्थाओं का गठन किया गया था. इसके बाद 2003 में बिजली क़ानून लाया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, ये प्रावधान भी था कि बिजली वितरण कंपनियां (discoms) को केंद्र सरकार के नीतिगत निर्देशों को मंज़ूर करना होगा.
समस्या की जड़ क्या है
बिजली के क्षेत्र में केवल वितरण को ही अकुशल मानने से बिजली की दरें तय करने में राजनीतिक दख़लंदाज़ी पर पर्दा पड़ जाता है. इसकी वजह ये है कि भारत की नौकरशाही व्यवस्था बिजली (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, मूलभूत ढांचे और विकास के लिए ज़रूरी अन्य सामाजिक लाभ) जैसी ग़रीब ग्रामीण जनता की बुनियादी ज़रूरत पूरी करने में भी नाकाम रही है. इससे ग़रीब तबक़े के लोग न तो अपनी आमदनी बढ़ा सके हैं और न ही अपनी ख़रीद पाने की क्षमता में इज़ाफ़ा कर सके हैं. यहां असली पाप तो ये है कि सरकार बड़े पैमाने पर फैली ग़रीबी को ख़त्म करने और ग़रीब घरों की आमदनी बढ़ा पाने में नाकाम रही है. इससे वो अपनी ज़रूरत की बिजली और अन्य सेवाओं का मूल्य अदा करने की हैसियत विकसित नहीं कर पाए हैं. मज़े की बात तो ये है कि राजनेता, अपनी ही इस नाकामी का भी फ़ायदा उठाते हैं और फिर वोट हासिल करने के लिए लोगों को सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराकर वाहवाही लूटते हैं. राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि आर्थिक सुधारों से लाइसेंस और परमिट देने के नाम पर तो राजनीतिक मुनाफ़ाख़ोरी कम हुई है. लेकिन, इसकी जगह जनता के संसाधन, ग़रीबों को मुफ़्त में देने के नाम पर वोट की राजनीति हो रही है. क्योंकि देश में ग़रीबों की तादाद, अमीरों से कई गुना ज़्यादा है.
राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि आर्थिक सुधारों से लाइसेंस और परमिट देने के नाम पर तो राजनीतिक मुनाफ़ाख़ोरी कम हुई है. लेकिन, इसकी जगह जनता के संसाधन, ग़रीबों को मुफ़्त में देने के नाम पर वोट की राजनीति हो रही है. क्योंकि देश में ग़रीबों की तादाद, अमीरों से कई गुना ज़्यादा है.
पिछले दो दशकों में चुनावों के दौरान राजनीतिक दल शायद ही कभी आर्थिक या सामाजिक नीतियों के मोर्चे पर होड़ लगाते दिखे हैं. इसके बजाय, सियासी पार्टियां कुछ तबक़ों को मुफ़्त में बिजली देने जैसे लॉलीपॉप को लेकर आपस में होड़ लगाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट का जुगाड़ कर सकें. बिजली जैसी बुनियादी सेवा सबको उपलब्ध कराने के बजाय, कुछ ख़ास नागरिकों को मुफ़्त में देने से ज़्यादा वोट हासिल होने की उम्मीद रहती है. मुफ़्त या सस्ती बिजली देने के वादे को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दल सामाजिक न्याय और संपत्ति के उचित बंटवारे का हवाला देते हैं. इससे उन्हें सामाजिक वैधता हासिल होती है. जबकि आज भी सत्ता सरकार और पूंजी की ही ग़ुलाम है. जैसा कि आंबेडकर ने बिल्कुल सही कहा था कि, एक ख़ास ‘वोट बैंक’ को मुफ़्त या सस्ती दरों पर बिजली देने से राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने जैसा फ़ौरी फ़ायदा होता है. जबकि, इसके दूरगामी नतीजे बेहद ख़राब होते हैं. क्योंकि, लागत से कम क़ीमत पर बिजली देने से वितरण कंपनियों की आर्थिक सेहत बिगड़ती है और उनके लिए मुनाफ़े में काम करना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए, बिजली वितरण कंपनियों की समस्या अकुशलता या अक्षमता नहीं है. असली समस्या राजनीतिक मुनाफ़ाख़ोरी है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV