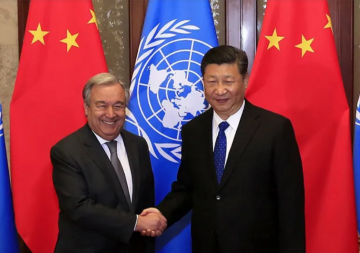कर्नाटक में हुई हालिया सियासी घटनाओं से अगर कोई एक बात फिर से सही साबित हुई है, तो वो है कि दल-बदल निरोधक क़ानून की नाकामी है. इस क़ानून का मक़सद था सियासी दलों में मौक़ापरस्ती और सत्ता के लालच में होने वाली फूट को रोकना. लेकिन लागू होने के साथ ही इस क़ानून का मखौल उड़ाया जाने लगा था. अगर हम इस बात की अनदेखी भी कर दें कि केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ने जिस तरह से जेडी (एस) और कांग्रेस के न चल पाने वाले गठबंधन में बग़ावत को हवा दी, तो भी ये एक तल्ख़ हक़ीक़त है कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के. आर. रमेश कुमार ने 14 (या ज़्यादा) बाग़ी विधायकों के इस्तीफ़े स्वीकार करने के बजाय उन्हें सदस्यता के ‘अयोग्य’ घोषित करने का विकल्प उस वक़्त चुना, जब इन विधायकों की पार्टी ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया था. हालांकि, ये कर्नाटक की अपनी अलग कहानी है कि स्पीकर ने कैसा बर्ताव किया.
जैसे ही मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल कर के सत्ता में वापसी की थी, तब से ही ये क़यास लगाए जाने लगे थे कि कर्नाटक सरकार में बग़ावत को हवा देकर सत्ता हासिल करना बीजेपी का पहला लक्ष्य होगा. बीजेपी ने कर्नाटक के पड़ोसी राज्य गोवा में तो कांग्रेस के क़रीब-क़रीब सभी विधायकों का दल-बदल करा कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था. ये दल-बदल निरोध क़ानून का मख़ौल उड़ाने का ट्रायल नहीं था, बल्कि सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया बेहद क़ामयाब सियासी मिशन था. फिर भी, संसद के बजट सत्र के दौरान दल-बदल निरोध क़ानून का ऐसा मज़ाक बनाए जाने पर किसी भी दल ने कोई सवाल नहीं उठाया, न ही बीजेपी के लिए कोई चुनौती पेश की.
जैसे ही मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल कर के सत्ता में वापसी की थी, तब से ही ये क़यास लगाए जाने लगे थे कि कर्नाटक सरकार में बग़ावत को हवा देकर सत्ता हासिल करना बीजेपी का पहला लक्ष्य होगा.
कर्नाटक के स्पीकर का बाग़ी विधायकों को ‘अयोग्य’ घोषित करने का फ़ैसला, जेडी (एस)-कांग्रेस साझा सरकार गिरने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बने बी.एस. येदियुरप्पा के लिए सरकार बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ. ये दल-बदल निरोधक क़ानून का उल्लंघन तो साफ़ तौर से था ही. कर्नाटक के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में एआईएडीएमके के ईडप्पी पलानिस्वामी की सरकार के बाद अब येदियुरप्पा भी बेहद मामूली बहुमत वाली सरकार के अगुवा हैं. दोनों ही राज्यों की विधानसभा में कुल सदस्यता से कम ही विधायक हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानिस्वामी जो ईपीएस के नाम से भी जाने जाते हैं. उन्होंने अब विधानसभा में पूर्ण बहुमत का जुगाड़ कर लिया है. हालांकि, राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए 22 विधानसभा सीटों के चुनाव में से 9 सीटें जीतने में ही क़ामयाबी हासिल की थी. आज भी उनके पास विपक्षी दलों से बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं हासिल है.
ज़मीनी तौर पर देखें तो येदियुरप्पा सरकार के बहुमत की असली परीक्षा विधानसभा में नहीं, बल्कि, कर्नाटक की सड़कों पर होगी. क्योंकि येदियुरप्पा ने सदन में तो अपना बहुमत साबित कर ही दिया है. उनका असल इम्तिहान तो तब होगा, जब चुनाव आयोग राज्य की खाली हुई विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव कराएगा. ये सीटें, बाग़ी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने या इस्तीफ़ा देने से ख़ाली हुई हैं. इस दौरान कर्नाटक की सियासी लड़ाई को हम अदालत में जाते हुए देखेंगे. क्योंकि अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने स्पीकर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा कर ही दिया है. हालांकि, विधायकों के अदालत जाने से पहले ही स्पीकर ने ख़ुद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है. अगर स्पीकर के. आर. रमेश कुमार ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देते, तो येदियुरप्पा सरकार उनके ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा देती. क्योंकि बीजेपी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि विधानसभा में उनके पास बहुमत है.
स्पीकर के पास अधिकार तो हैं, मगर..
विधानसभा अध्यक्ष के ख़िलाफ़ क़ानूनी दांव चलने के अलावा अयोग्य ठहराए गए विधायकों के पास सियासी दांव के तौर पर चलने के लिए कोई भी पासा नहीं है. सिवा इस संभावना के कि सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा अध्यक्ष के फ़ैसले को निरस्त कर के विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल कर दे. इस मामले में तर्क ये दिया जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास विधायकों के इस्तीफ़े अस्वीकार कर के उनकी सदस्यता रद्द करने का संवैधानिक अधिकार भले रहा हो, नैतिक अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं था. क्योंकि विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्ज़ी उस पार्टी ने दी थी, जिसने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया था. कोर्ट का सदस्यता रद्द करने के फ़ैसले को निरस्त करने का मतलब ये होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फ़ैसला नहीं लिया था.
अगर अयोग्य ठहराए गए विधायकों की विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो इनके नतीजे किसी भी करवट बैठ सकते हैं.
इसका तात्पर्य ये भी होगा कि विधायकों के त्यागपत्र का भी कोई संवैधानिक आधार नहीं है. इसलिए उनकी विधानसभा की सदस्यता बरक़रार रहेगी. इसका ये मतलब भी होगा कि विधानसभा में सदस्यों की कुल तादाद दोबारा बहाल हो जाएगी. इसका एक अहम पहलू ये भी होगा कि येदियुरप्पा सरकार का विधानसभा में बहुमत और भी मज़बूत हो जाएगा. क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन में बग़ावत को हवा दी और सरकार गिराने के लिए जो तरीक़ा अपनाया, उससे कर्नाटक की जनता का मूड कुछ भी हो सकता है. ऐसे में अगर अयोग्य ठहराए गए विधायकों की विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो इनके नतीजे किसी भी करवट बैठ सकते हैं.
विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य ठहराने का जो फ़ैसला किया, उसकी टाइमिंग का सवाल इसलिए अहम हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्पीकर को बाग़ी विधायकों के इस्तीफ़े पर फ़ैसला लेने का पूरा अधिकार है. कर्नाटक का ये विवाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए स्पीकर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अयोग्य ठहराए गए विधायकों की नई अर्ज़ी को सर्वोच्च अदालत स्वीकार कर सकती है. अगर विधायक, स्पीकर के फ़ैसले के विरुद्ध कोई नई अर्ज़ी नहीं दाख़िल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के विवाद के केस को अनिर्णीत मानकर इसे बंद भी कर सकता है.
अगर, सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के मौजूदा केस को दोबारा खोलकर, स्पीकर के. आर रमेश कुमार के फ़ैसले को निरस्त कर के विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल नहीं करता है, तो, संविधान के मुताबिक़, अगले छह महीने में विधानसभा की ख़ाली सीटों पर चुनाव कराने होंगे. किसी असामान्य परिस्थिति के सिवा चुनाव आयोग के पास इन ख़ाली सीटों पर चुनाव को टालने की कोई वजह मौजूद नहीं है.
हालांकि, विधानसभा की सीटें ख़ाली करने की घोषणा कर्नाटक के विधानसभा सचिवालय को करनी होगी. नए स्पीकर के चुने जाने के बाद हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने का इंतज़ार करें, अगर विधायक, पूर्व स्पीकर के फ़ैसले को चुनौती देते हैं, तो ही ऐसा होगा. तमिलनाडु में कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति में विधानसभा सचिवालय ने सीटों के ख़ाली होने की अधिसूचना जारी करने में अपने हिसाब से समय लिया था. उस वक़्त मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक की एक अदालत ने चार साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी. जिसके बाद तमिलनाडु के विधानसभा सचिवालय ने जयललिता की श्रीरंगम विधानसभा सीट को ख़ाली घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी.
दल-बदल निरोधक क़ानून के शब्दों पर ज़ोर, भावना पर नहीं
देश में दल-बदल निरोधक क़ानून बनाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जाना चाहिए. ये समझ से परे है कि राजीव गांधी उस वक़्त दल-बदल निरोधक क़ानून बनाने की क्यों सोची, जब वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर की वजह से प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता में आए थे. और उस वक़्त तक तो बोफ़ोर्स घोटाले का विवाद भी नहीं उठा था, न ही वी.पी. सिंह ने बग़ावत का बिगुल बजाया था. फिर भी, विशाल बहुमत वाली सरकार के अगुवा राजीव गांधी ने दल-बदल निरोध क़ानून बनाने के बारे में सोचा. शायद वो अपनी मां इंदिरा गांधी की छवि को लगे धक्के को पीछे छोड़ना चाहते थे और ‘आया-राम, गया-राम’ की राजनीति करने वाले नेता के दाग़ को धोने के इरादे से दल-बदल निरोधक क़ानून लेकर आए.
मज़े की बात ये है कि विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने इस्तीफ़े से पहले बयान दिया कि दल-बदल निरोधक क़ानून अपने मक़सद में पूरी तरह विफल रहा है. ये और बात है कि कर्नाटक के ही एक और मामले में (एस.आर.बोम्मई बनाम केंद्र सरकार, 1994) ही सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था कि किसी भी सरकार का बहुमत साबित करने की सही जगह सदन (लोकसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा) ही होगा. ये और बात है कि दल-बदल निरोधक क़ानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फ़ैसले के बाद, इस क़ानून की बाक़ी की कमियां जस की तस हैं.
उस समय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पीछे मक़सद ये था कि किसी भी राज्य की सरकार बनाने या गिराने में राज्यपाल के रोल को सीमित किया जाएगा. ताकि वो किसी भी दल में फूट को बढ़ावा या समर्थन न दे सके. उस फ़ैसले के क़रीब 25 वर्षों बाद आज दल-बदल निरोधक क़ानून केवल किताबी बनकर रह गया है. क्योंकि, सर्वोच्च अदालत के उस फ़ैसले के बाद से राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों को या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करने का मौक़ा देने में सावधानी बरतते आए हैं और उन्हें केवल सदन में ही बहुमत साबित करने को कहते हैं.
हाल के कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इस बारे में संवैधानिक नुमाइंदों के फ़ैसले रूटीन ही रहे हैं. हालांकि, कुछ मामलों में जब मुख्यमंत्रियों के पास पूर्ण बहुमत था, तो भी राज्यपालों ने उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा. इसी तरह, कुछ राज्यपालों, जैसे कर्नाटक के वजूभाई वाला और गोवा की मृदुला सिन्हा पर इस बात के आरोप लगे हैं कि जब केंद्र में सत्ताधारी पार्टी ने विरोधी दलों में फूट कराई, तो उन्होंने इन सियासी दांव-पेंचों की तरफ़ से आंखें मूंद लीं. कई मामलों में तो राज्यपालों ने ये कहकर नई ‘स्वस्थ’ परंपरा की शुरुआत करने से इनकार कर दिया, कि इसकी मिसाल ‘बोम्मई केस’ में नहीं दी गई है.
भले ही कोई भी सत्ता में रहा हो, लेकिन किसी ने भी न तो ईमानदारी से दल-बदल निरोधक क़ानून का पालन किया और न ही सुप्रीम कोर्ट के ‘बोम्मई फ़ैसले’ का पूरी तरह से सम्मान किया. इसकी एक मिसाल ही काफ़ी है कि जब राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो बिहार के राज्यपाल रहे बूटा सिंह ने नीतिश कुमार की पूर्ण बहुमत वाली लोकप्रिय सरकार को गिराने में अहम रोल अदा किया था. और बूटा सिंह ने ऐसा एक बार नहीं, बल्कि दो बार किया था. दोनों ही मामलों में संवैधानिक तरीक़े से चुनी गई सरकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को दख़ल देना पड़ा था, ताकि सियासी नैतिकता को फिर से बहाल किया जा सके (रामेश्वर प्रसाद और अन्य बनाम केंद्र सरकार, 2006).
2003 में लाए गए संविधान के 91वें संशोधन के ज़रिए पूर्व की ग़लती को सुधारा गया था. इस बदलाव के तहत विधानसभा में किसी भी राजनीतिक समूह में टूट के लिए दो-तिहाई विधायकों का साथ आना ज़रूरी था, तभी वो अयोग्य ठहराए जाने से बच सकते थे
यहां ये जानना दिलचस्प होगा कि किसी भी सरकार ने ‘बोम्मई केस’ में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी और न ही हालात बदलने की कोशिश की. इसके लिए न तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और न ही कोई संविधान संशोधन लाया गया, ताकि दल-बदल निरोधक क़ानून को सही मायनों में प्रासंगिक बनाया जाए और मज़बूत किया जा सके. केवल बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इस क़ानून में एक बदलाव किया था.
2003 में लाए गए संविधान के 91वें संशोधन के ज़रिए पूर्व की ग़लती को सुधारा गया था. इस बदलाव के तहत विधानसभा में किसी भी राजनीतिक समूह में टूट के लिए दो-तिहाई विधायकों का साथ आना ज़रूरी था, तभी वो अयोग्य ठहराए जाने से बच सकते थे. हाल ही में गोवा में हम ने देखा था कि कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 ने पहले पार्टी सदस्यता छोड़ी और फिर बीजेपी में शामिल हो गए, ताकि वो अयोग्य न ठहराए जा सकें.
यानी 1986 क मणिपुर स्पीकर केस से लेकर कर्नाटक के सबसे ताज़ा मामले तक, या उससे पहले पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद के सियासी ड्रामे तक, दल-बदल निरोधक क़ानून ने बहुत कुछ भुगता है. पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जब येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री नियुक्त करने को चुनौती दी गई, तो हाई कोर्ट का फ़ैसला विभाजित रहा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था. एक के बाद एक कई बार दल-बदल की घटनाओं के दौरान हम ने देखा है कि केंद्र में सत्ताधारी सरकारें क़ानून तोड़ने के मामले में लगातार दिलेर होती जा रही हैं. विधायक हों या फिर विधानसभा अध्यक्ष (जो मुख्यमंत्री का पद न हासिल करने की वजह से शायद ज़्यादा ही सियासी हो जाता है.) हर बार दल-बदल निरोधक क़ानून को तोड़ा-मरोड़ा गया है. इसकी अंतरात्मा से छेड़खानी की गई है. आज ये क़ानून महज़ कंकाल बनकर रह गया है. इसकी आत्मा का गला तो कई बार घोटा जा चुका है.
हर बार संसद ने इस क़ानून को तोड़े जाने की तरफ़ से आंख मोड़ ली है. तो अब शायद वक़्त आ गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही दख़ल दे और इस क़ानून की बुनियादी बातों पर फिर से ग़ौर करे (साथ ही इस में किए गए संवैधानिक बदलावों की भी समीक्षा करे), ताकि ये क़ानून और सख़्त हो. या फिर सर्वोच्च अदालत विधायिका को सलाह दे कि इस क़ानून में आमूल-चूल बदलाव किया जाए. ये तमाशा अब बंद होना चाहिए. और अब अगर कर्नाटक के बाग़ी विधायकों का मामला अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जिसकी उम्मीद है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास मौक़ा होगा कि वो दल-बदल क़ानून को मज़बूत बनाने की दिशा में पहल करे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV