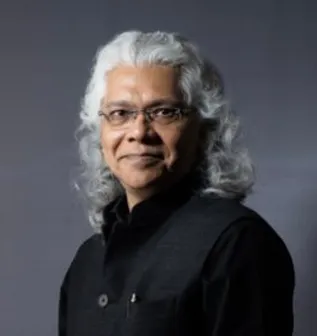हाल ही में एक मशहूर प्रकाशत ब्लूम्सबरी ने एक पुस्तक के प्रकाशन से अपने हाथ पीछे खींच लिए. इसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था. इस विवाद से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है. अब फ़र्ज़ी उदारवाद और इसका प्रचार करने वालों के पाखंड का पर्दाफ़ाश किया जाएगा. ब्लूम्सबरी के क़दम और इसे लेकर जो प्रतिक्रियाएं आईं, उसमें कुछ लोगों ने अपने आप को ‘लिबरल’ के डिब्बे में बंद कर लिया. और फिर ख़ुद को असली भारत के रक्षकों के तौर पर पेश करने की कोशिश की. मगर, उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि इस रिपैकेजिंग के बावजूद, उनके ‘लिबरल’ होने के दावों पर अब लोग यक़ीन करने को तैयार नहीं हैं. केवल दोबारा पैकेजिंग भर से उनका पाखंड छुपने वाला नहीं है.
ये झूठे उदारवादी इतिहास के ऐसे जहाज़ पर सवार हैं, जो उन्हें वक़्त के उस भौगोलिक इलाक़े में ले जा रहा है, जो हम फ्रांस (जहां अब केवल वॉल्टेयर के विचार ही सत्य नहीं रहे) या इटली (जहां किसी को फ़ासीवादी कह देने भर से वो फ़ासीवादी नहीं बन जाते, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले अगर अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो वो असली फ़ासीवादी के तौर पर सामने आते हैं) में देख चुके हैं. उदारवादियों का ये वैचारिक जहाज़ उन्हें भारत की अंतरात्मा यानी सनातन धर्म से दूर ले जा रहा है. इस जहाज़ पर अलग-अलग आकार के कंटेनर लदे हैं. जिनमें तमाम तरह के हित और विशेषाधिकार बंद हैं. और इन बंद डिब्बों में ही भारत के राष्ट्रवाद के धुर विरोधी विचार भी संरक्षित किए जाने की कोशिश हो रही है. और वैचारिक नौका पर सवार ये विशेषाधिकारों वाले कंटेनर, उदारवादियों को भारत की विशाल, गहरी और शक्तिशाली बौद्धिक परंपराओं से दूर ले जा रहे हैं. छद्म उदारवादी ये जाने या जानने की ख़्वाहिश के बग़ैर ही इसकी आलोचना करने में जुटे हैं. भारत की प्राचीन परंपराओं से जुड़े साहित्य का प्रकाशन रोकने पर तुले हैं. छद्म उदारवाद के वैचारिक बोझ से लदा ये पोत अब भारतीय परंपरा के बंदरगाह पर लंगर डालने योग्य नहीं रहा. इसकी वजह कोई क़ानूनी या नियामक अड़चन नहीं. बल्कि सच तो ये है कि भारत ऐसी छद्म विचारधाराओं के पालन पोषण वाले दौर से बहुत आगे जा चुका है.
ब्लूम्सबरी ने मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा की लिखी किताब, ‘देल्ही राइट्स 2020: द अनटोल्ड स्टोरी’ का प्रकाशन करने से इनकार कर दिया था. ब्लूम्सबरी के इस फ़ैसले से पढ़ने लिखने वाले लोग हैरान रह गए. नए चेहरे और वो नई आवाज़ें जो केवल अपनी ज़िद और मज़बूत इच्छाशक्ति, अपने विचारों की ताक़त से लेखक बने हैं, उन्होंने प्रकाशकों के इस गिरोह पर सवाल उठाए हैं. उनके दोहरे मापदंडों को उजागर किया है. फिर चाहे लेखक अमीष त्रिपाठी, मोनिका हालन और डेविड फ्रॉले हों, या फिर ब्यूरोक्रेट संजय दीक्षित और संजीव सान्याल. या वैज्ञानिक आनंद रंगनाथ और इतिहासकार विक्रम संपत हों. सबने प्रकाशकों के गिरोह के इस पाखंड को उजागर किया है.
अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की रक्षा करना हर उस व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, जो विचारों के कारोबार में है. फिर चाहे वो लेखक हो, विद्वान हो या पत्रकार. यहां पर कुछ ख़ास विषयों पर आक्रामकता और चुने हुए मुद्दों पर ख़ामोशी अख़्तियार करने जैसे विकल्प नहीं हैं. और फिर भी बड़े अफसोस की बात ये है कि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जो ब्लूम्सबरी के इस किताब के प्रकाशन से पीछे हटने के फ़ैसले का समर्थन कर रहे हैं. वो भी किताब को पढ़े बिना ही, क्योंकि अभी तक तो इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ. जिन लोगों को इस वैचारिक द्वंद युद्ध की ख़बर देर से लगी है, उन्हें ये बता दूं कि प्रकाशक ने इस किताब को प्रकाशित करने से इसलिए हाथ खींचे क्योंकि, प्रकाशन से पहले आयोजित होने वाली इस किताब के प्री-लॉन्च के कार्यक्रम में ऐसे लोग शामिल होने वाले थे, जिनके नामों पर प्रकाशक सहमत नहीं थे. जहां तक किताब के प्रकाशन की बात है तो बस एक ही सिद्धांत लागू होता है-हर किताब को प्रकाशित किया जाना चाहिए. फिर आपको जो किताब पसंद हो वो पढ़ें. उनकी आलोचना करें, जो पुस्तकें आपको पसंद नहीं आईं. और आपको कुछ ज़्यादा ही दिक़्क़त है, तो आप किसी किताब के बदले दूसरी पुस्तक लिख डालें. लेकिन, तकनीकी तौर पर किसी किताब को प्रतिबंधित करना (ऐसा केवल सरकार कर सकती है) या फिर किसी किताब के विरुद्ध प्रतिबंध जैसे क़दम उठाना ठीक वैसा ही है जैसे बिना सवाल, तर्क या शर्त के विरोध किया जाए. इस किताब के प्रकाशन से ब्लूम्सबरी का हाथ खींचने को एक व्यापक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है. ये एक त्रिपक्षीय युद्ध जैसा है.
प्रकाशक ने इस किताब को प्रकाशित करने से इसलिए हाथ खींचे क्योंकि, प्रकाशन से पहले आयोजित होने वाली इस किताब के प्री-लॉन्च के कार्यक्रम में ऐसे लोग शामिल होने वाले थे, जिनके नामों पर प्रकाशक सहमत नहीं थे.
पहला: प्लेटफॉर्म का संघर्ष
ब्लूम्सबरी एक बड़ा प्रकाशन संस्थान है. भारत में इसकी काफ़ी पहुंच है. ये देश में तरह तरह की किताबें प्रकाशित करता रहा है. एक हद तक, प्रकाशन के पेशे से जुड़े अन्य संगठनों जैसे कि पेंग्विन रैन्डम हाउस, हार्पर कॉलिंस, गीता प्रेस या फिर गरुड़ प्रकाशन (जो अब ये किताब प्रकाशित करने जा रहा है) की तरह ब्लूम्सबरी भी एक ऐसा मंच है, जो अलग-अलग तरह के विचारों को अपना मंच देता है. अलग-अलग वैचारिक समूहों से आने वाले लेखकों को अपनी किताबें प्रकाशित करने का अवसर देता है. जब एक किताब की पांडुलिपी को प्रकाशन कंपनी से मंज़ूरी मिल जाती है. और जब प्रकाशक ये तय कर लेते हैं कि वो ये किताब प्रकाशित करेंगे, तो फिर उस किताब में लिखे शब्दों को लेकर बहस समाप्त हो जाती है. ऐसे में कोई प्रकाशक अगर किसी किताब को इसलिए प्रकाशित करने से मना कर दे क्योंकि वो इस किताब के लॉन्च के अवसर पर किसी ख़ास व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति को पसंद नहीं करते, तो ये स्पष्ट रूप से किसी उदारवादी के नैतिक रूप से उच्च स्थान ग्रहण करने का बहाना भर है. ब्लूम्सबरी का किसी किताब के प्रकाशन पर सहमति जताने के बाद उसके प्रकाशन से हाथ खींचने को निश्चित रूप से लेखक चुनौती देंगे.
रमा लक्ष्मी आशंका जताती हैं कि अब इस किताब को पहले से कहीं अधिक शोहरत मिलेगी, जो शायद वैसी होगी, जिसकी ये किताब असल में ‘हक़दार’ ही नहीं है. सोचिए, बौद्धिकता पर इस क़दर विशेषाधिकार का दावा आख़िर कहां तक उचित है?
लेकिन, इस किताब के प्रकाशन से प्रकाशक के इनकार करने को लेकर जो परिचर्चा हो रही है, वो इससे भी ख़राब है. ये परिचर्चा न तो नैतिकता पर आधारित है. न ही इसमें किसी सिद्धांत का वज़न बढ़ाया जा रहा है और न ही इसके पीछे कोई वास्तविक तर्क दिया जा रहा है. जब भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर ऐसी विरोधाभासी परिचर्चा को देखते हैं, तो ज़रूरत ऐसी परिचर्चाओं को समर्थन देने वालों से सवाल करने की है. द प्रिंट की ओपिनियन्स एडिटर रमा लक्ष्मी ने इस बारे में जो आलोचनात्मक लेख लिखा, वो इसकी एक मिसाल है. रमा लक्ष्मी के लेख को पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आता कि वो प्रकाशक के हाथ खींच लेने की आलोचना कर रही हैं, या फिर इस मिसाल की आड़ में किसी और बात को बढ़ावा देने में जुटी हैं. रमा लक्ष्मी ने अपने लेख में मोनिका अरोड़ा को ‘आरएसस की समर्थक वकील’ कहा. इसके बाद रमा लक्ष्मी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात को लेकर जो उदाहरण दिया (मोनिका अरोड़ा का समर्थन करने से अधिक आसान सलमान रश्दी का बचाव करना था) उससे ऐसा लगा कि अपने जिस लेख की शुरुआत में रमा लक्ष्मी ने प्रकाशक के किताब को पब्लिश करने से हाथ खींच लेने की आलोचना की थी, उसी लेख में कुछ पैराग्राफ के बाद वो मोनिका अरोड़ा को ‘कट्टर हिंदुत्ववादी’ ठहराती नज़र आईं. इसके बाद, रमा लक्ष्मी ये अटकल लगाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले शासन के दौर में ये किताब ग़ायब नहीं होगी. ज़ाहिर है रमा लक्ष्मी शायद ये कहना चाहती थीं कि जो पिछली सरकार थी, वो होती तो ये किताब परिदृश्य से लापता हो चुकी होती! फिर रमा लक्ष्मी आशंका जताती हैं कि अब इस किताब को पहले से कहीं अधिक शोहरत मिलेगी, जो शायद वैसी होगी, जिसकी ये किताब असल में ‘हक़दार’ ही नहीं है. सोचिए, बौद्धिकता पर इस क़दर विशेषाधिकार का दावा आख़िर कहां तक उचित है?
दूसरा: इसके पीछे एक इकोसिस्टम है
ये स्पष्ट नहीं है कि मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा की लिखी किताब, ‘देल्ही राइट्स 2020:द अनटोल्ड स्टोरी’ प्रकाशित करने से क्यों मना कर दिया. जबकि उन्होंने संपादकीय स्तर पर इस किताब को हरी झंडी दे दी थी. इस बात के लिए जिस शख़्स-विलियम डेलरिम्पल पर उंगली उठाई जा रही है, वो प्रकाशन के व्यवसाय वाले इकोसिस्टम के सबसे ताक़तवर लोगों में से एक माने जाते हैं. पर, ईमानदारी की बात ये है कि आतिश तासीर ने जब ये कहा कि ‘विलियम डेलरिम्पल के बिना ये संभव नहीं होता. इस क़दम से यानी किताब का प्रकाशन रुकने से सरकार के शर्मनाक प्रचार के एक बिंदु पर रोक लगी है.’ तो विलियम डेलरिम्पल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. अभी जनता को इस बात का इंतज़ार है कि विलियम डेलरिम्पल इस बात की तस्दीक करते हैं अथवा इनकार करते हैं. लेकिन, जो लोग एक ‘आइडिया ऑफ़ इंडिया’ के अनजाने विचार को ज़ोर शोर से बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बातों को गंभीरता से देखें तो पता चलता है कि यक़ीनन एक इकोसिस्टम काम कर रहा है. जो लगभग एक बटालियन की तरह है और ये सुनिश्चित करता है कि ऐसा कोई भी ख़याल जो उनके विचारों से मेल न खाए, वो किसी सूरत में घुसपैठ नहीं कर सकता है. उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो कितने रूढ़िवादी मालूम होते हैं. मगर, ये वही लोग हैं जो एक मंच से तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के हक़ के लिए ज़बरदस्त भाषण देते हैं. वहीं दूसरे मंच से इस पर पाबंदी लगाने वाले क़दमों का जश्न मनाते हैं.
ये प्रकाशक और लेखक के बीच सीधी लड़ाई होनी चाहिए थी. मगर, अब ये लेखकों और असभ्य लोगों के साहित्यिक समूहों और इकोसिस्टम के बीच ऐसा संघर्ष बन गया है, जो किसी वैकल्पिक विचार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं. अब तक जिस तरह का हंगामा मचा है और आने वाले समय में जिस तरह की प्रतिक्रिया हम देखने वाले हैं, उसके बाद बहुत से मौजूदा और भविष्य के लेखक ब्लूम्सबरी से किनारा कर सकते हैं. ऐसा हुआ तो प्रकाशन कंपनियां विचारों के प्रचार का मंच न रह कर कुछ ख़ास विचारधाराओं को तरज़ीह देने वाले इको चैम्बर बन जाएंगे. इससे प्रकाशन के क्षेत्र में निम्नता का नया स्तर देखने को मिलेगा. इससे ये संकेत जाएगा कि अगर वो एक ख़ास विचारधारा को तरज़ीह देने वाले इकोसिस्टम के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो वैचारिक आदान प्रदान के अन्य मंचों के साथ क्या हो सकता है. ये एक तरह से दबी-छुपी सेंसरशिप ही है, जो बिना सरकार की दख़लंदाज़ी के हो रही है. इसमें एक इकोसिस्टम की जीत होती है. मगर मंच हार जाता है. और विचारों के आदान-प्रदान के ऐसे जितने भी मंच इस इकोसिस्टम के आगे घुटने टेकते हैं, वो धीरे धीरे अप्रासंगिक बनते जाएंगे. गरुड़ प्रकाशन के संस्थापक संक्रांत सानु के मुताबिक़ जिस किताब को छापने से ब्लूम्सबरी ने इनकार कर दिया, उसकी पंद्रह हज़ार प्रतिलिपियों की बुकिंग तो 24 घंटे से भी कम समय में हो गई.
ये प्रकाशक और लेखक के बीच सीधी लड़ाई होनी चाहिए थी. मगर, अब ये लेखकों और असभ्य लोगों के साहित्यिक समूहों और इकोसिस्टम के बीच ऐसा संघर्ष बन गया है, जो किसी वैकल्पिक विचार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं.
तीसरा: विचारधाराओं की ताक़त
जब तक ये संघर्ष दो संस्थाओं यानी प्रकाशकों और लेखकों के बीच बना हुआ है, तब तक तो ये सही रास्ते पर चलता कहा जाएगा. लेकिन, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो एक मंच के तौर पर अगर ब्लूम्सबरी कुछ ख़ास आवाज़ों को उस इकोसिस्टम के दबाव में ख़ामोश कर देता है, जिसके अंतर्गत वो काम करता है. तो इससे वो एक ख़ास वैचारिक खेमे का हिस्सा बन जाएगा. फिर प्रकाशन संस्था होने के बजाय उसे वैचारिक दृष्टि से देखा जाएगा. और तब ये एक ऐसा मुद्दा बन जाता है, जिस पर वाद-विवाद की ज़रूरत है. मिसाल के तौर पर अमेरिका में ट्विटर, फ़ेसबुक और यू ट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर इस बात का दबाव है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करें. 28 मई 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया था. इस कार्यकारी आदेश में उन्होंने ऑनलाइन सेंसरशिप को रोकने का फ़रमान इन प्लेटफ़ॉर्म को दिया था. इस आदेश को जारी करते हुए प्रेसीडेंट ट्रंप ने कहा था कि ऐसे मंचों यानी ‘सोशल मीडिया की पक्षपाती सेंसरशिप के चलते हमारे देश में राष्ट्रीय वाद-विवाद को क्षति पहुंच रही है.’ ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा ‘अच्छी नीयत से सेंशरशिप करने’ के दावे पर सवाल उठाए थे.
भारत के वैचारिक बाज़ार में पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय परिचर्चा में वामपंथ का दबदबा रहा है. इसे बदलने में वक़्त लगेगा. भारत विरोधी और हिंदू विरोधी संवाद की संरचना करने वालों ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया हुआ है. इससे एक ऐसा समृद्ध इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जो अपनी प्रशंसा को पसंद करता है, किसी भी हद तक जाकर अपने भाई-बंधुओं का बचाव करता है. विश्लेषण के उद्योग में अन्य सभी विचारों को कुचल कर संवाद के दायरे से बाहर कर देता है. वामपंथ के इस वैचारिक इकोसिस्टम का केंद्र लुटिएंस दिल्ली रही है. लेखक और पाठक दोनों ही इसी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हैं. लेकिन, उनका वैचारिक प्रभुत्व अब ख़त्म हो रहा है. और ऐसा नहीं है कि जो नई सरकार है वो इसमें कोई योगदान दे रही है. या सरकार इसे अपनी ताक़त से बदल रही है, ऐसा भी नहीं है. आज एक नई राजनीति का दौर है और वही मौजूदा सरकार को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सत्ता में ले आई है. तो ऐसे में इकोसिस्टम के सदस्य भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को अपने छीजते प्रभुत्व के लिए ज़िम्मेदार ठहराएं. पर सच ये है कि आज देश के नागरिक ही नए भारत के नए विचारों को नए तरीक़े से अभिव्यक्त करना चाहते हैं.
भारत के वैचारिक बाज़ार में पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय परिचर्चा में वामपंथ का दबदबा रहा है. इसे बदलने में वक़्त लगेगा. भारत विरोधी और हिंदू विरोधी संवाद की संरचना करने वालों ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया हुआ है.
और अंत में अभिव्यक्ति की आज़ादी अब स्वतंत्र है
नए भारत के इन सभी आकांक्षाओं की चाहत यही है कि वो वास्तविक भारत को पुनर्जीवित करें. ये परिवर्तन इसके साथ साथ बदल रहे बाज़ार के आयाम की ताक़त से आएगा. आज की तारीख़ में वामपंथी विचार का क्षेत्र बस नाम मात्र का ही बचा है. हालांकि, ये पूरी तरह समाप्त नहीं होगा. ये बचा रहेगा. और ऐसा होना भी चाहिए. क्योंकि ये हमें याद दिलाएगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. किस दिशा में नहीं जाना चाहिए. और वामपंथ की मौजूदगी हमें ये तो बताएगी ही कि किसी भी विचार का गला नहीं घोंटा जाना चाहिए. लेकिन, ये तय है कि वामपंथी विचारधारा, इसका इकोसिस्टम और संकुचित होते मंच हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे. उनके एकाधिकार को संस्थागत तरीक़े से चुनौती दी जाएगी. और इसके लिए चुन चुनकर क़दम उठाए जाएंगे. किताबों के प्रकाशन पर रोक लगाने के उनके क़दमों का ज़ोरदार तरीक़े से विरोध होगा. तकनीक आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम है. आज अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वयं को उन लोगों के शिकंजे से आज़ाद कर रही है, जो इसकी वकालत तो करते थे. पर, तरह तरह से इसका दमन करते रहते थे. वामपंथ का ये इकोसिस्टम, इसके विचारकों और मंचों को स्वयं को इन नए बदलावों के हिसाब से ढालना ही होगा.
पिछले सात दशकों में भारत की राजनीति ने अपने बौद्धिक क्षेत्र को पूरी तरह से वामपंथ के हवाले कर दिया. और ये मौक़ा मिलने के बाद लेफ्ट ने हर सच्चाई को अपने हिसाब से ढालने में पूरी ताक़त लगाई है. वो हमेशा इस विचार को पालते पोसते रहे हैं कि- भारत एक ऐसा देश है, जिसकी कोई हस्ती नहीं थी. जिसके पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं था, जो न कुछ करता था न कुछ सोचता था. भारत तो बस कायरों और ख़ुदग़र्ज़ राजाओं का देश था. भारत एक ऐसा देश था जिसका धर्म भी पिछड़ा हुआ था. जहां पर ज्ञान संबंधी व्यवस्था तो तब आई, जब बाहरी आक्रांताओं ने भारतीयों का परिचय नए धर्मों से कराया. हिंदू कट्टरपंथी होते हैं. बाक़ी सब शहीद और पीड़ित होते हैं. भारत तो एक बिखरा हुआ ज़मीनी इलाक़ा था. ये तो बाहर से आए विजेताओं ने इसे एक देश के तौर पर एक सूत्र में बांधा. ये एक ग़रीब और निम्न स्तर का देश था, जिसे पश्चिम ने ग़ुलाम बनाकर सभ्य बनाया. वामपंथ के इस वैचारिक प्रभुत्व को अब तक किसी ने चुनौती नहीं दी. ये एक छोटे से समूह द्वारा नियंत्रित था. इसे एक राजनीतिक ख़ानदान के अबाध शासनकाल से ताक़त मिलती रही. जो शासन तो करता था मगर प्रशासन नहीं देता था. ब्लूम्सबरी का विवाद हमें बताता है कि अब वामपंथी वैचारिक प्रभुत्व के दिन बस गिने चुने ही बचे हैं. अब गुज़रे ज़माने की विचारधाराएं, इकोसिस्टम और मंच आने वाले भारत को नहीं चलाएंगे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV