-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाते हुए भारत को मौजूद काउंटर इंटेलिजेंस ख़तरों के बारे में सावधान रहना चाहिए.
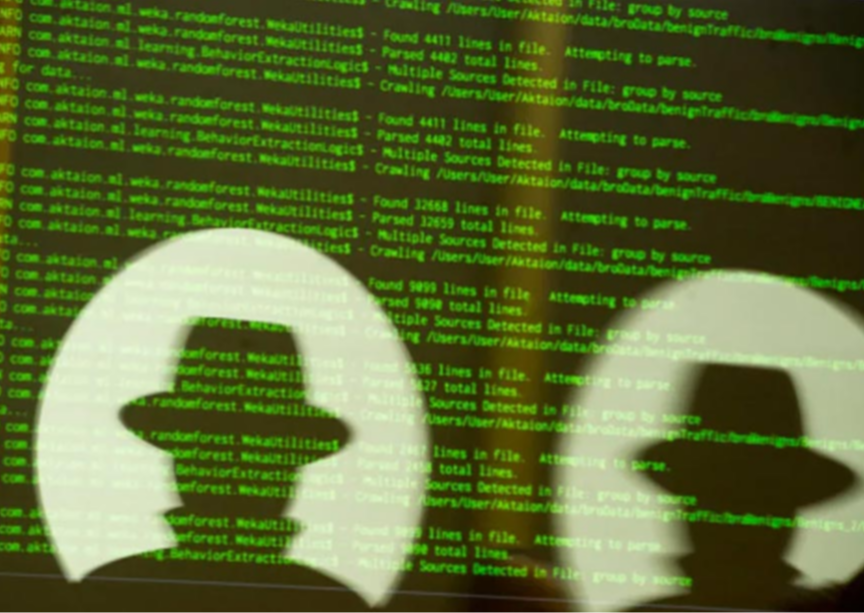
“गोपनीयता को लेकर मेरे भाई के कुछ विशेष नियम हैं और उनका ईमानदारी से पालन करने के लिए वो मुझे मजबूर करता है. जिन लोगों पर वो भरोसा करता है, उनकी संख्या बहुत कम है और वो उन्हें नहीं बढ़ाएगा. कम शब्दों में कहें तो वो न तो अरब लोगों पर भरोसा करता है, न यूरोप के लोगों पर. हम जो काम अकेले में करते हैं, उसमें धोखा केवल हम दे सकते हैं.”
माना जाता है कि ये शब्द फिलिस्तीन के आतंकवादी खलील ने जॉन ले कैरे के 1983 के उपन्यास द लिटिल ड्रमर गर्ल के पूछताछ करने वाले नायक चेयरमैन 'चार्ली' रॉस से कहे थे लेकिन ये एक बहुध्रुवीय युग में इंटेलिजेंस साझा करने की पहेली में भी अच्छी तरह से लागू हो सकते हैं. जैसे-जैसे बड़ी, मध्यम और छोटी ताकतें आज के समय में तेज़ी से उपलब्ध सामरिक साझेदारी के लिए विस्तृत जानकारी और पसंद का फायदा उठाना चाहती हैं, वैसे-वैसे इंटेलिजेंस गठबंधन का निर्माण- जो कि ऐतिहासिक रूप से सामरिक सहयोग/ताकत दिखाने का माध्यम है- पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.
किसी 'मिनीलेटरल' इंटेलिजेंस साझा करने के फ्रेमवर्क के भीतर उत्पन्न काउंटर इंटेलिजेंस की समस्याओं का अलग-अलग देश कैसे मुकाबला कर सकते हैं?
फिर भी इंटेलिजेंस साझा करने के साथ हमेशा काउंटर इंटेलिजेंस के विचार जुड़े रहते हैं. यहीं पर एक 'बड़े' दायरे के द्वारा 'विश्वासघात' का संभावित ख़तरा बढ़ाने को लेकर खलील की रहस्यमय टिप्पणी फैसला लेने पर असर डालती है. किसी 'मिनीलेटरल' इंटेलिजेंस साझा करने के फ्रेमवर्क के भीतर उत्पन्न काउंटर इंटेलिजेंस की समस्याओं का अलग-अलग देश कैसे मुकाबला कर सकते हैं? और भारत जैसे देश- जो कि क्षेत्रीय 'ज्यामितिक' इंटेलिजेंस कूटनीति में एक सक्रिय समर्थक और भागीदार है- के लिए इसका क्या मतलब है?
मौजूदा वैश्विक सुरक्षा की संरचना के लिए खुफिया गठबंधन/समूह अनिवार्य हो गए हैं. फाइव आईज़ अलायंस सबसे मशहूर हो सकता है- और कुछ हद तक इसका साझेदार संगठन जैसे कि ‘नाइन आईज’ (जिसमें फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स भी शामिल हैं) भी- लेकिन दुनिया में कई उदाहरण हैं. 70 के दशक में तीन बड़े वैश्विक खुफिया गठबंधन की स्थापना देखी गई. इनमें पहला गठबंधन था क्लब डी बर्ने जिसकी स्थापना यूरोप में फिलिस्तीनी आतंकी गतिविधियों की बढ़ती चुनौती को लेकर यूरोप के देशों के बीच आतंकवाद विरोधी प्रयासों में तालमेल के लिए की गई थी. बाद में इस संगठन में यूरोपियन यूनियन (EU) के सभी 27 सदस्य देशों को शामिल कर लिया गया. दूसरा और तीसरा गठबंधन ‘मिनीलेटरल’ था जिनकी स्थापना 1975 में अमेरिकी कांग्रेस की चर्च कमेटी के द्वारा CIA के गलत कामों का खुलासा करने के बाद CIA की कार्रवाई के घटते दायरे की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में की गई. 1976 में स्थापित मैक्सिमैटर अलायंस, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और स्वीडन शामिल थे, का निर्माण यूरोप पर ध्यान रखकर किया गया और ये अभी भी काम कर रहा है. वहीं सफारी क्लब, जिसमें फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब, मोरक्को और क्रांति से पहले के ईरान की इंटेलिजेंस सर्विस शामिल थीं, ने शीत युद्ध के बाद के दौर में अफ्रीका में सोवियत संघ के समर्थन वाले देशों और विद्रोही किरदारों के ख़िलाफ़ गुप्त ऑपरेशन के लिए तालमेल की कोशिश की.
मौजूदा समय की बात करें तो कनाडा और न्यूज़ीलैंड के शामिल होने की वजह से फाइव आईज़ के भीतर आंतरिक कमज़ोरी के बारे में चिंताए बढ़ गईं.
हालांकि काउंटर इंटेलिजेंस की चुनौतियां इस तरह के संगठनों के अस्तित्व और अभियान से अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं. 60 के दशक में अमेरिका ने सुनिश्चित किया कि फ्रांस को नैटो की खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था से अलग रख जाए. इसकी वजह ये थी कि CIA के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के इनर सर्कल में एक सोवियत ‘जासूस’ के कथित तौर पर होने की मुहैया कराई गई सूचना पर कार्रवाई करने में फ्रांस नाकाम रहा था. सफारी क्लब का अस्तित्व अपनी स्थापना के तुरंत बाद खत्म हो गया क्योंकि 1979 में ईरान की क्रांति के बाद तेहरान में एक नई सरकार ने सत्ता संभाल ली. मौजूदा समय की बात करें तो कनाडा और न्यूज़ीलैंड के शामिल होने की वजह से फाइव आईज़ के भीतर आंतरिक कमज़ोरी के बारे में चिंताए बढ़ गईं. कनाडा को लेकर इसलिए क्योंकि उसके सुरक्षा के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं की क्वालिटी आम तौर पर खराब है और न्यूज़ीलैंड को लेकर इसलिए क्योंकि चीन जैसी संशोधनवादी शक्तियों (मौजूदा प्रणाली को बदलने या ख़त्म करने की कोशिश करने वाली ताकत) के साथ उसका अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है. इसी तरह की चिंताएं यूरोप के इंटेलिजेंस सहयोग पर ग्रहण लगाती हैं. ऑस्ट्रिया, जो कि नाम के लिए अभी भी क्लब डी बर्ने का सदस्य है, को प्रभावी तौर पर उसकी कमज़ोर साइबर सुरक्षा की वजह से गठबंधन से बाहर रखा गया है. इसका एक गंभीर कारण ये है कि ऑस्ट्रिया उस समय तक अपने सहयोगी पश्चिमी देशों के ख़िलाफ़ जासूसी को बर्दाश्त करता है जब तक कि निशाने पर वो ख़ुद नहीं होता. वहीं बेल्जियम क्लब डी बर्ने का सदस्य होने और हाल के वर्षों में अपनी काउंटर इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ाने के बाद भी 2010 के करीब से कई जासूसी स्कैंडल से हिल गया है. इससे यूरोप की सुरक्षा को लेकर व्यापक ख़तरों के बारे में सवाल उठ रहे हैं.
हालांकि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद ये साफ है कि खुफिया गठबंधनों के भीतर सदस्यता सदस्य देशों के लिए व्यापक तौर पर सकारात्मक रही है. इससे उन्हें दुनिया के मंच पर बहुत ज़्यादा असर दिखाने की अनुमति मिली है. इसलिए चुनौती मौजूदा काउंटर इंटेलिजेंस की कमज़ोरियों को कम करते हुए सहयोग को बढ़ावा देना जारी रखना है.
भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पिछले एक दशक में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के भीतर भारत की विस्तृत भूमिका के केंद्र में अलग-अलग क्षेत्रीय खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था में उसकी अग्रणी भूमिका रही है. ये भूमिका सुरक्षा सहयोग के विशेष उद्देश्य के साथ-साथ मौजूदा बहुपक्षीय कूटनीतिक माध्यमों के अधीन के रूप में भी है. 2019 में भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) की स्थापना इन कोशिशों का एक मुख्य हिस्सा रही है. पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में ओवरहेड सैटेलाइट और रडार स्टेशन के ज़रिए बुनियादी सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) और इमेजरी इंटेलिजेंस (IMINT) इकट्ठा और उसे प्रोसेस करने के सेंटर के रूप में काम करने वाला IFC-IOR इस क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया कराने वाले के रूप में ख़ुद को स्थापित करने में भारत की कोशिशों के लिए महत्वपूर्ण रहा है. इस सेंटर के द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारियों ने 2023 के आख़िर से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की एंटी-पाइरेसी अभियानों में मदद की है. इन जानकारियों को IFC-IOR के गुरुग्राम मुख्यालय में तैनात उनके लाइज़न अधिकारियों के ज़रिए साझेदार देशों जैसे कि यूनाइटेड किंगडम (UK), फ्रांस, क्वॉड के साथी देशों और बांग्लादेश को भी मुहैया कराया जाता है.
भारत क्षमता दिखाने के लिए संसाधन के रूप में इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठनों की अपनी सदस्यता का भी लाभ उठाता है. IFC-IOR से मिली प्रोसेस्ड हाइड्रोग्राफिक इंटेलिजेंस को नियमित रूप से लाइज़न अधिकारियों के ज़रिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के साथी सदस्य देशों के साथ साझा किया जाता है. इससे सदस्य देशों को आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चेतावनी तो मिलती ही है, साथ ही पाइरेसी जैसी समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने में भी मदद मिलती है. भारत कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव के भीतर भी एक सक्रिय भूमिका निभाता है. 2011 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक द्विवार्षिक सुरक्षा संगठन है जो भारत, बांग्लादेश, सेशेल्स, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस के खुफिया अधिकारियों को एक साथ लाता है और साइबर सुरक्षा, तस्करी विरोधी प्रयासों और समुद्री जानकारी को फैलाने जैसे मुद्दों पर ध्यान देता है. भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर इंटेलिजेंस, विशेष रूप से रैंसमवेयर के मुकाबले और एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट एक्टर्स (ऐसा व्यक्ति या समूह जो कंप्यूटर नेटवर्क तक बिना अनुमति के पहुंच हासिल करने के लिए जटिल साइबर गतिविधियों का इस्तेमाल करता है) की पहचान के उद्देश्य से, बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में तालमेल के लिए बिम्सटेक के सुरक्षा माध्यमों का भी इस्तेमाल करता है.
भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर इंटेलिजेंस, विशेष रूप से रैंसमवेयर के मुकाबले और एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट एक्टर्स की पहचान के उद्देश्य से, बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में तालमेल के लिए बिम्सटेक के सुरक्षा माध्यमों का भी इस्तेमाल करता है.
हालांकि भारत की कोशिशें संभवत: उसी तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं जैसी चुनौतियां ऊपर बताए गए पश्चिमी देशों के सामने हैं. मालदीव में चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार के आने से कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसी व्यवस्था के सुचारू काम-काज पर पहले ही हानिकारक असर पड़ चुका है क्योंकि मालदीव ने दिसंबर 2023 में इस संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार किया था. वास्तव में भारत और चीन समर्थक मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद यामीन के प्रशासन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से 2014 से 2020 के बीच भी इस संगठन की बैठक टल चुकी है. ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे मंचों के सुचारू काम-काज के लिए राजनीतिक रूप से पैदा काउंटर इंटेलिजेंस की चुनौतियों को दिखाता है. इसी तरह चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के ज़रिए भारत के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय खुफिया गठबंधनों में भाग लेने वाली क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अपने साथ मिला सकता है. इससे सुरक्षा चिंताओं में बढ़ोतरी हो सकती है. इसलिए निम्नलिखित सिफारिशें पेश की जा सकती हैं:
पहली सिफारिश ये है कि भारत जिन बहुपक्षीय कूटनीतिक संगठनों में भागीदार है- जैसे कि बिम्सटेक और IORA- उनमें एक केंद्रीकृत काउंटर इंटेलिजेंस कमांड की स्थापना की जाए. सचिवालय से काम करने वाले इस कमांड में सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी शामिल होंगे और वो मिलकर काम करके खुफिया जानकारी साझा करने के साथ आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में एक-दूसरे से सीखेंगे. दूसरी सिफारिश है कि मौजूदा इंटेलिजेंस कूटनीति की कोशिशों का विस्तार किया जाए. जिन देशों में सुरक्षा नौकरशाही/इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ढंग से विकसित है जैसे कि भारत, वो किसी भी मजबूरी के ख़िलाफ़ सदस्य देशों के इंटेलिजेंस सिस्टम को बढ़ावा देने में सक्रिय कोशिशों में भाग लें. आख़िरी सिफारिश ये है कि क्लब डी बर्ने जैसे संगठनों की तरह सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति के आधार पर साझेदारों की सुरक्षा क्षमताओं की नियमित छानबीन की जाए.
इस तरह के संगठनों के भीतर काउंटर इंटेलिजेंस को स्वीकार करने और फिर उसके प्रबंधन के लिए विशेष तौर-तरीकों को अपनाने से ऊपर बताए गए कुछ ख़तरों की भरपाई हो जाएगी. आख़िर, काउंटर इंटेलिजेंस जो ख़तरे पैदा करते हैं उन पर नज़र रखते हुए सहयोग की समानांतर तलाश एक बहुध्रुवीय दुनिया में सफल और प्रभावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है. ये ऐसी चीज़ है जिस पर अलग-अलग देशों को अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए.
आर्चिष्मान गोस्वामी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोग्राम में M Phil की पढ़ाई करने वाले पोस्टग्रेजुएट छात्र हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Archishman Ray Goswami is a Non-Resident Junior Fellow with the Observer Research Foundation. His work focusses on the intersections between intelligence, multipolarity, and wider international politics, ...
Read More +