-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
दुविधा के बीच सही पसंद चुनने से लंबे समय में उसी तरह उच्च विकास को समर्थन मिल सकता है जैसे कि बुनियादी सुधार के एजेंडे को लागू करना.
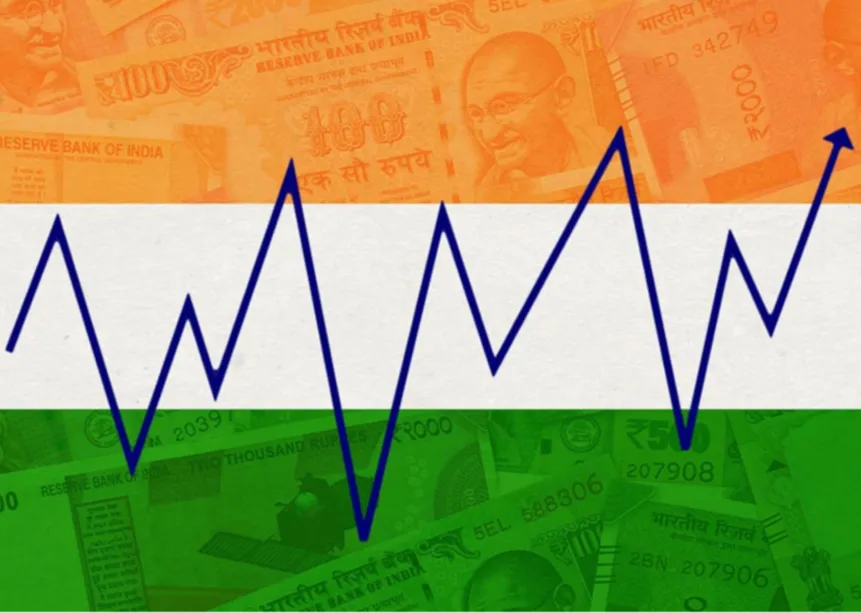
Image Source: Getty
भारत एक निर्णायक मोड़ पर है. विकास के साथ आने वाली नई चुनौतियों के मुताबिक हमारे संस्थानों के ढलने की तुलना में हमारी लंबे समय से निष्क्रिय आर्थिक क्षमता का एहसास तेज़ी से हो रहा है. 6.6 प्रतिशत की हमारी दीर्घकालीन विकास दर के ऊपर लगभग 0.7 प्रतिशत प्वाइंट की संभावित GDP बढ़ोतरी के साथ इस साल सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और महिलाओं समेत बेरोज़गारी की दर कम होना संकेत है कि भारत का युग शायद आ गया है. इस तरह की अच्छी परिस्थितियों में अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये सामान्य है कि उच्च विकास लाने वाले आर्थिक बलों के नाज़ुक संतुलन में रुकावट आने तक वो अतीत में काम आने वाली चीज़ों को जारी रखें.
दुनिया भर में, चाहे पूरब हो या पश्चिम, निकट समय में दूसरे पायदान की अर्थव्यवस्थाएं- यूरोप, भारत, बांग्लादेश और दक्षिण-पूर्व एशिया- विकास की रफ्तार पकड़ेंगी.
दो मामलों को लेकर सरकार अतीत की परंपराओं से हट रही है: पहला, सार्वजनिक वित्त आधारित विकास पर जारी निर्भरता पहले की इस आम राय से हटकर है कि निजी निवेश (घरेलू और विदेशी) को कल्याणकारी समर्थन को लेकर लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ सीमित संसाधन वाले लोकतंत्र में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए. दूसरा, ये आकलन कि निराशाजनक वैश्विक आर्थिक माहौल के बावजूद 7 प्रतिशत से ज़्यादा विकास निश्चित है.
दुनिया भर में, चाहे पूरब हो या पश्चिम, निकट समय में दूसरे पायदान की अर्थव्यवस्थाएं- यूरोप, भारत, बांग्लादेश और दक्षिण-पूर्व एशिया- विकास की रफ्तार पकड़ेंगी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को लगता है कि एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 2023 से 2025 तक औसत विकास दर धीमी होकर 5.4 प्रतिशत से 4.8 प्रतिशत हो जाएगी. इसका मुख्य कारण चीन के विकास में कमी आना होगा जो GDP के 5.2 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 4.1 हो जाएगी. पहले चीन की वजह से विकास की दर बढ़ती थी. विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसी अवधि के दौरान थोड़ा सुधार करते हुए 1.6 प्रतिशत की विकास दर से बढ़कर 1.8 पर पहुंचेंगी. हालांकि अमेरिका में विकास दर 2.5 से गिरकर 1.8 प्रतिशत हो जाएगी.
वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहायता नहीं करने वाले रुझानों को रोकने के लिए भारत ने सार्वजनिक वित्त और औद्योगिक विनियमन आधारित विकास के मॉडल को अपनाया है जिसे मौजूदा समय में विकसित अर्थव्यवस्थाएं समर्थन दे रही हैं. कुल सार्वजनिक कर्ज़ (केंद्र और राज्य सरकारों) पहले ही 2017-18 में GDP के 69.6 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में GDP के 86.5 प्रतिशत पर पहुंच चुका है जबकि इसका मानक GDP का 60 प्रतिशत है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं से हटकर भारत में प्रोत्साहन (स्टिमुलस) खर्च मुश्किल है, ख़ास तौर पर आमदनी और खपत बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च जो संसाधन की कमी को बढ़ाता है. भारत में केंद्र सरकार के फंड से चलने वाली योजनाओं की संख्या 2017-18 के 73 से बढ़कर 2024-25 के अंतरिम बजट में 173 हो गई है. कुल सरकारी खर्च (केंद्र और राज्य) 2017-18 के 17 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में वर्तमान GDP का 19 प्रतिशत हो गया.
कर्ज़ आधारित सार्वजनिक ख़र्च के विकास के मॉडल पर लगातार निर्भरता लंबे समय में वित्तीय प्रोत्साहन में चरणबद्ध तरीके से कमी के रूप में दिखती है.
2019-20 में कंपनियों को महत्वपूर्ण रियायत दी गई. टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया, वहीं 2024 तक बनी नई कंपनियों के लिए और भी कम 15 प्रतिशत टैक्स लगाया गया. अंतरिम बजट में नई कंपनियों के लिए प्रोत्साहन वाली टैक्स दर का विस्तार नहीं किया गया है लेकिन पूर्ण बजट में ऐसा हो सकता है. हालांकि, कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक जाल, जिसकी वजह से मौजूदा सरकार को हर क्षेत्र और हर जाति का समर्थन मिलता है, के कारण बढ़ते वित्तीय दबाव से और ज़्यादा टैक्स छूट की गुंजाइश सीमित है. केंद्र के बजट से खाद्य, ईंधन, उर्वरक पर सब्सिडी भुगतान 4.1 ट्रिलियन रुपये का है जो कि GDP का 1.2 प्रतिशत और कुल खर्च का 8.6 प्रतिशत है. सार्वजनिक परिवहन (रेल और सड़क) और इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों (पानी और बिजली) पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी सरकारी एजेंसियों का खज़ाना खाली करती है जबकि औद्योगिक सब्सिडी सरकारी बैंकों पर बोझ डालती है.
कर्ज़ आधारित सार्वजनिक ख़र्च के विकास के मॉडल पर लगातार निर्भरता लंबे समय में वित्तीय प्रोत्साहन में चरणबद्ध तरीके से कमी के रूप में दिखती है. सामान्य सोच के विपरीत वित्तीय परेशानी 2020-21 में कोविड-19 महामारी के पहले भी मौजूद थी. 2019-20 से पहले के पांच वर्षों में वित्तीय घाटे के मामले में जो हासिल किया गया था उसे 2019-20 में पलट दिया गया. 2013-14 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की सरकार के सत्ता से जाते समय वित्तीय घाटा 4.5 प्रतिशत पर था जो 2018-19 में गिरकर 3.4 प्रतिशत हो गया था. हालांकि इसमें कुछ हद तक कमी भ्रांति थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय घाटा के असली आकार को छिपाने वाले स्मार्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सुलझाकर 2019-20 में नई शुरुआत की और इस तरह 2019-20 में वित्तीय घाटा बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया जो कि 2013-14 की तुलना में थोड़ा अधिक था. इसके अगले साल 2020-21 में कोविड-19 की वजह से आई आर्थिक रुकावटों ने वित्तीय घाटा बढ़ाकर GDP का 9.2 प्रतिशत कर दिया. 2024-25 के अनुमानित 5.8 प्रतिशत वित्तीय घाटा से GDP के 4 प्रतिशत के मानक तक आने में 2026-27 तक का समय लगने की संभावना है जो कि 2019-20 में वित्तीय घाटा 4 प्रतिशत के पार जाने के पूरे सात साल के बाद है.
उदार नीति की तरफ वापसी के लिए संकेत का इंतज़ार है जो कि 2025-26 तक संभव है जब महंगाई का दबाव कम हो जाएगा.
अगले दो वित्तीय वर्षों में विकास सार्वजनिक निवेश से प्रेरित होगा. अच्छी तरह से सार्वजनिक खर्च के प्रबंधन के लिए इन्क्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो (वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात)- ऐसा मीट्रिक जो निवेश में संभावित खामियों के बारे में चेतावनी देता है- पर नज़र रखना आदत में शामिल होना चाहिए. टैक्स इकट्ठा करके या सार्वजनिक संपत्तियों के मुद्रीकरण (मोनेटाइज़ेशन) और सरकारी औद्योगिक संस्थानों एवं बैंकों का निजीकरण करके गैर-टैक्स राजस्व प्राप्त करने के मुश्किल विकल्पों की तुलना में लंबे समय तक सरकारी कर्ज के द्वारा समर्थित बजट की मजबूरियों से पूंजी के कम कुशल उपयोग का ख़तरा है और इस तरह महंगाई में बढ़ोतरी होती है.
9.53 प्रतिशत खाद्य महंगाई के साथ दिसंबर 2023 में खुदरा महंगाई की दर 5.69 प्रतिशत थी. RBI को उम्मीद है कि आने वाले समय में महंगाई की दर कम रहेगी लेकिन वो स्वीकार करता है कि 2024-25 की तीसरी तिमाही में 4.75 प्रतिशत के साथ 4 प्रतिशत के मानक से “काफी दूर” और “ख़तरनाक रूप से 5 प्रतिशत के नज़दीक” है. इसके परिणामस्वरूप महंगाई पर नियंत्रण के लिए फरवरी 2023 में तय 6.5 प्रतिशत का रेपो रेट बना हुआ है. उदार नीति की तरफ वापसी के लिए संकेत का इंतज़ार है जो कि 2025-26 तक संभव है जब महंगाई का दबाव कम हो जाएगा.
2023-24 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.3 प्रतिशत (NSO) रहने की उम्मीद है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 7 प्रतिशत (RBI) की संभावना है. आश्चर्य की बात है कि अंतरिम बजट 2024-25 में बहुत ज़्यादा सतर्क रुख अपनाते हुए अस्पष्ट रूप से वास्तविक विकास दर सिर्फ 5.8 प्रतिशत बताई गई है (10.5 प्रतिशत के नॉमिनल GDP विकास में 4.7 प्रतिशत की अपेक्षित महंगाई कम करके). IMF के अनुमान के मुताबिक 2023-24 में वास्तविक विकास दर 6.7 प्रतिशत और उसके अगले साल 6.5 प्रतिशत होगी. वित्त मंत्री सीतारमन ने शायद टैक्स और राजस्व के लक्ष्यों, जो कि विकास की संभावना से जुड़े हुए हैं, के मामले में धोखा खाने से बचने के लिए एक रूढ़िवादी, नॉमिनल GDP विकास दर अपनाया होगा. अगले दो साल तक मानक से बहुत अधिक लगातार महंगाई के साथ अधिक, महंगाई पर नियंत्रण वाली ब्याज दर विकास के लिए एक चुनौती पेश करती है. प्राइवेट सेक्टर की “एनिमल स्पिरिट” (आर्थिक अनिश्चितता के दौरान उपभोक्ताओं का विश्वास और वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाली भावनाएं) तभी जवाब देगी जब ज़्यादा विकास की उम्मीदें पूरी होंगी.
निकट भविष्य में भारत को राजनीतिक स्थिरता के फायदे मिलने की संभावना है जो कि निजी निवेश- विशेष रूप से विदेशी निवेश- को लोकतांत्रिक बदलाव के जोखिम से दूर रखेगा. इससे अत्याधुनिक तकनीकों को बाज़ार तक लाने में मदद मिल सकती है. इन तकनीकों में मौजूदा समय में प्रदर्शन के चरण वाली तकनीकें शामिल हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, रक्षा उपकरण, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन सीक्वेसटरिंग, लो कार्बन कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन और सेकेंड एंड थर्ड जेनरेशन (सेल्युलोसिक और शैवाल आधारित) बायोफ्यूल जो कि फसल आधारित बायोफ्यूल से अलग पानी और ज़मीन केंद्रित नहीं हैं और खाद्य उत्पादन से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं.
केंद्र सरकार को योजना संबंधी सीधे दखल से पीछे हटना चाहिए. उसका मूल संप्रभु काम-काज पर्याप्त चुनौतीपूर्ण है.
इसमें से कुछ भी आसान या सस्ता नहीं है, कम-से-कम राजनीतिक-अर्थव्यवस्था की दुविधा के कारण. मिसाल के तौर पर, सस्ते और सुरक्षित परिवहन और आवास के लिए बढ़ते, अधिकतर शहरी, मिडिल क्लास (लगभग 40 करोड़ लोग सालाना 50 हज़ार से 30 लाख रुपये के बीच कमाते हैं) की खपत की ज़रूरत को आकांक्षी वर्ग (लगभग 75 करोड़ आबादी) के सपनों के साथ संतुलित करना. या शहरों में आख़िरी मील की कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बस के साथ मेट्रो और दो शहरों के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी से आकांक्षी लोगों को फायदा होता है. 34 करोड़ निजी गाड़ियों, जिसमें हर साल 2 करोड़ की बढ़ोतरी होती है, के लिए हाइवे और रोड के निर्माण और उसे चौड़ा करने के मक़सद से कंक्रीट डालना मिडिल क्लास के लिए पसंदीदा है. इसी तरह किफायती नए घरों का निर्माण बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन के मामले में कुशल शहरी डिज़ाइन की अधिक शुरुआती लागत के बीच एक दुविधा है.
दुविधा के बीच सही पसंद चुनने से लंबे समय में उसी तरह उच्च विकास को समर्थन मिल सकता है जैसे कि बुनियादी सुधार के एजेंडे को लागू करना. केंद्र सरकार को योजना संबंधी सीधे दखल से पीछे हटना चाहिए. उसका मूल संप्रभु काम-काज पर्याप्त चुनौतीपूर्ण है. सरकार को बड़े पैमाने पर निजीकरण, निजी क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक वित्तीय समर्थन और डेटा से प्रेरित, बाज़ारों के हल्के-फुल्के रेगुलेशन के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को अधिक आर्थिक जगह देनी चाहिए. कम करना और अधिक काम सौंपना आश्चर्यजनक रूप से प्रोडक्टिव (उत्पादक) हो सकता है.
संजीव अहलूवालिया ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में एडवाइज़र हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +