-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
दुनिया के चार चोटी के नेताओं, यानी ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग और नरेन्द्र मोदी की उम्र 70 वर्ष से अधिक है और उम्मीद है कि वर्ष 2025 में ये चारों राजनेता एक बार फिर से भू-राजनीति की दिशा तय करेंगे.

किसी देश की व्यापक रणनीति का मतलब होता है कि वह अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों को पहचाने और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करें. इस ग्रांड स्ट्रैटेजी यानी व्यापक रणनीति के लिहाज़ से देखा जाए तो 2025 एक ऐसा वर्ष होगा, जिसमें दुनिया के ताक़तवर देशों और उभरते हुए राष्ट्रों के ‘लक्ष्यों’ (प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों) में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, साथ ही लक्ष्यों को हासिल करने के ‘माध्यमों’ यानी उन्हें प्राप्त करने के लिए ज़रूरी संसाधनों में लगातार तेज़ी दिखेगी. इतना ही नहीं इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के तौर-तरीक़ों को अपनाए जाने के दौरान वैश्विक स्तर पर ख़ासी उथल-पुथल भी दिखाई देगी. इसके अलावा, जिस प्रकार से आमने-सामने के युद्ध लगातार खिंचते चले जा रहे हैं और इन लड़ाइयों से आम नागरिकों को तमाम दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है, मानवीय संकट बढ़ा है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट (ICC) असहाय सा दिख रहा है, ऐसे में आने वाले साल में युद्धरत देशों के नेताओं का रवैया अगर सहयोगी नहीं होगा, तो कम से कम उनकी आक्रामकता में तो कमी ज़रूर दिखाई देगी. हालांकि, इन वैश्विक नेताओं को अपनी आक्रामकता को कम करने एवं सैन्य युद्ध के दौरान मिली नाक़ामी के बाद अपने रुतबे व गरिमा को बरक़रार रखने के लिए कुछ अलग तरह की रणनीतियां अपनाने की ज़रूरत होगी. अगले साल की पहली तिमाही में युद्ध की आग धीमी होती हुई दिखाई देगी और इसकी जगह पर नागरिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित होगा. नतीज़तन, साल की दूसरी या तीसरी तिमाही तक युद्धरत इलाक़ों में अमन-चैन की राह प्रशस्त होती दिखाई देगी. जबकि वर्ष की आखिरी तिमाही में दुनिया में एक ऐसे वातावरण को बनाने की परिकल्पना मज़बूती पकड़ेगी, जिसमें शांति, अर्थव्यवस्था और व्यापार पर मुख्य फोकस होगा.
कुल मिलाकर व्यापक रूप से यह कहना उचित होगा कि वर्ष 2025 चार ऐसे प्रमुख वैश्विक नेताओं के बीच वार्ताओं और बैठकों का साल होगा, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है. अगले साल की शुरुआत में 78 वर्षीय डोनाल्ड जे. ट्रंप का दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू होगा. अपने इस कार्यकाल में ट्रंप न केवल घरेलू स्तर पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें विकास पर ज़ोर होगा और नई नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित होगा, इसके साथ ही कम विनियमित और अधिक कारगर अर्थव्यवस्था के निर्माण पर फोकस होगा. इसके अलावा, नए ट्रंप प्रशासन द्वारा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में छिड़े युद्धों को समाप्त करने की दिशा में भी पहल की जाएगी. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्र 72 वर्ष है और वे संसाधनों एवं आधुनिक सैन्य हथियारों से संपन्न रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपना 20वां वर्ष पूरा कर रहे हैं. अगले साल यानी वर्ष 2025 में पुतिन अपने क्षेत्रीय विस्तार की मुहिम को जारी रखेंगे, लेकिन इसको लेकर काफ़ी एहतियात बरतेंगे और रणनीतिक स्तर पर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे. कहने का मतलब है कि वे कहीं अपने क़दम पीछे खींचने और कहीं डटे रहने की मिली जुली रणनीति का इस्तेमाल करेंगे और मनमुताबिक नतीज़े हासिल करने की कोशिश करेंगे. दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही सरकार और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उम्र भी 71 वर्ष हो चुकी है. देखा गया है कि उनके नेतृत्व में चीन का वैश्विक स्तर पर भू-राजनीति एवं व्यापार के क्षेत्र में आक्रामक रुख रहा है, लेकिन अगले साल लगता है कि वे अपने इस दबदबा क़ायम करने वाले रवैये में कमी लाएंगे और घरेलू अर्थव्यवस्था एवं देश के भीतर पैदा हो रहे असंतोष से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. इस सूची में चौथे वैश्विक नेता का नाम नरेन्द्र मोदी है, जिनकी उम्र 74 वर्ष की हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एवं सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री के रूप में वैश्विक स्तर पर उनकी मज़बूत छवि है. वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री मोदी विकास की ओर अग्रसर भारत की इस यात्रा को बरक़रार रखते हुए दुनिया में अपनी निष्पक्षता एवं रणनीतिक स्वतंत्रता को क़ायम रखेंगे. इसके साथ ही अपने रिश्तों का उपयोग करते हुए दुनिया की तीन महाशक्तियों यानी अमेरिका, रूस एवं चीन के बीच एक सशक्त माध्यम बनकर उन्हें वैश्विक शांति, विकास और कल्याण की राह पर ले जाने में सहायता करेंगे.
2025 एक ऐसा वर्ष होगा, जिसमें दुनिया के ताक़तवर देशों और उभरते हुए राष्ट्रों के ‘लक्ष्यों’ में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, साथ ही लक्ष्यों को हासिल करने के ‘माध्यमों’ यानी उन्हें प्राप्त करने के लिए ज़रूरी संसाधनों में लगातार तेज़ी दिखेगी.
अगले साल पूरी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी होंगी, जहां ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लेंगे, जिनका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा. इसके अलावा, इस बात की भी उम्मीद है कि नया ट्रंप प्रशासन वामपंथी नज़रिए वाली घरेलू आर्थिक नीतियों को बदलने पर ख़ास तौर पर ध्यान देगा. इतना ही नहीं, ट्रंप दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे युद्धों में अमेरिका की भूमिका को कम करने के बारे में भी फैसले लेंगे. ज़ाहिर है कि इन फैसलों का असर पूरे विश्व पर पड़ेगा. ट्रंप की दुनिया में चल रहे संघर्षों को ख़त्म करने और "अमेरिका को फिर से महान बनाने" से जुड़ी बातें भले ही असंभव, बड़बोली और लफ्फाजी जैसी लगती हों, लेकिन अपनी बातों को कहने का ट्रंप का यही तरीक़ा है. ट्रंप का यह अंदाज़ चलाकी के साथ उन्हें अपने क़दमों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है. काफ़ी समय से युद्ध लड़ रहे देश ज़ाहिर तौर पर अब थक चुके हैं और लड़ाई समाप्त करना चाहते हैं. ऐसे देशों को किसी ऐसे मध्यस्थ की तलाश है, जो उनके युद्ध को ख़त्म करने एवं शांति बहाली की पहल करें. ट्रंप उनकी इस अभिलाषा को पूरा करेंगे. युद्धों को खत्म करने की ट्रंप की काबिलियत ख़ास तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल व ईरान के बीच छिड़े छद्म युद्ध में परखी जाएगी. रूस-यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए ट्रंप को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के विस्तार को रोकने की ज़रूरत होगी, वहीं इजराइल-ईरान युद्ध के मामले में उन्हें पुचकारने और धमकाने वाली रणनीति अमल में लानी होगी. हालांकि, ऐसा करने से इन युद्धों का कोई स्थाई समाधान तो नहीं होगा, लेकिन इससे फौरी तौर पर शांति की स्थापना होगी और इससे भविष्य में राजनीतिक स्थिरता क़ायम करने के लिए रास्ता तैयार होगा.
ट्रंप अमेरिका को फिर से महान और शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी इस मुहिम को पूरा करने के लिए उन्होंने एलन मस्क एवं विवेक रामास्वामी को महत्वपूर्ण सरकारी दक्षता विभाग की ज़िम्मेदारी सौंपी है. ट्रंप ने इन दोनों को सरकारी ख़र्चे कम करने एवं निजी क्षेत्र के लिए बने नियम-क़ानूनों को कम से कम करने का काम सौंपा है. ज़ाहिर है कि इन दोनों क़दमों से अमेरिका को बहुत लाभ होगा, लेकिन साथ ही साथ इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी ज़बरदस्त असर पड़ेगा. ट्रंप के इन फैसलों के बाद धीरे-धीरे अमेरिका में बिजनेस करना सुगम होने लगेगा और दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार में विश्व भर के उद्योगपति निवेश के लिए उमड़ने लगेंगे. ऐसा होने पर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर कारोबारियों एवं निवेशकों की राह में रोड़ा बनने वाले पुराने नियम-क़ानूनों में तेज़ी के साथ बदलाव करने का दबाव बढ़ेगा. भारत जैसे देशों से अधिक दबाव यूरोपीय संघ (EU) पर पड़ेगा और ऐसा होना लाज़िमी है, क्योंकि यूरोपीय देश ऐसी किसी भी क़वायद के लिए कतई तैयार नहीं दिखते हैं. ट्रंप चीन, कनाडा और मेक्सिको पर शुल्क लगाने की भी योजना बना रहे हैं. हालांकि, भारत ऐसी किसी भी परिस्थिति के दौरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है. अगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं भी होता है, तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगी और ज़ाहिर तौर पर इससे अगले 12 महीनों में चीज़ों की क़ीमतों में इज़ाफा होगा और ब्याज दरों में भी कोई कमी नहीं होगी. गौरतलब है कि अमेरिकी नागरिक पहले ही ज़बरदस्त महंगाई से परेशान हैं और जब तक ट्रंप देशवासियों की आय बढ़ाने के साधनों को नहीं खोजते हैं, तब तक इन हालातों से देश के लोगों को रूबरू होना पड़ेगा.
हाल के महीनों में बीजिंग ने विभिन्न मुद्दों पर अपने पैर खींचे हैं और आक्रामकता में कमी की है. अगले साल चीन को तेज़ी के साथ अपने सांप-सीढ़ी के खेल को फिर से शुरू करना होगा. पिछले पांच वर्षों के दौरान चीनी मंसूबों पर नज़र डालें, तो उसने अपनी तेज़ प्रगति, कारोबार एवं जीडीपी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और ऐसा करके कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर अपना दबदबा क़ायम करने, अपनी विस्तारवादी हरकतों एवं दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व स्थापित करने को सही सबित करने की कोशिश की है. जिस प्रकार से चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उसका रियल एस्टेट का बुलबुला फूट रहा है, साथ ही दुनिया द्वारा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चीन के बजाए वियतनाम या भारत जैसे सस्ते विनिर्माण विकल्पों की ओर रुख किया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर चीन को झटका लगेगा. अगले साल चीन द्वारा ताइवान पर संभावित आक्रमण की धमकियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी और शायद तनाव अपने चरम पर पहुंचा हुआ दिखेगा. ट्रंप द्वारा पहले ही टैरिफ को लेकर कड़ा रुख जताया गया है और आने वाले महीनों में चीन के साथ अमेरिका की भू-आर्थिक तनातनी बढ़ना तय है. हालांकि, बीजिंग पहले ही अपनी पुख्ता तैयारी कर चुका है और उसने 33 अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में ज़ीरो-शून्य-टैरिफ नीति अपनाकर उन्हें अपने पाले में कर लिया है. इस नीति के ज़रिए बगैर किसी शुल्क के इन देशों में व्यापार होता है. हालांकि, यह सब ज़्यादा वक़्त तक नहीं चल पाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि वर्ष 2025 की पहली दो तिमाहियों में चीन और अमेरिका इस मुद्दे पर आमने-सामने खड़े दिखाई देंगे. चीन जहां अपने इस ख़ास तरह के वैश्वीकरण के साथ खड़ा होगा, वहीं अमेरिका डि-ग्लोबलाइजेशन के साथ यानी देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक मामलों में पारस्परिक निर्भरता के विरोध में खड़ा होगा.
अगले साल पूरी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी होंगी, जहां ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लेंगे, जिनका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा. इसके अलावा, इस बात की भी उम्मीद है कि नया ट्रंप प्रशासन वामपंथी नज़रिए वाली घरेलू आर्थिक नीतियों को बदलने पर ख़ास तौर पर ध्यान देगा.
इसके अलावा, फिलहाल चीन की दक्षिण चीन सागर में सैन्य आक्रामकता, ख़ास तौर पर फिलीपींस के साथ उसके सैन्य टकराव में कमी आएगी. पूरी दुनिया में अपना दबदबा क़ायम करने की चीन की मंशा पर फिलहाल पानी फिर जाएगा और पहले चीन जहां चाहे हमले करने लगता था, अब वह चुप्पी साध लेगा. लेकिन जिन इलाक़ों में उसने कब्ज़ा किया है, विशेष रूप से महासागरों में जहां-जहां चीन ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है, वहां वो अपनी आक्रामक गतिविधियों को अंज़ाम देता रहेगा. इसकी वजह यह है कि समुद्र में चीन के व्यापक हित छिपे हुए हैं और वह समुद्र में खनन के ज़रिए दुर्लभ खनिजों पर अपना अधिपत्य स्थापित करना चाहता है. अगर भारतीय सीमा पर चीन की मौज़ूदगी की बात की जाए, तो हाल ही में उसने अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की बात कही है. इससे पता चलता है कि भारत के साथ चीन शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, ताकि व्यापार एवं सीधी उड़ानों में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके. चीन में आए इस बदलाव के पीछे दो वजहें हैं. पहली वजह है कि आर्थिक हालातों के मद्देनज़र चीन व्यापार और निवेश के लिए भारत के साथ संबंध पुख्ता करना चाहता है, क्योंकि भारत एक बड़े बाज़ार और विनिर्माण केंद्र को तौर पर उभरा है. दूसरी वजह यह है कि चीन बाइडेन प्रशासन की जगह पर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने के बाद होने वाले राजनीतिक एवं रणनीतिक परिवर्तन से पैदा होने वाले हालातों के साथ तालमेल बैठाना चाहता है. ज़ाहिर है कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों यानी अमेरिका व भारत के बीच नज़दीकी बढ़ेगी. भारत और चीन के बीच रिश्तों में वर्ष 2024 की आख़िरी तिमाही में तनाव कम हुआ है और वर्ष 2025 में इसके और भी कम होने की उम्मीद है. अगर परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहीं और शी जिनपिंग के दिमाग में कोई नई ख़ुराफात नहीं आई तो वर्ष 2026 तक भारत व चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं, साथ ही दोनों के बीच रिश्तों की यह नई शुरुआत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने में भी कारगर साबित हो सकती है.
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बात की जाए तो रशियन फेडरेशन के रणनीतिक ग्रैंडमास्टर के तौर पर उन्होंने अपना दबदबा बरक़रार रखने के लिए उन्होंने अपनी तीन रणनीतियों को हक़ीक़त बनाया है. सबसे पहले, तो पुतिन ने यूक्रेन के 1,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घुसकर उस पर नियंत्रण कर लिया है, जहां से वे अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे. दूसरा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर यूक्रेन द्वारा अमेरिकी हथियारों की मदद से रूस के अंदरूनी इलाक़ों में हमले किए जाते हैं, तो वह परमाणु हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे. तीसरी बात, जो पुतिन ने साफ तौर पर कही है कि यूक्रेन को किसी भी सूरत में नाटो की सदस्यता नहीं दी जाए. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इन सारे घटनाक्रमों पर नज़र रखी जा रही है. अगर रूस और यूक्रेन के बीच यथास्थिति क़ायम रखी जाती है, तो फिलहाल यह युद्ध समाप्त हो सकता है, लेकिन इसमें कीव को अपना बड़ा इलाक़ा मास्को को देना पड़ेगा. पुतिन इस समाधान पर तैयार दिखाई देते हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फिलहाल इस समाधान को लेकर ज़्यादा सहज नहीं हैं. इसके अलावा, अगर यूक्रेन को युद्ध के लिए दी जाने वाली हथियारों की मदद रोक दी जाती है, या फिर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों को, जिनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, उन्हें इसका ख़ामियाजा भुगतना पड़ता है, तो फिर निश्चित रूप से यूक्रेन पर इस लड़ाई को ख़त्म करने का दबाव बढ़ जाएगा. और कुल मिलाकर कीव को शांति का यह रास्ता उसके न चाहते हुए भी मानने के लिए विवश किया जाएगा. ज़ाहिर है कि इस समाधान में शांति नहीं बल्कि नाराज़गी होगी. यह सब भले ही असहज सा लगे, लेकिन यह तय है कि यूक्रेन का 500 बिलियन डॉलर से पुनर्निर्माण करने के अमेरिकी वादे के साथ शांति स्थापना की यह कोशिश वर्ष 2025 के मध्य से आख़िरी तक परवान चढ़ने लगेगी.
यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम की बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन रूस के ख़िलाफ मार्च 2022 में लगाए गए स्विफ्ट (SWIFT) प्रतिबंधों को हटाने की मांग करेंगे. ज़ाहिर है कि यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम (UK), कनाडा और अमेरिका के कहने पर इन प्रतिबंधों को रूस पर लगाया गया था. अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से किसी देश की बैंकों को हटाना, देखा जाए तो इस व्यवस्था के सिद्धांतों और नियमों का उल्लंघन था. इस क़दम ने कहीं न कहीं पूरी दुनिया में भुगतान नेटवर्क को नियंत्रित करने वाली पश्चिमी देशों के सरकारों की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है. इस बातचीत से कहीं न कहीं स्थिति सामान्य होने का भरोसा पैदा होगा. ज़ाहिर है कि अन्य देशों को एक ऐसी वैकल्पिक भुगतान प्रणाली के बारे में सोचने और बातचीत करने की ज़रूरत है, जिस पर बीजिंग का नियंत्रण न हो. इसके अलावा, पश्चिमी क्लियरिंग हाउस द्वारा वर्तमान में ज़ब्त की गई 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रूसी संपत्तियों को मुक्त करने की मांग भी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा की जाएगी. हालांकि, पुतिन इन संपत्तियों पर मिलने वाले 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक ब्याज की मांग छोड़ सकते हैं.
आख़िर में भारत की बात की जाए, तो वर्ष 2025 में वैश्विक मुद्दों पर नई दिल्ली की भूमिका अहम बनी रहेगी. इसके साथ ही भारत न केवल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जिसकी नॉमिनल जीडीपी में अगले 12 महीनों में क़रीब 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी. साथ ही भारत भू-राजनीति और सुरक्षा के मामलों में भी एक महत्वपूर्ण देश बना रहेगा. पीएम मोदी ने पिछले पांच से सात सालों के दौरान अमेरिका और रूस दोनों के साथ रणनीतिक स्वतंत्रता के ज़रिए भरोसे की साझेदारी विकसित की है. चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध की बात हो, या फिर इजराइल-हमास-हिजबुल्लाह संघर्ष का मसला, पीएम मोदी ने दोनों ही टकरावों में शांति बहाली की कोशिश की हैं.
इन बातों को ज़मीनी स्तर पर सच साबित करना शायद इतना आसान नहीं होगा. पुतिन और बाइडेन ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और इस वजह से दोनों के बीच कोई सहज स्थिति नहीं बन पाई, वहीं पीएम मोदी ने दोनों नेताओं के साथ बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के ज़रिए बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है. मोदी के यह प्रयास वर्ष 2025 में भी जारी रहेंगे. यह अलग बात है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अपनी अलग सोच है और उनका अंदाज़ ए बयां भी जुदा है, वहीं राष्ट्रपति पुतिन अपना हर क़दम रणनीतिक लिहाज़ से सोच-समझ कर उठाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों नेताओं के बीच बातचीत को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में शांति समझौते पर पुतिन को पश्चिमी देशों के साथ सहमति जतानी होगी. जहां तक पश्चिम एशिया में इजरायल के संघर्ष की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी के कई पश्चिमी एशियाई देशों से अच्छे रिश्ते बने हुए हैं. हालांकि, इन प्रगाढ़ संबंधों में राजनीतिक या रणनीतिक मकसद हावी नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक और अस्तित्व पर मंडराने वाले ख़तरे की अहम भूमिका है. इन हालातों में पीएम मोदी के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे इस क्षेत्र में किसी भी युद्ध को अपना नैतिक समर्थन नहीं देते हुए, हालात को सामान्य करने के लिए की जाने वाली किसी भी बातचीत से जुड़ी पहलों में सक्रियता नहीं दिखाएं. मोदी को पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को अपने शांति समझौते पर विचार-विमर्श करने देना चाहिए. इस शांति स्थापना की पहल की शुरुआत फिलस्तीन में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नगरिकों की रिहाई से होनी चाहिए.
भारत की बात की जाए, तो वर्ष 2025 में वैश्विक मुद्दों पर नई दिल्ली की भूमिका अहम बनी रहेगी. इसके साथ ही भारत न केवल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जिसकी नॉमिनल जीडीपी में अगले 12 महीनों में क़रीब 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी.
इन सारे मसलों के अलावा, हिंद महासागर क्षेत्र के ज़रिए होने वाले व्यापार में, ख़ास तौर पर एनर्जी ट्रेड यानी तेल व प्राकृतिक गैस के व्यापार में नई दिल्ली की भूमिका बेहद अहम थी, आज भी है और वर्ष 2025 में भी रहेगी. आने वाले महीनों में यहां पर नई दिल्ली का वाशिंगटन के साथ रणनीतिक सहयोग सशक्त होगा. क्वाड में भारत की भागीदारी हिंद महासागर के पूर्वी किनारे पर सुरक्षा के लिहाज़ से महत्वपूर्ण साबित होगी. इसके अलावा, ट्रंप बेहतर सुरक्षा के लिए आर्थिक संबंधों पर भी नए सिरे से विचार करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं. उदाहरण के तौर पर ट्रंप ने हाल ही में मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. ऐसा करके उन्होंने इन दोनों देशों को अमेरिका में होने वाले प्रवासियों के अवैध प्रवेश को खत्म करने और उनकी सीमाओं से अमेरिका में होने वाली अवैध ड्रग्स व मादक पदार्थों की तस्करी, विशेष रूप से फ़ेंटेनाइल की तस्करी पर लगाम लगाने का स्पष्ट संकेत दिया है. अगर ये दोनों देश ट्रंप की इस बातों को मान लेते हैं, तो वह उनके सभी उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ समाप्त कर देंगे.
टैरिफ को लेकर ट्रंप के इस आक्रामक रवैये से निपटने के लिए भारत ने कमर ज़रूर कस ली है, लेकिन पीएम मोदी टैरिफ के मसले पर ट्रंप प्रशासन से बातचीत में अपनी भू-राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए. इसके साथ ही मोदी को भविष्य में अमेरिका के साथ रिश्तों को मज़बूती देने के लिए भारत की तेज़ प्रगति का लाभ उठाना चाहिए. ज़ाहिर है कि दुनिया की तमाम वैश्विक कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर नज़र लगाए हुए हैं और भारत को अगले दो या तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एवं वर्ष 2032 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक शक्ति बनते हुए देख रही हैं. ऐसे में ये वैश्विक कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहेंगी. ट्रंप और मोदी के बीच जब भी बैठक हो तो यह मुद्दा प्राथमिकता में रहे, ताकि भारत में वैश्विक कंपनियों का निवेश बढ़ सके. इस सभी बातों के अलावा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पीएम मोदी घरेलू स्तर पर श्रम, अनुपालन, भूमि और कृषि जैसे आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दें और इन मोर्चों पर सक्रियता के साथ क़दम उठाएं. ज़ाहिर है कि इनमें से श्रम और अनुपालन जैसे आर्थिक सुधारों को लागू करना फिर भी आसान है, लेकिन भूमि और कृषि जैसे मुद्दों पर बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत होगी.
निष्कर्ष
हाल के वर्षों के वैश्विक घटनाक्रमों पर नज़र डालें, तो वर्ष 2019 से 2022 के दौरान वैश्विक मुद्दों पर बीजिंग का आक्रामक रवैया हावी रहा है. वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और वर्तमान में भी यह युद्ध जारी है. वर्ष 2023 में हमास और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर आतंकवादी हमले किए और इनके जवाब में तेल अवीव ने भी हमले किए. इनके बीच टकराव की स्थिति आगे भी बनी रहेगी. जबकि वर्ष 2024 में सबने देखा कि किस प्रकार से वाशिंगटन की स्थिति कमज़ोर होती गई और कई वैश्विक मुद्दों पर उसका ढुलमुल रवैया दिखाई दिया, वहीं बीजिंग भी कई मायनों में आक्रामकता को छोड़कर अपने क़दम पीछे खींचते हुए दिखा. अगले साल यानी 2025 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद एक नया व्हाइट हाउस देखने को मिलेगा, जिसका असर हर तरफ होगा और पूरे साल दुनिया की अहम गतिविधियों को वही संचालित करेगा. ऐसे में दुनिया के रणनीतिक और आर्थिक जगत के लोगों को ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग और मोदी के बीच क्या बातचीत होती है, उनके आपसी रिश्ते किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इन सब पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत होगी.
गौतम चिकरमाने ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
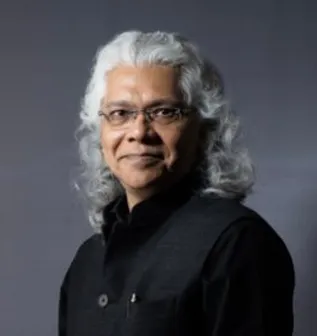
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +