-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
पुतिन की बीजिंग यात्रा रूस-चीन के बीच अब तक की सबसे मज़बूत साझेदारी को उजागर करती है. अमेरिकी दबाव के ख़िलाफ़ ऊर्जा, व्यापार और भू-राजनीति उन्हें और करीब ला रही है.

पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चीन दौरे का नतीजा रूस-चीन साझेदारी में और मज़बूती का संकेत देता है. रूसी राष्ट्रपति शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तियानजिन और जापानी सेना के ख़िलाफ़ चीन की जीत की 75वीं सालगिरह के अवसर पर तियानमेन स्क्वायर में सैन्य परेड देखने के लिए बीजिंग गए थे. ये यात्रा ऐसे समय हुई जब अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ रहा है और अमेरिका में ये चर्चा चल रही है कि जो देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ द्वितीयक (सेकेंडरी) प्रतिबंधों और टैरिफ को और सख्त किया जाए.
सैन्य परेड में पुतिन की मौजूदगी पहली बार नहीं था, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व था, ये चीन के प्रति रूस के अधिक झुकाव का संकेत देती है. परेड के इर्द-गिर्द जो दृश्य सामने आया वो ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में चीन के हितों को रूस अधिक महत्व दे रहा है.
इस बदलाव ने एक गैर-पश्चिमी क्षेत्रीय समूह के रूप में SCO के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया. सैन्य परेड में पुतिन की मौजूदगी पहली बार नहीं था, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व था, ये चीन के प्रति रूस के अधिक झुकाव का संकेत देती है. परेड के इर्द-गिर्द जो दृश्य सामने आया वो ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में चीन के हितों को रूस अधिक महत्व दे रहा है. पुतिन की इस यात्रा के दौरान 22 समझौते किए गए जिनमें ऊर्जा, विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्र शामिल हैं. पावर ऑफ साइबेरिया-2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए रूस, चीन और मंगोलिया के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी सहमति बनी. ये समझौता प्रमुख शर्तों को लेकर असहमति के कारण लंबे समय से टाला जा रहा था लेकिन इसको लेकर सफलता रूस-चीन गठजोड़ को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देती है.
90 के दशक से रूस और चीन ने राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को लगातार मज़बूत किया है. लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों के समाधान और मतभेदों के धीरे-धीरे दूर होने से उनके संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मज़बूत ज़मीन मिली. दोनों देशों ने यूरेशिया में सहयोग बढ़ाने और SCO एवं BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) जैसे अलग-अलग क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर तालमेल के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है. दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सहायक हितों को भी व्यक्त किया है और पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली व्यवस्था में सुधार की वकालत की है. साथ ही कनेक्टिविटी लिंक को मज़बूत करने और ग्लोबल साउथ (विकासशील देश) के साथ भागीदारी करने पर दोनों देशों ने समान विचार साझा किए हैं.
यूक्रेन में युद्ध और 2022 में रूस के ख़िलाफ़ लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के बाद चीन 2023 में यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर रूस का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया.
2000 के दशक में दोनों देशों के बीच सैन्य-तकनीकी साझेदारी मज़बूत हुई और चीन को हथियारों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस उभरा. 2010 के दशक में पश्चिमी देशों से दोनों देशों का विवाद बढ़ने के साथ चीन ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सुखोई-35 लड़ाकू विमान ख़रीदे. दोनों देशों ने अपने साझा सैन्य अभ्यास में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की. इसके बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में भी विस्तार हुआ. 2014 में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूस आर्कटिक और दूरदराज़ के पूर्व जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में चीन के निवेश (विशेष रूप से ऊर्जा, धातु विज्ञान और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में) को लेकर रूस अधिक इच्छुक हो गया. यूक्रेन में युद्ध और 2022 में रूस के ख़िलाफ़ लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के बाद चीन 2023 में यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर रूस का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया. चीन प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल नहीं हुआ. वास्तव में युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान रूस को महत्वपूर्ण तकनीकों के निर्यात में चीन ने प्रमुख भूमिका निभाई. युद्ध शुरू होने से पहले चीन के साथ रूस का द्विपक्षीय व्यापार 146 अरब अमेरिकी डॉलर था लेकिन तीन साल बाद 2024 में ये बढ़कर 245 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया (तालिका 1.1 देखें).
तालिका 1.1: 2014-2024 के बीच रूस-चीन द्विपक्षीय व्यापार (अमेरिकी डॉलर में)
स्रोत: रॉसस्टैट, यूनाइटेड नेशन (UN) कॉमट्रेड और चीन के कस्टम डेटाबेस से डेटा का संकलन
इस पृष्ठभूमि में 2025 में पुतिन का चीन दौरा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है. वैसे तो दोनों देशों के बीच संबंध अपने चरम पर हैं लेकिन नए सवाल भी उभर रहे हैं, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बाद या अमेरिका और रूस के बीच संभावित मेल-मिलाप की स्थिति में उनके संबंधों के भविष्य की राह को लेकर. पुतिन की अपेक्षाकृत लंबी चीन यात्रा के दौरान रूस के चंद्र धूल निगरानी उपकरण (लूनर डस्ट मॉनिटरिंग डिवाइस) को चीन के चांगई 7 अंतरिक्ष यान के साथ जोड़ने पर समझौता हुआ और बोलशॉय उसुरिस्की द्वीप को विकसित करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर सहमति बनी. हालांकि पाइपलाइन के निर्माण को लेकर MoU एक महत्वपूर्ण घटना थी. द्विपक्षीय संबंधों में ऊर्जा संबंध महत्वपूर्ण होने के साथ ऊर्जा के मामले में नए संपर्क बनाने को लेकर बातचीत द्विपक्षीय संबंधों के गहरा होने के बारे में बताती है और संकेत देती है कि यूक्रेन युद्ध के बाद के घटनाक्रम से संबंधों को अलग रखा जा रहा है.
रूस के द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात का एक प्रमुख घटक हाइड्रोकार्बन है. पूर्व की तरफ बढ़ने की रूस की योजना की पृष्ठभूमि में उसकी ऊर्जा रणनीति में बदलाव आया है जिसके तहत एशिया के बाज़ारों- विशेष रूप से चीन- को प्राथमिकता दी गई है और चीन को रूस से जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का और विस्तार करने की योजना बनाई गई है. ये पावर ऑफ साइबेरिया (POS) 1 पाइपलाइन के निर्माण में देखा जा सकता है जो पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) को पूर्वी साइबेरिया के याकुतिया से शंघाई तक पहुंचाती है. POS-1 के चालू होने के बाद रूस से चीन को PNG के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है. POS-1 की अधिकतम क्षमता 38 अरब घन मीटर (bcm) है; POS-2 पाइपलाइन इस क्षमता में 50 bcm की और बढ़ोतरी करती है और मंगोलिया के रास्ते से पश्चिमी साइबेरिया से गैस का परिवहन करेगी.
तालिका 1.2: रूस से चीन के गैस आयात की मात्रा (अरब घन मीटर में)
स्रोत: गैज़प्रॉम की वार्षिक रिपोर्ट का संकलन
इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये मेगा प्रोजेक्ट पिछले कई वर्षों से अधर में था. विशेषज्ञों ने कहा था कि दोनों देश मूल्य निर्धारण की शर्तों पर सहमत नहीं हो पा रहे थे और चीन किसी ख़ास समान (गैस) के लिए किसी एक बाज़ार पर अधिक निर्भर होने को लेकर चिंतित था. इससे पता चलता है कि चीन के लिए इस परियोजना का आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं था.
हाल का MoU मूल्य निर्धारण और तकनीकी पहलुओं पर विवरण नहीं देता, फिर भी POS-2 रूस और चीन के बीच संबंधों की सामान्य दिशा को समझने के मामले में एक प्रमुख परियोजना है.
रूस को लेकर समझौतावादी रवैया अपनाकर किसिंजर के उलट रणनीति तैयार करने के बारे में ट्रंप की बयानबाज़ी उस विचारधारा से आती है जो सोवियत संघ-चीन के संबंधों की शीत युद्ध की गतिशीलता के साथ समानताएं दिखाती है. 60 के दशक में चीन-सोवियत बंटवारे ने अगले दशक में चीन के साथ संबंध स्थापित करने में अमेरिका के लिए एक खालीपन पैदा किया. ये समानता अधूरी रह जाती है क्योंकि ये आज वैचारिक शत्रुता की अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देती है और दुनिया की राजनीति के वैश्वीकरण को अनदेखा करती है जिसने गठजोड़ में लेन-देन के तत्व को बढ़ाया है. इस प्रकार आधुनिक समय में रूस-चीन रिश्ते कनिष्ठ साझेदार/वरिष्ठ साझेदार के संबंध के बारे में कम है बल्कि ये भू-राजनीतिक बदलाव के द्वारा लाए गए मेल-जोल से प्रेरित है.
रूस यूरेशिया में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जो विदेश नीति को लेकर अलग-अलग दस्तावेज़ों (जैसे कि 2023 की रूसी संघ की विदेश नीति की अवधारणा) में दिखता है. संरचनात्मक असमानताओं को देखते हुए भी इस बात की संभावना नहीं है कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए रूस, चीन के साथ अपने रिश्ते को कमज़ोर करेगा, विशेष रूप से एक अनिश्चित ट्रंप प्रशासन की पृष्ठभूमि में.
इसके बावजूद अमेरिका के साथ संबंध सुधारने में रूस दिलचस्पी रखता है. संबंध सुधरने से सहयोग के रास्ते खुल सकते हैं जैसा कि पिछले दिनों अमेरिका-रूस वार्ता में दिखा था. इसके अलावा रूस ने अपने खनिज और ऊर्जा क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश का स्वागत किया था. प्रतिबंधों पर राहत मांगने की संभावना के अलावा अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार के पीछे रूस का तर्क है चीन के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी में कुछ हद तक संतुलन लाना.
पिछले अक्टूबर में कज़ान में चीन के साथ शुरू हुई बातचीत के आधार पर वैश्विक बहुध्रुवीयता को मज़बूती देने के बैनर के तहत रूस-चीन सहयोग के और गहरा होने का भारत के लिए भी अर्थ है जो व्यापक रूस से स्वागत योग्य है. अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भारत की समान लेकिन विरोधाभासी शिकायतें हैं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की वकालत करना और गैर-पश्चिमी राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग के माध्यम से व्यापार को मज़बूत करना.
भारत-रूस संबंधों की राह में अड़चन पैदा करने के उद्देश्य के साथ भारत के ख़िलाफ़ पिछले दिनों लगाए गए टैरिफ ने दोनों देशों के रिश्तों को और मज़बूत किया है. SCO जैसे संगठनों में रूस और चीन के साथ तालमेल को लेकर भारत अधिक इच्छुक हो गया है
भारत-रूस संबंधों की राह में अड़चन पैदा करने के उद्देश्य के साथ भारत के ख़िलाफ़ पिछले दिनों लगाए गए टैरिफ ने दोनों देशों के रिश्तों को और मज़बूत किया है. SCO जैसे संगठनों में रूस और चीन के साथ तालमेल को लेकर भारत अधिक इच्छुक हो गया है जबकि अतीत में भारत के आकलन में SCO का महत्व कम होता जा रहा था. हालांकि सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ कोई समाधान नहीं होने के कारण भारत, रूस-चीन साझेदारी (विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्र में) के संभावित रूप से गहरा होने को लेकर चिंतित है. रूस के आकलन में चीन का बढ़ता महत्व भारत की तुलना में चीन को लाभ पहुंचा सकता है, विशेष रूप से डिफेंस सिस्टम और प्लैटफॉर्म की डिलीवरी के मामले में. यहां तक कि रूस के द्वारा हथियारों की डिलीवरी में तेज़ी लाने के आश्वासन और भारत के साथ भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराने के बावजूद भारत, रूस-चीन साझेदारी के घटनाक्रम पर काफी हद तक सतर्क नज़र रखे हुए है.
रजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में जूनियर फेलो हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
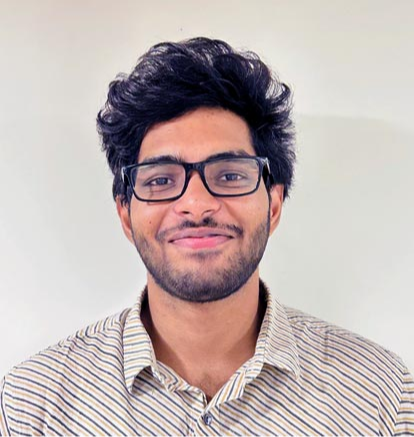
Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Junior Fellow with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia’s foreign policy and economy, and India-Russia relations. Siddharth is a ...
Read More +