-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
ट्रांसअटलांटिक तनावों एवं सैन्य आपूर्ति में ख़ामी के चलते भारत के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत डिफेंस इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र यूरोप के लिए आदर्श सहयोगी बनने की स्थिति में है.

Image Source: Getty
शीत युद्ध के बाद के दौर में यूरोप को व्यापार के मामले में प्रीवीलेज्ड स्टेटस् अर्थात विशेषाधिकारपूर्ण दर्ज़ा मिला हुआ था. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स (US) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका इसे बदलना चाहता है. वह यह तर्क देता है कि इस दर्ज़े की वजह से US के आर्थिक हितों को क्षति पहुंच रही है. ट्रंप के ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) अभियान के तहत उन्होंने यूरोपियन देशों पर रेसीप्रोकल यानी पारस्परिक टैरिफ्स् लागू किए हैं. ऐसा करते हुए वे इन देशों के US के मुकाबले लाभदायक व्यापार संतुलन की भरपाई करना चाहते हैं.
विवाद का एक और मुद्दा है. यह मुद्दा यूरोपियन सिक्योरिटी में आ रहे रणनीतिक अंतर अर्थात बदलाव से जुड़ा है. यह मुद्दा US की उस धारणा से पैदा हुआ है, जिसके तहत US का मानना है कि यूरोप अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) की सुरक्षा गारंटी पर यथोचित ख़र्च नहीं कर रहा है.
हालिया उकसाने वाले घटनाक्रमों के कारण तनाव में इज़ाफ़ा हुआ है. इन घटनाक्रमों में US के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा म्युनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस में दिए गए विवादास्पद बयान और यूरोप में धूर दक्षिणपंथी आंदोलनों, विशेषत: AfD (अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी) और ब्रिटेन के रिफॉर्म यूनाइटेड किंगडम, को एलन मस्क की ओर से लोकप्रिय प्लेटफॉर्म यानी मंच X के माध्यम से दिया जाने वाला समर्थन शामिल है.
ट्रांसअटलांटिक साझेदारी ने इसके पहले भी बिखराव की स्थिति देखी है. मसलन 1966 में फ्रांस ने NATO के सैन्य कमांड से बाहर निकलने का फ़ैसला किया था. या फिर 1970 और 1980 के दौर में व्यापार को लेकर तनाव देखा गया था.
ट्रांसअटलांटिक साझेदारी ने इसके पहले भी बिखराव की स्थिति देखी है. मसलन 1966 में फ्रांस ने NATO के सैन्य कमांड से बाहर निकलने का फ़ैसला किया था. या फिर 1970 और 1980 के दौर में व्यापार को लेकर तनाव देखा गया था. लेकिन इनमें से कोई भी तनाव वर्तमान तनाव जैसा तीखा नहीं था. इसकी शुरुआत ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी. उस वक़्त 2019 में NATO के शिखर सम्मेलन में ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच सार्वजनिक रूप से बहस हो गई थी. ट्रंप के दोनों कार्यकालों के बीच बाइडेन प्रशासन के दौरान यूरोपियन यूनियन (EU) के सहयोगियों ने अस्थायी रूप से इस तनाव को भूला दिया था. लेकिन अब ट्रंप की US के राष्ट्रपति के रूप में वापसी और उनके द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे सैन्य समर्थन को वापस लेने के फ़ैसले ने इस तनाव को इतना बढ़ा दिया है कि अब इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. NATO के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी-जनरल यानी सहायक महासचिव एंटोनियो मिसिरोली के अनुसार US तथा यूरोप के बीच मौजूदा तनाव लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को लेकर देखा जा रहा है. यह तनाव सारी समस्याओं का संगम कहा जाएगा, जिसकी वजह से अटलांटिक में सभी ओर उभरती सुरक्षा चुनौतियों को लेकर गहरा विभाजन होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है.
वर्तमान भूराजनीतिक चुनौतियां देखते हुए EU अपनी सुरक्षा और रक्षा नीतियों को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है. वह इन नीतियों को वर्सेल्स डिक्लेरेशन तथा 2022 के स्ट्रेटेजिक कंपास के उद्देश्यों से संरेखित करना चाहता है. 2022 के स्ट्रेटेजिक कंपास को 2030 तक EU की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने वाले ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जाता है. इस स्ट्रेटेजिक कंपास में कार्रवाई के चार प्रमुख मुद्दे रेखांकित किए गए हैं : एक्ट यानी कार्रवाई, सिक्योर यानी सुरक्षित, इन्वेस्ट यानी निवेश और पार्टनर अर्थात साझेदार (यूरोपियन यूनियन एक्सटर्नल एक्शन 2022). एक्ट के तहत EU अपने क्राइसिस यानी संकट के दौरान रिस्पोंस अर्थात प्रतिक्रिया देने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी (RCD) यानी तत्काल तैनाती क्षमता खड़ी करना चाहता है. इसके साथ ही वह इसके कमांड-एंड-कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी निर्देश तथा नियंत्रण ढांचे को मजबूत करना चाहता है. सिक्योर' के तहत 'प्री एम्प्टीव थ्रेट असेसमेंट' यानी ख़तरे को पहले ही भांप लेने पर बल दिया गया है. इसके साथ ही इंटेलीजेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करते हुए साइबर रक्षा को पुख़्ता करना है. 'इंवेस्ट' के तहत कटिंग एज टेक्नोलॉजी में निवेश करते हुए गैर यूरोपीय स्त्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए रणनीतिक ख़ामी को दूर किया जाएगा. और अंततः 'पार्टनर' के तहत EU अपने महत्वपूर्ण साझेदारों NATO तथा UN के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है. US ने यूरोपीय देशों से अपने रक्षा ख़र्च में इज़ाफ़ा करते हुए यूरोप की सुरक्षा में ज़्यादा योगदान देने को कहा है. फ्रांस लंबे समय से EU से यूरोप के लिए स्वायत्त रक्षा एवं सुरक्षा नीति विकसित करने की गुहार लगाता रहा है. लेकिन इस दिशा में पहले किए गए प्रयास आम सहमति के अभाव में विफ़ल रहे हैं. अब आम सहमति तो बन रही है लेकिन यह रक्षा एवं सुरक्षा के मामले में नहीं हो पा रही है. यह बात यूरोप की चिंता का कारण भी नहीं है. यूरोप की चिंता इस बात से बढ़ रही है कि उसके पास रक्षा उत्पादन क्षमता की कमी है. इसका कारण यह है कि वह लंबे समय से सुरक्षा के लिए US की सेना तथा सैन्य हथियारों के लिए US के रक्षा उद्योग पर निर्भर रहा है.
यूरोप की संचित GDP 18.5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से अधिक है, जबकि उसका डेट-टू-GDP अनुपात लगभग 81.6 फ़ीसदी है. मौलिक रूप से यूरोप को अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए अपनी सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने रक्षा ख़र्च को अपनी GDP के 3.5 फ़ीसदी तक बढ़ाने में कोई वित्तीय परेशानी नहीं होगी.
यूरोप की संचित GDP 18.5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से अधिक है, जबकि उसका डेट-टू-GDP अनुपात लगभग 81.6 फ़ीसदी है. मौलिक रूप से यूरोप को अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए अपनी सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने रक्षा ख़र्च को अपनी GDP के 3.5 फ़ीसदी तक बढ़ाने में कोई वित्तीय परेशानी नहीं होगी. लेकिन उसका रक्षा उद्योग अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहा है. उदाहरण के लिए फ्रेंच एयरोस्पेस कंपनी, डसॉल्ट के पास यूरोप, मध्यपूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशिया के विभिन्न देशों से लगभग 400 हवाई जहाजों की आपूर्ति करने का ऑर्डर है. इस कंपनी के पास फ्रांस में इतने विमान बनाने की उत्पादन क्षमता ही नहीं है. इसी प्रकार जर्मनी स्थित ऑटोमोटिव एवं हथियार निर्माता कंपनी राइनमेटल AG के पास सालाना 60,000–70,000 आर्टिलरी और अन्य शेल्स यानी गोले बनाने की क्षमता ही मौजूद है, जबकि आवश्यकता सालाना 1.1 मिलियन शेल की है. KNDS ग्रुप की नेक्सटर सिस्टम्स S. A. तथा क्रॉस-माफी/माफेई वेगमैन GmbH एंड Co. KG के पास 2024 के अंत तक 15.7 बिलियन यूरो के ऑर्डर का बैकलॉग पड़ा है. सीमित क्षमताओं के कारण यूरोप के अन्य रक्षा उत्पादक भी इसी तरह प्रभावित हैं.
यूरोपियन देश उभरते एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने रक्षा उद्योग का विस्तार करते हुए इसे आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में EU के रक्षा उद्योग से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला में भारत अहम भूमिका अदा कर सकता है. EU तथा भारत एक रक्षा एवं सुरक्षा संधि की संभावना पर विचार कर रहे हैं. इस संधि को पर्मानंट स्ट्रक्चर्ड को-ऑपरेशन (PESCO) यानी स्थायी संरचित सुरक्षा सहयोग भी कहा जाता है. यह ठीक उसी तरह होगी जैसी EU का जापान और दक्षिण कोरिया के साथ समझौता है. PESCO ढांचे के तहत EU सदस्य देश भारत के साथ संयुक्त रूप से साझा रक्षा क्षमताओं में निवेश और विकास भागीदार बन सकते हैं, ताकि सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल रेडीनेस अर्थात युद्ध के लिए तैयारी की स्थिति में इज़ाफ़ा किया जा सके. भारत को इसकी वजह से जहां आधुनिक तकनीकों तक पहुंच स्थापित करने में आसानी होगी, वहीं यूरोपियन देशों को भारत की मजबूत और प्रतिस्पर्धी उत्पादन सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा. लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि इन उत्पादकों को भारत में अपनी निर्माण इकाइयों की स्थापना करनी होगी.
EU ने अपने गोला-बारुद के स्टॉक में वृद्धि करने के लिए 500 बिलियन यूरो का प्रावधान किया है. भारत इससे भी लाभ उठा सकता है. बारुद गोले का निर्माण करने वाली भारतीय आयुध निर्माणियों के पास युद्ध के दौरान मांग में होने वाली तेजी के हिसाब से गोला-बारुद की आपूर्ति करने की क्षमता मौजूद है.
2014 में भारत ने अपने यहां ‘मेक इन इंडिया’ की पहल की. इस पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना है. इस पहल के तहत रक्षा विनिर्माण एक अहम उद्देश्य है. पिछले कुछ वर्षों में अनेक निजी खिलाड़ियों अर्थात उद्योगों ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया है. इनमें से रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, टाटा ग्रुप, भारत फोर्ज, अडानी समूह और महिंद्रा जैसे कुछ प्रमुख उद्योग समूह शामिल हैं. पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान स्वीडिश आर्म्स मैन्यूफैक्चरर, साब ने हरियाणा के झज्जर में अपनी विनिर्माण यूनिट स्थापित की है. वहां यह कंपनी कार्ल-गुस्ताफ एम4 हथियार का उत्पादन करेगी. L&T MBDA मिसाइल सिस्टम्स लिमिटेड, जो कोयंबटूर स्थित लार्सन एंड टुब्रो के साथ संयुक्त उपक्रम है, ने विभिन्न मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया है.
EU ने अपने गोला-बारुद के स्टॉक में वृद्धि करने के लिए 500 बिलियन यूरो का प्रावधान किया है. भारत इससे भी लाभ उठा सकता है. बारुद गोले का निर्माण करने वाली भारतीय आयुध निर्माणियों के पास युद्ध के दौरान मांग में होने वाली तेजी के हिसाब से गोला-बारुद की आपूर्ति करने की क्षमता मौजूद है. इन आयुध निर्माणियों ने अपनी विनिर्माण क्षमता को अत्याधुनिक बना लिया है और अब यहां हाई-टेक एम्युनिशन यानी गोला-बारुद का उत्पादन किया जा सकता है. इस हाई-टेक एम्युनिशन का उपयोग EU की सेना को आपूर्ति करते हुए उसकी क्षमता में इज़ाफ़ा किया जा सकता है. कुछ EU सदस्यों ने पहले से ही इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) अर्थात सार्वनजिक उपक्रमों को गोला-बारुद का ऑर्डर दे दिया है. निजी गोला-बारुद निर्माताओं के साथ संयुक्त उत्पादन किए जाने की संभावना भी बनी हुई है. क्योंकि कुछ विनिर्माताओं ने पहले ही EU कंपनियों के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है.
भारत को एक अग्रणी जहाज निर्माता बनाने की दिशा में भी भारत सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को एक मल्टी-बिलियन डॉलर कैश इंजेक्शन दिया है अर्थात इस कार्य के लिए बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया है. सरकार ने PSU शिपयार्ड्स को फंक्शनल और फाइनांशियल ऑटोनॉमी अर्थात कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्ता देने की योजना भी प्रस्तावित की है. रक्षा मंत्रालय में वर्तमान में मौजूद भारी-भरकम अफसरशाही की वजह से यह स्वायत्ता फिलहाल नदारद है. अपने हालिया 1 फरवरी 2025 के बजट में सरकार ने मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड (MDF) के लिए 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया है ताकि देश के मैरिटाइम अर्थता समुद्री क्षेत्र को सहायता की जा सके. इसके सहयोग से भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी शिपबिल्डिंग हब के रूप उभरने का अवसर मिल सकेगा.
डसॉल्ट इंडिया की ओर से ग्रेटर नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल (MRO) की स्थापना करने की प्रक्रिया चल रही है. इसकी क्षमता को बढ़ाकर उसका उपयोग EU देशों के लड़ाकू विमानों को मेंटेनेंस सपोर्ट देने के लिए किया जा सकता है. डसॉल्ट इंडिया और रिलायंस संयुक्त रूप से नागपुर में हवाई जहाज के पूर्जों का निर्माण करने पर काम कर रहे है. सफ्रान ने पहले ही हैदराबाद में एयरो-इंजिन यूनिट खोल दिया है. इसी तरह एयरबस के साथ समन्वय करते हुए टाटा समूह ने भी अपने वडोदरा, गुजरात की फैक्ट्री में C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू कर दिया है. इन यूनिट्स की क्षमता में विस्तार करते हुए EU देशों के लिए राफेल की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है.
भारत के पास एक मजबूत इंजीनियरिंग टैलेंट पुल, स्थापित रक्षा उत्पादन बुनियादी ढांचा, शोध एवं विकास पर ध्यान देने वाला एक विशाल रक्षा बजट और स्वदेशीकरण मौजूद है. ये बातें उसे जटिल सैन्य उपकरणों का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने और संभवत: इनका अन्य देशों को निर्यात करने की अनुमति देती हैं. घरेलू तथा विदेशी निजी खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDIs) समेत अन्य सुविधाएं देकर सरकारी नीतियां इन्हें प्रोत्साहित करने का काम कर सकती हैं. ऊपर की गई चर्चा से यह समीक्षा की जा सकती है कि भारत ने एक अपेक्षाकृत मज़बूत रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर लिया है, जिसके पास निर्यात को बढ़ावा देने की सरप्लस यानी अतिरिक्त क्षमता मौजूद है. इसके अलावा वह ‘मेक इन इंडिया’ के लिए विदेशी तकनीक को भी आत्मसात करने की क्षमता रखता है.
भारत ने एक अपेक्षाकृत मज़बूत रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर लिया है, जिसके पास निर्यात को बढ़ावा देने की सरप्लस यानी अतिरिक्त क्षमता मौजूद है. इसके अलावा वह ‘मेक इन इंडिया’ के लिए विदेशी तकनीक को भी आत्मसात करने की क्षमता रखता है.
लेकिन एक सवाल फिर भी रह ही जाता है और वह यह है कि क्या भारत दोनों हाथों से इस अवसर का लाभ उठाने को तैयार है? एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर भारत को EU के लिए निर्माण करने, अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने, संयुक्त विनिर्माण करने और तकनीकी विकास समन्वय स्थापित करने के अवसरों पर ध्यान देना चाहिए. यह बात सच है कि EU के भीतर भी सब कुछ यूरोप में विनिर्मित करने की मांग उठ रही है. लेकिन वहां की तात्कालिकता को देखते हुए तुरंत ऐसा करना संभव नहीं दिखाई देता. अत: सक्रिय नीतियों, कार्रवाई और चतुर कूटनीति के साथ भारत एक रक्षा उपकरण निर्यातक के रूप में उभर सकता है. ऐसा हुआ तो वह अल्पावधि में यूरोप को री-आर्म यानी पुन: हथियारों से लैस करने और लंबी अवधि में वह आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनकर उभर सकता है. इसके लिए भारत को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक छोटा, लेकिन दक्ष सेट-अप स्थापित करने पर विचार करना होगा. एक ऐसा सेट-अप जो सैन्य अभियान मोड में काम करते हुए इस मौके को भारत के लिए लाभ के अवसर के रूप में परिवर्तित कर सके.
(कर्नल दीपक कुमार, एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और भूराजनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
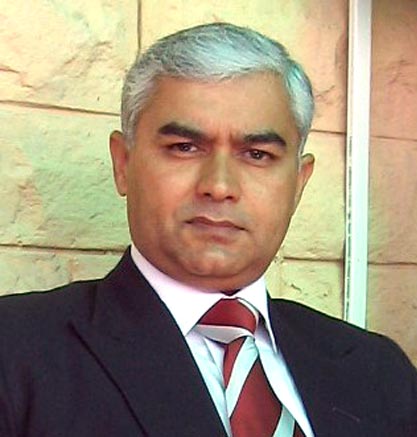
Colonel Deepak Kumar is an Army Veteran with more than three decades of command and staff experience in various terrains of India. His academic qualifications ...
Read More +