-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1991 में जहां भारत के सामने एक संकट से उबरने की चुनौती थी. वहीं, 2021 में भारत के सामने समृद्धि की अपेक्षाएं पूरी करने की चुनौती है.

89.1 करोड़ आबादी वाली कोई अर्थव्यवस्था कैसे यू-टर्न लेती है? 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने जिन बदलावों की शुरुआत की, उनके पीछे एक सड़ी हुई सियासत की गलती हुई व्यवस्था छुपी हुई थी. अपने लिए मुनाफ़ा तलाशने वाले इंस्पेक्टर थे. गहरी जड़ें जमाए बैठे कारोबारी थे. ये सब के सब अपने अपने हितों के एक ‘सिस्टम’ की डोर से बंधे हुए थे. इनकी पहचान वो बॉम्बे क्लब था, जिसे छिन्न भिन्न करना ज़रूरी था. इसके दूसरी तरफ़ विकास की नई राजनीति थी, जिसकी अगुवाई नए कारोबारी कर रहे थे. इन दोनों धुरियों के बीच में अवसरों का अथाह समंदर था. 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी बयान के हर अनुच्छेद से अगर लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों का फ़ायदा ज़रूर जुड़ा हुआ था, और जो पहले के ‘सब चलता है’ के नज़रिए वाले आलस्य के दलदल में फंसे हुए थे. इनमें से कई के पास पैसे की ताक़त थी- ये सिर्फ़ कुछ गिने चुने उद्योगपति भर नहीं थे, बल्कि इनमें अफ़सरशाही और राजनेता यानी ‘सिस्टम’ भी शामिल थे. आख़िर भारत ने इस बदलाव का सामना कैसे किया? ये लेख आर्थिक सुधार को आठ खिड़कियों से देखता है, और अर्थव्यवस्था के कई गतिशील हिस्सों और उनके आपसी संबंध के ज़रिए पिछले तीस वर्षों की पड़ताल करते हुए आने वाले दौर की भविष्यवाणी करता है.
हर अहम सुधार के साथ साथ उनके विरोध की प्रासंगिकता हमेशा बनी रही है. तीन दशक पहले बॉम्बे क्लब के विरोध का स्वरूप वित्तीय था. जब 1993 में गहरी जड़ें जमाए बैठे कुछ कारोबारियों के समूह ने बजाज आटो के प्रमुख राहुल बजाज के नेतृत्व में औद्योगिक नीति का विरोध किया था, तो उनको कोई राजनीतिक समर्थन नहीं मिला और ये विरोध ठंडा पड़ गया. उसके बाद के दौर में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के तूफ़ान में राहुल बजाज तो हार गए, लेकिन बजाज ऑटो जीत गया. वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही काम कृषि क्षेत्र के साथ कर रहे हैं, जो नरसिम्हा राव ने उद्योगों के साथ किया था. कृषि क्षेत्र 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा बनने से रह गया था. तीन कृषि क़ानून पारित किए जा चुके हैं. लेकिन, इस बार के सुधारों का जो अमीर किसान और बिचौलिए इन कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं, उनके पास न केवल पैसा है बल्कि उनके पीछे राजनीतिक समर्थन भी है. इन सुधारों से रातों-रात किसान नेता राकेश टिकैत की तो राजनीतिक हार होगी. लेकिन टिकैत जैसे लाखों किसानों की जीत होगी.
वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही काम कृषि क्षेत्र के साथ कर रहे हैं, जो नरसिम्हा राव ने उद्योगों के साथ किया था.
पीवी नरसिम्हा राव से लेकर नरेंद्र मोदी तक, पांच प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व वाली छह सरकारों ने नौ कार्यकालों में अपने राजनीतिक विचारों को बदला. ये बदलाव नियंत्रण से आज़ादी की ओर बढ़ने का है. आर्थिक सुधारों को अलग अलग राजनीतिक दलों से मिला समर्थन, देश की उन आर्थिक मांगों की नुमाइंदगी करता है, जिसकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों ने की है. इसमें कोई दो राय नहीं कि इस धरती पर राजनेता ही सबसे ज़्यादा बदलने वाले जीव होते हैं, जो ख़ुद को बदले हुए हालात के हिसाब से तुरंत ढाल लेते हैं. वो तुरंत ये राजनीतिक सबक़ सीख लेते हैं कि उनके वोटर और समर्थक क्या चाहते हैं, और वक़्त की बदलती धार के मुताबिक़ अपना रुख़ भी बदल लेते हैं. राजीव गांधी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शुरुआत की थी. अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मज़बूती दी. मनमोहन सिंह ने उसकी ताक़त को और बढ़ाया और अब नरेंद्र मोदी बड़ी संख्या में ये काम कर रहे हैं. इस दौरान हर नेता ने वही किया, जो जनता चाहती थी. राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजमार्ग, गांवों और क़स्बों को जोड़ने वाली सड़कें. आने वाले समय में यही दौर तमाम औद्योगिक और भौगोलिक क्षेत्रों में चलता रहेगा.
राजीव गांधी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शुरुआत की थी. अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मज़बूती दी. मनमोहन सिंह ने उसकी ताक़त को और बढ़ाया और अब नरेंद्र मोदी बड़ी संख्या में ये काम कर रहे हैं.
‘समाजवाद’ शब्द को 1976 में आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था. ये विडम्बना ही है कि संविधान के ‘मूलभूत संरचना’ की स्वघोषित धारणा देने वाली देश की न्यायपालिका ने इसे संविधान के मूल ढांचे से छेड़-छाड़ नहीं माना. संविधान की प्रस्तावना में इस छेड़खानी ने भारत को शुरुआत से अब तक ‘समाजवादी समाज’ के सिद्धांत से बांध रखा है. प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का जोड़ा जाना एक चक्र है. कार्यपालिका के नियंत्रण वाले योजना आयोग से लेकर, कार्यपालिका के नियंत्रण वाली 1956 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव, कार्यपालिका के नियंत्रण वाले केंद्रीय बजट से लेकर कार्यपालिका की अगुवाई में लेकिन, विधायिका के नियंत्रण वाली संसद, जिसे हर दौर की न्यायपालिका का आशीर्वाद मिलता रहा है. पीवी नरसिम्हा राव ने इस सड़ी गली व्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की थी. लेकिन, आज भी इस व्यवस्था की ऑक्टोपस जैसी भुजाएं नीतियां बनाने वालों के दिमाग़ों को जकड़े हुए हैं. भले ही आज भी पूंजीवाद भारत की नीतियां बनाने वालों की नज़र में हाशिए पर पड़ा हुआ है. लेकिन, सच तो ये है कि भारत एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहां पर दो अलग अलग विचारधाराएं समाजवाद और पूंजीवाद एक दूसरे से ताल में ताल मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं देश की जनता टकटकी लगाए समृद्धि के भरत नाट्यम का इंतज़ार कर रही है. बाज़ार ने नागरिकों को काफ़ी मूल्य दिए हैं. उन्हें निवेश से लेकर संचार और सफर और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं. फिर भी, हम जब भी संविधान के पन्ने पलटते हैं, तो ये पुराना पड़ चुका ‘समाजवाद’ का विचार हमें घूरता हुआ दिखाई देता है, जो हमारी भारतीयता को चुनौती देता है. हमारी समृद्धि की संभावनाओं को सीमित करता है. इसे बदलने और अब इसे भारत की आर्थिक आकांक्षाओं के अनुसार ढालने की ज़रूरत है
सच तो ये है कि भारत एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहां पर दो अलग अलग विचारधाराएं समाजवाद और पूंजीवाद एक दूसरे से ताल में ताल मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं देश की जनता टकटकी लगाए समृद्धि के भरत नाट्यम का इंतज़ार कर रही है.
1991 में बड़े आर्थिक सुधारों के ज़रिए कारोबार की व्यवस्था में बदलाव और उसके बाद धीरे धीरे किए गए सुधारों के चुनाव को लेकर बहस आज 2021 में भी जारी है. अब तक दोनों ही तरीक़ों ने अपने ढंग से काम किया है. 1991 में औद्योगिक नीति पर बयान ने आर्थिक नीति की नए सिरे से बुनियाद रखी; इसने कारोबार की शुरुआत करने, विकास करने या उसमें विविधता लाने में सरकार की दादागीरी को ख़त्म किया; लेकिन, उसके बाद जो आर्थिक सुधार किए गए हैं, वो कभी तेज़ गति से तो कभी धीरे धीरे किए गए. प्रत्यक्ष आयकर में तमाम सरकारों द्वारा धीरे धीरे की गई कमी हो या फिर बारी बारी से अलग अलग उद्योगों के लिए नियामक संस्थाओं का गठन (पूंजी बाज़ार के नियामक की स्थापना पीवी नरसिम्हा राव ने की. बीमा और पेंशन के नियामक की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की और रियल एस्टेट रेग्यूलेटर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बना) धीरे धीरे ही हुआ और इसके नतीजे मिले जुले ही रहे हैं. गुड्स ऐंड सर्विसेज़ टैक्स हों या तीनों कृषि क़ानून, ये दोनों ही धीरे धीरे सुधार करने की दशकों चली प्रक्रिया की ही उपज हैं, जो अब क़ानून की शक्ल में हमारे सामने हैं. वहीं, सुधारों की रफ़्तार के दूसरे छोर पर मनमोहन सिंह की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना है, जिसने लागू होने पर करोड़ों नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का कवच दिया. वहीं, नरेंद्र मोदी की जन धन योजना ने अब तक बैंकिंग से महरूम रहे देश के 30 करोड़ नागरिकों को रातों रात बैंक खातों की सुविधा दी. ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा रास्ता बेहतर है. अर्थशास्त्री चाहेंगे कि बड़े सुधार एक झटके में हों. लेकिन राजनीतिक ज़रूरत ये है कि लोकतांत्रिक संवाद के ज़रिए धीरे धीरे सुधारों के लिए माहौल तैयार किया जाए. इसका एक पहलू ये भी है कि थोड़ा थोड़ा करके होने वाले सुधारों पर अंत तक बहस ही होती रह सकती है. आज 21वीं सदी के भारत को तेज़ी से लिए जाने वाले नीतिगत फ़ैसलों की ज़रूरत है. इस समय तो ये रफ़्तार दूर का ख़्वाब लगती है. लेकिन, महामारी और इससे पैदा हुए आर्थिक संकट के चलते हो सकता है कि भारतीय राजनीति विकास को नई धार दे सके.
ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा रास्ता बेहतर है. अर्थशास्त्री चाहेंगे कि बड़े सुधार एक झटके में हों. लेकिन राजनीतिक ज़रूरत ये है कि लोकतांत्रिक संवाद के ज़रिए धीरे धीरे सुधारों के लिए माहौल तैयार किया जाए.
1991 से लेकर 2021 तक आर्थिक सुधारों की कहानी का मुख्य किरदार केंद्र सरकार ही रही है. 1991 में विनिवेश की शुरुआत (पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में) और 2003 में पारित वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन क़ानून (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में) से लेकर 1997 में 10-20-30 प्रतिशत के तीन स्तरीय आयकर व्यवस्था (देवेगौड़ा सरकार के दौरान) जो हाल के दिनों तक चलती रही थी और 2016 में बना इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में). ये सभी सुधार केंद्र सरकार द्वारा किए गए. लेकिन, अब ज़रूरत ये है कि सुधारों का ये कारवां राज्यों की तरफ़ बढ़े. या फिर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सुधार को आगे ले जाएं. जैसे कि मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया जीएसटी एक ऐसा सुधार है, जिसे लागू होने में लगभग चार दशक लग गए. पर, केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान के कारण हो या इससे बचने के लिए, ये क़ानून केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल से ही लागू किया जा सकता है. ये केंद्र और राज्यों के बीच सुधारों को लेकर सहयोग का एक मॉडल बन सकता है. क्योंकि, जीएसटी को पारित तो केंद्र सरकार ने कराया. लेकिन, मंडी के स्तर पर इसे लागू करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है. आगे चलकर सुधारों का केंद्र राज्य सरकार ही बनेंगे और ऐसा होना भी चाहिए, और जैसा कि हमने मौजूदा महामारी के दौरान देखा भी जब मध्य प्रदेश ने अपने यहां कारोबार करना काफ़ी आसान बनाया. वहीं तेलंगाना ने उद्यमियों को अपने यहां आकर्षित करने में पूरी ताक़त झोंक रखी है. भारत को 10 ख़रब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के चार राज्यों- महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक- को इंडोनेशिया के बराबर यानी लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बननना होगा. गुजरात और पश्चिम बंगाल को भी इनके ठीक पीछे पीछे चलना होगा. इन राज्यों में सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था की ताक़त बढ़ेगी.
भारत आज जहां पर है, वहां तक कभी नहीं पहुंच पाता अगर उसने अपने संस्थानों को नहीं बदला होता. एक बड़ा संस्थागत बदलाव तो ये था कि सरकारी नियंत्रण से हटकर ये ज़िम्मेदारी स्वतंत्र नियामक संस्थाओं के हाथ में चली गई, जिनकी नियुक्ति सरकार करती है. 1991 से 2021 के बीच भारत में सात नई नियामक संस्थाओं का गठन किया गया है- 1992 में सिक्योरिटीज़ ऐंड एक्सचेंज़ बोर्ड ऑफ़ इंडिया, 1997 में टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, 1999 में इन्श्योरेंस रेग्यूलेटरी डेवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया; 2002 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया; 2003 में पेंशन फंड रेग्यूलेटरी ऐंड डेवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया. एक और बड़े संस्थान जीएसटी काउंसिल का गठन केंद्र और राज्यों के स्तर पर किया गया है और राज्य स्तर पर रियल एस्टेट रेग्यूलेटर्स स्थापित किए गए हैं. आगे चलकर भारत को अपने संस्थागत ढांचे के बारे में सोचना होगा. जैसे कि ग्राहकों की ज़रूरतों पर आधारित संस्थान बनाने होंगे, न कि उद्योग विशेष के आधार पर. बीमा, पेंशन और म्युचुअल फंड के लिए अलग फंड मैनेजर के बजाय एक पेशेवर एसेट मैनेजर बनाना. इसी तरह, अब जबकि राज्य सरकारें अपने यहां सुधार करेंगी, तो पूंजी कहीं भी जाने के लिए आज़ाद होगी. इसके चलते राज्य सरकारों को ऐसे बौद्धिक संस्थान चाहिए होंगे, जो अपने यहां के संसाधनों, नियमों और बाज़ार की ख़ूबियां निवेशकों के सामने अच्छे से रख सकें. इससे उनकी मुक़ाबला कर पाने की क्षमता बेहतर होगी. हमें ये तो नहीं पता कि इससे राज्य किस ओर जाएंगे. लेकिन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त की गई आर्थिक सलाहकार परिषद बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया क़दम है. जिन दो और बड़े बदलावों की ज़रूरत है, वो हैं प्रशासनिक सुधार जिनसे उद्यमियों को हर दिन की सरकारी खींचतान से निजात मिले और न्यायिक सुधार जिससे कारोबारी विवादों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके. बाधा बनने के बजाय नए संस्थानों को उचित माहौल बनाने वाला बनाना होगा, जिससे वो नए भारत की रफ़्तार और उम्मीदों को पूरा कर सकें.
भारत आज जहां पर है, वहां तक कभी नहीं पहुंच पाता अगर उसने अपने संस्थानों को नहीं बदला होता.
21वीं सदी ने चीन नाम के एक दुष्ट देश का उदय होते देखा है. अब तक वो ख़ामोशी से अपनी आर्थिक ताक़त बढ़ा रहा था और सरकार के क़दमों से सब कुछ नियंत्रित करने ताक़त जुटा रहा था. उसका इरादा शुरू से ही आक्रामक तरीक़े से दुनिया पर दादागीरी जमाना था. इसीलिए अब भारत को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से तरक़्क़ी करनी होगी. अब जबकि चीन की आक्रामक महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाई जा रही है. एक के बाद एक क्षेत्र और देश ज़रूरी क़दम उठा रहे हैं. तो, दुनिया को नए बाज़ार, नए ग्राहकों, नई मैन्यूफैक्चरिंग और नई आपूर्ति श्रृंखलाओं की ज़रूरत है. सभ्य देशों के समूहों के बीच नए सिरे से गठबंधन बन रहे हैं. भौगोलिक रूप से भी (भारत सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है) और राजनीतिक रूप से भी (चीन की तानाशाही व्यवस्था के लोकतांत्रिक जवाब के रूप में) भारत विकास के इस अवसर को लपकने की सबसे अच्छी स्थिति में है और इसके साथ साथ वो सुरक्षा, शांति और व्यापार के तोहफ़े भी दुनिया को दे सकता है. लेकिन, इन सबके लिए ज़रूरी शर्त है एक ताक़तवर अर्थव्यवस्था की. सभी पूर्वानुमान ये कहते हैं कि भारत अगले दर्जन भर वर्षों में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. लेकिन, उस मंज़िल तक पहुंचने में कुछ वक़्त लगेगा और जो एक विचार जो भारत को उस मंज़िल की ओर बढ़ा सकता है, वो है और आर्थिक सुधार. इसमें कोई दो राय नहीं कि नई दुनिया भारत के बिना नहीं बन सकती, क्योंकि वो जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है. लेकिन, एक सच ये भी है कि सिर्फ़ सोचने भर से हम वहां नहीं पहुंच सकेंगे- इसके लिए सुधार करने होंगे.
पिछले तीस वर्षों ने सुधारों में भी बड़ा बदलाव होते देखा है. पहले वो कुछ सीमाओं और हिचक के साथ हो रहे थे, तो अब पूरे विश्वास और मर्ज़ी से किए जा रहे है. 1991 में नरसिम्हा राव ने जो आर्थिक सुधार किए उनकी बड़ी वजह ये थी कि भारत के सामने भुगतान का संकट और अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौतियां थीं. भारत ने सोना बेचने जैसे सारे विकल्प आज़मा लिए थे और कई दूसरे विकल्प सरकार के सामने विचाराधीन थे. ऐसे में उस वक़्त की सरकार ने न सिर्फ़ सुधारों के ज़रिए देश को एक बड़े संकट से उबारा बल्कि उसके सामने तरक़्क़ी का मौक़ा भी पेश किया. राव के बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी सुधारों का सिलसिला जारी रखा. लेकिन, सभी सफल नहीं रहे. हालांकि, सुधारों के लिए एक संकट और उसका सकारात्मक नतीजा निकलना एक ज़रूरी शर्त थी. लेकिन, ये पर्याप्त शर्त नहीं थी. सुधारों के लिए तब भी राजनीतिक स्थिरता चाहिए थी और आज भी ये सबसे ज़रूरी है. पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने गठबंधन सरकारों चलाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी प्रबंधन किया. मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गठबंधन का कोई दबाव नहीं है और वो पूरी इच्छाशक्ति से सुधार कर रहे हैं. निश्चित रूप से राज्यों के चुनाव केंद्र के फ़ैसलों पर असर डाल रहे हैं. लेकिन, कुल मिलाकर मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सुधारों को ज़्यादा आर्थिक आत्मविश्वास और राजनीतिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ाया है. हालांकि, चुनौतियों का स्वरूप अब बदल गया है. 1991 में जहां भारत के सामने एक संकट से उबरने की चुनौती थी. वहीं, 2021 में भारत के सामने समृद्धि की अपेक्षाएं पूरी करने की चुनौती है. अब धमकियों की जगह प्रोत्साहन ने ले ली है.
सभी पूर्वानुमान ये कहते हैं कि भारत अगले दर्जन भर वर्षों में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. लेकिन, उस मंज़िल तक पहुंचने में कुछ वक़्त लगेगा और जो एक विचार जो भारत को उस मंज़िल की ओर बढ़ा सकता है, वो है और आर्थिक सुधार.
अगर आप इन आठ खिड़कियों को एक साथ रखकर देखें, तो जो तस्वीर बनती है वो न सिर्फ़ हर नज़रिए, जियोपॉलिटिक्स के इतिहास से लेकर विचारधारा की रफ़्तार तक, की पेचीदगी दिखाती है, बल्कि इनके ज़रिए हर बार तस्वीर के सब रंग आपस में मिलकर एक नया रूप धर लेने का गुण भी जताते हैं. ये सब कुछ एक साथ होता है. ये कुछ कुछ ब्राउन के विचारों, घटनाओं और स्थिरता के एक साथ अलग अलग रफ़्तार से अलग दिशाओं में ख़ुद से ही गतिशील होने की अटूट ख़ूबी को भी दिखाती हैं, जो नीतियों पर असर डालती रही हैं. चीन के उभार का मतलब, मध्य युग के एक साम्राज्य का उदय है. नए संस्थानों का धीमी गति से आकार लेना समाज में बदलाव की लहर को पीछे धकेल रहा है. आज भले ही एक नाकाम विचारधारा के रूप में समाजवाद हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन भारत के संविधान के हर अनुच्छेद की प्रस्तावना वहीं से शुरू होती है. शायद लोकतंत्रों का यही मिज़ाज होता है- बदलाव के लिए किसी इंसान की अधीरता, किसी और की नज़र में आलस्य होती है. भारत के आर्थिक सुधार इन दोनों धुरियों के बीच खड़े थे और आज भी वैसे ही हैं. अब ये सुधार किस तरह से एक के बाद एक आने वाले चुनावों और एक एक कर उठाए जाने वाले नीतिगत क़दमों के चलते हुए राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच तालमेल बिठाकर 21वीं सदी के मध्य तक भारत को 20 हज़ार डॉलर प्रति व्यक्ति आय वाला देश बनाएंगे, यही बात सुधारों का स्वरूप तय करेगी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
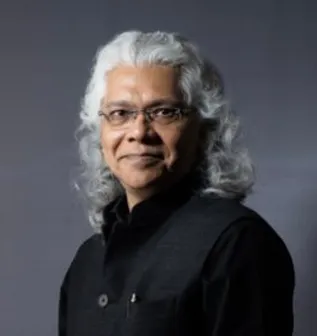
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +