-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) की पहल के ज़रिए लोबिटो कॉरिडोर के अंतर्गत व्यापक आर्थिक सेक्टर का जो विकास किया जा रहा है, उसका मकसद अफ्रीकी देशों में चीनी प्रभुत्व का मुक़ाबला करना है.

अफ्रीकी देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC), तंजानिया और जाम्बिया में कोबाल्ट, तांबा एवं लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का अकूत भंडार मौज़ूद है, लेकिन अभी तक आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक इन महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है. इन्हीं दुर्लभ खनिजों की वजह से हाल के दिनों में यह तीनों अफ्रीकी देश महाशक्तियों की होड़ के नए मंच के रूप में सामने आए हैं. देखा जाए तो लोबिटो कॉरिडोर (मानचित्र 1 देखें) की परिकल्पना अमेरिका की पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) पहल के अंतर्गत एक नया बुनियादी ढांचा विकसित करने के परियोजना के रूप में की गई है. तीन देशों को आपस में जोड़ने वाला लोबिटो कॉरिडोर तेज़ी के साथ इन देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) के समक्ष एक ताक़तवर विरोध के तौर पर उभर रहा है.
मानचित्र 1: दि लोबिटो कॉरिडोर
स्रोत : दि व्हाइट हाउस
लोबिटो कॉरिडोर मध्य अफ्रीका में स्थित है और इसके अंतर्गत जाम्बिया एवं DRC में मौज़ूद महत्वपूर्ण खनिज खदानों को अंगोला में लोबिटो पोर्ट से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया है. यह परियोजना हरित ऊर्जा विकास, टिकाऊ खनन, ऊर्जा भंडारण से लेकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल तक में निवेश को आगे बढ़ाती है. देखा जाए तो PGII के लोबिटो कॉरिडोर के तहत आर्थिक क्षेत्रों की जो भी व्यापक श्रृंखला है, उसका मकसद इस पूरे इलाक़े में चीनी दबदबे के विरुद्ध अपनी दमदार मौज़ूदगी दर्ज़ कराना है और उसका मुक़ाबला है.
इस समय दुनिया में जो संघर्ष चल रहे हैं, उन्होंने आम नागरिकों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के कभी न ख़त्म होने वाले दुष्चक्र के ख़तरे में डाल दिया है, जिसे हम हिंसा और सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता के तौर पर देख रहे हैं.
ज़ाहिर है कि इस मुक़ाबले में बीजिंग कहीं न कहीं दूसरे पक्ष से मज़बूत स्थिति में है और उससे काफ़ी आगे है. इसकी वजह यह है कि चीन ने उपरोक्त तीनों देशों में परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित कर लिया है, इसके साथ ही वो 'खनिजों के लिए बुनियादी ढांचे' से संबंधित समझौते कर रहा है. जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी सिर्फ़ चीन के क़दमों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं.
चीन ने BRI के ज़रिए पिछले एक दशक से अधिक समय से दुनिया भर में दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति को अपनाया है. चीनी की इस रणनीति को अफ्रीका में भारी सफलता मिली है और उसे अपने अनुकूल नतीज़े भी मिले हैं. वर्तमान में DRC में औद्योगिक कोबाल्ट और तांबे की लगभग 70 प्रतिशत खनन परियोजनाओं पर बीजिंग का नियंत्रण है. इसके अतिरिक्त चीन ने वर्ष 2018-23 के बीच मध्य अफ्रीका के कई दूसरे देशों जैसे कि ज़िम्बाब्वे, अंगोला और नामीबिया में लिथियम खनन से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. इसी प्रकार से ज़िम्बाब्वे में बीजिंग ने चीनी सरकार के स्वामित्व वाली लिथियम खदान के निकट में स्थित लिथियम-प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है. उल्लेखनीय है कि अंगोला में ग्रीन ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी दुर्लभ खनिजों का भंडार है और हरित परिवर्तन के लिए आवश्यक 51 महत्वपूर्ण खनिजों में से 32 खनिज, वहां प्रचुर मात्रा में मौज़ूद हैं. ये ऐसे दुर्लभ खनिज हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों, पवनचक्की जेनरेटर्स समेत विकसित चिप्स एवं सुपर कंप्यूटर के CPUs जैसी अत्यधिक अहम प्रौद्योगिकियों में किया जाता है. बीजिंग द्वारा अंगोला से ऊर्जा आयात के रूप में मुख्य रूप से पेट्रोलियम का आयात किया जाता है, जबकि है, चीन वहां दुर्लभ खनिजों के खनन से संबंधित समझौतों के लिए भी हाथ-पांव मार रहा है.
तालिका 1: मध्य अफ्रीका में चीन का BRI निवेश (2013-23)
स्रोत: UNCTAD निवेश रिपोर्ट; जाम्बिया, DRC और अंगोला के वित्त मंत्रालयों के बाह्य ऋण विभाग; AidData
अफ्रीकी देशों में चीनी निवेश से संबंधित तालिका-1 पर नज़र डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि बीजिंग ने मध्य अफ्रीका में तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक सेक्टरों में लगभग 22.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. ख़ास बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में चीन द्वारा जितना भी ऋण दिया गया है और निवेश किया गया है, उसका 80 प्रति हिस्सा अन्य वित्तीय प्रवाह प्रणाली के ज़रिए निवेश किया गया है. ज़ाहिर है कि वित्तीय निवेश का यह चीनी तंत्र अमेरिका की अगुवाई वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से चीन के इस नकदी प्रवाह और निवेश के बारे में जांच-पड़ताल करना बेहद मुश्किल हो जाता है. अफ्रीकी देशों में अपने इन्हीं निवेशों के बल पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन का दबदबा बेहद मज़बूत हो गया है. यही वजह है कि चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और निजी कंपनियों का वैश्विक स्तर पर खनिज प्रसंस्करण से जुड़े 85 प्रतिशत उद्योग पर प्रभुत्व है. इतना ही नहीं वर्तमान में तमाम प्रकार के दुर्लभ खनिजों के जो भी सक्रिय वैश्विक भंडार हैं, उनके 65 प्रतिशत से अधिक पर इन चीनी कंपनियों की या तो अच्छी-ख़ासी हिस्सेदारी है या फिर पूरा नियंत्रण है.
अफ्रीकी देशों में अपने इन्हीं निवेशों के बल पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन का दबदबा बेहद मज़बूत हो गया है. यही वजह है कि चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और निजी कंपनियों का वैश्विक स्तर पर खनिज प्रसंस्करण से जुड़े 85 प्रतिशत उद्योग पर प्रभुत्व है.
सरसरी नज़र से देखें, तो मध्य अफ्रीकी देशों के साथ बीजिंग के आर्थिक सहयोग का जो मॉडल है, वो पारस्परिक तौर पर लाभप्रद दिखाई देता है, यानी इससे दोनों पक्षों को फायदा हो रहा है. वर्ष 2006 में जब चीन ने अंगोला के साथ 'तेल के बदले बुनियादी ढांचा' (infrastructure for oil) समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके एवज में चीन ने पूरे अंगोला में इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, तभी से अंगोला, जाम्बिया और DRC ने चीन को भारी मात्रा में अपने प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात किया है. हालांकि, चीन के इस निवेश मॉडल का गहराई के साथ गहन विश्लेषण किया जाए, तो सामने आता है कि चीनी निवेश के लिए यह सब कोई आसान नहीं रहा है.
मध्य अफ्रीका के इन कम विकसित देशों में चीनी निवेश किसी संजीवनी से कम नहीं है. अपने घरेलू निवेशों को वित्तपोषित करने के लिए इन देशों की राष्ट्रीय सरकारें पेट्रोलियम या खनिज आपूर्ति गारंटी के माध्यम से मिलने वाले चीनी ऋण का इस्तेमाल करती हैं. इसका तात्पर्य यह है कि इन तीन देशों में ऋण के रूप में जो भी चीनी निवेश किया गया है, उसका पुनर्भुगतान कहीं न कहीं उनके प्राकृतिक संसाधनों के साथ गहराई से जुड़ा है. ज़ाहिर है कि प्राकृतिक संसाधनों की क़ीमत वैश्विक मांग पर निर्भर होती है और मांग के अनुसार इसके मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है, ऐसी परिस्थितियों में इन देशों को बीजिंग से ऋण भुगतान के पुनर्गठन का आग्रह करने के लिए मज़बूर होना पड़ता है. इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016 से 2023 के बीच चीनी सरकार की स्वामित्व वाली बैंकों ने DRC, जाम्बिया, ज़िम्बाब्वे और अंगोला में 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तेल और खनिज आपूर्ति से जुड़े ऋणों पर या तो दोबारा से बातचीत की है, या फिर उन्हें बट्टे-खाते में डाल दिया है या कहा जाए कि बैड लोन की श्रेणी में डाल दिया है.
लोबिटो कॉरिडोर के माध्यम से अमेरिका अब मध्य अफ्रीका में चीन के दबदबे का सामना करने के लिए अपनी पुख़्ता तैयारी कर रहा है. लोबिटो कॉरिडोर, जिसकी PGII के तहत कल्पना की गई है और जो कि G7 द्वारा शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम है, वो DRC, जाम्बिया और अंगोला में इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी को विकसित करने का भरोसा दिलाता है.
तालिका 2: लोबिटो कॉरिडोर के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाएं (2022-23)
स्रोत: यूएस पीजीआईआई फैक्टशीट, G7 हिरोशिमा प्रगति रिपोर्ट, G7 PGII पर जापान की फैक्टशीट
तालिका 2 के मुताबिक़ स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों देशों में G7 ने दो ग्रीन रेलवे कॉरिडोर यानी कि लोबिटो अटलांटिक रेलवे एवं और जाम्बिया-लोबिटो रेलवे (मानचित्र-1 देखें) के निर्माण के लिए क़रीब 2.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया है. इन ग्रीन रेलवे कॉरिडोर्स को डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से जोड़ा जाएगा. हरित रेलवे गलियारों के हिस्से के रूप में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (EU) की निजी कंपनियां अंगोला में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 500 MW की संयुक्त क्षमता वाली दो सौर परियोजनाओं का निर्माण करेंगी. ज़ाहिर है कि अमेरिका ने DRC और जाम्बिया में एयरटेल अफ्रीका के परिचालन को आगे बढ़ाने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सुविधा को भी बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं, अमेरिका, यूरोपीय संघ और इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले देशों बीच जो समझौता हुआ है, उसमें खनन, ऊर्जा अन्वेषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास और परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार जैसे अहम आर्थिक क्षेत्रों में आगे भी आर्थिक सहयोग की बात कही गई है.
हाल ही में आयोजित हुए महत्वपूर्ण ग्लोबल गेटवे (GG) फोरम और जी20 नई दिल्ली समिट के दौरान, G7 भागीदारों ने रेलवे लाइन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन हेतु कॉरिडोर के भागीदार देशों के साथ विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे.
हाल ही में आयोजित हुए महत्वपूर्ण ग्लोबल गेटवे (GG) फोरम और जी20 नई दिल्ली समिट के दौरान, G7 भागीदारों ने रेलवे लाइन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन हेतु कॉरिडोर के भागीदार देशों के साथ विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. इसके अतिरिक्त, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने तीनों कॉरिडोर साझीदार देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है. ग्लोबल गेटवे फोरम में DRC में प्रस्तावित रेलवे लाइन के शुरुआती स्थल यानी कामोआ-काकुला क्षेत्र (Kamoa-Kakula region) से निकलने वाले तांबे और कोबाल्ट के निर्यात के संबंध में लोबिटो कॉरिडोर विकसित करने वाली अफ्रीकी कंपनियों के संघ और G7 भागीदारों के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए.
मध्य अफ्रीका में अपनी पहुंच स्थापित करने के लिए अमेरिका ने भी सकारात्मक आर्थिक मज़बूती के मॉडल को अपनाया है, लेकिन देखा जाए तो उसके द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो कूटनीति अपनाई जा रही है, वह G7 के नज़रिए से कुछ अलग है. दृष्टिकोण में यह मतभेद उसके वित्तपोषण के मॉडल, ऋण वापसी के तरीक़ों, स्थिरता पर ध्यान देने, क्षमता बढ़ाने के उपायों को अमल में लाने और कामगारों के संबंधित मसलों में साफ तौर पर दिखाई देता है. PGII निवेश इन देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है. ज़ाहिर है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप और अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा इन देशों को जो पहले से कम-क्रेडिट की सुविधा प्रदान की गई है, उसके साथ PGII के निजी भागीदारों, जैसे कि सिटी ग्रुप द्वारा प्रदान किए गए नए क्रेडिट को जोड़ा गया है, इससे भी इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को गति मिली है. G7 की पहल इन देशों को विशेष वित्तीय उत्पाद भी प्रदान करती है, जैसे कि लंबी अवधि का स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण और दीर्घकालिक मुद्रा एवं ब्याज दर को बढ़ने से रोकना. उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के वित्तीय उत्पाद विकासशील देशों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निवेश हासिल करने वाले देशों में छोटे एवं मध्यम दर्ज़े के उद्यमों के विकास को बढ़ाने में मददगार हैं. मध्य अफ्रीकी देशों में G7 ने जिस प्रकार से स्थानीय कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की है, वो भी बहुत अहम है और कहीं न कहीं बीजिंग के मॉडल के ठीक उलट है. बीजिंग ने इन तीनों देशों में जो मॉडल अपनाया है, उसमें ऋणदाता और परियोजना का निर्माण करने वाले ठेकेदार (और कई मामलों में वहां कार्यरत कामगार भी) दोनों ही चीन के थे. इसके अलावा, G7 द्वारा जो भी निवेश किया जाता है, वो आधिकारिक विकास सहायता (ODA) प्रवाह के ज़रिए होता है, जिससे बहुपक्षीय बैंकों के बराबर रियायती ब्याज दरों की सुविधा मिलती है. ऐसा होने से पहले से ही ऋण के संकट से जूझ रही सरकारों पर वित्तीय बोझ कम हो जाता है. वास्तविकता यह है कि सामाजिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे आर्थिक क्षेत्रों में PGII से होने वाले नकदी प्रवाह को आधिकारिक अनुदान के रूप में प्रस्तावित किया गया है. जहां तक आधिकारिक विकास सहायता यानी ODA की बात है, अगर इसकी तुलना चीन के अन्य वित्तीय प्रवाह यानी OOF से की जाए तो, इन रियायती ऋणों में लंबी छूट अवधि के साथ ही ऋण भुगतान के लिए भी अधिक समय होता है. इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि चीन की सरकारी खनन कंपनियों द्वारा इस इलाक़े में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खनन मानकों एवं श्रम क़ानूनों का खुलेआम उल्लंघन भी किया जा रहा है.
ऐसा पहली बार नहीं है कि पश्चिमी देश अफ्रीका को उसके आर्थिक संकट से उबारने में सहायता करने के लिए एक उम्मीदों से भरा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम सामने लेकर आए हैं. पिछले दशकों में भी अफ्रीकी महाद्वीप में वाशिंगटन कॉन्सेंसस जैसी पहल सामने आई थी. हालांकि यह पहल परवान नहीं चढ़ पाई थी, लेकिन इसके ज़रिए अफ्रीका की व्यापक आर्थिक नीति और दिशा को पुनर्गठित करने का प्रयास किया था. हक़ीकत यह थी कि इसकी वजह से पहले से ही संकट में घिरे अफ्रीकी देशों की वित्तीय हालत और डगमगा गई थी. इस बार G7 द्वारा काफ़ी एहतियात बरती जा रही है और एक नए दृष्टिकोण के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है. इसके साथ ही G7 द्वारा इस बार चीन के ग़लत क़दमों से भी सबक लिया गया है. देखा जाए, तो PGII वित्तपोषण और निवेश में स्थिरता एवं पारदर्शिता, क्षमता निर्माण और स्थानीय कंपनियों एवं लोगों की व्यापक स्तर पर भागीदारी पर ध्यान देने के साथ ही चीन की बुनियादी ढांचा कूटनीति में जो भी कमज़ोर कड़ियां हैं, उन्हें रणनीतिक रूप से निशाना बना रहा है. चीन की तरह पश्चिमी देशों के लिए भी, दुर्लभ खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की होड़ में जीत हासिल करने और भविष्य को ताक़त देने के लिए मध्य अफ्रीकी देशों में अपनी दमदार मौज़ूदगी दर्ज़ कराना बेहद महत्वपूर्ण है. अब देखने वाली बात यह है कि G7 और उसके सहयोगी देश PGII पहल के अंतर्गत किए गए वादों को कितनी कुशलता से पूरा कर पाते हैं.
पृथ्वी गुप्ता ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम में जूनियर फेलो के रूप में कार्यरत हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
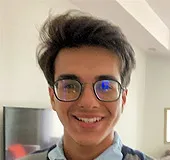
Prithvi Gupta is a Junior Fellow with the Observer Research Foundation’s Strategic Studies Programme. Prithvi works out of ORF’s Mumbai centre, and his research focuses ...
Read More +