-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारत और ब्राज़ील अपने संबंधों को मज़बूत कर रहे हैं, साथ ही व्यापार, जलवायु सहयोग और रणनीतिक मेल-जोल के माध्यम से ग्लोबल साउथ में बड़ी भूमिका निभाने पर उनकी नज़र है.

जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राज़ील यात्रा का समय अलग-अलग कारणों से बेहद महत्वपूर्ण था. मुख्य रूप से, एक और लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना को शामिल करते हुए इस यात्रा ने ग्लोबल साउथ (विकासशील देश) के प्रमुख देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के भारत के इरादे का संकेत दिया जो विकासशील देशों के साथ सहयोग को और आगे बढ़ाने में उसके व्यापक हितों के साथ मेल खाता है. दूसरा, इस यात्रा का महत्व बाद में और ज़्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि अमेरिका ने ब्राज़ील पर 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की जिसकी वजह से ब्राज़ील ने संबंधों में विविधता लाने की इच्छा जताई है. अंत में, भारत और ब्राज़ील ज़्यादातर वैश्विक मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं. इनमें वैश्विक संस्थानों में सबसे ज़रूरी सुधार लाना भी शामिल है. दुनिया भर में संघर्षों में बढ़ोतरी, अस्थिरता और आम सहमति में बिखराव के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तनाव को देखते हुए शायद ये भारत-ब्राज़ील के बीच संबंधों को मज़बूत करने का सबसे अच्छा समय है. ये दौरा अपने आप में उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उठाया गया सही कदम था. परंपरा के अनुसार पीएम मोदी ने अपने ब्राज़ील आगमन पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और भारत की विदेश नीति में सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों के महत्व को रेखांकित किया.
दुनिया भर में संघर्षों में बढ़ोतरी, अस्थिरता और आम सहमति में बिखराव के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तनाव को देखते हुए शायद ये भारत-ब्राज़ील के बीच संबंधों को मज़बूत करने का सबसे अच्छा समय है.
शिखर सम्मेलन और पीएम मोदी की यात्रा ब्राज़ील और भारत के हितों में बढ़ते मेल-जोल को उजागर करती हैं. उनका जुड़ाव ग्लोबल साउथ के महत्व और इसके सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता का प्रमाण है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम- “अधिक समावेशी और स्थिर शासन व्यवस्था के लिए विकासशील देशों के बीच सहयोग को मज़बूत करना”- ने ज़्यादा न्यायसंगत और प्रतिनिधि वाली वैश्विक व्यवस्था की भावना को व्यक्त किया. इसके अलावा, ब्राज़ील के सामने आई हाल की चुनौतियों को देखते हुए सहयोगात्मक ग्लोबल साउथ का दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रासंगिक है. ब्राज़ील ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है. चूंकि ब्राज़ील अपने व्यापार एवं निवेश के साझेदारों में विविधता लाना चाहता है, ऐसे में भारत एक आशाजनक समकक्ष के रूप में उभरता है.
भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और ब्राज़ील महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और संरचनात्मक समानता साझा करते हैं. दोनों देशों के बीच संपर्क की शुरुआत सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगाली साम्राज्य के विदेश में विस्तार के साथ हुई थी. इसकी वजह से ब्राज़ील और भारत- दोनों देशों की अच्छी बातों का विस्तार एक-दूसरे के महादेश में हुआ. दोनों देश अपेक्षाकृत रूप से नए लोकतंत्र, बहुसांस्कृतिक और आकार में महादेश के बराबर हैं जहां विशाल घरेलू बाज़ार मौजूद हैं. भारत और ब्राज़ील- दोनों देश सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौर से गुज़रे जो 20वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की व्यापारिक वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली को संतुलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है. उनके औद्योगीकरण ने फार्मास्यूटिकल्स एवं एयरोस्पेस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ाया, अच्छी तरह से संगठित क्षेत्रीय इनोवेशन प्रणाली, विशेष रूप से कृषि में, को विकसित किया और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की स्थापना की जिससे भविष्य में सहयोग के लिए मज़बूत नींव तैयार हुई.
हालांकि ब्राज़ील के मामले में ये प्रगति सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के साथ मौजूद है. विश्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, ब्राज़ील की लगभग 28 प्रतिशत जनसंख्या ग़रीबी रेखा के नीचे गुज़र-बसर करती है. पैमाने अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों देशों के शहरों को बुनियादी ढांचे से जुड़े बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उत्पादकता में सुधार और पारिवारिक खेती के लिए ज़मीन की उपलब्धता की तत्काल आवश्यकता है. ये क्षेत्र ब्राज़ील और भारत के बीच विकास से जुड़े साझा लक्ष्यों पर आधारित सहयोग के लिए आशाजनक बुनियाद प्रस्तुत करते हैं. इस तरह का तालमेल व्यापक रूप से ग्लोबल साउथ की भागीदारी के लिए एक मानक के रूप में काम कर सकता है. प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने अगले दशक में भारत-ब्राज़ील सहयोग को और मज़बूत करने के लिए छह स्तंभों को रेखांकित किया: रक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की रफ्तार में कमी, डिजिटलाइजेशन और उभरती तकनीकें एवं रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी. नए सिरे से इस भागीदारी के हिस्से के रूप में पीएम मोदी की हाल की यात्रा के दौरान 12 समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें आतंकवाद एवं संगठित अपराध से मुकाबला, डिजिटल समाधानों का आदान-प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों पर तालमेल, कृषि अनुसंधान सहयोग, गुप्त सूचना की रक्षा और बौद्धिक संपदा सहयोग पर ज्ञापन शामिल हैं.
जिस समय बहुपक्षवाद को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस समय एक अधिक समावेशी और संतुलित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए विकासशील देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करना आवश्यक है.
व्यापार और निवेश से जुड़े लक्ष्य भी समान रूप से महत्वाकांक्षी थे. मर्कोसुर (अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे) और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते का विस्तार करने के अलावा दोनों देशों का उद्देश्य अपने एयरोस्पेस उद्योगों में संबंधों को मज़बूत करना है. द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान समय के 12 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक समझौते तैयार करना शामिल है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा उपकरण, खनन, खनिज दोहन और तेल एवं गैस उद्योगों में वैल्यू चेन के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
भारत-ब्राज़ील के बीच गठबंधन में ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान रखा गया है. वैसे तो दोनों देशों के बीच जैव ऊर्जा और जैव ईंधन के क्षेत्र में पहले से ही कुछ सहयोग हो रहा है लेकिन इस दौरे ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस) में भागीदारी को जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया. ज़ोर इस बात पर है कि द्विपक्षीय संबंधों में स्वच्छ, सतत, न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए तुरंत आवश्यकता को और अनदेखा नहीं किया जा सकता है. ये अलग-अलग कम उत्सर्जन वाले स्रोतों, ईंधनों और तकनीकों का उपयोग करते हुए तकनीकी रूप से तटस्थ और एकीकृत दृष्टिकोण की वकालत करता है. ब्राज़ील ने कॉप 30 (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) से ठीक पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड की शुरुआत भी की थी. नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए जो ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु सामर्थ्य को दिए गए महत्व को उजागर करता है. प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और ब्राज़ील ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग में अनूठी क्षमताएं और नेतृत्व लाते हैं. उनकी पहल- विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल इनोवेशन और कृषि अनुसंधान में- न केवल घरेलू प्राथमिकताएं दर्शाती हैं बल्कि जलवायु सामर्थ्य के संबंध में विकासशील देशों में विकास के मापनीय मॉडल के रूप में भी काम कर सकती हैं.
ब्रिक्स समूह मौजूदा समय में विश्व की 48 प्रतिशत जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. जैसे-जैसे ब्रिक्स की अर्थव्यवस्थाएं पारस्परिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, वैसे-वैसे वो संगठन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण क्षमता का निर्माण करती हैं. भारत और ब्राज़ील जैसे बड़े साझेदारों के नेतृत्व में समूह के भीतर अधिक व्यापार इस संगठन के आंतरिक व्यापार के प्रवाह को संतुलित करने और चीन केंद्रित व्यापार के मंचों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है. ध्यान देने की बात है कि भारत और ब्राज़ील के बीच राजनीतिक तनाव की अनुपस्थिति उन्हें एक अधिक अनुरूप और विविधतापूर्ण ब्रिक्स का आर्थिक परिदृश्य तैयार करने में महत्वपूर्ण किरदार के रूप में प्रस्तुत करती है.
जिस समय बहुपक्षवाद को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस समय एक अधिक समावेशी और संतुलित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए विकासशील देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करना आवश्यक है. ये हासिल करने के लिए इन देशों को ज़्यादा नज़दीक होकर बातचीत करनी होगी और द्विपक्षीय आदान-प्रदान एवं रणनीतिक सहयोग को व्यापक करना होगा. जिन क्षेत्रों में ब्राज़ील और भारत के साझा हित हैं, वहां सहयोग को मज़बूत करने के लिए साझेदारी स्थापित करके और व्यवस्था को संस्थागत रूप देकर दोनों देश अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और मोदी एवं लूला के बीच द्विपक्षीय बैठक ने विकासशील देशों में सहयोग को मज़बूत करने के लिए एक मंच तैयार किया है और अराजकता के मौजूदा समय में स्थिरता का आभास दिया है.
मार्को एंटोनियो रोचा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपिनास के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं.

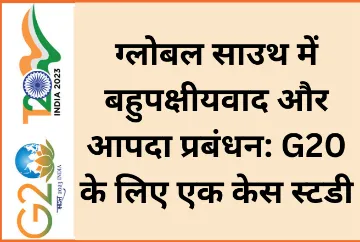
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Marco Antonio Rocha is an Associate Professor at the Institute of Economics at the University of Campinas (IE/Unicamp; Brazil), a Researcher at the Centre of ...
Read More +