-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
ये बात एकदम शीशे की तरह साफ़ है कि महामारी की दूसरी वेव या लहर ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है. शुरुआती अनुमानों के अनुसार, पहली वेव की तुलना में दूसरी लहर 1.7 गुना अधिक तेज़ है.
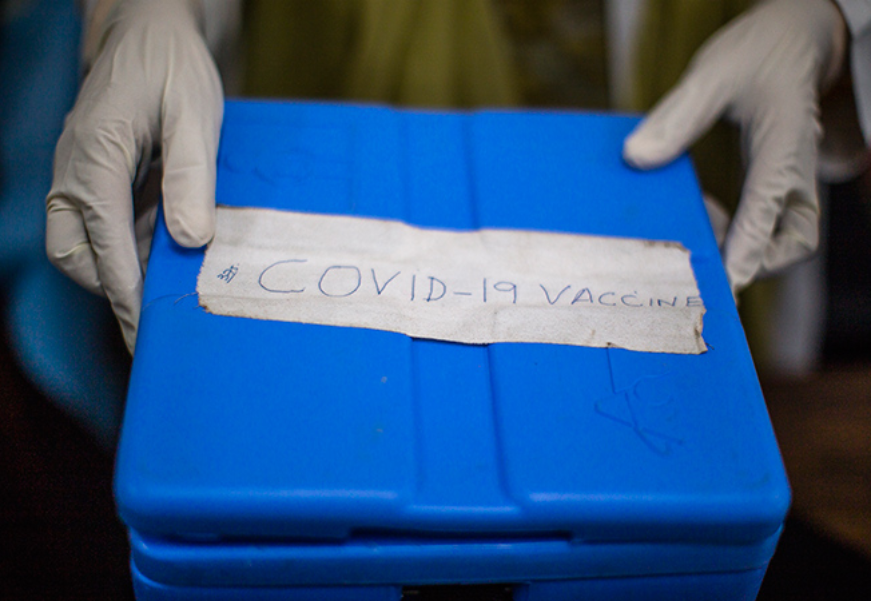
भारत अब पूरी तरह से कोरोना वायरस की दूसरी वेव की गिरफ़्त में आ चुका है. अब सवाल ये है कि क्या भारत कोविड-19 की सेकेंड वेव की चुनौती का, महामारी के पहले हमले की तुलना में बेहतर ढंग से सामना कर पाएगा? इस सवाल का जवाब मोटे तौर पर इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत ने कोरोना वायरस के पहले हमले से क्या सबक़ सीखे हैं.
इस समय भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामले, फरवरी की तुलना में दस गुने से भी अधिक आ रहे हैं. जबकि एक फ़रवरी 2021 को नए मामलों की संख्या 9 हज़ार से भी कम थी. अप्रैल के पहले हफ़्ते में हर दिन नए केस की संख्या एक लाख को पार कर चुकी थी. 8 अप्रैल को पूरे भारत में कोविड-19 के 1 लाख, 26 हज़ार, 789 नए मामले सामने आए थे. जबकि महामारी की पहली वेव जब मध्य सितंबर में शीर्ष पर पहुंची थी, उस समय एक दिन में अधिकतम 97 हज़ार नए केस सामने आ रहे थे. लेकिन, इस बार जब भारत में जांच और निगरानी की क्षमताएं काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं, तो भी संक्रमण के नए मामलों की संख्या पहली लहर की तुलना में काफ़ी तेज़ है.
महामारी की सेकेंड वेव के लिए कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट, जिनकी संक्रमण दर बहुत अधिक है, महामारी से उकताहट और कोविड-19 से बचाव के उपायों का पालन न करने जैसे कारण ज़िम्मेदार हैं.
इसी तरह, कोविड-19 से होने वाली मौतों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है. फरवरी की शुरुआत में जहां कोरोना वायरस से रोज़ाना क़रीब 90 लोगों की मौत हो रही थी. वहीं, अब ये संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है. हालांकि, तेज़ी से बढ़ते हुए नए केस और इस महामारी से हो रही मौतों में निश्चित रूप से फ़र्क़ दिख रहा है. आने वाले दिनों में इस महामारी से मौत की संख्या भी बढ़ने की आशंका है. महाराष्ट्र में इस महामारी से हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मेडिकल सुविधाओं जैसे कि ICU बेड की कमी बढ़ती जा रही है. महाराष्ट्र में ही कोविड-19 की सेकेंड वेव का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है.
महामारी की सेकेंड वेव के लिए कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट, जिनकी संक्रमण दर बहुत अधिक है, महामारी से उकताहट और कोविड-19 से बचाव के उपायों का पालन न करने जैसे कारण ज़िम्मेदार हैं. 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए कोरोना के टीकाकरण अभियान ने भी लोगों को इस महामारी के प्रति लापरवाह बना दिया है. ऐसे मौक़े पर सरकार द्वारा लोगों को सावधानी बरतने की सलाह का असर तब फीका हो जाता है, जब हाल के दिनों में कई विशाल राजनीतिक रैलियां आयोजित की गई हों और इनमें कोई भी मास्क पहने नहीं दिखा था. इसके अलावा हरिद्वार में आयोजित कुंभ में भी हर दिन क़रीब तीन करोड़ लोग जुट रहे हैं. इन बातों से जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि उनकी आस्था ही उन्हें इस महामारी से बचाएगी.
जब कोरोना की महामारी ने पहली बार हमला बोला था, तो उस समय इसे लेकर अनिश्चितता का माहौल था. केंद्र सरकार ने फ़ौरन ही हालात अपने नियंत्रण में ले लिए थे. वैसे तो स्वास्थ्य, राज्य का विषय है, फिर भी इस महामारी से जुड़े फ़ैसले केंद्र ले रहा था. अक्सर बिना राज्यों से सलाह मशविरे लिए ही फ़ैसले लिए जा रहे थे. 24 मार्च 2020 को पूरे देश में तब लॉकडाउन लगा दिया गया था, जब भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 525 केस ही थे और केवल 11 लोगों की इससे मौत हुई थी. केंद्र सरकार ने ये लॉकडाउन, 68 दिनों बाद 31 मई को हटाया था. उस समय देश में संक्रमण के कुल मामले एक लाख, 90 हज़ार, 606 थे और इस महामारी से तब तक देश भर में कुल 5408 लोगों की मौत हुई थी. महामारी का प्रसार तब तो धीमा था. लेकिन, बाद में उसने तेज़ी पकड़ ली और सितंबर के आख़िरी हफ़्ते में संक्रमण अपने शीर्ष पर पहुंच गया. नवंबर 2020 से जाकर नए केस की संख्या में गिरावट आनी दर्ज हुई थी.
लॉकडाउन का ब्रह्मास्त्र कोरोना के पहले वेव के दौरान इस्तेमाल किया जा चुका है और इस बेहद सख़्त क़दम के आर्थिक दुष्प्रभावों का एहसास होने का मतलब ये है कि अब देश में ऐसे उपायों की कोई गुंजाइश नहीं बची है.
हालांकि, अब जबकि सेकेंड वेव की गति बहुत अधिक तेज़ है, तो भी देश में कोई भी दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात नहीं कर रहा है. लॉकडाउन का ब्रह्मास्त्र कोरोना के पहले वेव के दौरान इस्तेमाल किया जा चुका है और इस बेहद सख़्त क़दम के आर्थिक दुष्प्रभावों का एहसास होने का मतलब ये है कि अब देश में ऐसे उपायों की कोई गुंजाइश नहीं बची है. बल्कि सच तो ये है कि आज केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी दोबारा पटरी पर लाने को बेक़रार है.
ऐसे में एकमात्र समाधान ये है कि कोरोना वायरस के टीकाकरण की रफ़्तार बढ़ाई जाए. जनवरी में टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले, लक्ष्य ये रखा गया था कि देश में वैक्सीन के ज़रूरमंद प्राथमिकता वाले क़रीब 30 करोड़ लोगों (इनमें एक करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, 45 साल से ज़्यादा आयु और अन्य बीमारियों के शिकार 14 करोड़ लोग और 13करोड़ 60 साल से अधिक आयु वाले लोग शामिल थे) को अगस्त 2021 (इस अवधि को बाद में बढ़ा दिया गया) तक कोरोना का टीका लगा दिया जाए. चूंकि, कोरोना के टीके की दो ख़ुराक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि पांच महीनों के भीतर क़रीब 60 करोड़ ख़ुराक देनी थी. इसके साथ-साथ देश में बच्चों, गर्भवती महिलाओँ और अन्य संक्रामक बीमारियों के लिए जो नियमित टीकाकरण अभियान चलते हैं, उन्हें भी जारी रखा जाना था.
भारत में एक विशाल टीकाकरण अभियान चलाया जाता रहा है, जिसके कारण आज भारत दुनिया भर में टीकों का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है. सालाना टीकाकरण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को क़रीब दर्जन भर संक्रामक बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं. एक मोटे अंदाज़े के मुताबिक़, भारत में हर साल क़रीब छह करोड़ लोगों को अलग अलग टीकों की 40 करोड़ से ज़्यादा ख़ुराक दी जाती है. इसका मतलब ये है कि हर महीने लगभग 3.4 करोड़ टीके लगाए जाते हैं. इनमें आप कोविड-19 के दस करोड़ टीके भी जोड़ दें, तो टीकाकरण की संख्या कई गुना बढ़ जाती है.
ये स्पष्ट है कि अभी भारत में कोविड-19 के टीकाकरण की रफ़्तार बहुत धीमी है. 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के पहले चरण में जब स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा रही थी, तो इसे लेकर उत्साह बहुत ही कम था. कोवैक्सिन (भारत बायोटेक द्वारा विकसित और निर्मित की जा रही वैक्सीन) को लेकर दिए गए बयानों ने ग़फ़लत को तब और बढ़ा दिया जब ये कहा गया कि अभी कोवैक्सिन को ‘क्लिनिकल ट्रायल’ की तरह ही दिया जा रहा है. क्योंकि उस समय, इस वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के आंकड़ों का इंतज़ार था. वहीं, कोविशील्ड (एस्ट्रा-ज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित) वैक्सीन को आपातकाल में इस्तेमाल किए जाने की इजाज़त दे दी गई थी. यूरोप से ये ख़बरें आई थीं कि कि 60 साल से ज़्यादा आयु के लोगों को कोविशील्ड की ख़ुराक इसलिए नहीं दी जा रही थी कि इससे लोगों के शरीर में ख़ून के थक्के बन रहे थे. 1 मार्च को सरकार ने 60 साल से ज़्यादा आयु और अन्य बीमारियों के शिकार 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण की हरी झंडी दे दी. वहीं, 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन देने की इजाज़त सरकार ने दे दी है.
देश में अब तक आठ करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है; वैक्सीन देने की मौजूदा दर क़रीब तीस लाख ख़ुराक प्रतिदिन है. इस दर से प्राथमिकता वाली आबादी के क़रीब 60 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य जुलाई या अगस्त महीने में नहीं पूरा किया जा सकता है.
जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, देश में 45 साल से अधिक आयु के लोग कुल आबादी का बस 22 प्रतिशत हैं. हालांकि, ये सच है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के 60 प्रतिशत मामले 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों के हैं, जबकि इस महामारी से मरने वाले 88 प्रतिशत लोग इसी आयु वर्ग के थे. इसके बावजूद, महामारी की दूसरी लहर ज़्यादा युवा लोगों को अपनी चपेट में ले रही है. क्योंकि वो खेतों, दुकानों, कारखानों और दफ़्तरों में दोबारा काम पर लौटे हैं.
देश में अब तक आठ करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है; वैक्सीन देने की मौजूदा दर क़रीब तीस लाख ख़ुराक प्रतिदिन है. इस दर से प्राथमिकता वाली आबादी के क़रीब 60 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य जुलाई या अगस्त महीने में नहीं पूरा किया जा सकता है. अगर हम ये मान लें कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के क़रीब 80 करोड़ लोगों को भी टीका दिया जाएगा, तो उनके लिए 1.6 अरब ख़ुराक की ज़रूरत होगी. मौजूदा दर के हिसाब से इन सब लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम नवंबर 2022 तक चलता रहेगा!
इस समय देश में 45,000-50,000 टीकाकरण केंद्र काम कर रहे हैं. इन सभी केंद्रों पर हर दिन क़रीब 100 लोगों को टीका लगाने की कोशिश होती है. हालांकि, लोगों में अनिच्छा का भाव और टीकाकरण को लेकर असरदार प्रचार अभियान न होने के चलते, बहुत से केंद्रों में टीका लगाने वाले बहुत कम तादाद में पहुंच रहे हैं. इसके अतिरिक्त टीकों की बर्बादी भी हो रही है. माना जा रहा है कि देश भर में क़रीब 7 प्रतिशत टीके बर्बाद हो रहे हैं. हर राज्य में ये संख्या अलग अलग है. इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने में कुछ न कुछ टीके तो ख़राब होंगे ही. लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हर ख़ुराक़ को बचाने की कोशिश युद्ध स्तर पर की जाए. इस दबाव के कारण, महामारी के सबसे अधिक प्रकोप से जूझ रहे राज्यों पर दबाव बढ़ा है. ऐसे में इस बात पर अचरज नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार से हर उम्र के लोगों को टीका लगाने की इजाज़त मांगी है. इन राज्यों की मांग ये भी है कि उन्हें टीका लगाने के लिए अपने नियम तय करने की इजाज़त मिले, जिससे कि वो अपने यहां की जनता की महामारी से रक्षा कर सकें और सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों में महामारी के प्रकोप की रोकथाम कर सकें.
पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ाया जाए, और हर दिन एक करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा जाए; इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिनकी उम्र 45 बरस से अधिक हो; लेकिन, 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देने का विकल्प खोल देना चाहिए.
ये बात एकदम शीशे की तरह साफ़ है कि महामारी की दूसरी वेव ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है. शुरुआती अनुमानों के अनुसार, पहली वेव की तुलना में दूसरी लहर 1.7 गुना अधिक तेज़ है. इस दर से कोरोना के नए केस प्रतिदिन 1 लाख 50 हज़ार केस से भी अधिक के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं. इसके बाद शायद संक्रमण की दर कम हो. दूसरी बात ये है कि, ये माना जा रहा था कि संक्रमण से मरने वालों की दर (CFR) इस वेव में कम है. लेकिन, ये बात भी ग़लत साबित हो चुकी है. क्योंकि 18 दिन पहले की तुलना में केस फैटेलिटी रेट (CFR) ये इशारा करती है कि महामारी की दूसरी वेव, पहली लहर के बराबर ही जानलेवा है. इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द सेकेंड वेव में भी मौत का आंकड़ा, पहली लहर की ही तरह प्रतिदिन के औसत 1200 तक पहुंच सकता है.
पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ाया जाए, और हर दिन एक करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा जाए; इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिनकी उम्र 45 बरस से अधिक हो; लेकिन, 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देने का विकल्प खोल देना चाहिए. हां, ये विकल्प स्थानीय हालात और उचित दिशा-निर्देशों के हिसाब से ही दिया जाना चाहिए. इसके लिए केंद्र सरकार को टीकाकरण केंद्रों का निर्धारण करने का अधिकार राज्यों को देना होगा. राज्यों पर ही ये ज़िम्मेदारी भी छोड़नी होगी कि वो 45 साल तक की आयु के किन लोगों को कोरोना की वैक्सीन दें. इस दौरान टीकाकरण अभियान की निगरानी के दिशा-निर्देश भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा ही जारी किए जाने चाहिए.
हर दिन क़रीब तीस लाख लोगों को टीका लगाने से, सरकार की हर महीने टीकों की 10 करोड़ ख़ुराक की मांग, पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट (SII) और भारत बायोटेक (BB) की क्षमताओं से अधिक है. इस समय सीरम इंस्टीट्यूट प्रति माह क़रीब 6.5 करोड़ ख़ुराक और भारत बायोटेक हर महीने क़रीब 40 लाख डोज़ ही तैयार कर पा रहे हैं. भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 8 मार्च 2021 को राज्यसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट के अनुसार, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन बनाने की क्षमता इस साल के मध्य तक 10 करोड़ डोज़ प्रति माह तक पहुंच जाएगी. वहीं, भारत बायोटेक इस साल के मध्य तक हर महीने कोरोना के क़रीब एक करोड़ टीकों का निर्माण करने लगेगी. इससे ज़्यादा टीकों के उत्पादन के लिए इन कंपनियों ने केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी है.
इस मामले में केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प है नहीं. सरकार ने टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, पिछले साल ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था. इस टास्क फोर्स ने वैक्सीन के विकास के लिए जांच केंद्र बनाने और अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग किया है. लेकिन, आज टीकों की मांग बिल्कुल अलग स्तर पर है. आज पहली प्राथमिकता इस बात की है कि सरकार द्वारा मंज़ूर कोविड-19 के दोनों टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सिन के उत्पादन की क्षमता का फ़ौरन विस्तार किया जाए.
सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन बनाने की क्षमता इस साल के मध्य तक 10 करोड़ डोज़ प्रति माह तक पहुंच जाएगी. वहीं, भारत बायोटेक इस साल के मध्य तक हर महीने कोरोना के क़रीब एक करोड़ टीकों का निर्माण करने लगेगी. इससे ज़्यादा टीकों के उत्पादन के लिए इन कंपनियों ने केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी है.
दूसरी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कोरोना वायरस के अन्य टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंज़ूरी दी जाए. रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक V के निर्माण के लिए रूस की कंपनी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (RDIF) ने भारत की पांच वैक्सीन निर्माता कंपनियों से समझौता किया है. इस समझौते के तहत वर्ष 2021 में टीकों की 85 करोड़ ख़ुराकें तैयार की जानी है. इसके अलावा भारत में कम से कम पांच और वैक्सीन हैं, जिनका विकास किया जा रहा है. इन्हें बीबायोलॉजिकल ई, ज़ायडस कैडिला, जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कि नाक से दी जाने वाली वैक्सी शामिल हैं.
इसी दौरान जॉनसन ऐंड जॉनसन द्वारा बनाए गए उस टीके को भी जल्द इस्तेमाल किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिसकी एक ही ख़ुराक देने की ज़रूरत होगी. ख़ास तौर से तब और जब इस टीके को भारतीय कंपनी बीबायोलॉजिकल ई देश में ही बनाएगी. अगर भारत सरकार को ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, तो निजी क्षेत्र द्वारा इसका आयात करके इस्तेमाल करने की छूट दी जानी चाहिए. बड़ी औद्योगिक कंपनियां, अपने कामगारों और उनके परिवारों के लिए ये ज़िम्मेदारी ख़ुशी ख़ुशी उठा लेंगी, ख़ास तौर से तब और जब उन्हें इस बात को लेकर भरोसा हो कि उनके यहां काम करने वालों को कोविड के चलते लगाई जा रही पाबंदियों से छूट दी जाए.
कोरोना की वैक्सीन की बर्बादी का राष्ट्रीय औसत लगभग 7 प्रतिशत है. इसमें अलग अलग राज्यों में बर्बादी का आंकड़ा अलग है. टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने से टीकों की ये बर्बादी रोकी जा सकेगी.
आज देश में कोरोना वायरस के परीक्षण की जो दर है, उसमें भी तेज़ी लाने की ज़रूरत है. इस समय देश में प्रतिदिन क़रीब 11 लाख कोरोना टेस्ट हो रहे हैं. ये आंकड़ा पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में किए जा रहे 15 लाख कोरोना टेस्ट से कहीं कम है. आज जबकि कोविड-19 का टेस्ट कराने की दर काफ़ी कम हो गई है, तो कोई कारण नहीं बनता कि हम हर दिन कम से कम बीस लाख या फिर इससे भी ज़्यादा कोविड टेस्ट करें.
और आख़िर में भारत ने कोरोना वायरस के केवल 11 हज़ार जीनोम का सीक्वेंस तैयार किया है, जो विश्व भर में हुए क़रीब 9 लाख सीक्वेंस का बस मामूली सा हिस्सा है. इनमें से भी वायरस के ज़्यादातर जीनोम सीक्वेंस को अमेरिका और ब्रिटेन में तैयार किया गया था. वायरस के जीनोम की बड़े पैमाने पर सीक्वेंसिंग करने से इसके नए वैरिएंट का पता जल्दी लगाने में मदद मिलती है. इनकी मदद से वायरस के म्यूटेशन का विश्लेषण भी आसान हो जाता है. इस कमी को पूरा करने में सबसे अच्छी भूमिका ICMR की प्रयोगशालाएं कर सकती हैं. इससे भारत में वैक्सीन का विकास करने वालों को भी मदद मिलेगी.
और अंत में, कोरोना वायरस की पहली वेव का सबसे अहम सबक़ ये था कि हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है. हर बात पर केंद्रीकृत नियंत्रण रखने के बजाय, ज़िम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए. इस समस्या पर संपूर्ण आधिकारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए केंद्र सरकार को केवल उन बातों पर ध्यान लगाना चाहिए, जो वो ख़ुद से कर सकती है. बाक़ी की ज़िम्मेदारियां उसे राज्य सरकारों को सौंप देनी चाहिए, जिससे वो ज़मीनी हालात का बेहतर प्रबंधन कर सकें. इसी तरह टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए किस तरह लोगों के बीच बात को रखना है, ये काम भी स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए. इससे वो स्थानीय आबादी के अनुरूप संवाद की रणनीति, माध्यम और तत्वों का विकास कर सकेंगे. जिससे टीकाकरण अभियान को बढ़ाया जा सकेगा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Ambassador Rakesh Sood was a Distinguished Fellow at ORF. He has over 38 years of experience in the field of foreign affairs economic diplomacy and ...
Read More +