-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
सीमा पर चीन के आक्रामक बर्ताव के बीच, उसके सीमा संबंधी नए क़ानूनों ने भारत के लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं.

23 अक्टूबर 2021 को चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने ‘ज़मीनी सीमा के क़ानून’ को मंज़ूरी दे दी. इस क़ानून में, चीन की सरहदों की रक्षा और सीमावर्ती इलाक़ों के एकीकरण से जुड़े प्रावधान हैं. सिर्फ़ सीमाओं को समर्पित ये चीन का पहला क़ानून है. इस वक़्त चीन की ज़मीनी सीमा क़रीब 22 हज़ार किलोमीटर लंबी है, जो रूस, भारत, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, भूटान, म्यांमार और नेपाल समेत कुल 14 देशों के साथ मिलती है.
नए क़ानून में ये कहा गया है कि चीन अपनी सभी थल सीमाओं पर सीमा बताने वाले चिह्न लगाएगा, जिससे कि उसकी सभी सीमाएं स्पष्ट रहें.
चीन का सीमाओं से जुड़ा ये क़ानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा; इसमें 62 अनुच्छेद और सात अध्याय हैं. इस क़ानून के दायरे में मोटे तौर पर ये बातें आती हैं:
a ज़मीनी सरहदों का परिसीमन और सर्वेक्षण
नए क़ानून में ये कहा गया है कि चीन अपनी सभी थल सीमाओं पर सीमा बताने वाले चिह्न लगाएगा, जिससे कि उसकी सभी सीमाएं स्पष्ट रहें. सीमा पर लगाए जाने वाले ऐसे सभी चिह्न संबंधित देश के साथ समझौते के तहत तय किए जाएंगे.
b सीमावर्ती इलाक़ों का प्रबंधन और उनकी रक्षा
सीमा से लगे इलाक़ों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और चीन के सशस्त्र पुलिस बल के हवाले की गई है. इस ज़िम्मेदारी के तहत सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग शामिल है.
इस क़ानून में सीमावर्ती इलाक़ों में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी कोई भी हरकत करने की मनाही है, जिससे ‘चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा या पड़ोस के मित्र देशों के साथ चीन के रिश्तों पर असर पड़े’. ऐसी गतिविधियों में सीमा पर संबंधित अधिकारी या संस्था के इजाज़त के बग़ैर किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी निर्माण करना शामिल है. यहां तक कि सीमा और उससे जुड़े मूलभूत ढांचे की रक्षा की ज़िम्मेदारी स्थानीय संगठनों और नागरिकों की भी होगी. जो सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सरहदों की रखवाली की ज़िम्मेदार सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे.
जहां तक सीमावर्ती इलाक़ों के विकास की बात है, तो इस क़ानून में कहा गया है कि चीन, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से चीन के नागरिकों के बीच ‘सामुदायिक एकता और चीनी राष्ट्र के प्रति जज़्बे को मज़बूत करेगा और नागरिकों को देश की क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी’, अपने देश और उसकी सुरक्षा के प्रति लोगों के जज़्बात को मज़बूत करेगी और सीमा पर रहने वाले चीन के नागरिकों के मन में एक साझा आध्यात्मिक राष्ट्र के निर्माण के भाव को बढ़ावा देगी.’ इसके लिए क़ानून में इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि चीन की सरकार सीमावर्ती इलाक़ों में जनता के लिए सेवाओं और मूलभूत ढांचे का विस्तार करेगी, उनके रहन-सहन को बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने में मदद करेगी.
अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के बाद चीन, इस बात से चिंतित हैं कि कहीं इस्लामिक उग्रवादी उसके शिंजियांग उइघुर स्वायत्तशासी क्षेत्र (XUAR) में घुसपैठ करके उसे अस्थिर करने की कोशिश न करें.
आख़िर में इस क़ानून में ये प्रावधान भी किया गया है कि युद्ध, हथियारबंद संघर्ष और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए ख़तरा बनने वाली घटनाओं जैसे कि जैविक और रासायनिक हादसों, प्राकृतिक आपदाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की घटनाओं के वक़्त चीन अपनी सीमाएं बंद कर देगा.
c सीमा संबंधी मामलों में पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग
जिन देशों के साथ चीन की सीमा लगती है, उनके लिए इस क़ानून में प्रावधान है कि इन देशों के साथ चीन के रिश्ते ‘समानता और आपसी लाभ’ पर आधारित होंगे. इसके अलावा, पड़ोसी देशों के साथ सीमा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए सैन्य और असैन्य, दोनों ही तरह की साझा समितियां बनाने का प्रावधान है. जिससे कि बातचीत से सीमाओं का प्रबंधन किया जा सके.
इस क़ानून में ये भी कहा गया है कि चीन को संबंधित पड़ोसी देशों के साथ किए गए सीमा संबंधी समझौतों का पालन करना चाहिए और सीमा से जुड़े सभी मसलों का हल बातचीत से किया जाना चाहिए.
चीन द्वारा इस क़ानून को अपनाने के कुछ दिनों बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि, ‘चीन द्वारा इकतरफ़ा तरीक़े से लाए गए इस क़ानून का सीमा के प्रबंधन से जुड़े मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं और सीमा से जुड़े अन्य मसलों पर पड़ सकता है. हम ये भी उम्मीद करते हैं कि चीन इस क़ानून के बहाने से भारत और चीन के सीमावर्ती इलाक़ों में कोई इकतरफ़ा क़दम उठाने से बाज़ आएगा.’ और, ‘इस क़ानून को पारित किए जाने से 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए ‘सीमा समझौते’ पर कोई असर नहीं पड़ेगा’. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ़ दो देश भारत और भूटान ही हैं, जिनके साथ चीन का कोई अंतिम सीमा समझौता नहीं है.
कुछ लोगों का कहना है कि भारत का ऐसी प्रतिक्रिया जताना बेवजह का है, क्योंकि क़ानून में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे विवादित कहा जाए. चीन के विदेश मंत्रालय ने बाद में ये सफ़ाई भी दी कि ये क़ानून लागू होने के बाद भी, चीन उन समझौतों का पालन करेगा, जिस पर वो पहले दस्तख़त कर चुका है. यहां पर इस बात का भी ख़याल रखना ज़रूरी है कि चीन ने सीमा के प्रबंधन वाली ये नीति भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के साथ साथ शायद कई अन्य बातों को ध्यान में रखकर बनाई है. अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के बाद चीन, इस बात से चिंतित हैं कि कहीं इस्लामिक उग्रवादी उसके शिंजियांग उइघुर स्वायत्तशासी क्षेत्र (XUAR) में घुसपैठ करके उसे अस्थिर करने की कोशिश न करें. चीन की एक और चिंता ये भी हो सकती है कि वो म्यांमार और वियतनाम के साथ अपनी थल सीमा को मज़बूत करना चाहता हो, ताकि इन देशों से अवैध घुसपैठ को रोक सके. क्योंकि, चीन में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के लिए इन देशों से अवैध घुसपैठ को ही ज़िम्मेदार बताया जा रहा है.
हालांकि, अगर हम सीमा पर चीन के हालिया आक्रामक रवैये को ध्यान में रखकर देखें, तो भारत सरकार की चिंताएं वाजिब लगती हैं. 2020 में चीन ने लद्दाख में गलवान घाटी, डेमचोक, डेपसांग और पैंगॉन्ग झील और सिक्किम तिब्बत सीमा पर अपने दावे को मज़बूत करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है. संघर्ष के दौरान दोनों देशों के कई सैनिक हताहत हुए थे. उससे पहले 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम में भी तनाव हुआ था, जो भूटान और चीन के बीच का विवाद इलाक़ा है. तब भी दोनों देश युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे.
चीन ने इस क़ानून को तब मंज़ूरी दी, जब सीमा पर दोनों देशों के बीच 18 महीने से ज़्यादा वक़्त से सैन्य तनातनी चल रही है और दोनों देशों के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता भी नाकाम रही थी
चीन के नए सीमा क़ानून से जुड़ी जो और भी चिंताजनक बात है, वो इसकी भाषा और पारित होने का समय है. चीन ने इस क़ानून को तब मंज़ूरी दी, जब सीमा पर दोनों देशों के बीच 18 महीने से ज़्यादा वक़्त से सैन्य तनातनी चल रही है और दोनों देशों के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता भी नाकाम रही थी. दोनों ही देशों ने लिए बातचीत नाकाम रहने के लिए एक-दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया था.
नया क़ानून, चीन की सरहदों को पवित्र और उल्लंघन से परे बना दिया है. चूंकि सीमा की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को दे दी गई है, जो भविष्य में सीमा विवाद के निपटारे के लिए किसी भी बातचीत के लिए बाधा बन सकती है. क्योंकि, हो सकता है कि चीन की सेना, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में अपने वास्तविक या दावे वाले इलाक़ों पर से क़ब्ज़ा छोड़ने से इंकार कर सकती है. आशंका इस बात की भी है कि चीन, ब्रह्मपुत्र या यारलुंग झैंगबो नदी से भारत की तरफ़ आने वाले बहाव को भी रोक सकता है. क्योंकि, इस क़ानून में कहा गया है कि, ‘सीमाओं के आर-पार स्थित नदियों और झीलों की स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी ज़रूरी उपाय किए जाएंगे’. किसी भी पनबिजली परियोजना को बनाने के लिए चीन इन्हीं प्रावधानों का हवाला दे सकता है. ऐसे प्रोजेक्ट भारत में तबाही लाने वाले भी हो सकते हैं. जबकि चीन इसे क़ानूनी रूप से जायज़ ठहराने के लिए आज़ाद होगा.
आख़िर में, चीन के इस क़ानून में सीमावर्ती इलाक़ों में आबादी की बसावट और मूलभूत ढांचे का विकास की बात भी कही गई है. चीन पहले भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास अपने दावे वाले इलाक़ों में ‘नागरिक’ आबादी को बसाने की रणनीति पर अमल करता आया है, जिससे वो इन इलाक़ों पर वो वाजिब मालिकाना हक़ जता सके. हो सकता है कि नया क़ानून लागू होने पर ऐसी घटनाएं और दोनों देशों के बीच विवाद के मसले और भी बढ़ जाएं.
ज़मीनी स्तर पर ये क़ानून चीन और भारत के संबंधों पर बहुत गहरा असर डालता नहीं दिखता. पिछले कई वर्षों से चीन भारतीय सीमा पर अपने दावों को लेकर काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाए हुए है. इससे पहले भी चीन विवादित इलाक़ों पर संघर्ष को बढ़ाने वाले क़दम उठाता रहा है. जैसे कि सीमा के पास सड़कें बनाना, आम लोगों की आबादी का इस्तेमाल करना और चीन की सेना द्वारा कई बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करना, जिससे कि वो अपनी दावेदारी और मज़बूत कर सके.
चीन का ये क़ानून अपने आप में चिंता का विषय नहीं है. बल्कि, चीन की सरकार और उसकी सेना का बर्ताव ही फ़िक्र की असल वजह है. क्योंकि पहले भी चीन ने तय क़ानूनों का अपने हिसाब से दुरुपयोग या उल्लंघन किया है. जैसा कि चीन में भारत के पूर्व राजदूत गौतम बंबावाले ने कहा है कि इस क़ानून में वही बातें हैं, जो चीन हमेशा से कहता आया है. असल में चीन की सेना की हरकतें और उन पर भारत की प्रतिक्रिया ही ज़मीनी स्तर पर कोई असर दिखाने वाली होंगी. इसीलिए, चीन द्वारा इस क़ानून को पारित करने पर भारत ने शायद ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया जता दी थी. लेकिन, डर इस बात का भी है कि आने वाले कुछ वर्षों के दौरान हम भारत की चिंताओं को सही साबित होते देख सकते हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
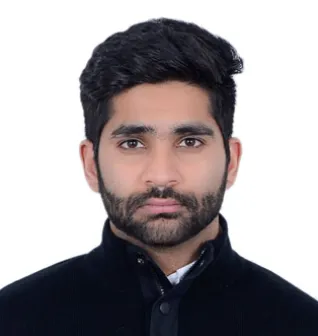
Udayvir Ahuja was a Programme Coordinator for the Strategic Studies Program, where, beyond operational aspects, he engages in writing and researching on contemporary subjects within ...
Read More +