-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
चीन को लेकर नीतियां बनाने से पहले भारत को चाहिए कि वो अपने यहां चीन के निवेश के हर पहलू की निगरानी रखने के लिए उचित व्यवस्था बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़े.
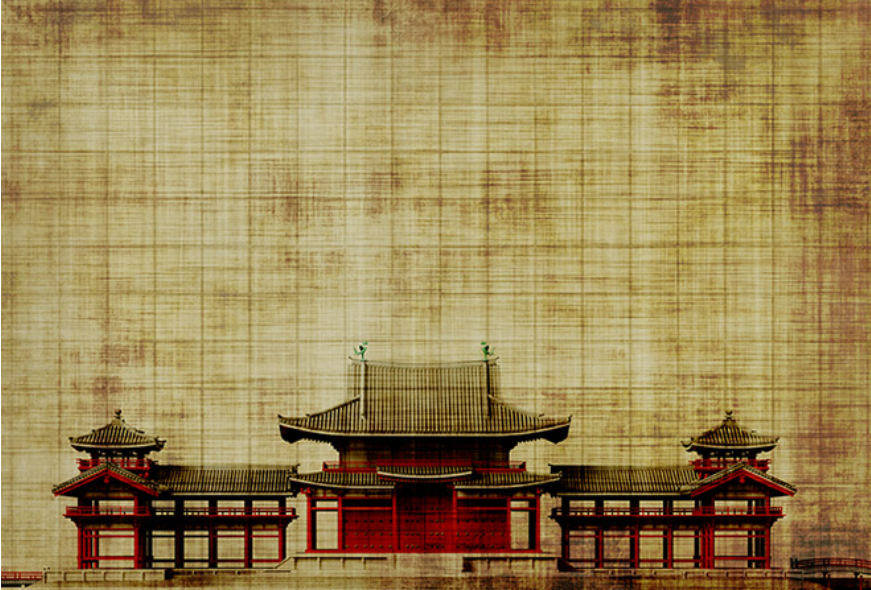
हाल ही में भारत ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव किया है. इसका मक़सद ये है कि देश में जिन कंपनियों की आर्थिक स्थिति ख़राब है, उन पर चीन को अपनी पूंजी की शक्ति से नियंत्रण स्थापित करने से रोका जा सके. इस बदलाव के बाद जिन देशों की ज़मीनी सीमाएं भारत मिलती हैं, वहां से होने वाले पूंजी निवेश के लिए पहले सरकार से मंज़ूरी लेनी ज़रूरी होगी. इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारत और चीन के संबंध का बेहद महत्वपूर्ण मोड़ है. लेकिन, इस विषय को भारत और चीन के संबंधों में आए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों से अलग करके नहीं देखा जा सकता है. भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में अर्थपूर्ण तरीक़े के बदलाव का ये दौर मई 2017 में शुरु हुआ था. तब भारत ने चीन द्वारा अपने बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से एशिया के सामरिक और व्यापारिक समीकरणों को बदलने के प्रयास पर ऐतराज़ जताया था. कई दशकों तक दुनिया के तमाम देश भारत और चीन को एक ही नज़रिए से देखते थे. उन्हें ये लगता था कि इक्कीसवीं सदी को ‘एशिया की शताब्दी’ बनाने की प्रतिभूति यही दो देश देते हैं. लेकिन, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आया. उस संकट को चीन ने दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने करने के अवसर के तौर पर देखा. चीन को लगा कि जब पश्चिमी देश वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, तो इस मौक़े का फ़ायदा उठाकर वो एक ऐसी दो ध्रुवीय या बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण कर सकता है, जहां पर उसका प्रभुत्व हो. और इस दौरान वो एशिया में सबसे शक्तिशाली देश बन जाए और इसकी रीति-नीति को अकेले ही निर्देशित करे. भारत को इस हक़ीक़त को समझने में काफ़ी वक़्त लगा. जब, भारत ने चीन से अपील की कि वो अपने बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) प्रोजेक्ट को बहुपक्षीय व्यवस्था के तौर पर विकसित करे, तो चीन ने भारत की इस अपील को बार बार अनसुना कर दिया. और डोकलाम में चीन और भूटान के बीच लगने वाली सीमा पर आक्रामक रुख़ अपनाया. तनातनी का ये केंद्र, भारत की कमज़ोर नस यानी ‘चिकेन नेक’ वाले भौगोलिक क्षेत्र के बेहद क़रीब था. भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को बाक़ी देश से जोड़ने का ये इकलौता गलियारा है.
चीन को लगा कि जब पश्चिमी देश वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, तो इस मौक़े का फ़ायदा उठाकर वो एक ऐसी दो ध्रुवीय या बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण कर सकता है, जहां पर उसका प्रभुत्व हो. और इस दौरान वो एशिया में सबसे शक्तिशाली देश बन जाए और इसकी रीति-नीति को अकेले ही निर्देशित करे
अब कोरोना वायरस की महामारी ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो दुनिया की नई भौगोलिक और आर्थिक सच्चाइयों का सामना करे. मगर, इस दिशा में अभी भारत के लिए बहुत कुछ करना बाक़ी है. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव की जो तलवार भारत ने चलाई है, वो दुधारी है. इससे अगर वो अपने आर्थिक हितों का संरक्षण करने का प्रयास कर रहा है. तो, इससे भारत को अपने आर्थिक हितों की क्षति भी उठानी पड़ सकती है. चीन, आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. और जैसा कि मार्च में ब्रूकिंग्स इंडिया के लेख, ‘फॉलोविंग द मनी: चाइना इनकॉरपोरेशन्स ग्रोइंग स्टेक्स इन इंडिया चाइना रिलेशन्स’ में अनंत कृष्णन ने आकलन किया है कि चीन ने पिछले छह वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कम से कम आठ अरब डॉलर का निवेश किया है.
अगर भारत 2030 के दशक की शुरुआत तक, ख़ुद को दस ख़रब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का स्वप्न साकार करना चाहता है, तो चीन के साथ अच्छे व्यापारिक और निवेश के संबंध के बिना इस लक्ष्य को प्राप्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा. हालांकि, चीन के आर्थिक बर्ताव के कम से कम दो ऐसे आयाम हैं, जिनकी अनदेखी करने का जोखिम भारत को नहीं लेना चाहिए. पहली बात तो ये है कि चीन, आपसी निर्भरता का ‘सशस्त्रीकरण’ करने का प्रयास कर रहा है. जब से चीन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में आया है, तब से इसने घातक औद्योगिक हथियारों का इस्तेमाल करके वैल्यू चेन की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास किया है. इसके लिए चीन ने अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में असंतुलन को बढ़ाया है. और वैश्विक प्रतिद्वंदिता को भी क्षति पहुंचाने का काम किया है.
चीन की इन अबाध महात्वाकांक्षाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के साथ साथ चीन के प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को हासिल करने के बीच संतुलन बनाना बेहद दुरूह कार्य है. इस विषय में नीतिगत निर्णय करने से पहले भारत को चाहिए कि वो अपने यहां हो रहे चीन के पूंजी निवेश की सख़्त निगरानी की सुदृढ़ व्यवस्था को विकसित करे.
और चीन के बर्ताव के जिस दूसरे पहलू की भारत को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि वो डिजिटल भूमंडलीकरण के आकार को अपने हिसाब से गढ़ने का प्रयास कर रहा है. वो इसके लिए अपनी डिजिटल परिकल्पनाओं को डिजिटल सिल्क रूट से निर्यात कर रहा है. साथ ही साथ, अपने ‘मेड इन चाइना 2025’ की पहल के माध्यम से वो सामरिक औद्योगिक तकनीकों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है.
चीन की इन अबाध महात्वाकांक्षाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के साथ साथ चीन के प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को हासिल करने के बीच संतुलन बनाना बेहद दुरूह कार्य है. इस विषय में नीतिगत निर्णय करने से पहले भारत को चाहिए कि वो अपने यहां हो रहे चीन के पूंजी निवेश की सख़्त निगरानी की सुदृढ़ व्यवस्था को विकसित करे. जैसा कि अनंत कृष्णन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जो आधिकारिक आंकड़े हैं, उनसे भारत में चीन के कुल पूंजी निवेश की पूरी तस्वीर साफ़ नहीं होती. क्योंकि चीन ने अपनी सहयोगी कंपनियों और अन्य वाणिज्यिक माध्यमों से भी भारत में काफ़ी पूंजी निवेश किया हुआ है. हमें, भारत के प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की नीति में हालिया बदलाव को केवल इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि भारत ने अपने यहां चीन के पूंजी निवेश की राह में बाधाएं खड़ी की हैं. वो भी इसलिए क्योंकि चीन ने अपने बाज़ार में भारतीय डेयरी उत्पादकों, आईटी सेवाओं दवा कंपनियों के प्रवेश की राह में बाधाएं खड़ी की हैं.
भारत को अपने उन औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो उसकी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए लगाई गई हालिया पाबंदियों में स्पष्टता और वर्गीकरण का अभाव दिखता है. चीन से होने वाला हर पूंजी निवेश भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा नहीं है. उदाहरण के तौर पर, ऑटोमोबाइल उद्योग में चीन का पूंजी निवेश, भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए उतना बड़ा ख़तरा नहीं है. जितना तकनीकी क्षेत्र में चीन के निवेश से है. फिर चाहे वो 5G तकनीक के मूलभूत ढांचे का विकास हो या इससे जुड़े अन्य उद्योगों में निवेश हो.
भारत और चीन के संबंध आज उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, जिस राह पर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का व्यापक स्वरूप चल रहा है: मतलब ये कि मुक्त और खुले व्यापार का युग ख़त्म हो गया है. भविष्य का भूमंडलीकरण, बंद व्यवस्था वाला होगा. जहां पर आर्थिक संबंध की बुनियाद राजनीतिक विश्वास होगा
और आख़िर में भारत को नए क़ानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे. अमेरिका और यूरोपीय संघ तक ने चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ऐसे व्यापक प्रतिबंधों का सहारा नहीं लिया है. जबकि इन देशों में चीन ने आक्रामक तरीक़े से कई संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों का अधिग्रहण किया है. फिर भी, चीन के आक्रामक पूंजी निवेश को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश हर सेक्टर से जुड़े अलग क़ानूनी विकल्पों जैसे कि डेटा संरक्षण के क़ानून और कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के क़ानूनों में बदलाव का सहारा लिया है. इसके अतिरिक्त, अमेरिका और यूरोपीय संघ, चीन के आक्रामक पूंजी निवेश को रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं का भी सहारा ले रहे हैं. जैसे कि अमेरिका ने इसके लिए कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनाई है, जो हर प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की समीक्षा करती है. बिना उचित वैधानिक और नियामक प्रतिबंधों का इस्तेमाल किए, अगर भारत ऐसे क़दम उठाता है, तो उसे चीन से भी ऐसे ही प्रतिबंधों के पलटवार का सामना करना पड़ सकता है.
भारत और चीन के संबंध आज उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, जिस राह पर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का व्यापक स्वरूप चल रहा है: मतलब ये कि मुक्त और खुले व्यापार का युग ख़त्म हो गया है. भविष्य का भूमंडलीकरण, बंद व्यवस्था वाला होगा. जहां पर आर्थिक संबंध की बुनियाद राजनीतिक विश्वास होगा. इस नए परिवेश से भारत को लाभ होना तय है. अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों के साथ भारत के नज़दीकी राजनीतिक संबंध हैं. इस कारण से चीन की तुलना में भारत के साथ आर्थिक संबंध रखना इन व्यापारिक क्षेत्रों के लिए ज़्यादा सुरक्षित विकल्प होगा. अब अगर आगे चलकर विश्व व्यापार संबंध में ये दौर आना तय है. तो, भारत को चाहिए कि वो अपने साझीदारों के साथ मिलकर काम करे और चीन के आर्थिक बर्ताव को परिवर्तित करने का प्रयास करे.
यह लेख मूलरूप से द इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित हो चुका है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +