-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारत के औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा लोचदार और टिकाऊ बनाने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग एक अहम क़दम है.
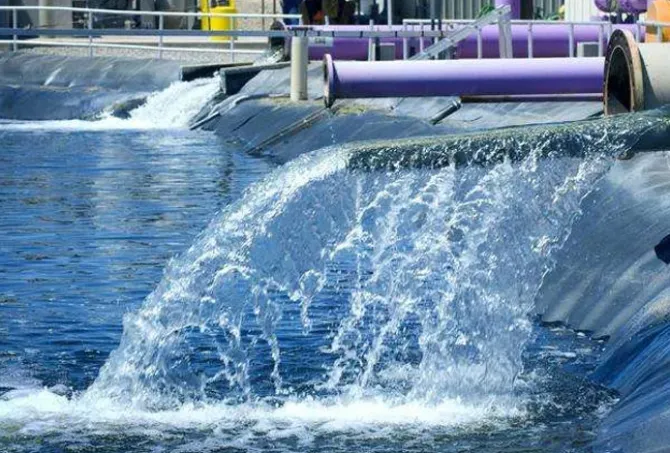
भारत में कृषि क्षेत्र पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. भूगर्भजल पर 62 फ़ीसदी निर्भरता के साथ इस सिलसिले में स्थानीय परिवर्तन दिखते हैं. बहरहाल, हालिया अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि जलीय क्षेत्र का 8-10 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें पूरी कर रहा है और ये मांग क़रीब 2 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रही है. प्राकृतिक संसाधन से जुड़े इस क्षेत्र का औद्योगिक सेक्टर की ओर ऐसा रुझान औद्योगिकरण की अहमियत का प्रमाण है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तपोषित परियोजनाओं ने अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की रफ़्तार बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है. इनमें दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) और चेन्नई-बैंगलोर औद्योगिक गलियारा (CBIC) शामिल हैं.
पिछले कुछ दशकों में मेक इन इंडिया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) स्कीम, क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) जैसी योजनाओं ने घरेलू विनिर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और नतीजतन जल संसाधन की औद्योगिक मांग में इज़ाफ़ा कर दिया है. इन योजनाओं ने राज्य सरकारों के निवेश को छोटे पैमाने वाले औद्योगिक बुनियादी ढांचे से विशाल उद्योगों की ओर मोड़ने में सहयोगकारी भूमिका अदा की है.
मौजूदा वक़्त में औद्योगिक नीतियों और योजनाओं में बजट और क्षेत्र के आवंटन को प्राथमिकता दी गई है. इस स्वरूप ने विशाल पैमाने वाली औद्योगिक योजनाओं में ज़मीन को प्रधान प्राकृतिक संसाधन बना दिया है. ज़मीन की उपलब्धता और अधिग्रहण निर्णायक कारक बनकर देश भर में औद्योगिक क्षेत्रों की मौजूदगी को आकार देने लगे हैं. प्राकृतिक संसाधनों (ख़ासतौर से पानी) के इस्तेमाल की बारी आमतौर पर ज़मीन के आवंटन के बाद आती है. नतीजतन जल संसाधन का अकार्यकुशल नियोजन सामने आता है.
पानी की बढ़ती किल्लत और जलवायु परिवर्तन के चलते औद्योगिक योजनाओं और प्रबंधन क्रियाओं में पानी को टिकाऊ रूप से जोड़े जाने की क़वायद बेहद ज़रूरी हो गई है. इस लेख में हम औद्योगिक नियोजन में जल प्रबंधन की प्रासंगिकता की चर्चा करेंगे. आगे हम इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को अत्याधुनिक बनाने की ज़रूरत पर भी ग़ौर करेंगे. नीति और प्रयोग के क्षेत्र में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी की ग़ैर-हाज़िरी पर भी चर्चा की जाएगी.
फ़िलहाल औद्योगिक क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति 2 मुख्य स्रोतों से होती है. राज्य सरकार के औद्योगिक विभाग आमतौर पर वाणिज्यिक तौर पर औद्योगिक जलापूर्ति के कनेक्शन मुहैया कराते हैं. इसके अलावा उद्योगों को ख़ुद के ख़र्च पर स्थानीय जलाशयों/नहरों से पानी उठाने की भी इजाज़त दी जाती है. साथ ही पूरक के तौर पर उन्हें निजी बोरवेलों और पानी के टैंकरों से हासिल पानी के इस्तेमाल की भी मंज़ूरी दी जाती है.
उद्योगों के लिए भू-जल, पानी का एक अहम स्रोत है. बहरहाल इस क्षेत्र में कोई नियमन नहीं हैं और ना ही इसका कोई हिसाब-क़िताब रखा जाता है. उद्योगों को भू-जल के दोहन के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है. भले ही कुछ क़ानूनों के ज़रिए इस प्रकार के दोहन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन इनकी तामील कराने की क़वायद का साफ़ तौर पर अभाव दिखता है. उद्योग पानी की उपयोग की गई मात्रा के बारे में ख़ुद ही जानकारी देते हैं. इस प्रक्रिया का ना तो कोई नियमन है और ना ही राज्यसत्ता द्वारा पाइप के ज़रिए मुहैया कराई जाने वाले पानी की तरह कड़ाई से इसकी जांच-पड़ताल की जाती है. नतीजतन बिना किसी नियमन के पानी का इस्तेमाल किए जाने की लत को बढ़ावा मिलता है.
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के बाद के योगदान में डिजिटल ट्विन तैयार करने की क़वायद को शामिल किया जा सकता है. डिजिटल ट्विन भौतिक दुनिया, उसके समीकरणों और प्रक्रियाओं का आभासी प्रतिबिंब है.
लचर प्रशासन और बिना नियमनों वाले औद्योगिक इस्तेमाल के घालमेल से स्थानीय (भूगर्भ) जल स्तरों पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ता है. इससे स्थानीय पर्यावरण, बिरादरियों और यहां तक कि इन उद्योगों के भविष्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है. ख़ासतौर से भूगर्भजल की आपूर्ति पर निर्भर रहने वाले सूखा-ग्रस्त इलाक़ों के लिए ऐसे हालात दिखाई देते हैं. पानी की माप करने के तरीक़े में ख़ामियों की वजह से कमज़ोर प्रशासनिक ढांचा और लचर हो जाता है.
ऐसे ही एक मसले में कर्नाटक औद्योगिक और विकास बोर्ड (KIADB) ने औद्योगिक क्षेत्रों की योजना बनाते वक़्त पानी की उपलब्धता के मानचित्रण की कोशिश की है. ये जल संसाधन के गतिशील मानचित्रण की व्यवस्था तैयार करने की क़वायद के साथ-साथ किया गया प्रयास है. इसमें औद्योगिक भू-जल के प्रयोग को भी शामिल किया जाता है. कर्नाटक की नई जल नीति 2022 में भी भू-जल के अनियंत्रित वाणिज्यिक दोहन के निपटारे की कोशिश की गई है. इसके ज़रिए एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. भले ही ये क़दम मददगार हैं लेकिन ये पूर्ववर्ती नीतियों और योजनागत प्रयोगों में ख़ामियों की ओर इशारा करते हैं. यहां स्टार्टअप लागतों से जुड़े कई मसले सामने हैं. बहरहाल, इस कड़ी में नवाचार की तेज़ रफ़्तार प्रौद्यिगिकियों और पूरी तरह से मानकीकृत स्वीकार्यताओं, क्रियाविधि के हिसाब से स्वीकार्यता के अभाव और क्रियान्वयन से जुड़े मसलों को प्राथमिक मुद्दों की तरह रेखांकित किया जाता रहा है. औद्योगिकीकरण की क़वायद के बार-बार सामने आने वाले ऐसे नतीजों की बुनियादी वजह आधारभूत नियोजन का अभाव और औद्योगिक क्रियान्वयन पर बढ़ी हुई निर्भरता है. इस हालात के पीछे क्रियाविधि से जुड़ा एक और मसला पानी (के इस्तेमाल) से जुड़े भरोसेमंद डेटा का घोर अभाव है. भू-जल स्तरों और उनके उपयोग के आकलन के लिए प्रौद्योगिकीय तौर-तरीक़ों के मिले-जुले स्वरूप के इस्तेमाल के साथ-साथ ज्ञान प्रणालियों के दूसरे स्वरूपों का प्रयोग शुरू करना एक बड़ी चुनौती है. इस लेख में हम भू-स्थानिक मैपिंग और प्रौद्योगिकियों के ज़रिए इस खाई को पाटने के एक तरीक़े की चर्चा करेंगे ताकि बेहतर जल प्रबंधन और पुनर्जीवन क्रियाओं को आसान बनाया जा सके.
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनेक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की एक ताज़ा धुरी है. इसकी जड़ें खनन और अंतरिक्ष पर्यवेक्षण से जुड़ती हैं. लिहाज़ा औद्योगिक जल प्रबंधन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग सहज ज्ञान के आधार पर है. ‘जल प्रबंधन’ के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुसंधानों में भू-स्थानिक सूचना प्रणालियां (GIS) और रिमोट सेंसिंग (RS) प्रमुख तत्व रहे हैं. हालांकि नियमन और प्रायोगिक दायरे में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहद मामूली रहा है.
भू-जल स्तरों, उनके उपयोगों और उपभोक्ताओं का मानचित्रण और उनका डेटाबेस बनाए रखना इस दिशा में पहली चुनौती है. भारत के असैनिक अंतरिक्ष संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ-साथ जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के 434 जलाशयों की निगरानी के लिए India-WRIS का गठन किया है. ये मंच उपयोगकर्ताओं को आकलन, निगरानी, नियोजन और विकास के मक़सद से समग्र और संदर्भित जल संसाधन डेटा के बारे में सर्च करने, पहुंच बनाने, कल्पना करने, समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है. साथ ही एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की भी सहूलियत मुहैया कराता है. बहरहाल ‘एकल खिड़की समाधान’ के बावजूद ये क़वायद औद्योगिक क्षेत्र में जलाशयों, सतही पानी या भू-जल की उपयोगिता को नज़रअंदाज़ करती है. इसकी बजाए इसमें शहरी और कृषि उपयोगिता पर तवज्जो दिया जाता है. आपूर्ति श्रृंखला के मांग पक्ष में उद्योग एक बेहद बड़ा क्षेत्र है. इसके बावजूद पानी के प्रयोग का निर्धारण करने में मौजूद इस खाई के चलते नियामक अभ्यासों और प्रयोग में बड़ा अंतर आ जाता है.
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के बाद के योगदान में डिजिटल ट्विन तैयार करने की क़वायद को शामिल किया जा सकता है. डिजिटल ट्विन भौतिक दुनिया, उसके समीकरणों और प्रक्रियाओं का आभासी प्रतिबिंब है. इससे हमें असल-जीवन के हालातों का बनावटी स्वरूप तैयार करने और उनके प्रभावों का विश्लेषण करने की सहूलियत होती है. भौतिक दुनिया में मौजूद इकाइयों की उनके संदर्भित वर्चुअल मॉडलों के डेटाबेस से नुमाइंदगी, दक्ष रूप से जुड़ी होती है. इससे साथ जुड़े परिणाम सामने आते हैं. हालांकि इसके बावजूद ये भौतिक प्रणालियों (जैसे पाइप्स, पंप्स, वाल्व्स और टैंक) में सौदों के संदर्भ में कारोबारी सहूलियत मुहैया कराते हैं. इनमें ऐतिहासिक डेटा सेट्स, जैसे मौसम के रिकॉर्ड्स और वास्तविक समय के गतिशील संवाद शामिल होते हैं.
ऊपर के दोनों उपायों से भू-जल के बदलते स्तरों में उपयोग के हिसाब से माप करने में योगदान मिलता है. इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन और मैपिंग में मदद मिलती है.
सैटेलाइट्स और डिजिटल ट्विन्स जैसी टेक्नोलॉजी को परे रखें तो सैद्धांतिक भू-स्थानिक प्रयोगों में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली तमाम क्रियाविधियों से क्षेत्रीकरण, पानी की पड़ताल करने और प्रबंधन करने में मदद मिलती है. औद्योगिक जल प्रतिचित्रण नियमनों और दिशानिर्देशों में शैनॉन के एन्ट्रॉपी मॉडल(उस ऊर्जा का परिमाण जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती) जैसे उपाय शामिल किए जा सकते हैं. इस मॉडल में प्रणाली के एन्ट्रॉपी और उसकी अव्यवस्था के परिमाण के बीच एक-दूसरे पर आधारित संबंधों की माप की जाती है. साथ ही बूलियन मॉडलिंग (जिसमें शर्तिया संचालकों के प्रयोग के नतीजे के तौर पर सामने आए दोहरे नक़्शों के तार्किक संयोग शामिल होते हैं) और अन्य भी जुड़े होते हैं. इन्हें पानी के मानचित्रण को बढ़ाने और जल संसाधनों के दोहन को कम से कम करने के लिए प्रभावी रूप से अमल में लाया जा सकता है.
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में सरकारी निवेश सिर्फ़ राष्ट्रीय समर्थन के बूते ही पर्याप्त हो सकती है. इससे संस्थागत स्तर पर एकीकरण सुनिश्चित हो सकता है, जिससे सभी संबंधित विभागों को सूचना के भंडार तक पहुंच बनाने और उनमें योगदान देने की छूट मिल जाती है.
निष्कर्ष के तौर पर भले ही नीति और नियोजन में प्रौद्योगिकी को शामिल करना एक प्रभावी ज़रिया है, लेकिन इन क्रियाओं की स्टार्टअप लागत हतोत्साहित करने वाली है. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर राज्यसत्ता के स्तर पर निवेश करना ख़र्चीली क़वायद हो सकती है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बजट आवंटन की ज़रूरत पड़ सकती है. इसके अलावा निष्पक्ष और न्यायसंगत बढ़त के लिए सभी राज्यों के जुड़ाव की दरकार होती है.
ऐसी प्रौद्योगिकी के सिलसिले में वित्तीय आवंटन तो अक्सर समस्या का एक हिस्सा भर होती है. आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से डेटा संग्रह करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना अक्सर मानव संसाधन के मोर्चे पर एक अनदेखी लागत होती है. इसके अभाव से प्रौद्योगिकी की व्यवस्थागत स्वीकार्यता की नाकामी पैदा होती है.
कोष और कुशल श्रम के सीमित स्तरों के अलावा प्रशासनिक ढांचों में मौजूद दरारों से भी एकीकृत डेटाबेस और प्रबंधन प्रणाली की मौजूदगी चुनौतीपूर्ण क़वायद बन जाती है.
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में सरकारी निवेश सिर्फ़ राष्ट्रीय समर्थन के बूते ही पर्याप्त हो सकती है. इससे संस्थागत स्तर पर एकीकरण सुनिश्चित हो सकता है, जिससे सभी संबंधित विभागों को सूचना के भंडार तक पहुंच बनाने और उनमें योगदान देने की छूट मिल जाती है. ये क़वायद बेहद अहम है क्योंकि एक इकलौती राज्यसत्ता के तहत कई विभाग, उद्योग और जल से जुड़े क्षेत्र की निगरानी करते हैं. ऐसे में इन संस्थागत पैमानों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी को स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया फ़ायदेमंद रहेगी.
वैसे तो इन तमाम चुनौतियों पर ग़ौर करना ज़रूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया की लागत एक ठोस जल प्रबंधन प्रणाली में निवेश की ज़रूरत से आगे नहीं निकलनी चाहिए. दरअसल राज्यसत्ता के लिए टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक गलियारों में भारी-भरकम निवेश की क़वायद तात्कालिक रूप से आवश्यक है. जल संसाधन की रक्षा के लिए भू-जल प्रबंधन एक अहम कारक है. नए ज़माने की प्रौद्योगिकी, कार्यकुशल श्रम और राष्ट्रीय प्रशासनिक ढांचों में बढ़े हुए भरोसे के तौर पर ये बचाव अधिकतम उपभोग और टिकाऊ उत्पादन के लिए भूमि और जल संसाधनों को उत्प्रेरक बनने में मददगार साबित होंगे.
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और अपने यहां विनिर्माण का केंद्र स्थापित करने की भारत की कोशिशों के बीच औद्योगिक क्षेत्र की मज़बूती और टिकाऊपन बेहद अहम हैं. ऐसे में ताज़ा क्रियाविधियों के मेलजोल से भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग इस रास्ते में उठाया जाने वाला अगला आवश्यक क़दम है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.