-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
दोनों देशों की रणनीतिक मजबूरियां, ख़ासकर जिनका ताल्लुक़ हिंद-प्रशांत में चीन पर लगाम लगाने से है, अब निकट व्यापारिक संबंधों में बदल चुकी हैं.
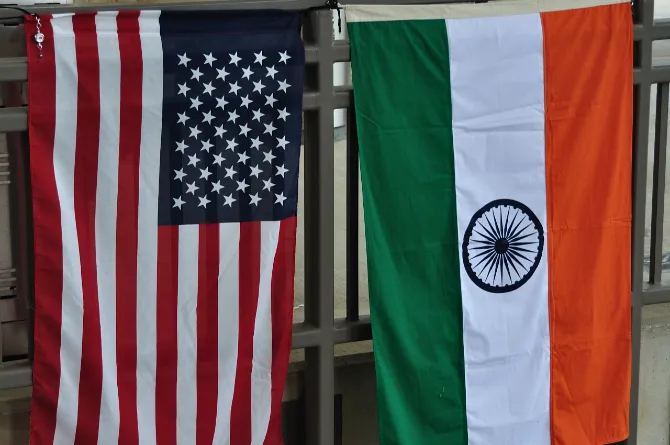
India-Australia trade deal: रणनीतिक ज़रूरतों से निर्देशित है भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार सौदा
10 साल लंबी बातचीत के बाद, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आख़िरकार पिछले सप्ताह ‘भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते’ पर दस्तख़त किये. इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन ने शिरकत की. यह रेखांकित करते हुए कि ‘इतने महत्वपूर्ण समझौते पर इतनी छोटी अवधि में सहमति बनना दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे को दिखाता है’, मोदी ने बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया कि यह ‘हमारे (भारत-ऑस्ट्रेलिया) द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है.’ मॉरिसन ने ज़ोर दिया कि यह समझौता दिल्ली के साथ कैनबरा के रिश्तों में अकेला सबसे बड़ा सरकारी निवेश है. अपने देश में नज़दीक आ रहे चुनावों के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि ‘यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के किसानों, विनिर्माताओं, उत्पादकों वग़ैरह के लिए दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बड़ा दरवाज़ा खोलेगा.’
भारत एक ऐसे देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता क़ायम करने की कोशिश कर रहा है जो भरोसेमंद साझेदारों के साथ कारोबार करने को तैयार है, और कई सारे ‘अर्ली हॉर्वेस्ट’ समझौतों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है.
अंतरिम समझौते से भारत में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत कई सेक्टरों को फ़ायदा होने की उम्मीद है, जबकि साथ ही यह भारत को निर्यात होने वाली ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं में से 85% से ज़्यादा पर शुल्क को हटाता है. यह ऐसे अहम वक़्त में हो रहा है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अपनी व्यापार नीति का पुन: आकलन कर रहे हैं. भारत एक ऐसे देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता क़ायम करने की कोशिश कर रहा है जो भरोसेमंद साझेदारों के साथ कारोबार करने को तैयार है, और कई सारे ‘अर्ली हॉर्वेस्ट’ समझौतों (मुक्त व्यापार समझौते से पहले अपेक्षाकृत सीमित दायरे के समझौतों) को अंतिम रूप देने में व्यस्त है. बीजिंग द्वारा व्यापार को बतौर हथियार इस्तेमाल किये जाने (जिसकी मार ऑस्ट्रेलिया भी सह रहा है) के बाद से, ऑस्ट्रेलिया अपने निर्यात बाज़ार का विविधीकरण कर चीन पर अपनी व्यापारिक निर्भरता घटाना चाह रहा है.
पहले, व्यापार को भू-राजनीतिक तनाव घटाने के साधन के रूप में देखा जाता था. ‘आओ हम ज़्यादा व्यापार करें और दोस्त बन जाएं’ – अतीत का मंत्र था. आज, वह दौर आ गया है जहां देश केवल दोस्तों और समान सोच वाले देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं. व्यापार और तकनीक के एजेंडे को भू-राजनीति चला रही है, और यह हिंद-प्रशांत में भू-राजनीतिक एजेंडे का सम्मिलन (कन्वर्जेंस) है, जिसकी वजह से भारत-ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं. हिंद-प्रशांत समुद्री भूगोल वह धुरी है जिसके इर्द-गिर्द नई दिल्ली और कैनबरा अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं का नक्शा खींच रहे हैं. भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के बतौर, बैरी ओ’फैरेल ने अकाट्य ढंग से कहा है, ‘हमारा (भारत और ऑस्ट्रेलिया का) भूगोल हमें सीधे दुनिया के रणनीतिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बीचोबीच रखता है. और जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ज़्यादा बहु-ध्रुवीय होती जायेगी, क्षेत्र की दृढ़ता की परीक्षा होगी.’ ओ’फैरेल के मुताबिक़, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक शांतिपूर्ण और समावेशी हिंद-प्रशांत, जहां सभी राष्ट्रों के अधिकारों का उनके आकार की परवाह किये बग़ैर सम्मान किया जाता है, सुनिश्चित करने की साझा ज़िम्मेदारी स्वीकार की है.
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध पिछले कुछ सालों में तेज़ी से विकसित हुए हैं. दोनों राष्ट्रों ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट पर दस्तख़त किये हैं, जो दोनों को एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देता है और सैन्य साझेदारी बढ़ाता है.
यूक्रेन संकट पर मतभेदों के बावजूद, भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने रिश्ते में ऊपर की दिशा में गति बनाये रखने को अब भी प्रतिबद्ध हैं. नई दिल्ली और कैनबरा जब तक अपने भू-राजनीतिक खेल को और ऊपर नहीं ले जाते हैं, एक बहुध्रुवीय हिंद-प्रशांत मृगतृष्णा (छलावा) ही बना रहेगा. यह दिलचस्प है कि इस बारे में जो सहमति अभिजात्य वर्ग के स्तर पर रही है, अब वह नीचे के स्तर पर भी पहुंच रही है. जैसाकि, एक हालिया रायशुमारी आंकड़ा दिखाता है कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में जनता एक-दूसरे को ‘भरोसेमंद’ साझेदार के रूप में देखती है. क्षेत्रीय परिवेश को आकार देने की एक-दूसरे की क्षमता में यह विश्वास, जिससे दोनों अग्रणी साझेदार के बतौर उभर रहे हैं, उस तौर-तरीक़े के चलते है जिसमें दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व इस साझेदारी को हिंद-प्रशांत के भविष्य को आकार देने के लिए अत्यावश्यक समझता है. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध पिछले कुछ सालों में तेज़ी से विकसित हुए हैं. दोनों राष्ट्रों ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट पर दस्तख़त किये हैं, जो दोनों को एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देता है और सैन्य साझेदारी बढ़ाता है. दोनों देशों ने 2020 में अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक भी बढ़ाया, जो ‘आपसी समझ-बूझ, भरोसे, साझा हितों, और क़ानून के शासन व लोकतंत्र के साझा मूल्यों’ पर आधारित है. यह ‘समावेशी वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा समर्थित खुले, मुक्त, नियम-आधारित हिंद-प्रशांत’ को बढ़ावा देने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी संलग्नता मज़बूत करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है. यह व्यापक रणनीतिक साझेदारी अपने भीतर नियमित उच्चस्तरीय राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य संलग्नता को समेटे हुए है, जिसका नतीजा विभिन्न स्तरों पर भरोसे में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होना है.
चीन द्वारा आक्रामक नीति दिखाना निस्संदेह एक अहम कारक रहा है, जिसने दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय दायरे के मामले में ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है. चीन की बढ़ती दावेदारियों के बीच, समान सोच वाले राष्ट्रों के बीच निकट सहयोग को गति मिली है. वर्षों से, चीन के संबंध में भारत फूंक-फूंक कर क़दम रखने की कोशिश करता रहा है. लेकिन अब हिसाब बदल गया है. समान सोच वाले देशों के साथ हाथ मिलाना और चीन के ख़िलाफ़ एक ज़्यादा सख़्त रवैया इख़्तियार करना अब कोई रैडिकल बात नहीं लगती. ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए, एक ‘मुक्त और खुला’ हिंद-प्रशांत क्षेत्र हासिल करने के लिए ज़्यादा मज़बूत साझेदारी बेहद ज़रूरी है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे समान सोच वाले देशों के बीच मज़बूत द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को आकार देने के लिए बेहद अहम बने रहेंगे.
हिंद-प्रशांत में महत्वपूर्ण संस्थानिक विकास भी हुए हैं. इनमें सबसे पहले है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्वॉड को सर्वोच्च नेताओं के स्तर तक ले जाना. 2007 में जब एक चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) की शुरू में कल्पना की गयी, तो नई दिल्ली और कैनबरा दोनों ही इस तरह के मंच में पूरे दिल से लगने के इच्छुक नहीं थे. लेकिन जब 2007 से 2017 के दौरान चीनी दावेदारी नियंत्रण से बाहर हो गयी, तो क्वॉड का पुनरुत्थान हुआ और तब से, यह एक नाटकीय उदय की कहानी है. अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के लिए, क्वॉड साझा लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रेखांकित करने का एक मंच उपलब्ध कराता है. ये लक्ष्य हैं : एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जहाज़ों के गुज़रने की आज़ादी, और क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा. क्वॉड का उदय, सदस्य देशों के भीतर भी और उससे परे भी, ‘हिंद-प्रशांत’ की एक रणनीतिक अवधारणा के रूप में स्वीकृति का संकेत है. आज, क्वॉड क्षेत्र की बड़ी शक्तियों द्वारा सोच में परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करता है. और, कोविड, जलवायु संकट, बेहद अहम तकनीकों के अभाव तथा आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए क्वॉड का एजेंडा आज काफ़ी विस्तृत है. इसके लिए वह सदस्य देशों की विशिष्ट क्षमताओं को एक जगह ला रहा है और भविष्य का क्वॉड गढ़ रहा है. मुद्दे आधारित गठबंधन, जो औपचारिक गठबंधनों की बनिस्बत अपने स्वभाव में ज़्यादा लचीले, उद्देश्य आधारित और राजनीतिक हैं, हिंद-प्रशांत में जैसे-जैसे अपनी छाप छोड़ेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे समान सोच वाले देशों के बीच मज़बूत द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को आकार देने के लिए बेहद अहम बने रहेंगे. अपने हालिया व्यापारिक समझौते के साथ, नई दिल्ली और कैनबरा ने संकेत दे दिया है कि वे अपनी भूमिका को गंभीरता से ले रहे हैं.
ओआरएफ हिन्दी के साथ अब आप Facebook, Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं. नए अपडेट के लिए ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. हमारी आधिकारिक मेल आईडी [email protected] के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +