-
CENTRES
Progammes & Centres
Location

89 उपन्यास लिखने वाले प्रतिभाशाली लुई लामोर ने कई बार लिखा है कि बंदूक से लड़ने वाले के लिए सिर्फ़ फ़ुर्तीला होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सटीक निशाना लगाना भी आना चाहिए; तो वो इत्मीनान से बंदूक निकाले, सावधानी से निशाना लगाए और उसके बाद ही ट्रिगर दबाए. अक्सर जल्दबाज़ी में नीतियों का ट्रिगर दबाने वाले वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को शायद लामोर से सबक़ सीखने की ज़रूरत है. पिछले तीन महीनों में जिन तीन नीतियों का ऐलान किया गया है- इनमें से दो तो पिछले एक हफ़्ते के दौरान घोषित की गई- ने ऐसी छवि बनाई है कि भारत में नीति निर्माण, पहले गोली दाग़ने और फिर निशाना साधने के सिद्धांत पर किया जाता है. अचानक किसी नीति का ऐलान करके हैरान करने का नुस्खा तभी चलता है, जब सारी संभावित कमज़ोरियों (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन-धन योजना इसकी मिसाल है) को पहले ही दूर कर लिया जाए, न कि जल्दबाज़ी में की गई घोषणा के बाद किया जाए.
16 मई को वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया कि लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस योजना के तहत क्रेडिट और डेबिट कार्ड से छोटे लेन-देन के लिए भी 20 प्रतिशत टैक्स स्रोत पर काटा जाएगा. इस नीतिगत घोषणा पर हंगामा मच गया. जिसके बाद, नीति में संशोधन करते हुए, सात लाख रुपए तक के लेन-देन के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए जाने ख़र्च को इस टैक्स से छूट देने की सफ़ाई पेश की गई. इस दौरान सरकार, बिना सोचे समझे चले गए अपने ही चले दांव से बचती और चकराई हुई नज़र आई. सुरजीत भल्ला ने लिखा कि, ‘सरकार फ़ौरन इस अनुदार रेमिटेंस पॉलिसी को वापस ले: भारत की बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा विदेश में किए गए ख़र्च पर लगाया गया 20 प्रतिशत टैक्स, अपने ताज़ा बदलाव के बाद भी पीछे की ओर लौटने वाला क़दम है, और इससे न तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और न ही राजस्व बढ़ेगा.’
विदेश में ख़र्च पर 20 प्रतिशत टैक्स लगाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि 19 मई को रिज़र्व बैंक ने ऐलान किया कि दो हज़ार रुपए के नोट चलन से वापस लिए जाएंगे. हालांकि इनकी वैधता बनी रहेगी. रिज़र्व बैंक का ये क़दम नोटबंदी है या नहीं, इस पर तो अब अदालतों में बहस होगी. लेकिन, जो बात पक्के तौर पर हुई है वो ये है कि इससे रिज़र्व बैंक, जिसने हाल ही में आए दो संकटों (मेड इन चाइना कोविड-19 महामारी और मेड इन रशिया/NATO के यूक्रेन संघर्ष के दौरान) के दौरान बहुत शानदार काम किया था, उसकी विश्वसनीयता को भारी चोट ज़रूर पहुंची है. अगर किसी इंसान के पास ज़रा भी अक़्ल है, तो वो इस क़दम को ज़ायज़ ठहराने के लिए दिए गए रिज़र्व बैंक के ‘क्लीन नोट्स’ के तर्क पर विश्वास नहीं करेगा. जनता से कहा गया कि वो ‘इस वक़्त लागू दिशा-निर्देशों और अन्य नियम क़ायदों के मुताबिक़’ अपने दो हज़ार के नोट बैंकों में जमा कराएं. इसके साथ साथ बैंकों से कहा गया कि दो हज़ार के नोट जमा कराने आने वालों के KYC (अपने ग्राहक को जानो) नियमों का पालन किया जाना चाहिए. एक और हंगामा बरपा और तीन दिन बाद रिज़र्व बैंक ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें दो हज़ार के नोट जमा कराने के लिए KYC के नियमों का पालन करने की शर्त हटा दी गई थी. ज़ाहिर है कि इस चक्कर में रिज़र्व बैंक ने काला धन रखने वालों को पकड़ने का एक मौक़ा गवां दिया.
दो महीने पहले मार्च 2023 में केंद्रीय बजट ने डेट (Debt) म्युचुअल फंड को दिया जाने वाला इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया था. इससे किसको फ़ायदा होगा? कारोबारी बैंकों को. इसमें किसका नुक़सान है? वो निवेशक जो डेट (Debt) फंड में निवेश करने का जोखिम लेते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय को जोखिम वाली सुरक्षा और बिना किसी ख़तरे वाले फिक्स्ड डिपॉज़िट के बीच का फ़र्क़ नहीं पता. जिसमें ज़्यादा जोखिम होगा, उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होगी, और उस उत्पाद में नुक़सान होने का ख़तरा भी शामिल होगा. इसके लिए हम वित्त मंत्रालय को दोष नहीं दे सकते. क्योंकि इसके बड़े अधिकारी अभी भी ख़ज़ाने से मिलने वाले वेतन, भत्तों और महंगाई के हिसाब से बढ़ने वाली पेंशन पर जी रहे हैं, जो उनके और उनके जीवनसाथी के लिए पर्याप्त है. इसके अलावा उन्हें पूरी ज़िंदगी देश की बेहतरीन और कई मामलों में तो विश्व की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होती है. मोनिका हालान ने लिखा कि, ‘ये जो संशोधन किया गया है, वो बाज़ार के लिए बहुत ख़राब संकेत है. ख़ास तौर से जोखिम लेने वाले उन लोगों के लिए जो बाज़ार से जुड़े डेट मार्केट उत्पादों में निवेश का मन बना ही रहे थे.’
इससे क्या संकेत मिलता है? भारत, धीरे धीरे शायद यूपीए के दौर वाली नीतिगत अनिश्चितता वाले दौर की ओर लौट रहा है. अगर सरकार काला धन पकड़ने के लिए दो हज़ार के नोट को बंद करना चाह रही है, तो ये एक नेक मक़सद है. फिर ख़राब नीति और चकरा देने वाले संदेश से इस पर शक क्यों पैदा करना? अगर सरकार ज़्यादा टैक्स जुटाना चाहती है, तो बख़ूबी कर सकती है- भारत पहले भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का क़हर झेल चुका है- लेकिन बिना सोचे समझे क्यों? ईमानदार करदाता तो इस नीतिगत ज़ुल्म को भूलकर, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और वो किसी अगली बड़ी चीज़ पर अपना ध्यान लगाएंगे; वहीं, भ्रष्ट लोग बच निकलने के नए तरीक़े निकाल लेंगे. लेकिन, भ्रष्ट लोगों के जुर्म की सज़ा, ईमानदार करदाताओं को देने के लिए सरकार नई नीतियों का दांव आज़माए, उससे पहले उसके लिए पेश है आठ बिंदुओं की वो टूलकिट, जिसकी मदद से सरकार आर्थिक नीति निर्माण को जांचने परखने के बाद लागू करे.
सरकार के अधिकारी जो अधिसूचनाएं या नियम जारी करते हैं, उस पर चुनावों का सामना करने वालों की निगरानी नहीं होती. ये व्यवस्था संविधान में निहित है. किसी भी लोकतंत्र में क़ानून बनाने का काम संसद और विधानसभाएं करती हैं. जबकि, उस क़ानून से जुड़े बारीक़ नियम क़ायदे वो अधिकारी बनाते हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, और उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती. मिसाल के तौर पर उपरोक्त तीन नीतियों का दोष, बात बात पर नियमों का हवाला देने वाले ‘ब्यूरोक्रेट’ पर मढ़ा जा रहा है. लेकिन, सियासी तौर पर देखें तो आरोपों की बौछार का सामना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को करना पड़ रहा है. इसे बदलने की ज़रूरत है और इनके मातहत अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी.
भारत को नीतिगत दस्तावेज़ की एक प्रक्रिया तय करने की ज़रूरत है. इस प्रक्रिया में उस समस्या की सटीक परिभाषा तय करना भी शामिल होगा, जिसके निदान के लिए कोई क़ानून, नियम या अधिनियम बनाया जा रहा हो. उदाहरण के तौर पर सभी क़ानूनों का एक ‘छोटा शीर्षक’ होता है. 2017 के गुड्स ऐंड सर्विसेज़ टैक्स का शीर्षक इस प्रकार है: ‘राज्यों के बीच सेवाओं और सामान की आपूर्ति और उनसे जुड़े या उनके कारण पैदा होने वाले मसलों पर केंद्र द्वारा टैक्स लगाने और जमा करने का क़ानून.’ इन पंक्तियों के पीछे वाद-विवाद और परिचर्चाओं के दस्तावेज़ का विशाल भंडार है. नीति निर्माण की प्रक्रिया को भी यही नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है.
सरकार द्वारा बनाए जाने वाले क़ानूनों या नीतियों के बाद कुछ नाकामियां भी देखने को मिलती है. ये बाज़ार की असफलता हो सकती है; मिसाल के तौर पर 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाने से पहले शेयरों के कारोबार में पारदर्शिता की कमी. ये एक सामाजिक असफलता भी हो सकती है; उदाहरण के लिए, महिलाएं केवल 25 प्रतिशत म्युचुअल फंड की मालिक हैं. इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए एक नीति की ज़रूरत है. ये कोई विनियामक नाकामी भी हो सकती है; जैसे कि, भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे लोगों को बेचे जा रहे घटिया उत्पादों से ग्राहकों को सुरक्षित बनाने में नाकामी. ऐसी असफलताओं को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए: कोई नीतिगत बदलाव कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है?
क़ानून बनाने से लेकर नियम में बदलाव तक हर नीति को चाहिए कि वो अपनी असफलता को ज़ाहिर करे. आज आंकडों से भरपूर दुनिया में ये काम आसानी से हो सकता है. डिस्क्लोज़र्स के बारे में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक स्टडी उस विश्लेषण पर आधारित थी जिसमें पाया गया था कि वित्त वर्ष 2022 में फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) के शेयरों का कारोबार करने वाले 10 में से 9 (89 प्रतिशत) लोगों को लगभग 1.1 लाख रुपए का औसत नुक़सान हुआ था. इस सूचना को सामने रखे जाने से नियमों में बदलाव का सफर ज़रूरत बन गया. आंकड़ों और उनके विश्लेषण पर आधारित नीतियां उनसे तो कई गुना बेहतर होती हैं, जो बस फ़ौरी तौर पर अच्छा माहौल बनाने के लिए बनाई जाती हैं.
लेकिन, इतना भी पर्याप्त नहीं है. एक ही आंकड़ा और उसके विश्लेषण से अलग अलग नीतिगत समाधान निकाल सकते हैं. ऊपर हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन में नुक़सान के नतीजों को देखते हुए, तीन विकल्प हो सकते हैं. पहला, निवेशकों के लिए मौद्रिक बाधा तय करें: जैसे कि केवल वही लोग F&O में निवेश कर सकते हैं, जिनके पास पांच करोड़ रुपए से ज़्यादा की वित्तीय संपत्ति हो. दूसरा, दलालों के इस क्षेत्र में दाख़िले के लिए शर्त लगा दें: वही शर्त मगर जिसमें जवाबदेही ब्रोकर्स की हो. और तीसरा, डिसक्लोज़र को बढ़ावा दें: ये मानकर चलें कि निवेशकों को ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें सतर्क करें. इस समस्या का समाधान इन तीनों में से किसी भी एक विकल्प से हो सकता है. लेकिन, सबसे कम लागत और सबसे ज़्यादा असरदार प्रक्रिया का पता लगाना नीति निर्माताओं की ज़िम्मेदारी है.
TCS के साथ क्या होगा? कितना पैसा जमा किया जाएगा और जो लोग पहले ही टैक्स अदा कर चुके हैं, उनको कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे? क्या ये टैक्स लगाने का वाक़ई कोई फ़ायदा होगा? क्या इससे होने वाले लाभों की तुलना में विदेश यात्रा पर जाने वाले हर नागरिक पर ये बोझ लादना फ़ायदेमंद है? फिर चाहे वो अपने बच्चे के विदेश में रहने का ख़र्च उठा रहा हो (शिक्षा के मामले में छूट है), या फिर विदेशी धरती पर स्वास्थ्य की किसी समस्या से जूझ रहा हो. अगर इस मामले में प्रशासनिक निवेश की तुलना में मौद्रिक लाभ नहीं है, तो ये बताएं कि TCS से भारी-भरकम और चोरी-छुपे किए गए लेन देन का पता किस तरह लगाया जाएगा? अगर इस नीति से यह उम्मीद है कि ऐसे कम से कम हज़ार लोग ही पकड़े जा सकेंगे, तो ये बात बताएं और इस नीति को वाजिब ठहराएं, जिससे लोग इसका समर्थन कर सकें. अन्यथा, कोई दूसरा विकल्प तलाश करें.
आम तौर पर ये माना जाता है कि निर्वाचित मंत्री और चुनिंदा अफ़सरों के पास ही सारी अक़्ल है. ऐसा कभी था नहीं और 21वीं सदी में तो इस सोच को ज़ोर-शोर से ख़ारिज कर दिया जाएगा. एक बार जब आंकड़े जुटा लिए जाएं, विश्लेषण कर लिया जाए और नीतिगत विकल्प तय हो जाएं, तो फिर नीतिगत प्रस्तावों को टिप्पणी के लिए देश के सामने रखें, ताकि दूसरे पक्ष के लोग भी उस पर अपनी राय दे सकें. चौंकाने वाला फ़ैसला किसी को पसंद नहीं आता- न तो सरकार को, न कंपनियों को और न ही नागरिकों को. फिर कहना होगा कि इस मामले में SEBI शानदार काम कर रही है. सेबी ने म्यूचुअल फंड पर एक कंसल्टेशन पेपर जनता के सामने ऑनलाइन रखा है, ताकि निवेश के इन साधनों को निवेशकों अधिक कुशल बनाया जा सके. लोग इस पर 1 जून 2023 तक अपनी राय दे सकते हैं. 21वीं सदी में नीतियों को उनसे प्रभावित होने वालों के मुंह पर दे मारना, वैसा ही अहंकार मालूम होता है, जैसा 1947 से पहले के दौर में था. ये बात सही है कि आज़ाद भारत की व्यवस्था, औपनिवेशिक मालिकों की नक़ल करके ही तैयार की गई है. लेकिन, अब जनता इसे स्वीकार करने वाली नहीं है. लोगों की नाराज़गी भुगतने से बेहतर है उन्हें सलाह मशविरे का हिस्सा बना लिया जाए. दो हज़ार के नोट वापस लेने जैसे संवेदनशील मसले जिन्हें गोपनीय रखने की ज़रूरत है, उन्हें इसके दायरे से अलग रखा जाए.
ख़राब नीतियां बनाना आसान है. मगर, उन्हें लागू करना कहीं अधिक चुनौती भरा काम है. इसके बीच में वो भ्रष्ट आर्थिक एजेंट होते हैं, जो ख़राब सरकारी नीतियों का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने के लिए करते हैं. देश में लाइसेंस परमिट का राज तो 1991 में औद्योगिक नीति पर बयान के साथ ही ख़त्म होने लगा था. लेकिन, देश में इंस्पेक्टर राज अभी भी बना हुआ है. ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक स्टडी के मुताबिक़ देश में कारोबारियों को कुल मिलाकर 69,233 नियमों का अनुपालन करना पड़ता है; इनमें से 26,134 अनुपालन ऐसे हैं, जिनका उल्लंघन पर जेल जाना पड़ सकता है. लेकिन, आज अगर देश की जेलें कारोबारियों से नहीं भर रही हैं, तो ज़ाहिर है, ये फ़ासला रिश्वत देकर पाटा जा रहा है. ये ख़राब नीतियां हैं, जिनमें से कुछ को जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2022 के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा. अभी ये विधेयक लागू होने का इंतज़ार कर रहा है. आगे चलकर ये सरकार और नियामकों की ज़िम्मेदारी होगी कि वो अनुपालन की पूरी राह का ख़ाका बनाएं और उसे जनता को बताएं.
मेहनतकश और ईमानदार करदाताओं पर ख़राब नीतियों और आलसी नीति निर्माण का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए. नाम ज़ाहिर करके शर्मिंदगी का जुर्माना या नाम बताकर गर्व करने का प्रोत्साहन देने जैसा कोई उपाय लागू करना चाहिए. तयशुदा सेवाकाल वाले अफ़सरों की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए. उन्हें गुमनामी और ग़ैर-जवाबदेह सेवा प्रदाताओं के नाम पर बच निकलने और छिपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. अन्यथा हर नीति का ठीकरा संगठन के प्रमुख के सिर पर फूटेगा. जैसे कि वित्त मंत्रालय की टैक्स संबंधी भयंकर ग़लतियों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को और दो हज़ार के नोट वापस लेने या फिर नोटबंदी के लिए रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत को दोषी ठहराया गया. इसी तरह F&O के निवेशकों के डिसक्लोज़र का सारा श्रेय सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को दिया जाएगा. उत्तरदायित्व का लोकतांत्रीकरण करने की ज़रूरत है और इसे लागू किया जा सकता है.
आज जब भारत इसी दशक के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ़ आगे बढ़ रहा है, तो नियम-क़ायदों को इस सफ़र के साथ साथ ही चलना होगा. उन्हें पूंजी को नुक़सान पहुंचाए बिना उनका नियमन करना होगा. उन्हें बिना शोर-शराबे के कंपनियों का नियमन करना होगा. उन्हें ईमानदार लोगों को परेशान किए बग़ैर अपराधियों को पकड़ना होगा. हमारी जानकारी के मुताबिक़ भविष्य के लिहाज़ से ज़रूरी ये मानक तय करने में SEBI की भूमिका एक बाहरी की है. वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक को ख़ास तौर पर और दूसरे मंत्रालयों और नियामक संस्थाओं को आम तौर पर सीखना, ख़ुद को ढालना और उम्मीदों पर ख़रा उतरना होगा.
और सबसे बड़ी बात, बिना निशाना लगाए तीर चलाने से बचें.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
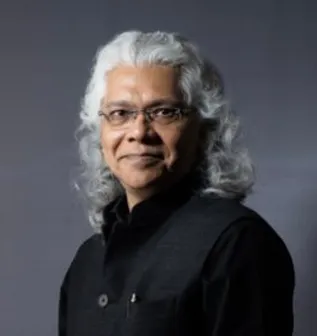
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +