-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
अमेरिकी प्रतिबंधों ने अनायास ही चीन को अपने अनुसंधान व विकास और नवाचार में तेज़ी लाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे वह अब पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने लगा है.
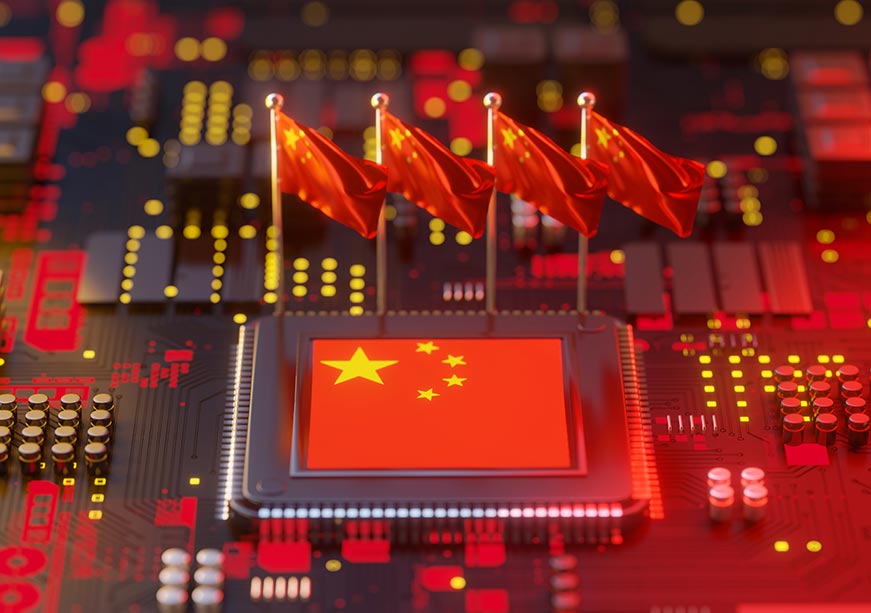
Image Source: Getty
विश्व प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका ‘नेचर’ ने अपने सूचकांक में बताया है कि चीन के एक क्षेत्रीय विश्वविद्यालय सिचुआन यूनिवर्सिटी (एससीयू) ने हाल ही में वैज्ञानिक शोध के मामले में स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, ऑक्सफ़ोर्ड और टोक्यो यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष 11वां स्थान हासिल किया है. सूचकांक में शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेखों के आधार पर किया गया है. 'नेचर' ने इसके लिए पांच विषय तय किए थे, जो हैं- जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान.
भले ही इस सूची में हार्वर्ड सबसे ऊपर है, लेकिन एससीयू से पहले के सभी नौ विश्वविद्यालय भी चीन के ही हैं. पिछले दिनों चीन को इसलिए दुनिया भर में सुर्ख़ियां मिली थी, क्योंकि उसने ओपेन-सोर्स एआई मॉडल डीप-सीक बनाया है, पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ताकतवर बनने के लिए उसने अपने कदम पिछले दशक में ही तेज़ कर दिए थे.
इसी क्रम में, एससीयू जैसे विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए विशेष उपाय किए. इन उपायों में शामिल था- उच्च-स्तरीय शोधकर्ताओं को आकर्षित करना, पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना, उद्योग-विश्वविद्यालय साझेदारी को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान व सहयोग को गति देना. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय ने दर्जनों देशों व क्षेत्रों से 5,000 से अधिक श्रेष्ठ शोधकर्ताओं को बुलाया और सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जापान व दक्षिण कोरिया जैसे देशों में प्रचार अभियान चलाए. वर्ष 2008 से चीन ‘थाउजेंड टैलेंट प्रोग्राम’, यानी हजार प्रतिभा कार्यक्रम नामक अभियान चला रहा है, जिसका मक़सद विदेशों में रहने वाले चीनी और गैर-चीनी वैज्ञानिकों को पर्याप्त पैसे देकर चीन में काम करने के लिए बुलाना है.
पिछले महीने, चाहे इरादतन हो या संयोगवश, हम चीन की तकनीक़ी उपलब्धियों से जुड़ी खबरों में डूबते-उतरते रहे हैं. हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं कि महीने के अंत में चीन द्वारा कथित तौर पर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना लिए जाने संबंधी खबरों का मक़सद अपना रुतबा दिखाना था. इन विमानों की तस्वीरें काफी कम ऊंचाई पर खींची गई थीं और संभवतः अमेरिका में माहौल बनाने के लिए इन तस्वीरों को जारी किया गया था. इसी तरह, डीप-सीक आर1 चैटबॉट एप भी प्रभावित करने के लिए लांच किया गया, जो लांच के तुरंत बाद एपल के एप स्टोर से सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मुफ़्त एप बन गया. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि डीप-सीक कंपनी शायद ही अपने चैटबॉट लांच को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकती थी.
पिछले तीन वर्षों में, अमेरिका ने न सिर्फ अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप तक चीन की पहुंच को सीमित करने का काम किया है, बल्कि इन चिप को बनाने के लिए जिन विशेष उपकरणों की ज़रूरत होती है, उनको भी चीन तक नहीं पहुंचने दिया है.
पिछले तीन वर्षों में, अमेरिका ने न सिर्फ अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप तक चीन की पहुंच को सीमित करने का काम किया है, बल्कि इन चिप को बनाने के लिए जिन विशेष उपकरणों की ज़रूरत होती है, उनको भी चीन तक नहीं पहुंचने दिया है. इसका मक़सद था लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी बड़े भाषा मॉडल विकसित करने की चीन की क्षमता को प्रभावित करना. डीप-सीक ने कहा भी है कि उसके मॉडल को एनवीडिया एच800 चिप पर प्रशिक्षित किया गया था. एनवीडिया एच800 एक एआई चिप है, जिसको एनवीडिया ने प्रतिबंध के बाद ख़ास तौर से चीनी बाजार के लिए विकसित किया है.
हालांकि, एच800 पर भी 2024 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन ऐसा होने से पहले ही कंपनी ने हजारों चिप जमा कर लिए थे. डीप-सीक ने दावा किया है कि उसके मॉडल में जो चिप लगी हैं, वह पश्चिमी देशों में समान प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाली महंगी चिप की तुलना में काफ़ी कम कीमत की हैं. इस दावे पर विश्वास इससे भी होता है कि उसने एक वैज्ञानिक शोध-पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यह मॉडल कैसे बनाया गया और इसकी कम लागत किस तरह से सस्ते एआई मॉडल के निर्माण को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा.
वैसे, अमेरिका ने तो हाल के महीनों में अपने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है, पर अब उसने एआई चिप पर अमेरिकी नियंत्रण बढ़ा दिया है. उसने सभी देशों को तीन हिस्सों में बांटा है- पहले में अमेरिका और उसके 18 सहयोगी व साझेदार राष्ट्र हैं, जैसे- ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन आदि। दूसरे हिस्से में जिन देशों को रखा गया है, वहां निर्यात की जाने वाली चिप की संख्या तय कर दी गई है, साथ ही लाइसेंस और ‘एंड-यूजर सर्टिफिकेट’ को अनिवार्य बना दिया गया है, यानी यह सुनिश्चित किया गया है कि चिप खरीदने वाला ही इसका इस्तेमाल करेगा, उसे किसी दूसरे को नहीं बेचेगा. चीन और भारत को इसी समूह में रखा गया है. तीसरा स्तर उत्तर कोरिया, इराक, ईरान और रूस जैसे देशों का है, जिनको किसी भी कीमत पर तकनीक़ नहीं दी जाएगी.
मेड इन चाइना
उल्लेखनीय है कि चीन शुरू से ही अपने यहां प्रमुख तकनीकों का ‘पुनर्निर्माण’ या पुनर्विकास करने की कोशिश करता रहा है, फिर चाहे उसे वह तकनीक़ जिस भी तरह से मिली हो- चाहे वह खरीदी गई हो, चोरी की गई हो या विदेशी कंपनियों को मजबूर करके हासिल की गई हो. इसका शुरुआती उदाहरण हाई-स्पीड रेल (एचएसआर) तकनीक़ है. अपने देश में एचएसआर तकनीक़ विकसित करने में विफल रहने के बाद 2002 से 2008 के दौरान चीन ने चार बड़े अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं- कावासाकी, बॉम्बार्डियर, एल्सटॉम और सीमेंस के साथ समझौते किए. इन समझौतों के तहत कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे अपनी तकनीक़ चीनी साझेदारों के साथ साझा करेंगी.
इसका नतीजा यह हुआ कि साल 2009 तक चीन को एचएसआर तकनीक़ के कई पहलुओं की जानकारी मिल गई, जिनमें डिजाइन, विनिर्माण प्रक्रिया, परिचालन संबंधी तंत्र आदि शामिल थे. इसके साथ-साथ, चीन ने 500 कंपनियों व 25 विश्वविद्यालयों को जोड़ते हुए एक व्यापक घरेलू आपूर्ति शृंखला बनाई और चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी (सीआरआरसी) का गठन किया, जिसका मक़सद तकनीक़ व प्रौद्योगिकियों के प्रसार का प्रबंधन करना था. आज स्थिति यह है कि विश्व में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का 60 फ़ीसदी हिस्सा चीन में है.
वैसे तो चीन की नीति हमेशा ही स्वदेशी तकनीक़ को बढ़ावा देने की रही है, लेकिन 2015 में और उसके आसपास, उसने पर्यावरण हितैषी और अभिनव तकनीक़ पर ज़ोर देने के लिए ‘मेड इन चाइना’ योजना शुरू की, जो काफी सफल रही और चीनी कंपनियां कई उद्योगों में शीर्ष स्थान पर पहुंच गईं. पिछले अक्टूबर में ब्लूमबर्ग की एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने पांच प्रमुख प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता हासिल कर ली है, जो हैं- यूएवी, सौर पैनल, ग्राफीन, हाई-स्पीड रेल और इलेक्ट्रिक वाहन व बैटरी. साथ ही, उसने कंप्यूटर चिप, एआई, रोबोट, मशीनी औजारों, बड़े ट्रैक्टर, दवा और एलएनजी जहाजों जैसी प्रौद्योगिकियों में भी बड़े देशों को ‘टक्कर’ देने की क्षमता विकसित कर ली है.
वैसे तो चीन की नीति हमेशा ही स्वदेशी तकनीक़ को बढ़ावा देने की रही है, लेकिन 2015 में और उसके आसपास, उसने पर्यावरण हितैषी और अभिनव तकनीक़ पर ज़ोर देने के लिए ‘मेड इन चाइना’ योजना शुरू की, जो काफी सफल रही और चीनी कंपनियां कई उद्योगों में शीर्ष स्थान पर पहुंच गईं.
कुछ तकनीक़ी श्रेष्ठताएं इस सूची में शामिल नहीं हैं, जिनमें से एक है क्वांटम तकनीक़, जिसके बारे में ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने बताया है. अखबार बताता है कि ‘क्वांटम संचार में चीन आज निश्चय ही सबसे ऊपर है’, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में अमेरिका काफी आगे है और क्वांटम सेंसिंग में दोनों देश ‘एक दूसरे के बराबर’ हैं.
दूसरा क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी तकनीक़, कृषि जैव प्रौद्योगिकी और जैव-विनिर्माण में प्रगति शामिल है. अमेरिका बुनियादी या मूलभूत अनुसंधान में आगे है, जबकि चीन का ज़ोर उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में है.
पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली उन्नत सामग्रियों, डाटा रिकॉर्ड रखने वाले ब्लॉकचेन, स्मार्ट उपकरणों को एक-दूसरे व क्लाउड से जोड़ने वाली तकनीक़ इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, एडिटिव मैन्युफ़ैक्चरिंग (थ्रीडी प्रिटिंग), स्वच्छ ऊर्जा तकनीक़, अंतरिक्ष तकनीक़, 5जी और दूरसंचार जैसे अन्य क्षेत्रों में भी चीन आगे है.
यहां तक कि डीप-सीक ने तुलनात्मक रूप से कम सक्षम चिप का उपयोग करते हुए जो सफलता हासिल की है, वह संकेत है कि यदि उसके पास उच्च-क्षमता की चिप होती, तो वह कहीं बेहतर मॉडल बना सकती थी. यह सब देखकर समझा जा सकता है कि आखिर क्यों चीन की तकनीक़ी तरक्की को अमेरिका धीमा करना चाहता है. हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंधों का उलटा प्रभाव भी पड़ रहा है और चीन को अपने अनुसंधान और विकास-प्रयासों व नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए इससे प्रेरणा मिल रही है, जिसका दुष्प्रभाव अमेरिका पर लंबे समय तक पड़ सकता है.
बहरहाल, चीन ने अब अपने ‘मेड इन चाइना’ या ‘थाउजेंड टैलेंट प्रोग्राम’ के बारे में दावे करना अब बंद कर दिया है, ताकि दुनिया का ध्यान इस तरफ न जाए.
बहरहाल, चीन ने अब अपने ‘मेड इन चाइना’ या ‘थाउजेंड टैलेंट प्रोग्राम’ के बारे में दावे करना अब बंद कर दिया है, ताकि दुनिया का ध्यान इस तरफ न जाए. उसकी यह रणनीति तीन हिस्सों में बंटी है- पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित प्रौद्योगिकियों की नकल करना, युवा और उत्पादक वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं का बड़ा समूह बनाना, और तीसरा, पूरी तरह से उन नई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान लगाना, जिनमें पश्चिम के पास उस तरह का नेतृत्व नहीं है, जैसे कि फ़ोटोनिक कंप्यूटिंग, मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफ़ेस, परमाणु संलयन और टेलीमेडिसिन आदि.
(मनोज जोशी ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में प्रतिष्ठित फ़ेलो हैं)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +