-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारत में जिस प्रकार चीनी उद्योगों (ईवी के साथ-साथ उद्योगों) के स्थानांतरित होने का सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा है, कुछ चीनी रणनीतिकारों का मानना है कि जो वैश्विक हालात हैं, उनमें ऐसा होना लाज़िमी है.
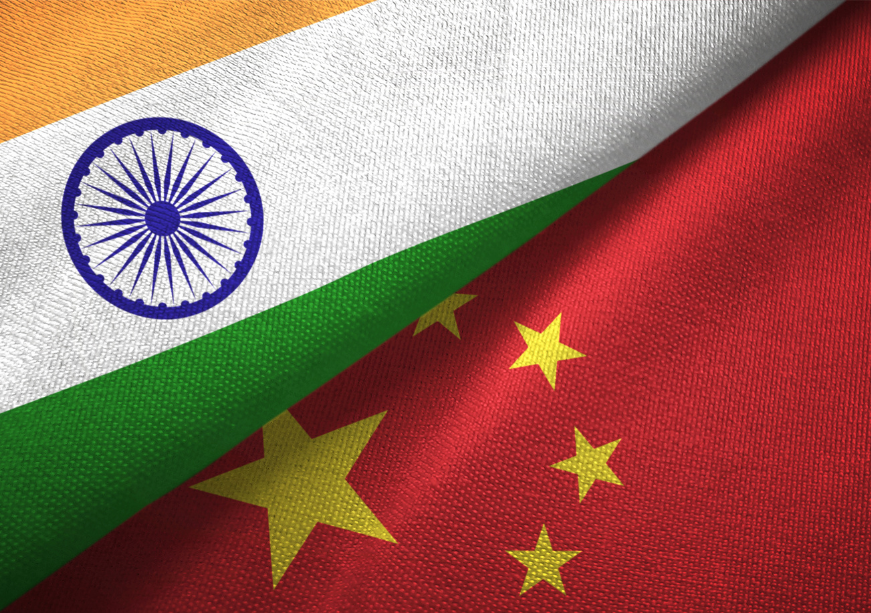
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की सत्ता पर तीसरी बार वापसी हो चुकी है. इसके बाद से ही चीनी मीडिया और वहां के सोशल मीडिया पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी द्वारा किए गए बड़े-बड़े वादों व दावों का मुद्दा छाया हुआ है. चीन में इस बात की चर्चा ज़ोरों पर है कि क्या "मोदीनॉमिक्स 3.0" अपने वादों को हक़ीक़त में बदल पाएगा. यानी चर्चा हो रही है कि आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी दोगुना करने के वादों को पीएम मोदी क्या पूरा कर पाएंगे.
मोदी को इन परिस्थितियों में भूमि, श्रम और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों की गति को न केवल धीमा करना पड़ सकता है, बल्कि इससे भारतीय विनिर्माण सेक्टर का विकास भी बाधित हो सकता है.
आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने तीसरी बार सत्ता में आने पर भारत की अर्थव्यवस्था शीर्ष पर ले जाने और भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने जैसे तमाम वादे किए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी वादा किया था कि अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट को चीनी बाज़ार का विकल्प बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करेंगे और इसके लिए कई नीतिगत क़दम उठाएंगे. हालांकि, आज नरेन्द्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसके बावज़ूद चीनी विश्लेषकों के जेहन में चुनाव पूर्व किए गए वादों के पूरा होने को लेकर संदेह बना हुआ है और वे सवाल उठा रहे हैं कि देश के मौज़ूदा राजनीतिक हालातों में मोदी क्या अब अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा पहना पाएंगे? कई विश्लेषकों के मुताबिक़ चूंकि भारत में अब गठबंधन की सरकार है और वर्तमान हालातों में प्रधानमंत्री मोदी को जन सरोकार वाली नीतियों को अपनी प्राथमिकता में रखना पड़ सकता है. यानी पीएम मोदी को इन परिस्थितियों में भूमि, श्रम और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों की गति को न केवल धीमा करना पड़ सकता है, बल्कि इससे भारतीय विनिर्माण सेक्टर का विकास भी बाधित हो सकता है.
मौज़ूद वक़्त में वैश्विक विनिर्माण सेक्टर में चीन की हिस्सेदारी भारत की तुलना में क़रीब आठ गुना अधिक है. यानी वैश्विक विनिर्माण सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से भी कम है, जबकि चीन की हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत है. ऐसे में सवाल उठना लाज़िमी है कि भारत की इतनी कम हिस्सेदारी के बावज़ूद चीन “मेक इन इंडिया” नीति से इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? चीनी विश्लेषक और चीन की फोडन यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर लिन मिनवांग ने अपने एक ताज़ा लेख में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है. लिन मिनवांग के मुताबिक़ वर्ष 2010 और 2014 के दरम्यान चीन एवं भारत अर्थव्यवस्था में जो अंतर बहुत बढ़ गया था, उसमें अब एक नए तरह का बदलाव नज़र आ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वर्तमान में भी दोनों देशों के आर्थिक सामर्थ्य में बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है, लेकिन दोनों देशों की आर्थिक ताक़त के बीच में जो अंतर साल-दर-साल बढ़ता जा रहा था, पिछले दो वर्षों में उसकी गति कमी हुई है. मिनवांग के अनुसार भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण कई देशों के साथ चीन के आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों में खटास पैदा हो गई है और अलगाव जैसे हालात बन गए हैं. इन परिस्थितियों में तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय बाज़ार की ओर रुख किया है. इस तरह के घटनाक्रमों ने जहां एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का काम किया है, वहीं इनका चीन की आर्थिक स्थित पर प्रतिकूल असर पड़ा है. इतना ही नहीं, मिनवांग ने आर्थिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए इस परिवर्तन को चीनी विनिर्माण उद्योग के लिए ख़तरा बताते हुए आगाह भी किया है. इसके साथ ही उन्होंने चीनी सरकार में बैठे लोगों से भी आग्रह किया है कि वे तीसरी बार भारत की सत्ता में लौटे पीएम मोदी यानी मोदी 3.0 की आर्थिक व औद्योगिक नीतियों पर पैनी नज़र रखें.
वर्तमान में जिस प्रकार से भू-राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है, उसमें भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” नीति ने चीन को ख़ास तौर पर परेशानी में डाल दिया है. मौज़ूदा वैश्विक राजनीति में ऐसा माना जा रहा है कि ‘मेक इन इंडिया’ पॉलिसी कई देशों, विशेष रूप से अमेरिका को लुभा रही है और इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन का वर्चस्व कम हुआ है. ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 2018 से ही अमेरिका ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और चिप निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चीन को रोकने के लिए, उसकी भूमिका को सीमित करने के लिए तमाम क़दम उठाए और वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने की भरकस कोशिश की है. लेकिन वास्तविकता में अमेरिका इसमें नाक़ाम साबित हुआ है. ज़ाहिर है कि वर्तमान में चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, उसकी दशा और दिशा तय करने में अगले पांच वर्ष बेहद अहम हैं. इन हालातों में चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका उसी की तरह संभावनाओं से भरे भारत के साथ न केवल अपने रिश्ते मज़बूत कर सकता है, बल्कि उसका इस्तेमाल भी कर सकता है. गौरतलब है कि भारत कई मायनों में चीन के समान है, जैसे कि भारत की जनसंख्या चीन के बराबर है और भारत का बाज़ार भी बहुत व्यापक है. इसके अलावा भारत एक ऐसी उभरती अर्थव्यवस्था है, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. कुल मिलाकर व्यापार और आर्थिक लिहाज़ से देखा जाए तो चीन के विरुद्ध भारत कहीं न कहीं अमेरिका के लिए "तुरुप का इक्का" साबित हो सकता है.
दूसरी तरफ, चीन को भी इसकी भली-भांति जानकारी है कि चीन और अमेरिका के बीच चल रही भू-राजनीतिक होड़ के बारे में भारत को न केवल अच्छे से पता है, बल्कि इससे जो रणनीतिक मौक़े पैदा हो रहे हैं, उनसे भी वह वाकिफ है और उनका अधिक से अधिक रणनीतिक फायदा उठाना चाहता है. देखा जाए तो जिस प्रकार से भारत ने रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी से अपने हाथ खींचे है, वो कहीं न कहीं चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने और "मेक इन इंडिया" नीति को ताक़त देने का ही एक प्रयास है. इतना ही नहीं, जिस तरह से भारत द्वारा चीनी कंपनियों और उनकी ओर से किए जाने वाले निवेश पर अड़ंगा लगाया गया है, वो साफ तौर पर बताता है कि भारत का मकसद चीनी कंपनियों को दरकिनार कर उनसे अलगाव करना है. इसके अलावा, भारत की इन कोशिशों से यह भी पता चलता है कि वह अमेरिका और यूरोपीय देशों की कंपनियों के साथ, ख़ास तौर पर रणनीतिक उद्योगों या फिर भविष्य के उद्योगों से संबंधित कंपनियों के साथ साझेदारी करने का इच्छुक है.
भारत में चीन के नए राजदूत जू फीहोंग ने हाल के दिनों में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे साफ पता चलता है कि चीन में घरेलू स्तर पर मोदीनॉमिक्स 3.0 को लेकर कितनी घबराहट है. जब सभी की नज़र भारत में लोकसभा चुनाव के नतीज़ों पर थी, तब भारत में नए-नए नियुक्त हुए चीनी राजदूत फीहोंग ने देश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू-लपट के बारे में चिंता ज़ाहिर करते हुए हरित परिवर्तन की ज़रूरत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था. चीनी राजदूत ने अपनी पोस्ट में न सिर्फ़ हरित परिवर्तन प्रौद्योगिकी को लेकर चीन की विशेषज्ञता के बारे में बताया था, बल्कि नई दिल्ली में नई सरकार से जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी के उपजे हालातों का सामना करने के लिए चीन के साथ मिलकर कार्य करने का भी अनुरोध किया था. चीनी राजदूत ने अपने एक अन्य ट्वीट में संकेत दिए थे कि चीन नई दिल्ली में बनने वाली नई सरकार के साथ न्यू एनर्जी व्हीकल यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) या बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी के सेक्टर में सहयोग करने का इच्छुक है. ज़ाहिर है कि बिजली या बैटरी से चलने वाले वाहनों के निर्माण में चीन की विशेषज्ञता है और भविष्य में चीन की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने वाले उद्योगों में जो तीन नए उद्योग शामिल हैं, उनमें यह एक प्रमुख औद्योगिक सेक्टर है. चीनी राजदूत ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया था कि दिल्ली की सड़कों पर जापानी, कोरियाई, अमेरिकी और जर्मन कारों की भरमार है, तो फिर न्यू एनर्जी वाली कारों को बेचने पर चीन को ही क्यों ओवरकैपेटिसी का आरोप मढ़ा जाता है?
भारत की इन कोशिशों से यह भी पता चलता है कि वह अमेरिका और यूरोपीय देशों की कंपनियों के साथ, ख़ास तौर पर रणनीतिक उद्योगों या फिर भविष्य के उद्योगों से संबंधित कंपनियों के साथ साझेदारी करने का इच्छुक है.
भारत में चीन के राजदूत ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जो बाते कहीं हैं, उन्हें नज़रंदाज़ करने के बजाय गहराई से समझना ज़रूरी है. सभी को पता है कि चीन न्यू एनर्जी व्हीकल उत्पादन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार हो गया है. परंपरागत रूप से नई ऊर्जा से संचालित वाहनों के उत्पादन में महारत रखने वाले पश्चिमी देशों और जापान को पछाड़ते हुए हाल ही में चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है. हालांकि, चीन को इस उपलब्धि के साथ ही कई व्यापक चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है. चीन में निर्मित इलेक्ट्रिक और बैटरी संचालित वाहनों के लिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार हैं, लेकिन अब उसके लिए वहां अनुकूल माहौल नहीं है और उसे अपने उत्पादों को वापस मंगाना पड़ रहा है. इसके साथ ही चीन के घरेलू बाज़ार में भी न्यू एनर्जी व्हीकल्स की मांग में भारी कमी आई है.
चीन ने हमेशा से ही अपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को, जो कि अमेरिका या यूरोपीय देशों में ख़ास तौर पर जगह बनाने में नाक़ाम रहे हैं, उन्हें भारत के बाज़ारों में बेचने का काम किया है. देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश जहां कम मूल्य वाले उत्पादों का बड़ा मार्केट है और ऐसे भारतीय बाज़ारों में चीन को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बेचने में दिक़्क़त भी नहीं हुई है. हालांकि, चीनी विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने देर से ही सही, लेकिन चीन की इस रणनीति को न सिर्फ़ समझा है, बल्कि इससे सीख भी ली है. इसे इस बात से समझा जा सकता है कि चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने एक समय भारत के बाज़ार पर कब्ज़ा सा कर लिया था और भारत के नए उभरते स्मार्टफोन निर्माण उद्योग को ही एक प्रकार से नष्ट कर दिया था. लेकिन समय रहते भारत ने ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए चीनी कंपनियों के निवेशों पर न केवल पाबंदी लगाई, बल्कि उन पर निगरानी के भी पुख़्ता इंतज़ाम किए. इसी क्रम में भारत ने चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स और बीवाईडी जैसी बड़ी ऑटो कंपनियों के भारी-भरकम निवेश को दो बार नामंजूर कर दिया है. इतना ही नहीं, भारत ने जिन चीनी कंपनियों को भारत में निवेश की मंजूरी दी है, उसमें इस बात को सुनिश्चित किया है कि उनकी भारतीय हिस्सेदार कंपनी के पास इतनी हिस्सेदारी हो, जो उसे नियंत्रित कर सके. चीनी ऑटो कंपनी और भारतीय मोटर व्हीकल कंपनी के संयुक्त उपक्रम SAIC-MG India के मामले से यह स्पष्ट हो जाता है. मीडिया में छपी ताज़ा ख़बरों के मुताबिक़ आने वाले दिनों में भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीनी व भारतीय कंपनियों के बीच और तमाम दूसरे साझा उपक्रमों को स्वीकृति दे सकती है, लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि इन संयुक्त उद्यमों में भारतीय भागीदार कंपनी के पास चीनी कंपनी की तुलना में अधिक हिस्सेदारी होनी चाहिए. इतना ही नहीं, भारत अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लेकर आया है. इस नीति में भारत में निवेश करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को टैक्स में राहत देने की बात कही गई है.
वर्तमान में चीनी न्यू एनर्जी गाड़ी कंपनियों को जिस तरह तमाम वैश्विक बाज़ारों में तमाम दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है, उसने पिछले कुछ महीनों में चीन के घरेलू ऑटो मार्केट में उथल-पुथल मचा दी है और वहां क़ीमतें कम करने की होड़ शुरू हो गई है. ऐसे में चीनी पर्यवेक्षक इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं चीन के घरेलू मार्केट में इलेक्ट्रिक और बैटरी संचालित वाहन निर्माता कंपनियों के बीच मची यह मार-काट और तेज़ी से गिरती क़ीमतें देश के न्यू एनर्जी व्हीकल निर्माण सेक्टर को ही तबाह न कर दें. साथ ही यह भी चिंता है कि इस सेक्टर की नई और इनोवेटिव चीनी कंपनियां इन हालातों में कहीं नए-नए प्रयोगों से मुंह न मोड़ लें. इन हालातों में कई लोगों का मानना है कि कि चीनी वाहन निर्माता कंपनियों के पास अब विदेशी बाज़ारों में अपने पैर फैलाने के लिए सीमित विकल्प ही बचे हैं. यानी अगर चीनी कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं, तो उन्हें न चाहते हुए भी न केवल संयुक्त उपक्रम स्थापित करने होंगे, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को भी साझा करना पड़ेगा.
इन सारे घटनाक्रमों को लेकर बीजिंग न सिर्फ़ चिंतित है, बल्कि उसका मानना है कि दुनिया में वर्तमान में चल रही चौथी औद्योगिक क्रांति में जिस प्रकार से चीन अग्रणी भूमिका निभा रहा है, यह सब उसकी राह में रोड़ा अटकाने के लिए उसके विरुद्ध किया गया एक मिलाजुला हमला है. चीन में एक वेबसाइट में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक़, “अमेरिका द्वारा चीन की टेक इंडस्ट्री पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है; अगले 50 वर्षों तक यूरोप चीनी ऑटो बाज़ार पर अपना दबदबा रखना चाहता है; भारत इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित होना चाहता है और भारत ऐसा पश्चिमी देशों की मदद लेकर , साथ ही चीन को पीछे धकेलकर करना चाहता है.” इस आर्टिकल में इन सभी देशों की आलोचना भी की गई है और कहा गया है कि ये देश “चीन की 70 वर्षों की कठिन मेहनत” को ज़मीन में मिलाना चाहते हैं. इस लेख में जो बातें कही गई हैं, कुछ इसी तरह की चर्चाएं इन दिनों चीन के रणनीतिक हलकों में भी चल रही हैं.
आने वाले दिनों में भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीनी व भारतीय कंपनियों के बीच और तमाम दूसरे साझा उपक्रमों को स्वीकृति दे सकती है, लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि इन संयुक्त उद्यमों में भारतीय भागीदार कंपनी के पास चीनी कंपनी की तुलना में अधिक हिस्सेदारी होनी चाहिए.
जहां तक भारत का मसला है, तो यह बेहद अहम है कि चीन से होने वाले आयात में बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, कई चीनी रणनीतिकारों का यह मानना है कि चीन से भारत को होने वाले आयात में यह बढ़ोतरी अस्थायी है और यह कुछ ख़ास बाज़ारों की प्रमुख कंपनियों की मांग में वृद्धि होने की वजह से है, साथ ही ये वो कंपनियां, जो हाल ही में चीन को छोड़कर भारत में स्थापित हुई हैं. कुछ चीनी रणनीतिकार इसका उलट सोचते हैं और इनके मुताबिक़ चीन से तमाम तरह के उद्योगों (ईवी और अन्य उद्योगों) का स्थानांतरण अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह काफ़ी लंबे अर्से से हो रहा है और जो हालात पैदा हुए हैं उनमें चीनी कंपनियों के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है. इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल के चलते पैदा होने वाले ख़तरों और बढ़ती लागत से बचने जैसे तमाम मुद्दों के चलते चीनी कंपनियों ने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से बाहर दूसरे देशों में ले जाना शुरू कर दिया है. देश से बाहर जाने वाले चीनी उद्यमों ने ख़ास तौर पर भारत जैसे बाज़ारों को चुना है. क्योंकि भारत में उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम है, श्रम और संसाधनों की लागत कम है, साथ ही वहां उत्पादों के लिए बड़ा मार्केट भी है. इसके अलावा, भारत जैसे देशों में विनिर्माण इकाई स्थापित करने से चीनी कंपनियों को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के "रीशोरिंग/नियरशोर/फ्रेंडशोरिंग" सिस्टम में प्रवेश करने, यानी इन देशों में अपना बिजनेस जमाने में मदद मिल सकती है. भारत में चीनी कंपनियों के स्थानांतरित होने के पीछे दूसरा कारण यह है कि जो चीनी कंपनियां भारत में अपना बिजनेस स्थापित करने की इच्छुक नहीं है या इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर रही हैं, उन्हें भी भारत में स्थापित हो चुकीं, या स्थापित होने की योजना बना रही शीर्ष कंपनियों, जिनमें मल्टीनेशनल कंपनियां और चीनी कंपनियां दोनों ही शामिल हैं, द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और भारत में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए मज़बूर किया जा रहा है.
चीन से भारत को होने वाले आयात में यह बढ़ोतरी अस्थायी है और यह कुछ ख़ास बाज़ारों की प्रमुख कंपनियों की मांग में वृद्धि होने की वजह से है, साथ ही ये वो कंपनियां, जो हाल ही में चीन को छोड़कर भारत में स्थापित हुई हैं.
चीन के रणनीतिक गलियारों में इन सारे हालातों के मद्देनज़र तमाम सवाल उठ रहे हैं. जैसे कि एक सवाल यह है कि इससे पहले कि भारत में स्थानीय स्तर पर विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित हो, भारतीय बाज़ार में भारतीय प्रतिद्वंदी कंपनियों पर बढ़त हासिल करने के लिए बीच के इस वक़्त का किस प्रकार से बेहतर और प्रभावी तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए? दूसरा सवाल यह है कि चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ी उद्योग में बदलाव लाने और उसे अपग्रेड करने के लिए भारत के बाज़ारों में उपलब्ध मौज़ूदा अवसरों (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत की टैक्स में छूट की नीति का लाभ समेत) का किस प्रकार से लाभ उठाया जाए? यानी ऐसा करके “मेड इन इंडिया” और “मेड इन चाइना” के बीच का अंतर और किस प्रकार बढ़ाया जाए. कहने का मतलब है कि चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पाद भारतीय कंपनियों की तुलना में उन्नत हो जाएं, जिससे दोनों के बीच तुलना एक प्रकार से बेमानी हो जाए.
आख़िर में, कोई भी व्यक्ति यह आसानी से कह सकता है कि चीन और भारत के बीच एलएसी पर ज़बरदस्त सैन्य टकराव की स्थिति है और सभी का ध्यान उसी पर है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष की तरह ही भीषण जियो-इकोनॉमिक यानी भू-आर्थिक लड़ाई भी साथ-साथ चल रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच चल रही इस आर्थिक खींच-तान पर भी उतना ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है. चीन के रणनीतिक हलकों में यह चर्चा आम है कि वर्ष 2020 में एलएसी पर चीन द्वारा घुसपैठ की जो कोशिश की गई थी, उसके पीछे भी कहीं न कहीं चीन का यही भू-आर्थिक दृष्टिकोण था. भविष्य में भी एलएसी पर चीन क्या क़दम उठाता है, उसके पीछे भी निश्चित तौर पर उसकी यही भू-आर्थिक सोच होगी.
अंतरा घोसाल सिंह ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो हैं.


The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Antara Ghosal Singh is a Fellow at the Strategic Studies Programme at Observer Research Foundation, New Delhi. Her area of research includes China-India relations, China-India-US ...
Read More +