-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
ये सवाल वामपंथ या दक्षिणपंथ का नहीं है. यूरोप की समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं .
.png)
यूरोप की राजनीति में दक्षिणपंथ की ओर बढ़ता झुकाव, लोकतंत्र की मौत नहीं, बल्कि इसकी जीत है. आकांक्षाएं व्यक्त करने के ज़रिए के तौर पर लोकतंत्र हमेशा अपने आपको दुरुस्त करने वाली व्यवस्था है. एक संस्था के तौर पर जनतंत्र, वोट की ताक़त के ज़रिए नेतृत्व में शांतिपूर्ण परिवर्तन का माध्यम बनता है. वहीं मतदाता अतार्किक नहीं होते. बल्कि, वो लोकतंत्र के समझदार भागीदार होते हैं, जो तमाम विकल्पों में से अपने लिए सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करते हैं. अगर हम लोकतंत्र को नागरिकों पर वामपंथ और दक्षिणपंथ के दो विपरीत ध्रुवों वाले विकल्प के तौर थोपने के सरल नज़रिए से देखें, तो असल में ये वामपंथ के बेअसर होने की अति है, जिसने दक्षिणपंथ के लिए रास्ता खोला है. लेकिन, सही शब्द ‘दक्षिणपंथ’ नहीं, बल्कि ‘बदलाव’ है. जैसा कि ब्रिटेन के आम चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि असल में तो वामपंथ सत्ता में लौट रहा है.
ईसाई यूरोप में कुछ भी नया नहीं हो रहा है. हो सकता है कि ये चौंकाने वाली बात लगे, शायद. लेकिन, नयापन तो क़तई नहीं है. सच तो ये है कि अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ होता, तो यूरोप ने अपने लोकतंत्र के मापदंडों को नए नए नाम देकर पूरा किया होता. ये सॉफ्ट पावर का हथियार, जो उसने अपनी भू-राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया है. मिसाल के तौर पर वी-डेम, लोकतंत्रों को चार मोटे वर्गों में बांटता है- बंद लोकतंत्र (जैसे कि चीन या सऊदी अरब), चुनावी तानाशाही (रूस या यूक्रेन), चुनावी लोकतंत्र (ब्राज़ील, पोलैंड) और उदारवादी लोकतंत्र (जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली).
भारत को चुनावी तानाशाही कहकर बुलाया जाता है. हम यूरोप की राजनीति में आ रहे इस दक्षिणपंथी झुकाव को दुनिया के अंत के तौर पर नहीं देखते, बल्कि मतदान की सामान्य प्रक्रिया मानते हैं. हैरानी तो वामपंथी झुकाव वाले कुछ मुट्ठी भर विचारकों के लिए है, जो इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. ये सच्चाई कि राजनीति, मतदाताओं की इच्छा के साथ राजनीतिक रूप से संवाद नहीं कर पा रही है, तो ये एक स्तर की असहिष्णुता ही कही जाएगी. जो ‘उदारवादी लोकतंत्रों’ या फिर ‘चुनावी लोकतंत्रों’ वाला बर्ताव तो नहीं है. उनका रवैया तो ‘बंद तानाशाही’ या फिर ‘चुनावी तानाशाही’ कहे जाने वाले देशों जैसा है.
एक संस्था के तौर पर जनतंत्र, वोट की ताक़त के ज़रिए नेतृत्व में शांतिपूर्ण परिवर्तन का माध्यम बनता है. वहीं मतदाता अतार्किक नहीं होते. बल्कि, वो लोकतंत्र के समझदार भागीदार होते हैं, जो तमाम विकल्पों में से अपने लिए सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करते हैं.
चुनावों से पहले और नतीजों के बाद विकल्पों की जगह लेते दंगे और जीत के बाद भड़कने वाली हिंसा, यूरोप के तानाशाही के गर्त में गिरते जाने का सिर्फ़ एक पहलू है. यूरोप की शब्दों के चतुर जाल में गढ़कर पेश की जाने वाली लोकतांत्रिक परिचर्चा का झुकाव चीन की तरफ़ होता जा रहा है और ये लोकतांत्रिक परंपराओं पर लगा एक गहरा दाग़ है. एक के बाद दूसरे देश में चुनाव के दौरान होने वाला राजनीतिक संपर्क हर गुज़रते दिन के साथ छिछला होता जा रहा है और ये सब उस महाद्वीप में हो रहा है, जो ख़ुद के लोकतंत्र का रचनाकार होने का झूठा दावा करता फिरता है.
‘दक्षिणपंथी’ झुकाव
जिसे यूरोप का बढ़ता ‘दक्षिणपंथी’ झुकाव कहा जा रहा है, उसकी बारीक़ी से पड़ताल करने की ज़रूरत है. ये समीक्षा न केवल राजनीतिक बदलाव या फिर उसके साथ हो रही हिंसा के लिए नहीं, बल्कि उन आकांक्षाओं के विस्तार की भी पड़ताल है, जो वामपंथ और दक्षिणपंथ के हल्के द्वंद के दायरे में नहीं आती हैं. जिसे दक्षिणपंथी झुकाव के तौर पर देखा जा रहा है, वो असल में एक के बाद एक सत्ता में आने वाली वामपंथी सरकारों के राजनीतिक नाकारेपन का नतीजा है, जो नागरिकों के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों का कोई हल निकाल पाने में नाकाम रहा है. असल में ये समस्याओं के समाधान की मांगों का समागम है, जिसे वामपंथ की दूसरों पर उंगली उठाने वाली विचारधारा के पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है. इसकी वजह से सत्ता भीतर से खोखली हो गई है, और वो जनकल्याणवाद के दायरे से बाहर के मसलों पर बेअसर साबित हो रही है. इसकी सबसे बुलंद मिसाल अप्रवास की समस्या है.
कुल मिलाकर, अप्रवासियों को सबसे ज़्यादा स्वीकार करने के मामले में यूरोप का नंबर रूस, अमेरिका और भारत के बाद आता है. यूरोप ने अप्रवासियों और शरणार्थियों का स्वागत किया है. उनकी तथाकथित पीड़ा से हमदर्दी जताई है, और रूस, अमेरिका और भारत की ही तरह उन लोगों को अपने करदाताओं की क़ीमत पर खाना, रिहाइश और अवसर मुहैया कराए हैं. लेकिन, आंकड़ों के हिसाब से से देखें तो यूरोप के तीन सबसे बड़े देशों (फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन) में रहने वाले अप्रवासियों की कुल तादाद, उन अप्रवासियों की संख्या की केवल एक तिहाई है, जिन्हें भारत ने पनाह दी है. ये बात और है कि अमेरिका, भारत और यूरोप- तीनों ही अवैध अप्रवास की समस्या से नहीं निपट पा रहे हैं. फिर चाहे इसकी रोकथाम हो या अप्रवासियों का प्रबंधन.
जिसे यूरोप का बढ़ता ‘दक्षिणपंथी’ झुकाव कहा जा रहा है, उसकी बारीक़ी से पड़ताल करने की ज़रूरत है. ये समीक्षा न केवल राजनीतिक बदलाव या फिर उसके साथ हो रही हिंसा के लिए नहीं, बल्कि उन आकांक्षाओं के विस्तार की भी पड़ताल है, जो वामपंथ और दक्षिणपंथ के हल्के द्वंद के दायरे में नहीं आती हैं.
सुन्न पड़ी सरकारों की वजह से अवैध अप्रवासियों के हौसले बुलंद हैं, और उन्होंने यूरोप के क़ानूनों को ही उसके ख़िलाफ़ हथियार बना लिया है. बड़े पैमाने पर अप्रवासियों के आने की वजह से आज जर्मनी, ‘सामाजिक निष्क्रियता’ का शिकार है. अप्रवासियों द्वारा बलात्कार की बढ़ती वारदातों की वजह से इटली की सहिष्णुता घटती जा रही है. पिछले साल एक टीचर पर चाकू से हमले के बाद से फ्रांस भी अप्रवास पर पुनर्विचार कर रहा है और वहां संसद के लिए हो रहे मतदान को ‘जिहादी आतंकवादी हमलों का देर से हो रहा असर’ बताया जा रहा है. स्पेन अप्रवासियों की बेलगाम बाढ़ में डूब रहा है और वो इसे अपनी ‘क्षेत्रीय अखंडता’ पर हमले के रूप में देखता है. आयरलैंड में दंगे हो रहे हैं और वो ‘आयरलैंड में स्वागत’ को ख़त्म करके अप्रवासियों के साथ नरमी से पेश आने की नीति से पीछा छुड़ा रहा है. 2023 के अंत में जिसे लोग यूरोप में सभ्यताओं के संघर्ष के तौर पर देख रहे थे, वो अब स्पष्ट रूप से दक्षिणपंथ के पक्ष में जनादेश है.
एक ज़रूरी शर्त के तौर पर सरकारें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सबसे बड़े क़ानून और व्यवस्था के मूलभूत ढांचे को दुरुस्त करती हैं. लेकिन, समय के साथ साथ ज़रूरत की प्रासंगिकता ख़त्म हो जाती है. इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है. सुरक्षा के ऊपर आराम को तरज़ीह दी जाने लगती है. एक समृद्ध अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय की ऊंची दर, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा और कम महंगाई जैसे सामाजिक जनहित की सेवाएं-यूरोप को अब इन आरामों की लत लग गई है. तथाकथित ज़ुल्मों से भागकर यूरोप में दाख़िल हो रहे अप्रवासियों- जिनमें से ज़्यादातर फ़ौज में दाख़िल होने की उम्र वाले हैं, महिलाएं या बच्चे नहीं- ने एक और ‘पुरुष समस्या’ को जन्म दिया है, जिसे इस आराम का ही एक हिस्सा मान लिया गया था. आख्यानों से डरकर ऐसे क़ानून पारित किए गए हैं, जो अप्रवासियों को संरक्षण तो देते हैं. लेकिन, उनसे उत्तरदायित्व की कोई अपेक्षा नहीं रखते. इन क़ानूनों के बदले में कई अप्रवासी, उदारवादी, खुले और स्वतंत्र यूरोप को एक ऐसे स्याह, अराजक, रुढ़वादी धार्मिक समाज में तब्दील करना चाहते हैं, जिनसे बचने के लिए ही इन अप्रवासियों ने यूरोप में पनाह ली थी.
‘दक्षिणपंथ की ओर झुकाव’ असल में यूरोप की एक विकल्प की मांग है, जिससे मतदाताओं को अपेक्षा है कि वो क़ानून और व्यवस्था के मामले में बेहतर काम करेंगे. अपने अपने मतदाताओं की सेवा करने के प्रयास में, हो सकता है कि राजनेता ऐसा व्यवहार करें, जो शायद पेंडुलम को दूसरी तरफ़ झुका दे.
वैश्विक लहर
पूरे यूरोप में घट रही इन घटनाओं और उदाहरणों को आपस में जोड़ने वाली बात न तो वामपंथ का कुप्रबंधन है और न ही दक्षिणपंथ से महान आकांक्षाओं का नतीजा है. पोलैंड जैसी कुछ गिनी चुनी मिसालों को छोड़ दें, तो ये एक वैश्विक लहर है जो सत्ता के साथ साथ मिलने वाली ज़िम्मेदारियों से निपट पाने की नाकामी है. किसी भी सरकार की पहली भूमिका, मिसाल के तौर पर जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने व्यक्त किया और जो लोकतांत्रिक देशों के सभी मतदाताओं की आकांक्षा होती है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा एवं क़ानून व्यवस्था दें. जब ये समझौता टूट जाता है और जैसा कि हम यूरोप में घटित होते देख रहे हैं, तो मतपत्र बदलाव का इकलौता माध्यम बन जाता है. अभी तो ख़ामोश बहुमत के वामपंथ पर यक़ीन को ध्वस्त कर दिया गया है. इस तरह, आज विकल्प के तौर पर जो बदलाव देखा जा रहा है, उसका झुकाव दक्षिणपंथ की ओर है.
‘दक्षिणपंथ की ओर झुकाव’ असल में यूरोप की एक विकल्प की मांग है, जिससे मतदाताओं को अपेक्षा है कि वो क़ानून और व्यवस्था के मामले में बेहतर काम करेंगे. अपने अपने मतदाताओं की सेवा करने के प्रयास में, हो सकता है कि राजनेता ऐसा व्यवहार करें, जो शायद पेंडुलम को दूसरी तरफ़ झुका दे. अप्रवास विरोधी इस लहर में शायद वो वैध अप्रवासी भी बह जाएं, जो सही प्रक्रिया के ज़रिए दाखिल हुए हैं. इससे भी बुरी बात ये है कि जिन लोगों ने ‘समावेशी नज़रिए’ के साथ सच्चे पीड़ितों की तरफ़ मदद का हाथ बढ़ाया है, वो शायद एक नई राजनीति की वजह से उनको ‘अलग थलग करने’ वाली दिशा में परिवर्तित हो जाएं. या फिर, अगर समझदार राजनेताओं के हाथ में कमान जाती है, तो यूरोप शायद अपने नागरिकों के साथ नया समझौता करे और बेहतर व्यवहार के आधार पर एक नया संतुलन क़ायम करे.
अब चाहे जो कुछ हो, जहां तक बाद लोकतंत्र के लिए ख़तरे की है, तो अगले पांच साल तक, यूरोप ऐसा महाद्वीप होगा, जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी, और ख़ुद यूरोप को सावधान रहना होगा कि बरसों से वो जिन हवालों के ज़रिए भारत जैसे समृद्ध गहरे और स्वस्थ लोकतंत्र पर उंगली उठाता रहा है, कहीं ख़ुद भी उसी पतन के गर्त में न डूब जाए. हक़ीक़त तो ये है कि एक सियासी वैचारिक सांप अब अपनी ही पूंछ को कुतर रहा है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
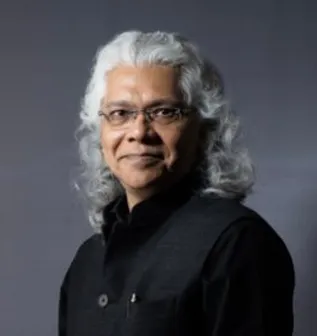
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +