-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
अगर भारत, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव से मुक़ाबला करना चाहता है, तो फिर उसे इस इलाक़े में अपने आर्थिक निवेश और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों को बढ़ाना होगा.
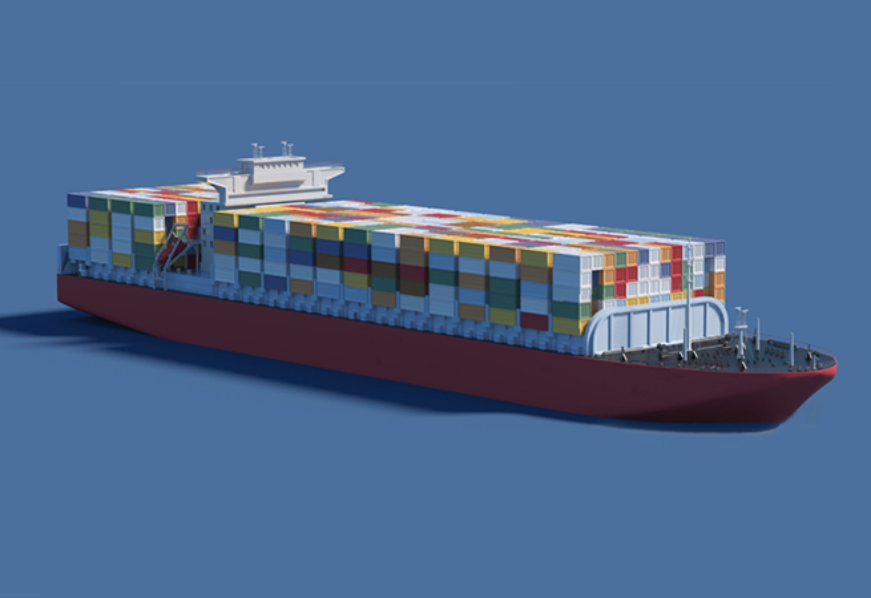
ये द चाइना क्रॉनिकल्स सीरीज़ का 127वां लेख है.
अन्य लेख यहां पढ़ें.
हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत व्यापक आर्थिक अवसरों वाला क्षेत्र है. फिर चाहे उत्पाद हों या फैक्टर के बाज़ार- क्योंकि इस क्षेत्र में कम से कम 38 देश स्थित हैं, जहां पर दुनिया की 65 फ़ीसद या 4.3 अरब आबादी रहती है. दुनिया की कुल GDP में से हिंद प्रशांत का हिस्सा क़रीब 63 प्रतिशत माना जाता है. सच तो ये है कि दुनिया का पचास प्रतिशत से ज़्यादा समुद्री कारोबार इसी इलाक़े से होकर गुज़रता है. हिंद प्रशांत क्षेत्र में आए तमाम बदलावों में से जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वो इस इलाक़े के देशों के बीच आपसी या क्षेत्रीय साझेदारियों की शक्ल में सामने आया है. इसके अलावा, इस इलाक़े में चीन की बढ़ती गतिविधियों से निपटने के लिए बाहरी ताक़तों के साथ भी ताल-मेल काफ़ी बढ़ा है.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध काफ़ी मज़बूत कर लिए हैं. चीन के साथ व्यापार में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान का पलड़ा भारी है. चीन के साथ इनका व्यापार सरप्लस में है. वहीं, सिंगापुर और भारत के संबंध व्यापार घाटे वाले हैं. चीन के साथ व्यापार में सरप्लस होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार हैं, और इन देशों से चीन को निर्यात उनकी अपनी अर्थव्यवस्था में काफ़ी अहम योगदान देता है. इसी वजह से, तमाम राजनीतिक उतार चढ़ावों के बावजूद ये देश चीन के साथ आर्थिक संबंधों में सौहार्द बनाए रखने को अहमियत देते हैं- जिससे कि उनके उत्पादों की चीन में मांग कम न हो जाए.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध काफ़ी मज़बूत कर लिए हैं. चीन के साथ व्यापार में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान का पलड़ा भारी है. चीन के साथ इनका व्यापार सरप्लस में है.
हिंद प्रशांत के देशों के साथ चीन का व्यापार हमेशा ही बहुत बड़े पैमाने पर होता आया है और ये लगातार बढ़ भी रहा है; इसे हम आंकड़ों में भी देख सकते हैं. पिछले क़रीब डेढ़ दशक से हिंद प्रशांत के देशों के साथ चीन का व्यापार लगातार बढ़ता ही रहा है. इस कारोबार में गिरावट की गिनी चुनी मिसालें ही देखने को मिलती हैं- जैसे कि 2007-08 के दौरान. इसके पीछे हम वैश्विक वित्तीय संकट का हाथ देख सकते हैं, जिससे अगले कुछ वर्षों में उबरने के सबूत भी हमारे सामने हैं.
Figure 1: हिंद प्रशांत के प्रमुख देशों के साथ चीन का व्यापार (अरब डॉलर में)
स्रोत: वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन (WITS), विश्व बैंक से लेखक के अपने आंकड़े.
हिंद प्रशांत के देशों के साथ चीन के ऐसे पेचीदा कारोबारी रिश्तों की बड़ी वजह हम, क्षेत्रीय वैल्यू चेन में चीन की अहम भूमिका को मान सकते हैं. ये एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश अपने व्यापार और निवेश को चीन से अलग करके, पश्चिम के अन्य देशों के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं. उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया के कृषि उत्पाद वैश्विक वैल्यू चेन (GVCs) पर बहुत अधिक निर्भर हैं. इस वैल्यू चेन के आयात का एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है. सच तो ये है कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी स्मार्टफ़ोन बनाने में काम आने वाले उच्च तकनीक के कल पुर्ज़ों को बनाने के लिए चीन पर निर्भर हैं. फिर इन्हीं कल पुर्ज़ों की मदद से एप्पल, शाओमी, लेनोवो और हुआवेई जैसी कंपनियां अपने स्मार्टफ़ोन बनाती हैं- इनके ज़्यादातर उपकरण चीन में असेंबल किए जाते हैं, और फिर वहा से इनका निर्यात होता है.
सच तो ये है कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी स्मार्टफ़ोन बनाने में काम आने वाले उच्च तकनीक के कल पुर्ज़ों को बनाने के लिए चीन पर निर्भर हैं.
चूंकि चीन, अन्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के मामले में दुनिया में सबसे आगे है. इसलिए, इसका असर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी दिखता है. चीन और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आदान प्रदान, भारत द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी की तुलना में कहीं अधिक है. पिछले कई वर्षों के दौरान चीन ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव के विस्तार के ज़रिए इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और राजनीतिक नेटवर्क को काफ़ी बढ़ा लिया है. जबकि BRI के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि इसके तहत मदद पाने वाले ज़्यादातर देश लंबे समय के लिए क़र्ज़ के जाल में फंस जाते हैं. ये बात, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका के सहारा देशों के विकासशील देशों के लिए एक बड़ा मसला रही है.
चीन के साथ बढ़ती आर्थिक और जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता एक बड़ा कारण है, जिसके चलते भारत अपना ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित कर रहा है. चीन द्वारा कोविड-19 की महामारी रोकने में गड़बड़ी करने के आरोप, भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों के दौरान सैन्य तनातनी, ऑस्ट्रेलिया से जौ के आयात पर चीन द्वारा 80 प्रतिशत व्यापार कर लगाने और सबसे अहम बात ये कि महामारी के दौरान जिस तरह चीन के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में ख़लल पड़ा, उसने हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के आर्थिक नज़रिए को काफ़ी हद तक बदल दिया है. यहां तक कि हिंद प्रशांत के मसले पर आम तौर पर पर सीमित प्रतिक्रिया देने वाले दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के गठबंधन (ASEAN) ने वर्ष 2019 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आसियान के दृष्टिकोण की शुरुआत की थी. इस तरह से आसियान देशों ने संकेत दिया था कि वो अपने आस-पास के क्षेत्र के बदलते समीकरणों पर नज़र रख रहे हैं.
एक बड़ी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय ताक़त होने के नाते भारत भी हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने पर काफ़ी ज़ोर दे रहा है. साल 2020 में कन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ (CII) के एक अध्ययन के मुताबिक़, हिंद प्रशांत क्षेत्र के चुने हुए 20 देशों के साथ भारत का व्यापार 2001 से आठ गुना बढ़ चुका है. 2001 में जहां इन सभी देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 33 अरब डॉलर था. वहीं, साल 2020 में ये 262 अरब डॉलर के स्तर तक जा पहुंचा था. हालांकि, कई अलग-अलग कारणों से हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते और नेतृत्व की भूमिका अभी सीमित ही है. इसमें सर्विस सेक्टर में एकरूपता, जो IT उद्योग पर केंद्रित है; भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत का बेहद कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; भारत में ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारी कमी, जो ख़ुद को क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ सकें, शामिल हैं.
ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे जो देश चीन के ख़िलाफ़ मोर्चेबंदी की अगुवाई कर रहे हैं, वो भी आर्थिक मामलों में ऐसी ही रणनीति अपनाते हैं. ये सभी देश चीन को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अहम ख़तरा तो मानते हैं.
भारत का आर्थिक प्रदर्शन, इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव से निपटने के लिए क़तई पर्याप्त नहीं है. वैसे तो भारत, आसियान को अपनी हिंद प्रशांत रणनीति का केंद्र बताता है और आसियान देशों के साथ क़रीबी आर्थिक और सामरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन, आसियान देशों के साथ व्यापार की बात करें, तो चीन की तुलना में भारत का इन देशों के साथ व्यापार कहीं नहीं ठहरता है. पिछले बारह साल से चीन, आसियान देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बना हुआ है, और इस साल तो यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर आसियान, चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार समूह बन गया.
Figure 2: चीन आसियान का व्यापार बनाम भारत आसियान के बीच व्यापार 2020-21 (अरब डॉलर में)
स्रोत: लेखक के अपने, चीन के इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े.
आसियान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मज़बूत बनाना, दक्षिणी पूर्वी एशिया और व्यापक हिंद प्रशांत इलाक़े में भारत की आर्थिक हैसियत के लिए ख़ास तौर से अहम है. क्योंकि, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक बढ़त होने के चलते ही चीन, इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मज़बूती दे पा रहा है. चीन का आक्रामक विस्तार, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के लिए एक अहम सामरिक और सुरक्षा संबंधी सिरदर्द बना हुआ है. लेकिन, चीन के साथ आर्थिक संबंधों से होने वाली समृद्धि के चलते ये देश ऐसा कोई क़दम उठाने से पहले दो बार सोचते हैं, जिससे चीन के नाख़ुश होने का डर होता है. ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे जो देश चीन के ख़िलाफ़ मोर्चेबंदी की अगुवाई कर रहे हैं, वो भी आर्थिक मामलों में ऐसी ही रणनीति अपनाते हैं. ये सभी देश चीन को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अहम ख़तरा तो मानते हैं. लेकिन, चीन के साथ व्यापारिक संबंध इन देशों को चीन के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर बना देती है.
इसीलिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर भारत अपनी सामरिक अहमियत बढ़ाना चाहता है, तो फिर उसके लिए अपनी आर्थिक क्षमता का विस्तार करना होगा और इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के प्रयासों में भी तेज़ी लानी होगी. चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वो तकनीकी रूप से उन्नत दक्षिणी कोरिया या ताइवान जैसे देशों से मुक़ाबला कर सके, तो इन देशों के साथ किसी व्यापार समझौते का हिस्सा बनने से भारत के घरेलू उद्योगों को चोट पहुंचने का डर बना हुआ है. क्योंकि, व्यापार समझौता हुआ तो अन्य देशों से भारत में सस्ता माल आएगा. इन समस्याओं को देखते हुए भारत के सामने चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की है.
(इस लेख से जुड़े रिसर्च में योगदान के लिए लेखक, पॉन्डिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जेल्विन जोस के आभारी हैं)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead, World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at Observer Research Foundation (ORF). He ...
Read More +