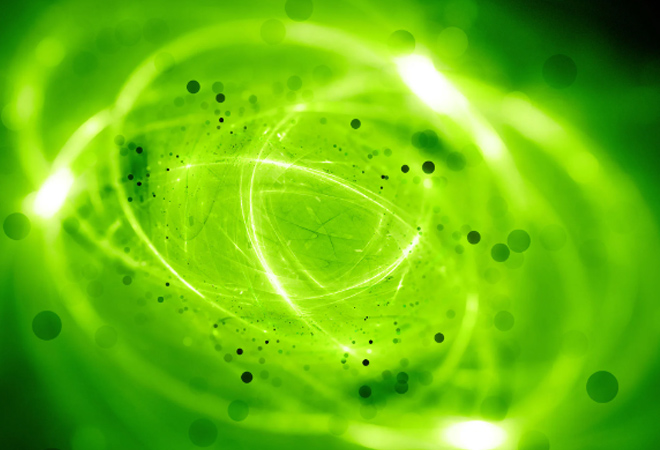
70 के दशक में अपनी कल्पना के समय से फ्यूज़न रिएक्टर मानवता के लिए एक बड़े मायावी लक्ष्य की तरह बना हुआ है. जीवाश्म ईंधन की बढ़ती दुर्लभता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की उनकी प्रवृत्ति के साथ फ्यूज़न रिएक्टर टेक्नोलॉजी ने एक नया रास्ता दिखाया और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्सुकता के साथ इसकी तरफ देखा जाने लगा. हालांकि, इस मामले में इसे काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि मानवता गतिरोध की तरफ पहुंच गई है. लेकिन नेशनल इग्निशन फेसिलिटी (अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थित लेज़र आधारित रिसर्च डिवाइस) में पिछले दिनों की महत्वपूर्ण खोज ने इस पुराने लक्ष्य को हासिल करने में एक नई उम्मीद जगाई है और ये आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा के एक भरोसेमंद स्रोत को प्राप्त करने के लिए अहम है.
न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है?
न्यूक्लियर फ्यूज़न या परमाणु संलयन प्रकृति के द्वारा तारों जैसे कि सूर्य के भीतर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है. ये विश्व में ऊर्जा उत्पादन का सबसे कुशल ज्ञात रूप है. न्यूक्लियर फ्यूज़न एक स्टैंडर्ड यूरेनियम आधारित फिज़न रिएक्शन (विखंडन प्रतिक्रिया) की तुलना में चार गुना ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता है और वो भी बिना किसी रेडियोएक्टिव कचरे के. एक फ्यूज़न रिएक्शन उस वक्त होता है जब हल्के नाभिकों के संयोजन (लाइटर न्यूक्ली कंबाइन) के साथ दो परमाणु भारी नाभिक वाला परमाणु बनाते हैं. इस तरह बनने वाले परमाणु का द्रव्यमान घटक परमाणुओं के कुल द्रव्यमान की तुलना में कम होता है और ये खोया हुआ द्रव्यमान आइंस्टीन की द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता संबंध (E=mc2) के हिसाब से ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है. आम तौर पर दो हल्के परमाणु हाइड्रोजन एटम यानी कि ड्यूटेरियम (D) और ट्राइटियम (T) के थोड़े भारी रूप (आइसोटोप) होते हैं जिनका अंतिम उत्पाद हीलियम एटम होता है.
ऊर्जा उत्पादन के काम में फ्यूज़न रिएक्शन के व्यावहारिक होने के लिए इसे एक नियंत्रित और टिकाऊ (कंट्रोल्ड एंड सस्टेनेबल) ढंग से किया जाना चाहिए ताकि निकली हुई ऊर्जा का इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने में किया जा सके जिससे कि बिजली का उत्पादन होगा.
किसी फ्यूज़न रिएक्शन की कुशलता एक मात्रा, जिसे गेन कहा जाता है, से पता चलती है जिसे इस तरह परिभाषित किया गया है:
इसका उद्देश्य 1 से अधिक गेन हासिल करना है. हालांकि इसे व्यावहारिक रूप से लागू करना काफी मुश्किल है. इसका प्रमुख कारण ये है कि फ्यूज़न हासिल करने के लिए दो घटक नाभिकों का सबसे पहले संयोजन होना चाहिए जिसके लिए उनके पारस्परिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से पार पाने की ज़रूरत होती है जो दोनों के पॉज़िटिव चार्ज होने की वजह से कठिन है. इसने फ्यूज़न हासिल करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है.
फ्यूज़न रिएक्टर्स के प्रकार
सूरज के मामले में परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉन छिन जाते हैं और काफी ज़्यादा तापमान की वजह से पॉज़िटिवली चार्ज्ड आयन में बदल जाते हैं. इसके नतीजतन आयन और इलेक्ट्रॉन का घना क्षेत्र बनता है जिसे प्लाज़्मा कहा जाता है. इन परिस्थितियों में ये संभव है कि आयन अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से पार पाने और फ्यूज़न होने देने के लिए पर्याप्त रूप से अधिक वेलोसिटी (काइनेटिक एनर्जी) हासिल कर ले. ये वास्तव में फ्यूज़न रिएक्टर में इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है. इसमें अंतर बस इतना है कि उच्च तापमान कृत्रिम ढंग से तैयार किया जाता है. इसे हासिल करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं.
मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूज़न (MCF) प्लाज़्मा को नियंत्रित करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड (चुंबकीय क्षेत्र) का इस्तेमाल करता है जो कणों को रिएक्टर वॉल से टकराने से रोकती है, ऐसा नहीं होने पर वो धीमे हो जाते. ऐसे रिएक्टर का सबसे प्रभावी आकार एक डोनट या गोलाकार होता है. टोकामक और स्टेलारेटर इस तरह के गोलाकार रिएक्टर के कुछ उदाहरण हैं. अतीत में ज़्यादातर रिएक्टर इस तकनीक पर आधारित थे.
-
इनर्शियल कन्फाइनमेंट
इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूज़न में हाई-एनर्जी लेज़र बीम को ईंधन के पैलेट पर केंद्रित किया जाता है जो इसके भीतर फ्यूज़न के लिए आवश्यक काफी अधिक तापमान उत्पन्न करता है. MCF के मामले में मैग्नेटिक फील्ड की जगह इसमें पेलेट का बाहरी हिस्सा फट जाता है और ये रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए जवाबदेह है.
रिएक्टर के कुछ दूसरे रूप भी अस्तित्व में हैं जैसे कि वो रिएक्टर जो इन दोनों पद्धतियों (मैग्नेटाइज्ड टारगेट फ्यूज़न और जो फ्यूज़न को फिज़न के साथ जोड़ते हैं) के संयोजन का इस्तेमाल करते हैं.
NIF में महत्वपूर्ण खोज
फ्यूज़न को हासिल करने में व्यावहारिक परेशानियों से पार पाने के लिए कुछ आसान तरीके ईजाद करने के बावजूद फायदे की उम्मीद कुछ देर के लिए ही बनी रही. हालांकि, दिसंबर 2022 में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी अंतत: सफलता या सकारात्मक ऊर्जा लाभ हासिल करने में कामयाब रही. बाद में जुलाई 2023 में ये अपने प्रयासों को दोहराने में सक्षम रही लेकिन इस बार और भी अधिक लाभ के साथ. दोनों ही मामलों में इनर्शियल कन्फाइनमेंट का तरीका इस्तेमाल किया गया जिसमें ईंधन के पैलेट पर लेज़र बीम दागा गया. ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई है और इसने एक ऐसी तकनीक में दिलचस्पी फिर से बढ़ा दी है जिसके बारे में माना जाता था कि एक लंबे समय से बेकार पड़ी हुई है.
व्यावसायिक संचालन के उद्देश्य से व्यावहारिक होने के लिए NIF को अपना आउटपुट कम-से-कम 1,00,000 प्रतिशत बढ़ाने की ज़रूरत है.
फ्यूज़न इंडस्ट्री एसोसिएशन की ग्लोबल फ्यूज़न इंडस्ट्री रिपोर्ट 2023 के मुताबिक फ्यूज़न उद्योग में वैश्विक निवेश बढ़कर 6.2 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है जो पिछले साल के मुकाबले 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर ज़्यादा है. अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने भी पिछले दिनों न्यूक्लियर फ्यूज़न पावर प्लांट विकसित करने वाले आठ स्टार्टअप्स में 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का एलान किया है. इस तरह ये कहा जा सकता है कि NIF में विकास ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया है.
वैसे तो ये निश्चित तौर पर खुशी मनाने की एक वजह है लेकिन इसके साथ-साथ बड़ी चेतावनी भी आती है. ऊर्जा के मामले में जिस फायदे का यहां ज़िक्र किया गया है वो केवल रिएक्शन से मिलने वाला फायदा है. इसमें लेज़र को चलाने के लिए या रिएक्शन के उद्देश्य से दूसरे उपकरण में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी इनपुट एनर्जी को शामिल नहीं किया गया है. इन सभी बातों को शामिल करने के बाद जो “कुल फायदा” हम हासिल करते हैं वो अभी भी 1 से काफी कम होता है. व्यावसायिक संचालन के उद्देश्य से व्यावहारिक होने के लिए NIF को अपना आउटपुट कम-से-कम 1,00,000 प्रतिशत बढ़ाने की ज़रूरत है. इस तरह, फ्यूज़न रिएक्टर टेक्नोलॉजी में ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण खोज है लेकिन व्यावसायिक तौर पर बिजली उत्पादन के रास्ते में अभी भी काफी व्यावहारिक परेशानियां बनी हुई हैं.
भारतीय परिदृश्य
फ्यूज़न टेक्नोलॉजी के मामले में भारत एक बड़े किरदार के तौर पर उभरा है और ये इसके विकास में अग्रणी रहा है. भारत सरकार के द्वारा 1982 में MCF पर रिसर्च करने के लिए प्लाज़्मा फिज़िक्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी. 1986 में ये प्रोग्राम इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज़्मा रिसर्च (IPR) में तब्दील हो गया और इस तरह 1989 में भारत के स्वदेशी टोकामक आदित्य का निर्माण हुआ. इसके बाद भारत ने एक बड़े अर्ध-स्वदेशी टोकामक को विकसित किया जिसे स्टीडी स्टेट सुपरकंप्यूटिंग टोकामक (SST-1) नाम दिया गया और जो 2013 में पूरी तरह से कमीशन किया गया. IPR ने 2027 में इसके दूसरे वर्ज़न SST-2 की योजना का भी खुलासा किया है.
2005 में भारत इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (IETR) प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला सातवां सदस्य बन गया. ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक रिएक्टर बनाने की कोशिश के लिए एक वैश्विक पहल है. ITER-इंडिया को IPR की देखरेख में स्थापित किया गया है और ये प्रोजेक्ट को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जवाबदेह है. इसने दूसरे उपकरणों के साथ-साथ रिएक्टर को रखने के लिए पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रायोस्टैट, एक वैकम एप्लिकेशन स्टेनलेस स्टील जहाज़, मुहैया करा दिया है.
भारत ने एक बड़े अर्ध-स्वदेशी टोकामक को विकसित किया जिसे स्टीडी स्टेट सुपरकंप्यूटिंग टोकामक (SST-1) नाम दिया गया और जो 2013 में पूरी तरह से कमीशन किया गया. IPR ने 2027 में इसके दूसरे वर्ज़न SST-2 की योजना का भी खुलासा किया है.
निजी निवेश एक प्रमुख क्षेत्र है जहां भारत पीछे है. इसका कारण परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 है जो परमाणु ऊर्जा केंद्रों को विकसित करने और चलाने का बोझ सरकार पर रखता है. घरेलू प्राइवेट कंपनियों को सिर्फ “जूनियर इक्विटी पार्टनर” के तौर पर शामिल होने की अनुमति है और उनकी भूमिका पुर्जों (कंपोनेंट) की सप्लाई और कंस्ट्रक्शन तक सीमित है. हालांकि, पिछले दिनों नीति आयोग के द्वारा बनाई गई सरकारी समिति ने परमाणु ऊर्जा उद्योग में विदेशी निवेश पर लगी पाबंदी को हटाने और घरेलू प्राइवेट कंपनियों की ज़्यादा भागीदारी की इजाज़त देने की सिफारिश की है.
भारत के लिए एक सुनहरा मौका
फ्यूज़न रिएक्टर के ज़रिए ऊर्जा का व्यावसायिक उत्पादन अभी भी कम-से-कम एक दशक दूर है लेकिन ये भारत को हालात के नयेपन का फायदा उठाने के लिए एक सुनहरा मौका मुहैया कराता है. NIF के प्रयोग ने इनर्शियल कन्फाइनमेंट के ज़रिए न्यूक्लियर फ्यूज़न को हासिल करने के लिए एक नए रास्ते को खोला है और भारत के लिए ये फायदेमंद होगा कि इस पर ध्यान दे और इस तकनीक में निवेश करे क्योंकि ये साफ है कि यही वो रास्ता है जहां भविष्य है. ये न सिर्फ भविष्य में जीवाश्म ईंधन के एक विश्वसनीय विकल्प की पेशकश करता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि 2070 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को समय से काफी पहले हासिल कर लिया जाए.
प्रतीक त्रिपाठी ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रैटजी एंड टेक्नोलॉजी में प्रोबेशनरी रिसर्च असिस्टेंट हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.



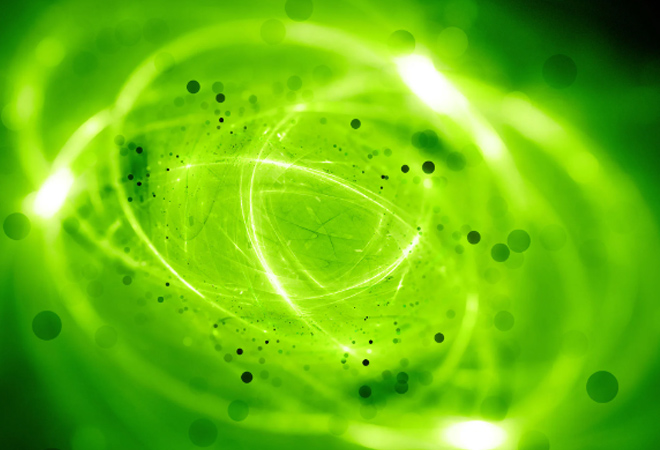
 PREV
PREV

