-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
मातृ एवं नवजात शिशु पोषण के बीच पोषण के अंतर को ख़त्म करना ज़रूरी है. शिशु मृत्युदर कम करके वैश्विक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है.

Image Source: Getty
यह लेख "स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य" शृंखला का हिस्सा है.
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मां और नवजात शिशु की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. ये बात उन देशों या क्षेत्रों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है, जहां खाद्य असुरक्षा, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक-आर्थिक असमानताएं जैसी समस्याएं मौजूद हैं. इनकी वजह से सामाजिक-आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी होती है और स्थायी विकास की राह में भी इनसे बाधाएं उत्पन्न होती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, गर्भावस्था या प्रसव के दौरान हर साल 2,87,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है. 4.9 मिलियन बच्चों की अपने पांचवें जन्मदिन से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं, जबकि उनकी मौत को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है. इतना ही नहीं 1.9 मिलियन बच्चे मृत पैदा होते हैं. मेडिकल जर्नल लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मातृ शिक्षा को बाल कुपोषण का एक प्रमुख भविष्यवक्ता माना जा सकता है. हालांकि मातृ शिक्षा का बाल कुपोषण पर कितना सटीक प्रभाव पड़ता है, इस पर अभी शोध जारी है. सतत विकास लक्ष्य-2 (एसडीजी-2) को हासिल करने के लिए मातृ और बाल पोषण की समस्या पर बात करना, इसका समाधान करना महत्वपूर्ण है. एसडीजी-2 का लक्ष्य भूख को ख़त्म करना, पोषण को बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसके अलावा मां और बच्चे के पोषण में अंतर को पाटना सतत विकास लक्ष्य-3 को हासिल करने के लिए आवश्यक है. एसडीजी-3 सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है.
खराब मातृ स्वास्थ्य ही गर्भावस्था, प्रसव और शैशवावस्था (शिशु की 5 साल की उम्र से कम की अवस्था) के दौरान होने वाली जटिलताओं का मुख्य कारण है. इसका संबंध आम तौर पर कुपोषण से होता है. रिसर्च में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त आहार सेवन खराब मातृ पोषण का सबसे बड़ा कारण है. इसका मां और बच्चे दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. भोजन का उपलब्ध नहीं होना, आर्थिक मुसीबत, पोषण संबंधी सलाह की कमी, भोजन संबंधी मान्यताएं और लिंग मानदंड जैसी बाधाएं उचित पोषण तक पहुंच में बाधा पैदा करती हैं.
खराब मातृ स्वास्थ्य ही गर्भावस्था, प्रसव और शैशवावस्था (शिशु की 5 साल की उम्र से कम की अवस्था) के दौरान होने वाली जटिलताओं का मुख्य कारण है. इसका संबंध आम तौर पर कुपोषण से होता है.
लैंगिक असमानता मां और नवजात बच्चे के स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती है, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में. घर और समुदाय के भीतर महिलाओं के पास निर्णय लेने की सीमित शक्ति होती है. इसकी वजह से अक्सर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी देर से या फिर अपर्याप्त पहुंच होती है. हाल ही में हुए एक मेटा-विश्लेषण ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश के महत्व को स्वीकार किया है. आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों ने विभिन्न मानव विकास संकेतकों, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है. इस तरह का कार्यक्रम योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं. आखिर में इसके बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं.
इसके अलावा, मातृ आहार में सुधार के लिए ज़रूरी हस्तक्षेप किए जाने चाहिए. इसमें भोजन-आधारित कार्यक्रम, आहार संबंधी व्यवहार में बदलाव लाना और ऐसी कृषि को शामिल किया जा सकता है, जिसमें पोषक तत्व हों. कुपोषण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है. इसकी वजह से कई बार महिलाएं प्रसव के बाद अवसाद का भी शिकार होती हैं. हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार मां का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर मां का मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो इससे बच्चे की सही देखभाल बाधित हो सकती है. इससे मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है.
कई देशों में गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है. इसकी एक बड़ी वजह ये है कि पूरक आहार तक उनकी पहुंच सीमित होती है. खाने में पोषक तत्वों की कमी से गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है. खाद्य असुरक्षा मां और बच्चे के कुपोषण को बढ़ाती है. खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों, अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष और जलवायु परिवर्तन से ये समस्या और भी बढ़ जाती है. निम्न और मध्यम आय वाले 94 देशों (एलएमआईसी) में किए गए एक अध्ययन में 0-5 साल की उम्र के 32 प्रतिशत बच्चों में बौनेपन का प्रचलन पाया गया. अध्ययन में ये पाया गया कि बड़े बच्चों में बौनेपन की दर अधिक थी. इसकी वजह शायद ये थी कि वो कुपोषण और बार-बार होने वाले संक्रमणों से प्रभावित होते थे. इसने उनकी सामान्य वृद्धि पर असर डाला. इसे देखते हुए गर्भवती माताओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए जाने ज़रूरी हैं. इसमें उन्हें स्तनपान, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन पहल और सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ावा देने वाली जानकरियां दी जानी चाहिए.
सही मातृ पोषण जन्म के परिणामों और बच्चों के दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है. एक वैश्विक व्यवस्थित समीक्षा ने निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में मातृ पोषण में सुधार के रास्ते में बाधा डालने वाले कई प्रमुख कारणों की पहचान की. इनमें घरेलू भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, वित्तीय बाधाएं, गर्भावस्था के दौरान उचित वजन बढ़ाने और आहार सेवन के बारे में जानकारी की कमी और आहार संबंधी सही सलाह की कमी शामिल है. उच्च कुपोषण दर वाले देशों में मातृ स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए इन सभी मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है.
समस्या के दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान के लिए कई स्तर पर काम करने की ज़रूरत होती है. इसमें आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि को शामिल किया जाता है. इसे लेकर कई ज़रूरी कदम उठाए भी गए हैं. इन कार्यक्रमों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए. मज़बूत स्वास्थ्य सेवा नीतियों की वकालत की गई. इसका असर ये हुआ कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. जो क्षेत्र सीमित संसाधन वाले हैं, वहां दीर्घकालिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता महत्वपूर्ण है.
खाद्य सहायता और नकद हस्तांतरण जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कमज़ोर आबादी को फौरी राहत पहुंचाती हैं, विशेष रूप से संकट के समय में. एक व्यवस्थित समीक्षा में ये भी पाया गया कि छह महीने से कम उम्र के छोटे और पोषण संबंधी ज़ोखिम वाले शिशुओं के लिए व्यापक देखभाल पैकेज में माताओं को शामिल करने से स्वास्थ्य परिणामों में काफ़ी सुधार हो सकता है.
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की उपलब्धता के बावजूद कई योजनाएं कमज़ोर आबादी तक पहुंचने में नाकाम रही. इसकी बड़ी वजह कार्यान्वयन में कमी रही. एक अध्ययन के मुताबिक, कम संसाधन वाले क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कमज़ोर निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन में कमी के प्रमुख कारण रहे. इनसे निपटने के लिए नीतियों में समावेशिता और स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. नीतियां स्थानीय संदर्भों के अनुकूल होनी चाहिए और इनमें मज़बूत सामुदायिक भागीदारी को शामिल करना चाहिए. प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के बीच मिल-जुलकर कोशिश करने की ज़रूरत होती है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपलब्ध संसाधन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें.
इसके अलावा, मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए मज़बूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की भी आवश्यकता होती है. प्रसवपूर्व की अवस्था से लेकर बच्चे के पैदान होने तक देखभाल की पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए. सरकारों और निवेशकों को मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए. ऐसी पहलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि निम्न आय वर्ग की महिलाओं को उच्च मातृ मृत्यु दर का सामना करना पड़ता है. इसका मुख्य कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त पोषण और रहने की खराब स्थिति है. संसाधनों को अंतिम ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए सभी हितधारकों को इन योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्थानीय रीति-रिवाजों के आधार पर सलाह देने, पोषण निगरानी को बढ़ावा देने, शिशु देखभाल पर परामर्श देने और स्तनपान को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उच्च ज़ोखिम वाले समूहों की पहचान करके और उनके बारे में आंकड़े जुटाने चाहिए. इसके बाद आंकड़ों के आधार पर ऐसे कमज़ोर समूहों तक लक्षित मदद पहुंचाए जाने से उनकी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी होंगी. गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को स्वस्थ भोजन, स्तनपान के महत्व और संतुलित शिशु आहार के बारे में शिक्षित करने से कुपोषण की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है.
स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए नवजात शिशु की देखभाल और मातृ पोषण पर सामुदायिक शिक्षा आवश्यक है. ऐसी योजनाओं का समर्थन किया जाना चाहिए, जिनसे गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. कृषि परियोजनाओं और खाद्य वितरण प्रणालियों को बनाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए. इसे सब्सिडी, कृषि के बेहतर बुनियादी ढांचे खाद्य कीमतों को स्थिर करने वाली नीतियों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है. ये कार्यक्रम तब विशेष रूप से प्रभावी होते हैं जब इन योजनाओं में उन समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का सम्मान किया जाता है, जिनके लिए वो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. आहार संबंधी कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय को ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए. स्थानीय समुदाय के लोग पोषक आहार कार्यक्रम में उस क्षेत्र में प्रचलित खाद्य पदार्थों को एकीकृत करते हैं. इन कार्यक्रमों में अगर विश्वसनीय सामुदायिक नेताओं का सहयोग मिले तो इससे अक्सर उच्च भागीदारी दर और अधिक स्थायी परिणाम देखने को मिलते हैं. इस तरह की ज़मीनी स्तर की पहल ये सुनिश्चित करती हैं कि पोषण संबंधी हस्तक्षेप सांस्कृतिक रूप से सही हों, जिससे उन्हें बेहतर स्वीकृति मिले और व्यवहार में धीरे-धीरे लेकिए लगातार परिवर्तन हो.
हालांकि इसके लिए सिर्फ वैश्विक सहयोग ही पर्याप्त नहीं है. मातृ और शिशु पोषण में अंतर को कम करना अनिवार्य है. कुपोषण के मूल कारणों को दूर करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयास महत्वपूर्ण हैं. कृषि ढांचे में सुधार, लक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और समुदाय-संचालित शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से टिकाऊ और दीर्घकालिक समाधान हासिल होंगे. इससे हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि कमज़ोर आबादी के पास वो संसाधन उपलब्ध हों, जो उनके विकास के लिए ज़रूरी हैं.
एक व्यवस्थित समीक्षा में ये भी पाया गया कि छह महीने से कम उम्र के छोटे और पोषण संबंधी ज़ोखिम वाले शिशुओं के लिए व्यापक देखभाल पैकेज में माताओं को शामिल करने से स्वास्थ्य परिणामों में काफ़ी सुधार हो सकता है.
हालांकि, असली चुनौती इन उपायों को व्यापक स्तर पर लागू करना है, जिससे स्थायी बदलाव लाए जा सकें. इन कार्यक्रमों की सफलता की कुंजी सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करने में है. साथ मिलकर वो एक ऐसी समग्र और परस्पर जुड़ी प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं, जो एक-दूसरे क्षेत्र का सहयोग कर सके. लक्षित निवेश, तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक स्थिरता के साथ हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी मां या बच्चा कुपोषित या स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ना रहे.
वैश्विक एकजुटता और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य का निर्माण किया जा सकता है. माताओं, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को मज़बूत बनाया जा सकता है. अब सिर्फ बात करने का नहीं बल्कि काम करने का समय आ चुका है. स्वस्थ जीवन ही, एक व्यक्ति और पूरी दुनिया, दोनों के उज्जवल भविष्य में योगदान देता है.

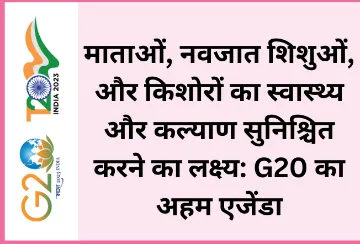
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

With 18 years of experience, Rohini Saran leads nutrition-sensitive programs focused on maternal and child health across diverse sectors. Expertise in strategic communications, policy advocacy, ...
Read More +